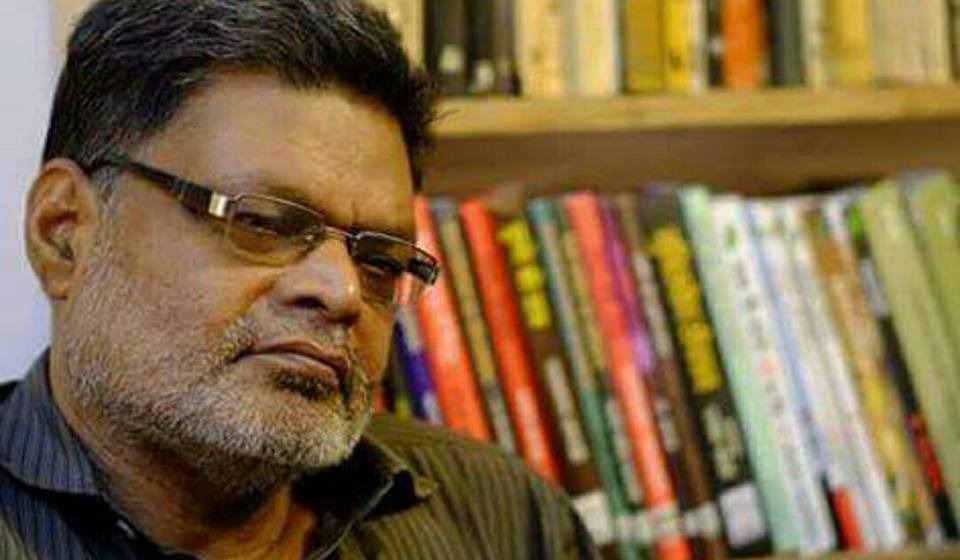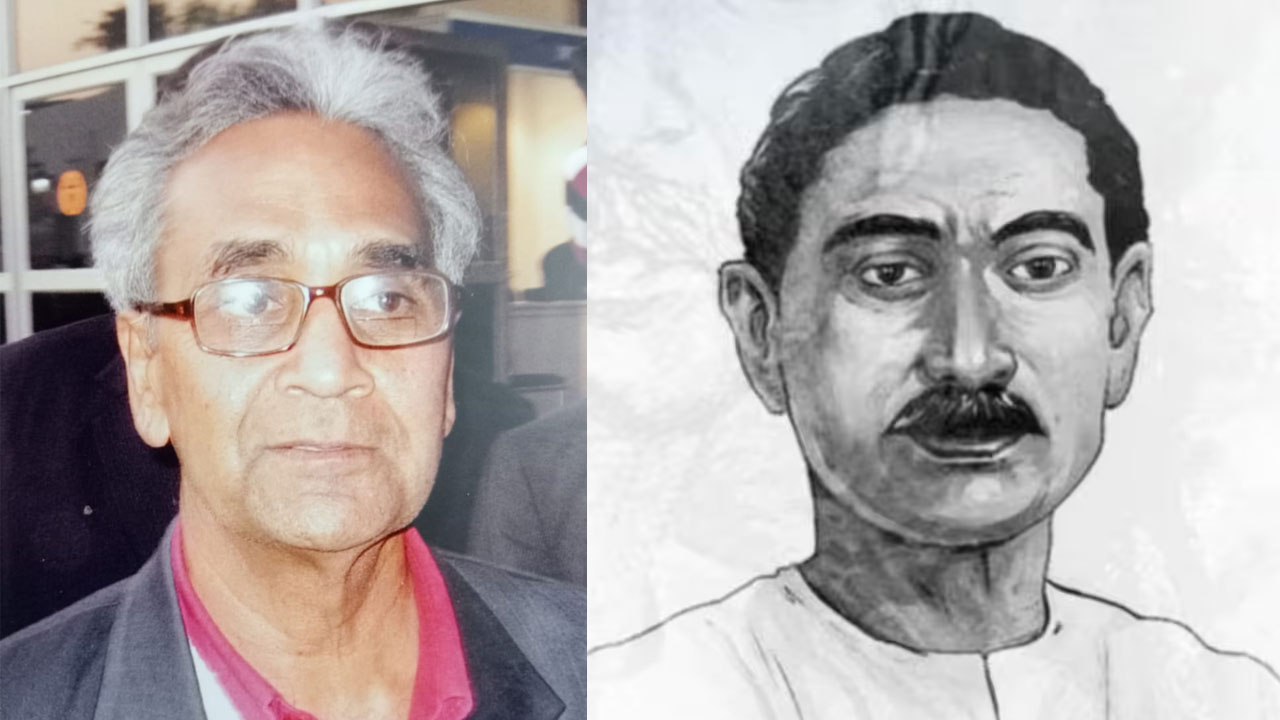भारतीय समाज का स्तरीकरण ब्राह्मणवाद की जिस सामाजिक वैचारिक व्यवस्था के तहत किया गया था उसमें ‘पवित्रता’ का पाखंड
खड़ा कर शूद्र, अतिशूद्र और पिछड़ों के वैचारिक स्तर पर संगठित होने की संभावनाओं को हर काल में दबाया गया। चूंकि इन तीनों का संगठित होना इस व्यवस्था का समूल अंत कर सकता था, इसलिए सामाजिक स्तर पर भारत में चले समतामूलक आंदोलनों के दौरान पिछड़ों को सवर्णों ने अपने पाले में लेने की कोशिश की। मूल खतरा ब्राह्मणवादी हिन्दू धर्म के विखंडन का था जिसे धर्म और आस्था के नवीन प्रारूप सेही बचाया जा सकता था।
आर्य समाज इस नवीन पारूप का उदाहरण है जो औपनिवेशिक भारत में शूद्र, अतिशूद्र और पिछड़ों की एकता को तोडऩे की कोशिश था, क्योंकि ये तीनों ही शोषण की संरचनाओं से उत्पन्न अनुभवजन्य ज्ञान को संवाद के स्तर पर लाकर मुक्ति की विस्तृत चेतना की ओर ले जा रहे थे। इसलिए ब्राह्मण धर्म के लिए जरूरी था कि वह कला, साहित्य और भू-संबंधों की संरचनाओं को विभाजनकारी रूप में स्थापित करे।
 स्वातंत्रयोत्तर भारत में यह प्रवृत्ति तमाम स्तरों पर तीव्र गति से बढ़ी। जहां दलित साहित्य की बढ़ती लोकप्रियता से सवर्ण साहित्यकार चिंतित थे, वहीं उन्हें ‘ओबीसी’ साहित्य की दस्तक का भी आभास हो चुका था और हिन्दी के एक ‘महान’ आलोचक ने पूरे सवर्ण समाज की इस ‘पीड़ा’ को ‘साहित्य में आरक्षण नहीें’ के जुमले के तहत उजागर किया। दरअसल, उन्हें जो खतरा था, वह ओबीसी साहित्य से न होकर उस दौर में रची जा रही ‘बहुजन साहित्य’ की उस अवधारणा से था जिसमें दलित, स्त्री, आदिवासी और ओबीसी को शामिल किया गया था, क्योंकि इससे सदियों से उनके द्वारा रची गई ‘विभाजनकारी’ रणनीति को नेस्तनाबूद किया जा सकता था। यह केवल कला और साहित्य पर ही नहीं बल्कि ‘ज्ञान’ के उन तमाम क्षेत्रों पर लागू था जहां बहुजन की दस्तक शुरू हो गई थी। जब यह आलोचक चिल्ला रहे थे, वह दौर ठीक वही था जब पिछड़ों की पहली फौज भारतीय अकादमिक सवर्ण वर्चस्व के पहले घेरे को ध्वस्त कर रही थी। वह सवर्ण वर्चस्व को न केवल प्रतिनिधित्व के स्तर पर तोडऩे की कोशिश कर रही थी बल्कि हजारों साल से कैद किए गए ज्ञान को मुक्त करने की ओर भी बढ़ रही थी। राजनीति में जिस तीव्र गति से बहुजन की भागीदारी बढ़ रही है, उतनी गति से शायद साहित्य और कला में यह नहीं हो रहा है क्योंकि प्रकाशन व आलोचना से लेकर सम्पूर्ण पठन-पाठन पर सवर्णों का एकाधिकार रहा है। इसमें भी अफ सोस नहीं होना चाहिए कि ‘प्रगतिशीलता’ का चोला धारण किए आलोचकों ने अंतत: सवर्ण आलोचक का फ र्ज ही अदा किया है।
स्वातंत्रयोत्तर भारत में यह प्रवृत्ति तमाम स्तरों पर तीव्र गति से बढ़ी। जहां दलित साहित्य की बढ़ती लोकप्रियता से सवर्ण साहित्यकार चिंतित थे, वहीं उन्हें ‘ओबीसी’ साहित्य की दस्तक का भी आभास हो चुका था और हिन्दी के एक ‘महान’ आलोचक ने पूरे सवर्ण समाज की इस ‘पीड़ा’ को ‘साहित्य में आरक्षण नहीें’ के जुमले के तहत उजागर किया। दरअसल, उन्हें जो खतरा था, वह ओबीसी साहित्य से न होकर उस दौर में रची जा रही ‘बहुजन साहित्य’ की उस अवधारणा से था जिसमें दलित, स्त्री, आदिवासी और ओबीसी को शामिल किया गया था, क्योंकि इससे सदियों से उनके द्वारा रची गई ‘विभाजनकारी’ रणनीति को नेस्तनाबूद किया जा सकता था। यह केवल कला और साहित्य पर ही नहीं बल्कि ‘ज्ञान’ के उन तमाम क्षेत्रों पर लागू था जहां बहुजन की दस्तक शुरू हो गई थी। जब यह आलोचक चिल्ला रहे थे, वह दौर ठीक वही था जब पिछड़ों की पहली फौज भारतीय अकादमिक सवर्ण वर्चस्व के पहले घेरे को ध्वस्त कर रही थी। वह सवर्ण वर्चस्व को न केवल प्रतिनिधित्व के स्तर पर तोडऩे की कोशिश कर रही थी बल्कि हजारों साल से कैद किए गए ज्ञान को मुक्त करने की ओर भी बढ़ रही थी। राजनीति में जिस तीव्र गति से बहुजन की भागीदारी बढ़ रही है, उतनी गति से शायद साहित्य और कला में यह नहीं हो रहा है क्योंकि प्रकाशन व आलोचना से लेकर सम्पूर्ण पठन-पाठन पर सवर्णों का एकाधिकार रहा है। इसमें भी अफ सोस नहीं होना चाहिए कि ‘प्रगतिशीलता’ का चोला धारण किए आलोचकों ने अंतत: सवर्ण आलोचक का फ र्ज ही अदा किया है।
यही कारण है कि ‘बहुजन’ की अवधारणा हाशिए के पूरे समाजों के इतिहास लेखन से प्रसार पा रही है। जोतिबा फु ले और सावित्रीबाई फुले के स्थान पर भारतेंदु हरिश्चंद्र और महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व को महिमामंडित करने का कार्य इन्हीं तथाकथित प्रगतिशील आलोचकों का है। मजेदार तो यह भी है कि इन आलोचकों की चिंताएं किसान और मजदूर के सर्वहारा वर्ग की भी कतई नहीं थीं। वे कलावाद और जनवाद के बीच अपनी जातीय पहचान के आसपास ही मंडराते रहे। जबकि बहुजन की अवधारणा में बुद्ध से लेकर फुले तक किसान और मजदूर की चिंताओं और संघर्ष को आत्मसात् किया गया है। दलित और पिछड़ों द्वारा रचित संगीत के सात स्वरों को भी ‘शास्त्रीय’ के सवर्ण लिबास में ढंकते वक्त किसी ने यह जानकरी भी नहीं दी कि यह लोक सम्पत्ति है जिसका रचयिता बहुजन रहा है। ‘ज्ञान लूट’ में चेतना का पूरा स्तर ही द्विजों को आधार मानकर रचा गया है। ऐसे में हिन्दी के उन आलोचक की चिंता असल में द्विज वर्चस्व को बनाए रखने की चिंता ही कही जा सकती है।
जोतिबा फुले का ‘किसान का कोड़ा’ नाटक भारतीय उपमहाद्वीप में कृषक वर्ग की समस्याओं का बेहतरीन दस्तावेज कहा जा सकता है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश के द्वंद्व का सटीक विश्लेषण किया गया है। लेकिन इसे साहित्य के इतिहास में जान-बूझकर नजरंदाज किया गया।
एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि भारतीय समाज में ‘सामाजिक समानता’ की अवधारणा बुद्ध से पूर्व किसी विचारक में दिखाई नहीं देती है। इसे अवधारणात्मक स्तर पर फु ले ने विकसित किया। अब सवाल यह है कि जिस सांस्कृतिक संरचना में ‘सामाजिक समानता’ की अवधारणा तक नहीं है, उस सांस्कृतिक संरचना के साहित्य को ‘जनता का साहित्य’ कैसे माना जा सकता है? असल में तो उसे ‘साहित्य’ ही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह समाज विकास में योगदान देने की बजाय यथास्थितिवादी है। इसलिए भारतीय साहित्य तो ‘बहुजन साहित्य’ से ही प्रारम्भ होता है। इससे इतर जो सवर्ण लेखन है उसे ‘शोषण का औजार’ कहा जा सकता है।
बहुजन के साहित्य की धारा तो बहुत लम्बी है लेकिन मजेदार बात यह भी है कि बहुजन साहित्य को निकाल दिया जाए तो तथाकथित हिन्दी साहित्य में मात्र लुगदी बचेगी। यहीं पर उन आलोचक महोदय की छटपटाहट समझी जा सकती है। आखिर वे इस ‘लुगदी’ के बल पर कैसे ‘महान’ आलोचक बन सकते हैं जबकि उनकी आलोचना के सारे औजार तो सवर्ण हैं। यह महत्वपूर्ण है कि सवर्ण चिंतकों का समाजिक परिवर्तन का आकलन ही गलत साबित हो गया है। जैसा कि इन आलोचक का कहना था कि समाज के बद्धमूल संस्कारों को खत्म करने में सौ दो-सौ साल का समय लगेगा। बहुजन की राजनीतिक चेतना से लेकर सांस्कृतिक परिवर्तन की तमाम बयारों को देखने के बाद स्थिति में बदलाव हो रहा है और यह समय-सीमा भी गलत साबित हो रही है। जब उनकी सामाजिक समझ पर इतना बड़ा आघात हो रहा है तब क्या यह सवाल बिल्कुल नहीं पूछा जाना चाहिए कि उनके तथाकथित ‘प्रगतिशील’ आंदोलन के तर्कों में कितनी सवर्ण रूढिवादिता थी?
(फारवर्ड प्रेस के जुलाई, 2014 अंक में प्रकाशित)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +919968527911, ईमेल : info@forwardmagazine.in