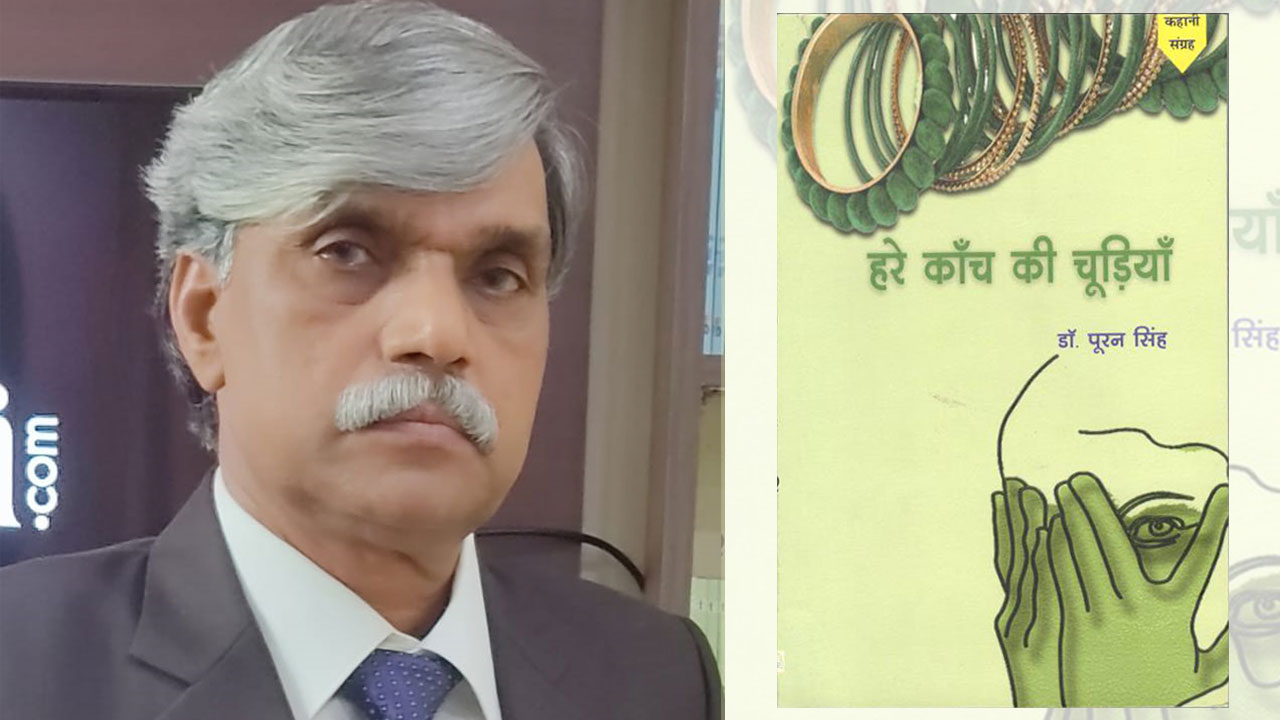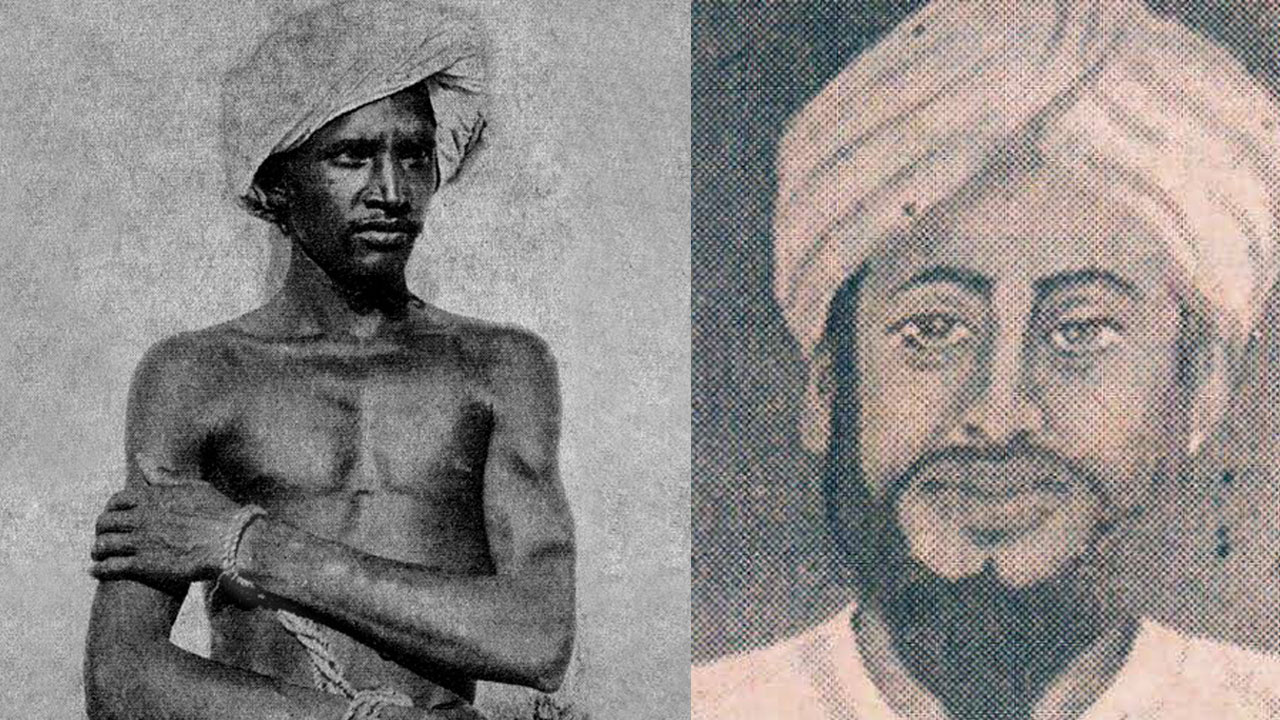इन सवालों पर बात करने से पहले सन 1988 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के उस प्रयोग को समझना होगा, जो सत्ता की परवान चढ़ा और अपने ही व्यक्तिगत अंतर्विरोधों के चलते टूट भी गया। 11 अक्टूबर 1988 को कांग्रेस मंत्रीमंडल से बगावत कर बाहर आए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लोकदल, कांग्रेस (एस) और अपने जनमोर्चा को मिलाकर जो जनता दल बनाया, वह तीन बुनियादी कारणों से सफल हो सका था। पहला, राजीव गाँधी की कांग्रेस सरकार बोफोर्स भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरी थी व उसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी माहौल बना हुआ था। दूसरा, 1 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद का ताला खुलने के कारण मुसलमान नाराज थे और कांग्रेस के विकल्प की तलाश में थे। तीसरे, पिछड़ी जातियों, खासकर यादवों में, नए और उर्जावान नेतृत्व का उभार राजनैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तरप्रदेश और बिहार में निर्णायक रूप ले रहा था। इन तीनों कारणों से विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में जनता दल को भारी जनसमर्थन प्राप्त हुआ।
 1988 की परिस्थितियों के बरक्स, अगर 2014 में हम इन तीनों कारकों की रोशनी में एकीकरण के नये प्रयासों को देखें तो जनता परिवार के एकीकरण की संभावनाएं अपने आप धराशायी हो जाती हैं। मसलन इन पार्टियों के लगभग सभी बड़े नेता, जो एक से अधिक बार मुख्यमंत्री पद तक पर आसीन रह चुके हैं, खुद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव पर सजायाफ्ता होने के कारण चुनाव लडऩे पर प्रतिबंध है। इसलिए इस प्रयास में शामिल दलों को भ्रष्टाचार के सवाल पर बोलने का नैतिक अधिकार तक नहीं है। वहीं इन पार्टियों के आंतरिक संरचना में अपने परिवार से बाहर की ‘जनता’ लगभग निषिद्ध है। इसमें अपवाद सिर्फ जदयू हो सकती है, जिसमें उपरी पदों पर तो परिवारवाद नहीं है लेकिन दूसरे स्तरों पर जरूर है। जाहिर है, ऐसे में पुनर्गठित जनता दल में अध्यक्ष और दूसरे महत्वपूर्ण ओहदों पर कौन हो, यह बड़ा पेचीदा सवाल होगा।
1988 की परिस्थितियों के बरक्स, अगर 2014 में हम इन तीनों कारकों की रोशनी में एकीकरण के नये प्रयासों को देखें तो जनता परिवार के एकीकरण की संभावनाएं अपने आप धराशायी हो जाती हैं। मसलन इन पार्टियों के लगभग सभी बड़े नेता, जो एक से अधिक बार मुख्यमंत्री पद तक पर आसीन रह चुके हैं, खुद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव पर सजायाफ्ता होने के कारण चुनाव लडऩे पर प्रतिबंध है। इसलिए इस प्रयास में शामिल दलों को भ्रष्टाचार के सवाल पर बोलने का नैतिक अधिकार तक नहीं है। वहीं इन पार्टियों के आंतरिक संरचना में अपने परिवार से बाहर की ‘जनता’ लगभग निषिद्ध है। इसमें अपवाद सिर्फ जदयू हो सकती है, जिसमें उपरी पदों पर तो परिवारवाद नहीं है लेकिन दूसरे स्तरों पर जरूर है। जाहिर है, ऐसे में पुनर्गठित जनता दल में अध्यक्ष और दूसरे महत्वपूर्ण ओहदों पर कौन हो, यह बड़ा पेचीदा सवाल होगा।
दूसरे, जिस मुस्लिम वोट बैंक ने इन पार्टियों को सत्ता दिलाई, उसे इन पार्टियों की सरकार में भी सिवाय बदहाली और सांप्रदायिक हिंसा के कुछ नहीं मिला। नीतीश और देवगौड़ा तो भाजपा के साथ सत्ता में भी रह चुके हैं, और मुलायम भी पिछली साढ़े तीन साल से भाजपा के अघोषित समर्थन से सरकार चला रहे हैं। यानी इस परिवार के सबसे बड़े वोट बैंक का उससे मोहभंग हो चुका है, और अगर कहीं कुछ रुझान है भी तो वह मजबूरीवश ही है।
तीसरा, जिन पिछड़ी जातियों की राजनीतिक-सामाजिक अस्मिता को लालू, नीतीश और मुलायम संबोधित कर रहे थे, वे अब न तो उनके पार्टियों के प्रभाव में हैं और ना ही उनकी नई आकांक्षाओं की वाहक ही ये पार्टियां बन सकती हैं। कारण है हिन्दुत्ववादी एकता की सोशल इंजीनियरिंग के नारे के साथ आई भाजपा, जो पिछड़ों और दलितों को उनके ‘स्वाभिमान’ के अनुरूप जगह देने का दावा कर रही है। पिछड़ों का एक बड़ा और निर्णायक हिस्सा मोदी के साथ इसलिए भी खड़ा हो गया है कि पहली बार पिछड़े समाज से आने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है।
यानी, लालू, मुलायम और नीतीश अपने मूल जातिगत आधार से भी हाथ धो बैठे हैं। इस स्थिति की दूसरी वजह यह है कि इन पार्टियों ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया। अपने जातिगत जनाधारों को धर्मनिरपेक्ष बनाने की कोई कोशिश ही नहीं की क्योंकि खुद उनके लिए भी धर्मनिरपेक्षता सिर्फ एक नारा था, जिसे चुनावों के दौरान ही लगाया जाना था और बाकी समय नर्म हिंदुत्व के इर्द-गिर्द अपनी जातियों को गोलबंद करना था ताकि सवर्ण वर्चस्व वाली पार्टियों के साथ हिंदुत्ववादी सामाजिक-राजनीतिक दायरे में बना रहा जा सके। इसीलिए नब्बे के शुरूआती दिनों के बाद कभी भी सपा-बसपा की तरफ से यह नारा नहीं दुहराया गया ‘मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्रीराम’, जो वे भाजपा के राममंदिर आंदोलन के उभार के दौरान लगाते थे और ना ही कभी वे संविधान के अनुच्छेद 341 को हटाने की मांग करते दिखते हैं, जिससे कि दलित मुसलमानों को आरक्षण का लाभ मिल सकता था। आप एक साथ सेक्यूलर और साम्प्रदायिक नहीं हो सकते।
ऐसे में जनता दल को पुनर्जीवित करने की कवायद किसी वैकल्पिक राजनीति के निर्माण से ज्यादा अपनी जातियों पर अपनी चौधराहट कायम रखने की कुंठित और हताश कोशिश ही ज्यादा लगती है, जिसके सफल होने का दावा शायद ही कोई करे। वैसे भी, अस्मितावादी राजनीति की उम्र तभी तक होती है, जब तक कि वह किसी बड़ी अस्मिता में समाहित न हो जाए। चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, भाजपा ने यह कर दिखाया है। सपा, राजद और जदयू का समय समाप्त हो चुका है।
(फारवर्ड प्रेस के जनवरी, 2015 अंक में प्रकाशित)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +919968527911, ईमेल : info@forwardmagazine.in