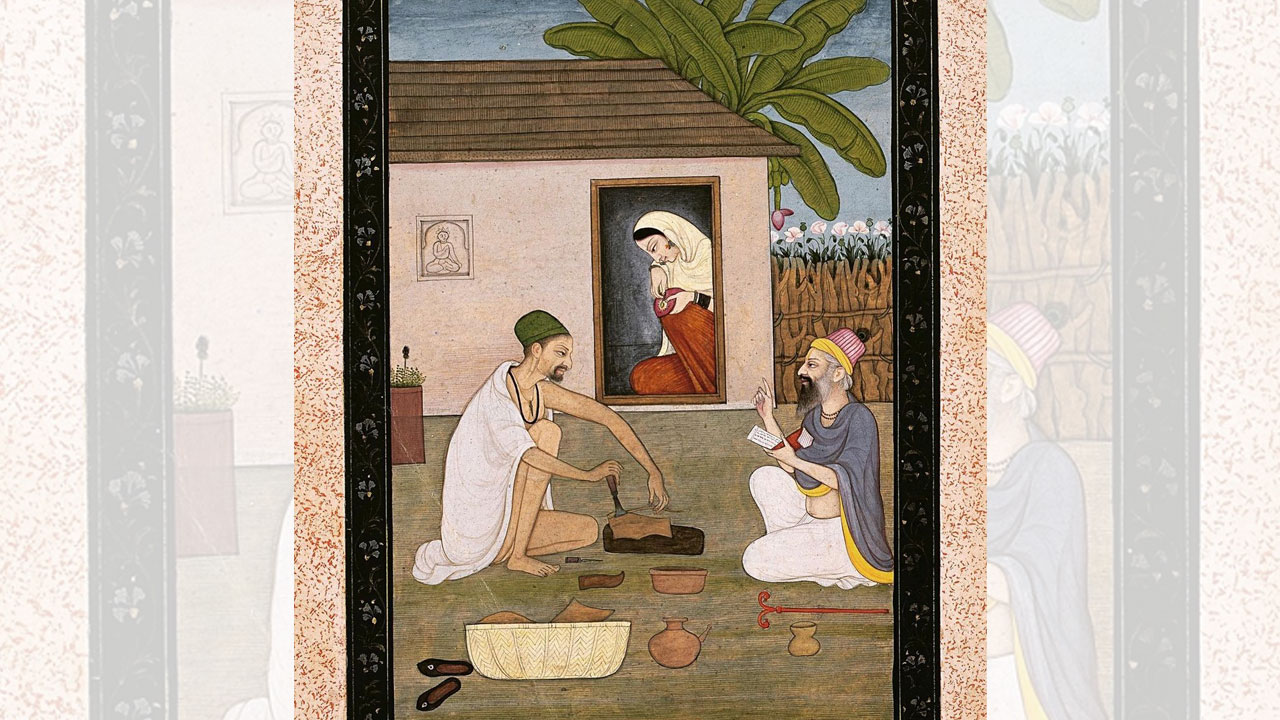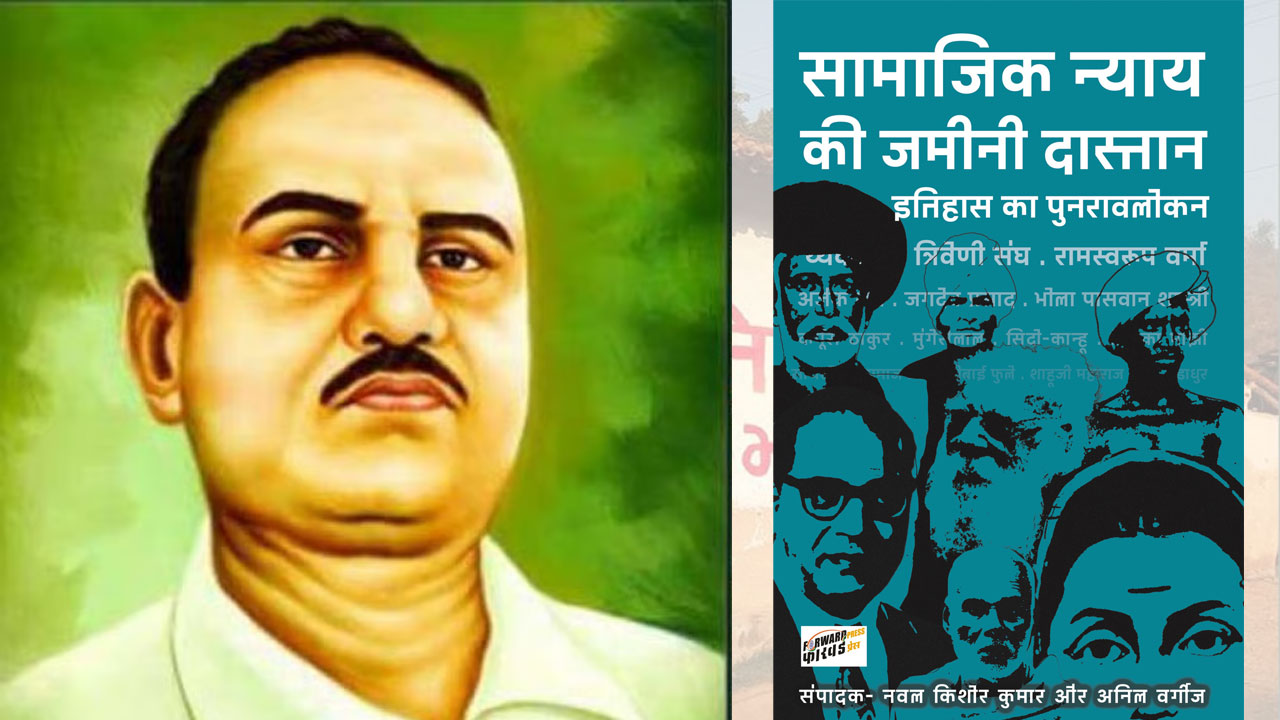गोंड जनजातीय समाज और गोंडी धर्म के विशेषज्ञ आचार्य मोतीरावण कंगाली (2 फरवरी, 1949 – 30 अक्टूबर, 2015) के विषय में अब बौद्धिक जगत में उत्सुकता बढ़ने लगी है। वे न केवल अपनी विशेषज्ञता के लिए बल्कि अपने इस विशेष ज्ञान के माध्यम से सामाजिक विमर्श की एक विशेष दिशा निर्मित करने के लिए भी सदियों तक जाने जाएंगे। उन्होंने अपने जमीनी अध्ययनों से जिस विमर्श को आरम्भ किया है, वह भारत के धार्मिक दार्शनिक अतीत और भविष्य दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जो लोग समाजशास्त्रीय और मानवशास्त्रीय अर्थ में इतिहास सहित धर्म के क्रमविकास को समझना चाहते हैं, उनके लिए डॉ. मोतीरावण कंगाली एक दुर्लभ विद्वान हैं। साहित्य और इतिहास के किस्से कहानियों की मुर्दा दुनिया में समाज या धर्म से जुड़े विमर्श खोजने वालों के लिए वे ऐसे स्वर्णिम सूत्र उपलब्ध कराते हैं जो अब से पहले कभी देखे सुने नही गए थे।

असल में डॉ. कंगाली को और उनके कामों को आधुनिक समाजशास्त्रीय विमर्श में पूरी तरह लाने में कुछ समय लगेगा, इसके अपने कारण हैं जो समझे जा सकते हैं। ये कारण न सिर्फ डॉ. कंगाली के कामों को वृहत्तर भारतीय समाज के प्रति अनुपलब्ध बनाये रखने के लिए जिम्मेदार रहे हैं, बल्कि आगे चलकर यही कारण जब अपनी पूरी नग्नता में समझ लिए जाएंगे तब इन्ही कारणों की पृष्ठभूमि में डॉ कंगाली को एक महान शोधकर्ता के रूप में पहचान मिल सकेगी। ईमानदार विद्वानों के साथ यही होता आया है, उनके मार्ग की बाधाएं ही बाद में उनके लिए सीढिया बन जाती हैं।
डॉ. कंगाली के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि वे खुद गोंडी समाज के सदस्य होने के नाते गोंडी भाषा, धर्म और परम्पराओं सहित पूरे गोंडी दर्शन की वृहत्तर पारिस्थितिकी के सम्बन्ध में एक इनसाइडर की दृष्टि रखते हैं। हालांकि बाहर से आने वाले अध्येता या शोधकर्ता भी अपने सहभागी अध्ययन से बहुत कुछ जान लेते हैं, लेकिन उनका अध्ययन हमेशा ही विषय से न्याय नही कर पाता है। सहभागी समाजशास्त्रीय अध्ययन की अपनी सीमायें हैं, बहुत सफल होने पर भी यह अध्ययन कुछ ख़ास अर्थों में असफल ही रह जाते हैं। उन कुछ ख़ास अर्थों को समझना जरूरी है तभी हम डॉ कंगाली के कृतित्व को और उसकी दिशा को समझ सकेंगे।
किसी भी प्रकृति के समाजशास्त्रीय अनुसन्धान की किसी समाज या संस्कृति विशेष में एक सीमा होती है। यह सीमा अक्सर ही उस समाज के बाहर से आने वाले अध्येताओं के लिए एक दुर्निवार और अदृश्य रुकावट बन जाती है। ऐसी रुकावटें असल में किसी भी देश या संस्कृति के अपने क्रमविकासीय इतिहास में जन्मी असुरक्षाओ के गर्भ से जन्म लेती हैं। इन असुरक्षाओं को पहचानना जरुरी है। ये असुरक्षाएं न सिर्फ भारत के मुख्यधारा के समाज और धर्म की विशेष कमजोरियों को उजागर करती हैं, बल्कि ये असुरक्षाएं भविष्य हेतु उस “करणीय” की ओर भी इशारा करती हैं जो अब तक किया ही नहीं गया है। ये एक सटीक निदान की तरह है, जो बीमारी के कारण की पहचान और उसके सम्यक उपचार – दोनों को संभव बनाता है। डॉ. कंगाली या उनके कामों से जुड़े गोंडी जनजातीय समाज के बारे में जब भी बात होगी तो वह बात अनिवार्य रूप से इन असुरक्षाओं और इनके गर्भ से जन्म लेने वाले विशेष आग्रहों और दुराग्रहों को उनकी नग्नता में उजागर करती चलेगी। यह एक अनिवार्यता है इससे अन्यथा कोई उपाय ही नहीं है। इस प्रक्रिया को इतना निर्मम और कष्टपूर्ण होना ही चाहिए। इसके अलावा एक ईमानदार विमर्श का इस पक्षपात से भरे समाज में जमीन तक उतारने का अन्य कोई मार्ग ही नहीं है।
भारत के विशेष सन्दर्भ में ऐसी असुरक्षाओ में सबसे ऊपर आती है धर्म दर्शन से जुडी असुरक्षा। इसका सीधा सम्बन्ध मुख्य धारा के धर्म की पहचान के खो जाने के भय से है। दूसरी असुरक्षा धर्म दर्शन के विकास की व्याख्या से जुडी है। तीसरी असुरक्षा मुख्य धारा की भाषा के आधिपत्य के खो जाने के भी से जुडी है और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण असुरक्षा एक भिन्न राष्ट्रीयता के उभार के भय से जुडी है। इन चार असुरक्षाओं के आईने में हम डॉ. मोतीरावण कंगाली को और उनके काम को समझने का प्रयास करेंगे।

गोंडी समाज या किसी भी अन्य जनजातीय या दलित समाज की वर्तमान भारत में जो स्थिति है उसे समझना एक जटिल काम है। जटिलता इसलिए है कि एक अलिखित इतिहास वाले देश में सैकड़ों उप-संस्कृतियों और उतने ही धर्म दर्शनों का आपस में संघर्ष चलता रहा है। ये संघर्ष स्वयं में इतना बहुआयामी है कि इसमें तथाकथित मुख्य धारा के हिन्दू समाज के लिए भी एक तर्कपूर्ण इतिहास विमर्श व समाज विमर्श को नही ढूंढा जा सकता। खुद हिन्दू समाज की समस्याओं का उद्गम किन विशेष प्रवृत्तियों में है यही अपने आपमें एक भयानक पहेली है। अब सीधी सी बात है कि अगर हिन्दू समाज के ही उद्गम और क्रमविकास को ढूंढ पाना असम्भव है तब जनजातीय या दलित समाज के संबन्ध में स्पष्टता की तो उम्मीद ही कैसे की जा सकती है?
इस विवशता में थोड़े और गहरे जाना होगा। यह बहुआयामी विवशता है, इसमें न सिर्फ विरोधी धर्म दर्शनों का आपसी टकराव शामिल है बल्क इसके साथ अलग-अलग जीवन शैलियों और राष्ट्रीयताओं के संघर्ष भी शामिल हैं। ये संघर्ष सामान्यतया आधुनिक इतिहास के अर्थों में ही देखे गये हैं। लेकिन हमे समझना चाहिए कि इतिहास में बहुत आरम्भ से ही धर्म दर्शन व संस्कृति के साथ-साथ राष्ट्रों और राज्यों के संघर्ष भी चलते आये हैं। इन संघर्षों को अक्सर ही राष्ट्रीयताओं के संघर्षों की तरह पेश करने से परहेज किया गया है। भारत में इस तरह के परहेज का आग्रह इतना प्रभावी रहा है कि यह अपने आप में स्वयं इतिहास और इतिहास लेखन के विरूद्ध ही एक संगठित षड्यंत्र बन चुका है। इस देश के मुख्य धारा के धार्मिक,सामाजिक, साहित्यिक विमर्श में दलितों या आदिवासियों का सदियों तक उल्लेख न होना कोइ भूल चूक की बात नही है। यह एक निर्णयपूर्वक अमल में लायी गयी रणनीति रही है। इस षड्यंत्र को इसकी मौलिक प्रेरणाओं सहित और इन प्रेरणाओं को आकार देने वाली असुरक्षाओं के सहित भी देखना होगा। तभी हम समझ पाएंगे कि इतने लंबे इतिहास में भारत में समाजशास्त्र क्यों नही पैदा हो सका,साथ ही अधिक महत्वपूर्ण रूप से हम यह समझ सकेंगे कि डॉ. कंगाली जैसे विद्वान सामाजिक ऐतिहासिक और धार्मिक दार्शनिक विमर्श की दिशा में कौन-सा आयाम खोल रहे हैं।
भारतीय समाज की समस्याएं जितनी बड़ी और बहुआयामी हैं उतना ही बड़ा और बहुआयामी होने को हर वो प्रयास बाध्य होगा जो इस समस्या के उचित निदान या उपचार के लिए संगठित होगा। इसीलिये डॉ. कंगाली के विराट अध्ययन को हम चरण दर चरण समझने का प्रयास करेंगे। वे सीधे सीधे भारतीय समाज की विशिष्ठ समस्याओं की तरफ एक दार्शनिक या समाजशास्त्रीय अंदाज में इशारा नहीं करते हैं, वह उनका विषय भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उनके गोंडी समाज के संबंध में किये गए अध्ययनों से जो एक नेरेटिव उभरता है वह अपने विस्तृत रूप में उन सभी प्रश्नों के हल की तरफ अनिवार्य संकेत करता है जो सब भाँति से सामाजिक और धर्म-दार्शनिक विकास के प्रश्न माने जाते हैं। उनकी खोजें और अनुवाद जिस ढंग से और जिस दिशा में गये हैं वे काल के तीनों आयाम में एक सुसंगत और तर्कपूर्ण विमर्श का द्वार खोलती हैं।
अक्सर ही समाजशास्त्रीय विमर्श इतिहास या धर्म दर्शन को बहुत प्रगाढ़ता से नहीं छूते हैं, इसी तरह ऐतिहासिक विमर्श भी एक समाज या संस्कृति के ज़िंदा तत्वों को उनकी समग्रता में नहीं छू पाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। लेकिन भारत के लिए इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ इतने लंबे ज्ञात इतिहास में न समाजशास्त्रीय विमर्ष उभर सका है न इतिहास का विमर्श उभर सका है। समाजशास्त्र या इतिहास विमर्श तो बहुत दूर की बात है एक समाज बोध और इतिहास बोध तक का यहाँ अभाव रहा है, यहाँ समाज एक अखंड रचना न होकर हजारों जातियों और कई वर्णों का एक ऐसा आत्मघाती समुच्चय रहा है जो न अंदर की तरफ विकास करता है न बाहर की तरफ।इसकी दोनों दिशाएँ आपस में संघर्ष करती रही हैं इसीलिये समाज को या राष्ट्र को इतना अवकाश ही नहीं मिला कि वह इन मूर्खताओं से बाहर निकल कर विज्ञान तकनीक और लोकतंत्र का निर्माण कर सके।
ऐसी ऐतिहासिक निर्वात की अवस्था में अलग-अलग विषयों से आने वाले विवरण या विमर्श स्वयं में खंडित ही रहे हैं और न केवल वे इतिहास सहित समाज के ऐतिहासिक क्रमविकास को अधूरे ढंग से पेश करते रहे हैं बल्कि सुदूर भविष्य में सरकने वाली उपचारमूलक प्रक्रियाओं के लिए भी अब तक खंडित और अधूरा मार्ग ही उपलब्ध करवा पाए हैं। यह स्थिति स्वयं में कारण भी है और परिणाम भी है। यही कारण है कि यहाँ के प्रचलित धर्म ने जिन विषयों को जिन रूपों में जनसामान्य तक पहुंचाने के जो जो मार्ग निर्मित किये हैं वे विषय, वे रूप और वे मार्ग – सब कुछ बहुत हद तक बाँझ साबित हुए है। इसी का परिणाम है कि जिसे हम मुख्य धारा का धर्म या संस्कृति या इतिहास कहते हैं वह इस देश की बहुसंख्यक जनसंख्या और उनके समाज सहित उनकी जीवन विधियों के वैविध्य के बारे में बिलकुल मौन खडा है। जिस प्रचलित व प्रचारित धर्म दर्शन और जिस सामाजिक या व्यक्तिगत आचारशास्त्र का महिमापूर्ण उल्लेख संस्कृत या क्लिष्ट हिंदी ने सुदूर अतीत में या उसके बाद दिया है, वह दलित, जनजातीय और स्त्री समाज के विषय में बहुत महत्वपूर्ण सूचनाओं और प्रवृत्तियों को रिकार्ड ही नहीं कर रहा है। एक सचेतन उपेक्षा है, जो भारत के ज्ञात इतिहास में इतिहास बोध और इतिहास लेखन के विरुद्ध पुराण बोध और पुराण लेखन को संगठित करती आयी है।
अगर ये भारत के इतिहास बोध और ऐतिहासिक न्यायबोध पर एक आरोप है तो इसे कैसे देखा समझा जाए? इसे कैसे अनुभव किया जाए? इसका बहुत सीधा सा उत्तर है। इसका पता लगाने का एक सूत्र है। यह खोज की जाए कि प्रचलित धर्म, कर्मकांड और धर्म या संस्कृति के प्रयासपूर्वक प्रचारित इतिहास में बहुसंख्यक जनता की मान्यताओं और जीवन दर्शन का कितना और किस रूप में प्रतिनिधित्व हो रहा है? इस एक सूत्र से हम जान पायेंगे कि एक कमजोर इतिहास बोध ने न सिर्फ एक कमजोर धर्म बोध व न्याय बोध के गर्भ से जन्म लिया है बल्कि हम ये भी देख सकेंगे कि इन कमजोरियों ने मिलकर इस खंडित और दिशाहीन समाज की रचना कैसे की है।

इस बड़े विस्तार में एक नजर देखने पर ही हम डॉ. मोतीरावण कंगाली के कार्यो का सही मूल्य आंक सकेंगे. इतने विस्तार में जाने पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं और कुछ लोग ये दावा कर सकते हैं कि स्वयं डॉ. कंगाली इस विस्तारित अर्थ में अपना काम नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर हम उनके काम की प्रकृति को समझेंगे तो इस तरह का प्रश्न स्वय में निर्मूल हो जाता है। वे भारत में प्रचलित इस “परजीवी धर्म” और “दिशाहीन संस्कृति” से परे जिस मौलिक धर्म और अपने उद्गम व लक्ष्य में आत्मविश्वास से भरी जिस संस्कृति को खोजकर सामने ला रहे हैं – उससे बहुत हद तक ये साफ़ होता है कि वे कहे अनकहे रूप में किस समग्रता में काम कर रहे थे। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि उनके काम को सही सन्दर्भों में देखकर हम अनेक प्रश्नों को उनकी बहुआयामी समग्रता में एकसाथ सुलझा सकते हैं।
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in