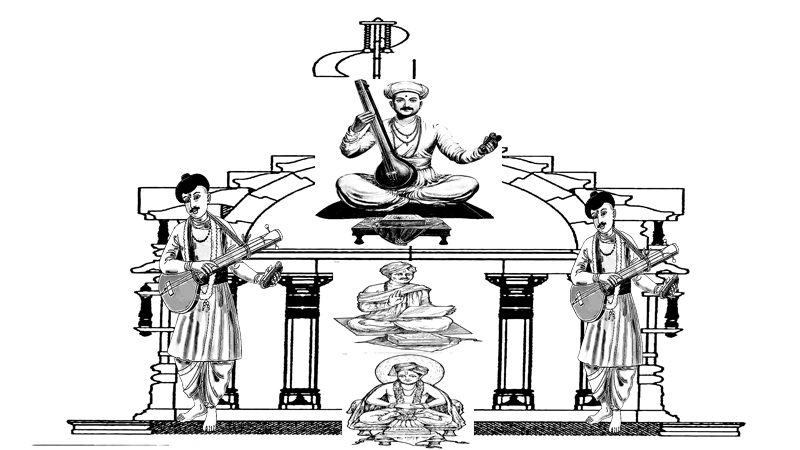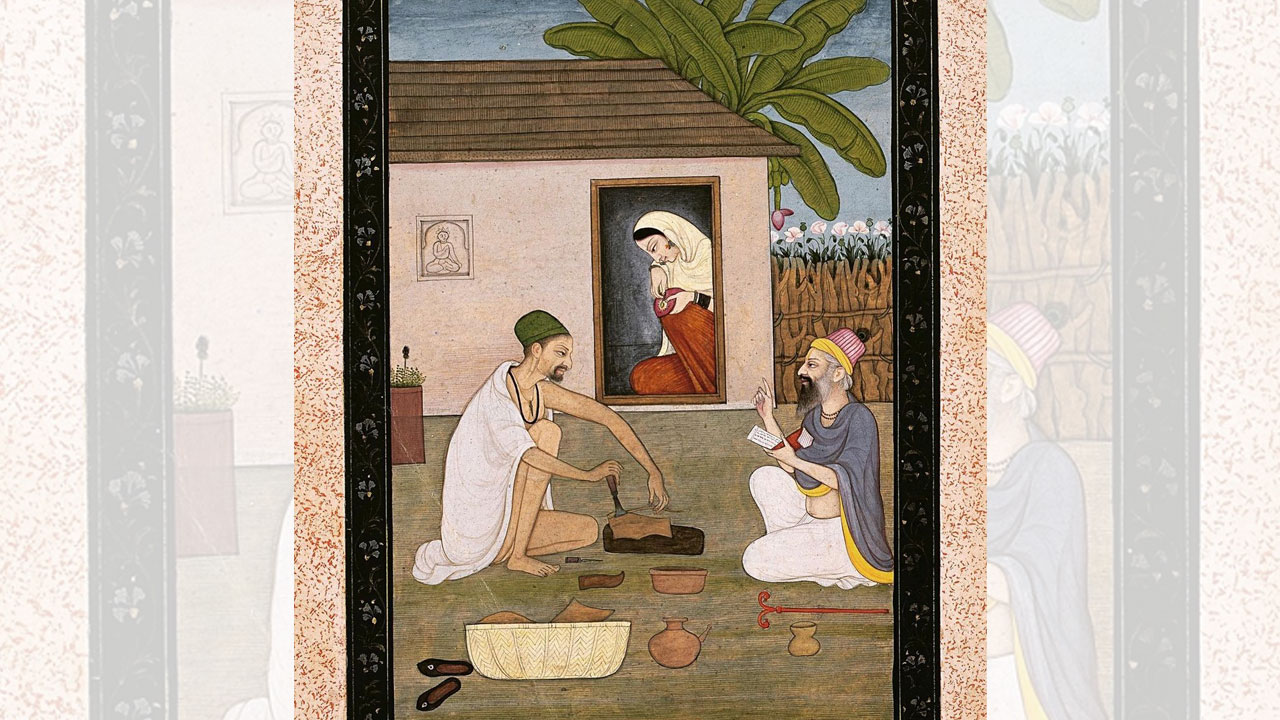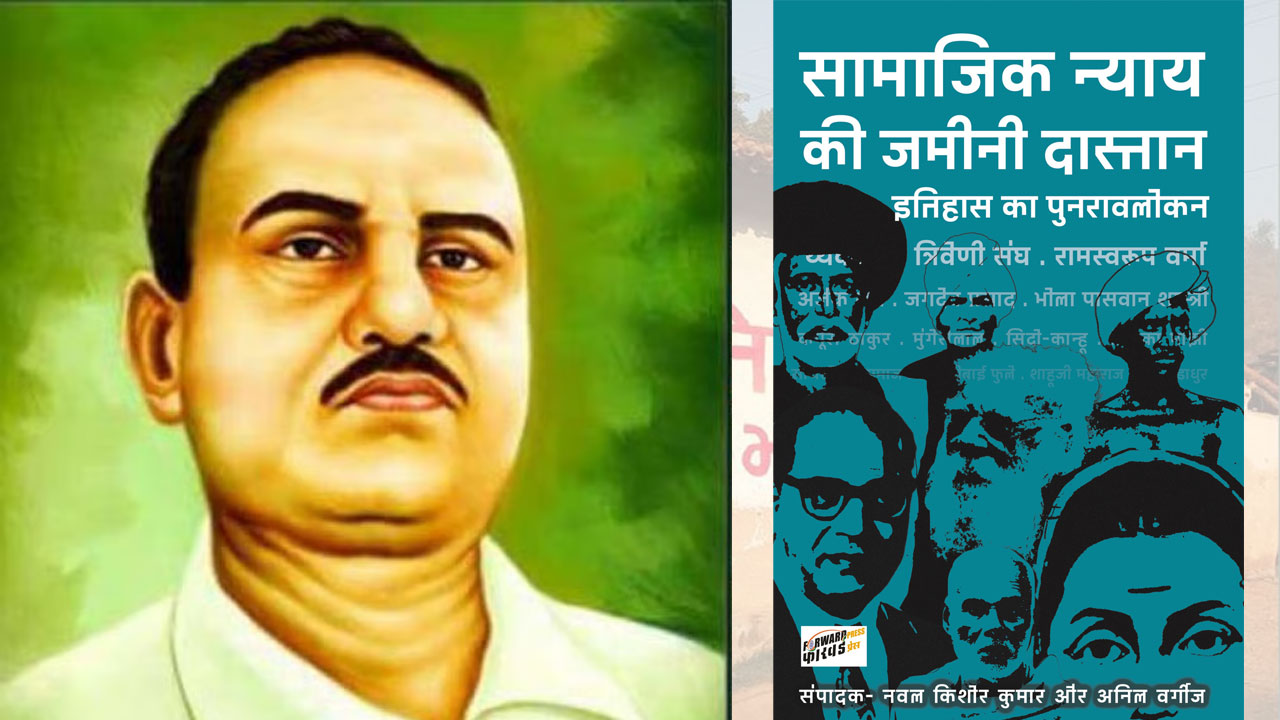कल्पना कीजिए एक भव्य मंदिर की, जिसे सदियों की मेहनत के बाद, उसके प्रति प्रेम से वशीभूत, शूद्रों द्वारा मराठियों व विशेषकर शूद्रों के, मक्का के रूप में निर्मित किया गया हो और यह मंदिर भविष्य में श्रद्धा-भक्ति की अन्य महान रचनाओं का प्रेरणास्रोत बना। मैं महाराष्ट्र में पला-बढ़ा और यद्यपि मैं एक गैर-मराठी कवि था, तथापि मैं इस विशाल मंदिर-विशेषकर उसके कलश-से प्रभावित हुए बगैर न रह सका। फिर आता है 19वीं सदी का एक आधुनिक शूद्र लेखक-चिंतक, जो इस शानदार इमारत से मुंह फेर लेता है और एक नया निर्माण शुरू करता है। उसके इस पूर्ण अस्वीकार, जिसके बारे में आज भी हम बहुत कम जानते हैं, के पीछे के कारणों को बहुजन साहित्य को सूत्रबद्ध करने के इच्छुक लोगों को समझना चाहिए। आगे बढऩे के पहले उन्हें इस अस्वीकार के कारणों और आधारों का विवेचन और आकलन करना चाहिए।
तुकाराम की कविताओं के अपने अद्भुत अनुवाद पर आधारित अपनी पुस्तक (सेज तुका, पेंग्विन, नई दिल्ली, 1991) में दिवंगत मराठी कवि व कलाकार दिलीप चित्रे लिखते हैं :
तुकाराम की समकालीन, यद्यपि उम्र में उनसे कुछ छोटी, बाहिनाबाई सिऊरकर ने भक्ति की वरकारी परंपरा का वर्णन करने के लिए मंदिर के रूपक का प्रयोग किया है। वे लिखती हैं कि ज्ञानदेव ने उसकी नींव रखी, नामदेव ने उसकी दीवारें बनाईं, एकनाथ ने उसके केंद्रीय स्तंभ का निर्माण किया और तुकाराम, उसके कलश बने। जैसा कि बाहिनाबाई के वर्णन से स्पष्ट है, वरकारी परंपरा का निर्माण इन चार महान संतों और उनके अनेक प्रतिभासंपन्न अनुयायियों ने किया था। उनकी यह मान्यता बिल्कुल सही है कि वह एक सामूहिक कलात्मक कृति थी, जिसके विभिन्न भागों का निर्माण अलग-अलग शताब्दियों में अलग-अलग लोगों द्वारा किया गया था और इन टुकड़ों को जोड़कर एक पूर्णाकार दिया गया था-एक ऐसा पूर्णाकार जो केवल सामूहिक परंपरा से ही अस्तित्व में आ सकता था। मराठी वरकारी कवियों की उपलब्धियों की तुलना केवल एक अन्य कलाकृति से की जा सकती है…और संयोगवश वह भी महाराष्ट्र में हैं-अजंता के भित्तिचित्र और एलोरा की मूर्तिकला और स्थापत्य…।
चित्रे, तुकाराम की महानता के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। वे कहते हैं कि तुकाराम वैश्विक दृष्टि से और विशेषकर उनकी मराठी भाषा और संस्कृति के, एक ऐसे कवि थे जो लाखों लोगों की प्रेरणा का स्रोत थे।
अत: तुकाराम न केवल मराठी के अंतिम महान भक्ति कवि थे बल्कि वे सही अर्थों में, पहले आधुनिक मराठी कवि भी थे। उनकी सोच, उनकी कविता की विषयवस्तु, तकनीक और दृष्टिकोण के लिहाज से, निस्संदेह, यह कहा जा सकता है कि वे मध्यकालीन और आधुनिक मराठी कविता को जोडऩे वाली सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थे।
मराठी साहित्य में तुकाराम के दर्जे की तुलना अंग्रेजी में शेक्सपीयर या जर्मन में गेटे से की जा सकती है। वे एक ऐसे अमर कवि थे जिनके लेखन से मराठी भाषा की अपूर्वता व उसकी विशिष्ट साहित्यिक संस्कृति की झलक मिलती है। तुकाराम के बाद कोई ऐसा मराठी लेखक नहीं हुआ जिसने मराठी की साहित्यिक संस्कृति पर इतना गहरा और व्यापक प्रभाव डाला हो। तुकाराम की कविता ने साहित्यिक मराठी ही नहीं बल्कि उस मराठी भाषा को भी गढ़ा, जो आज पांच करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। शायद उनके प्रभाव की तुलना हम बाइबल के किंग जेम्स संस्करण के (सन् 1611 में) प्रकाशन के अंग्रेजी भाषा पर पड़े प्रभाव से कर सकते हैं। यही कारण है कि तुकाराम की कविताओं का इस्तेमाल, आज भी लाखों अशिक्षित लोग प्रार्थना करने या ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं।
तुकाराम की मराठी, ग्रामीण महाराष्ट्र में आम आदमी द्वारा बोली जाने वाली मराठी है। वह श्रेष्ठी वर्ग की भाषा नहीं है। वह ब्राह्मण पुरोहितों की भाषा नहीं है। वह आम आदमी की भाषा है-किसान की, व्यापारी की, कारीगर की, मजदूर की और गृहणी की। उनकी भाषा और उनके बिंब, लोगों के रोजाना के अनुभवों पर आधारित हैं यद्यपि इसके साथ ही, उसमें कई विभिन्न तरीकों से और संदर्भों में सत्य को प्रकाश में लाने और आपके ज्ञान में वृद्धि करने की क्षमता भी है। तुकाराम ने आम बोलचाल की भाषा में ऐसी उत्कृष्ट रचनाएं की हैं जिनकी प्रकृति वैश्विक है।
फुले शूद्र-अतिशूद्र मराठी आमजनों से संवाद स्थापित करना चाहते थे। ऐसे में, क्या उनके लिए यह स्वाभाविक न होता कि वे इस महान कवि की वाणी का इस्तेमाल करते-उस वाणी का, जो उनके जन्म से दो शताब्दियों पूर्व शांत हो चुकी थी। फुले पर अपनी उत्कृष्ट रचना (कॉस्ट, कनफिल्क्ट एण्ड आईडियोलाजी-महात्मा जोतिराव फुले एण्ड लो कास्ट प्रोटेस्ट इन नाईनटींथ सेंचुरी वेस्टर्न इंडिया, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1985) में रोजालिण्ड ओ. हेनलान लिखती हैं :
सभी प्रमुख समाज सुधारक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते थे और वे उन मुद्दों, जिन्हें वे भारत के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे, पर चर्चा के लिए एक साझा मंच का निर्माण करना चाहते थे। यह कोशिश पश्चिमी भारत के लिए बिल्कुल नई थी। भारतीय धार्मिक जीवन में तर्कवितर्क की परंपरा अवश्य थी परंतु तब तक यह बहस केवल किसी संप्रदाय या पंथ विशेष के अनुयायियों के बीच ही हुआ करती थी। उदाहरणार्थ, पश्चिमी भारत के भक्ति पंथों में भी बहस और चर्चा का क्षेत्र सीमित था। पश्चिमी प्रोटेस्टेंट मिशनरियों के पूर्वी (बंगाल से शुरू कर) व पश्चिमी भारत (मुख्यत: महाराष्ट्र) में प्रभाव के चलते हुए सामाजिक व धार्मिक सुधारों की पृष्ठभूमि में भक्ति कवियों की रचनाओं को एक नई दृष्टि से देखने की शुरुआत हुई। मिशनरियां इन्हें मराठीजनों के ईसा मसीह तक पहुंचने के पुल के रूप में देखती थीं। यहां तक कि ब्राह्मण वामनराव तिलक, जिन्हें मराठी में प्रकृति पर केन्द्रित अपनी कविताओं के कारण महाराष्ट्र का वर्डसवर्थ
कहा जाता है, ने भी कहा है कि तुकाराम वह पुल थे, जिसे पार कर वे ईसा तक पहुंचे।
जिस दौर में फुले और उनके साथी सामाजिक और आध्यात्मिक सुधार के अपने कार्य में जुटे थे, उसी समय भक्ति कवियों से संबद्ध एक अन्य सुधार आंदोलन भी प्रारंभ हो गया। ओ. हेनलान लिखती हैं : पश्चिमी भारत में उस दौर में जो धार्मिक सुधार आंदोलन चले, उनमें से सबसे जाना-पहचाना है प्रार्थना समाज। सन् 1860 में परमहंस मण्डली के विघटन के बाद, उसके कुछ सदस्यों ने सन् 1867 में प्रार्थना समाज का गठन किया…समाज के सदस्यों को उम्मीद थी कि मूर्तिपूजा व जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक बुराईयों का परोक्ष रूप से विरोध, आमजनों को अधिक स्वीकार्य होगा, क्योंकि परमहंस मंडली का इन बुराईयों पर बिना किसी लागलपेट के किया गया सीधा हमला, असफल रहा था। एमजी रानाडे ने सन् 1869 में प्रार्थना समाज की सदस्यता ली। जल्दी ही वे संस्था के सबसे प्रभावशाली सदस्य बन गए और उन्होंने उसके धार्मिक विचारों को सुसंगत बनाने का कार्य शुरू किया। रानाडे का तर्क था कि दुनिया के सभी धर्म, विकास के दौर में हैं और अंतत: वे शुद्ध ईश्वरवादी बनेंगे…। धर्म के विकासरत् होने की बात करने के साथ-साथ, प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र के संत-कवियों, विशेषकर 17वीं सदी के संत तुकाराम, में विशेष रुचि दिखलानी शुरू की। प्रार्थना समाज, तुकाराम को एक पुराने किस्म का ईश्वरवादी समझता था। प्रार्थना समाज के बढ़ते प्रभाव के साथ महाराष्ट्र के बुद्धिजीवी, धर्म के एक ऐसे स्वरूप की खोज में जुट गए जिसमें वह सब शामिल होगा जो हिन्दू परंपरा का श्रेष्ठ व अंगीकार करने योग्य हिस्सा है और साथ ही उसमें हिन्दू परिवर्तनवादियों व यूरोपीय पर्यवेक्षकों द्वारा धर्म में बताई गई कमियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। नए स्वरूप की यह तलाश, उन्हें संत कवियों की रचनाओं की ओर ले गई जो अपने भगवान से अतिशय प्रेम करते थे और इस प्रेम की जड़, हिन्दू धर्म में थी। साथ ही, वे जाति की कट्टर विभाजक रेखाओं के खिलाफ भी थे और ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा के हामी नहीं थे। जातिप्रथा और ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धाभाव, तत्कालीन हिन्दू धर्म का अनिवार्य हिस्सा था।
फुले की संत तुकाराम सहित सभी संत कवियों के प्रति सोच जटिल और कुछ-कुछ अस्पष्ट थी। प्रार्थना समाज की तरह वे यह देख सकते थे कि भक्ति कवियों ने बहु-ईश्वरवाद, मूर्तिपूजा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व को खारिज किया था। दिवंगत मराठी लेखक व आलोचक जीपी देशपांडे (द वल्र्ड ऑफ आईडियास इन मार्डन मराठी, तूलिका, नई दिल्ली, 2006) लिखते हैं : तृतीय रत्न (1855) में मूर्तिपूजा के विरुद्ध ओजपूर्ण तर्क हैं…परंतु यह आश्चर्य का विषय है कि उन्होंने भक्ति आंदोलन और मूर्तिपूजा के बारे में उसके विचारों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। ध्यानेश्वर, जिन पर फुले ने अपनी कुछ रचनाओं में निशाना साधा है, ने मूर्तिपूजा के खिलाफ अभंग लिखे हैं। अभंग एक ऐसा छंद है जिसका प्रयोग संत कवियों के बीच बहुत लोकप्रिय था। फुले ने स्वयं भी कई अभंग लिखे परंतु उन्होंने उनके लिए एक नया शब्द इस्तेमाल किया ‘अखण्ड’। उन्होंने अपने तर्कों को मजबूती देने के लिए उस परंपरा का इस्तेमाल नहीं किया जो महाराष्ट्र के शूद्रों और अतिशूद्रों के बीच लोकप्रिय थी। तीक्ष्णबुद्धि देशपांडे यह समझने में असफ ल रहे कि फुले ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ अपने युद्ध में संत कवियों जैसे शक्तिशाली हथियार का प्रयोग क्यों नहीं किया।
 परंतु ओ. हेनलान फुले की नब्ज पर हाथ रखने में सफल रहीं : इस धार्मिक परंपरा के मराठी संत-लेखकों की अधिकांश रचनाओं में आध्यात्मिकता और जातिगत उच्चता के बीच किसी भी संबंध के अस्तित्व से इनकार किया गया है। इस परंपरा में यह माना जाता है कि किसी व्यक्ति का ईश्वर के प्रति प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे उसकी जाति कोई भी क्यों न हो। इस मुद्दे पर 17वीं सदी के भक्ति
परंतु ओ. हेनलान फुले की नब्ज पर हाथ रखने में सफल रहीं : इस धार्मिक परंपरा के मराठी संत-लेखकों की अधिकांश रचनाओं में आध्यात्मिकता और जातिगत उच्चता के बीच किसी भी संबंध के अस्तित्व से इनकार किया गया है। इस परंपरा में यह माना जाता है कि किसी व्यक्ति का ईश्वर के प्रति प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे उसकी जाति कोई भी क्यों न हो। इस मुद्दे पर 17वीं सदी के भक्ति
संत तुकाराम ने विशेष जोर दिया है। परंतु उनकी यह सोच कभी उनके द्वारा उन धार्मिक मूल्यों से लोहा लेने या उनका खंडन करने के बौद्धिक प्रयास का आधार नहीं बनी, जो मूल्य जातिगत पदानुक्रम पर जोर देते हैं और ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताते हैं। वे व्यक्तिगत तौर पर भक्तों को आध्यात्मिक शांति पाने में मदद करते रहे परंतु उन्होंने कभी ब्राह्मणों की सत्ता को सीधी चुनौती नहीं दी…। इस विश्लेषण को कई अन्य भारतीय विद्वानों ने दुहराया है व इसकी पुष्टि की है। इनमें शामिल हैं जयंत के. लेले व आर. सिंह (ट्रेडिशन एण्ड मार्डेनिटी इन भक्ति मूवमेंट्स, लेंग्वेज एण्ड सोसायटी : स्टेह्रश्वस टूवर्डस एन इंटीग्रेटिड थ्योरी, बीआरआईएलएल, लाईडेन, 1989):
फुले ने संत कवियों को ऐसे कर्मकांडी, आत्मनिंदक संन्यासी बताया जिन्हें ‘इहलोक’ से कोई मतलब नहीं था। उन आमजनों, जिनके प्रति वे फिक्रमंद थे और जिनकी ओर से वे बोलते थे, से सीधे संवाद के अभाव में फुले, वरकारी कवियों की इस द्वंद्वात्मक परंपरा को स्वीकार नहीं कर सके, जिसमें ये कवि लोगों के लिए सांत्वना और शांति के स्रोत तो थे परंतु वे गरीबों को दमन के खिलाफ उठ खड़े होने की प्रेरणा नहीं देते थे। यहां तक कि फुले ने अपनी कविताओं के छंद को वह नाम (अभंग) तक देने से इनकार कर दिया क्योंकि इस छंद का प्रयोग मुख्यत: वरकारी कवियों ने किया था। वरकारियों की सोच का यह अस्वीकार, वरकारी ग्रंथों और संतों के आचरण के पारंपरिक विवेचना पर आधारित था और भक्ति व चिडविलास की इसी विवेचना का इस्तेमाल (बालगंगाधर) तिलक ने आगे चलकर रानाडे के बुद्धिजीवियों के खिलाफ अपने तर्कों में किया।
यद्यपि देशपांडे, फुले द्वारा भक्ति कवियों के साहित्यिक अस्वीकार को पचा नहीं सके परंतु वे उसे दर्शन के स्तर पर स्वीकार करते हैं :
‘धर्मविचार’ पर कोई भी चर्चा जोतिराव फु ले (1827-1890) से प्रारंभ होनी चाहिए। फुले शायद ऐसे पहले विचारक थे जिन्होंने ‘अवतार कल्पना’ की अवधारणा पर हमला किया…डा. आंबेडकर की संस्कृत (या वैदिक) धर्म व पाली (या अवैदिक) धर्म के बीच अंतर की समझ की जड़ें, फुले द्वारा वैदिक या ब्राह्मणवादी धर्म व उनके सार्वजनिक सत्य धर्म के बीच किए गए अंतर में खोजी जा सकती हैं। बेहतर तो यह होगा कि हम फु ले के लेखन को दर्शन की बजाय आलोचनात्मक सैद्धांतिकी के रूप में देखें और सूक्ष्मता से विचार करने पर यह साफ हो जाएगा कि फुले का लेखन ‘विताड़’ की श्रेणी में आता है जो कि नैयायिक परंपरा का शब्द है और जिसका अर्थ है दर्शन के स्तर पर पारंपरिक सोच से पूर्ण विलगता। फुले ने धर्म का विताड़ प्रस्तुत किया। वे शायद भारत के पहले आधुनिक चिंतक थे, जिन्होंने भारतीय समाज को वैदिक या ब्राह्मणवादी व अवैदिक या गैर-ब्राह्मणवादी धर्मों के बीच के दार्शनिक विभेदों के आधार पर वर्गीकृत किया। इस तरह, उन्होंने संघर्ष के मूल या मुख्य क्षेत्र का सीमांकन किया और वह भी उसे बिना नस्लीय या जाति-आधारित संघर्ष का स्वरूप दिए।
यद्यपि फुले ने पूरे तौर पर-दर्शन व कविता दोनों संदर्भों में मराठी भक्ति कवियों की वरकारी परंपरा को उसमें मौलिकता व उग्रता के
अभाव के आधार पर खारिज कर दिया था परंतु उन्होंने उत्तर भारत के संभवत: सबसे महान भक्ति कवि कबीर के भी विचारों को स्वीकार नहीं किया। इसके बारे में ओ हेमलोन लिखती हैं : अब हम सत्यशोधक समाज की स्थापना के ठीक पहले के समय की बात करेंगे जहां हमें इस बात के सबूत मिलते हैं कि फुले और उनके साथियों पर कबीर के विचारों का प्रभाव था। तुकाराम हनामंत तिंजन, जो आगे चलकर सत्यशोधक समाज के सदस्य बने, बतलाते हैं कि समाज की स्थापना के कुछ महीनों पहले से, फुले के मित्र और साथी हर इतवार को पुणे में उनकी दुकान पर इकट्ठा होते थे। इनमें कबीर पंथ के एक सदस्य ध्यानगिरी बुवा भी शामिल थे। ध्यानगिरी कबीर द्वारा लिखित ‘बीजक’ को ब्रज भाषा से मराठी में अनुदित कर उपस्थित लोगों को सुनाते थे। पुस्तक में ब्राह्मणों के स्वार्थी दृष्टिकोण और उनके कुकर्मों का विशद्वर्णन है। तिंजन लिखते हैं कि फुले बहुत लंबे समय सेयह मानते थे कि गैर-ब्राह्मणों की समस्याओं का मूल, ब्राह्मणों के दृष्टिकोण में है। उनकी इस मान्यता को कबीर का भी समर्थन प्राप्त है, यह जानकर वे उन व्यावहारिक कदमों पर विचार करने लगे जिनसे गैर-ब्राह्मणों की स्थिति में सुधार आएगा। वहां उपस्थित लोगों ने फुले के इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि उन्हें एक संगठन का गठन करना चाहिए। लंबे विचार-विमर्श के बाद इस संगठन के लिए सत्यशोधक समाज का नाम चुना गया और 24 सितंबर, 1873 को इसका औपचारिक रूप से गठन हुआ। मैं इस ऐतिहासिक घटना का पूरा विवरण जानते-बूझते दे रहा हूं। स्पष्टत: फुले को यह समझ में आ रहा था कि कबीर व मराठी वरकारी भक्ति कवियों की रचनाओं में कुछ मूल अंतर थे। आम्बेडकर, जिनका जन्म फुले की मृत्यु के एक वर्ष बाद, एक कबीरपंथी परिवार में हुआ था, को मानो कबीर का दर्शन और उनकी रचनाएं विरासत में प्राप्त हुई थीं। यहां तक कि उनके गुरुओं की सूची में बुद्ध के बाद कबीर थे और तत्पश्चात् फुले। आम्बेडकर ने भी अपने गुरु की तरह, मराठी भक्ति कवियों की रचनाओं को खारिज किया।
परंतु आंबेडकर, फुले की तरह, साहित्यिक लेखक व आलोचक नहीं थे। देशपांडे और अन्य आलोचक मानते हैं कि फुले के लिए, भक्ति कवियों से जाने-अनजाने प्रभावित हुए बगैर मराठी में कोई भी साहित्यिक लेखन करना लगभग असंभव रहा होगा। वे लिखते हैं कि फुले की कविता पर ‘सत्रहवीं शताब्दी के भक्ति कवि तुकाराम का गहरा प्रभाव था।’ और यह कि ‘विभिन्न भक्ति कवियों का, उनके द्वारा किया गया आकलन..मराठी सामाजिक-साहित्यिक आलोचना की शुरुआत कहा जा सकता है।’ अंत में, फुले द्वारा भक्ति कवियों को स्पष्ट तौर पर खारिज करने से उपजे दो पश्नों के उत्तर की दरकार है। पहला, वस्तुनिष्ठ मराठीसाहित्यिक आलोचकों का यह प्रश्न कि भक्ति कवियों को खारिज करने से फु ले की साहित्यिक, विशेषकर काव्यात्मक लेखन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई या गिरावट आई? दूसरा प्रश्न, जिस पर
सामाजिक इतिहासविद् अनंतकाल तक बहस कर सकते हैं वह यह है कि इससे क्या ब्राह्मणविरोधी आंदोलन की गहराई और उसकी व्यापकता बढ़ी या घटी?
सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बहुजन साहित्य का निरुपण करने वाले और उसके पैरोकार, आधुनिक बहुजन साहित्य केपितामह फुले से क्या सीख सकते हैं।
(फारवर्ड प्रेस, बहुजन साहित्य वार्षिक, मई, 2014 अंक में प्रकाशित )