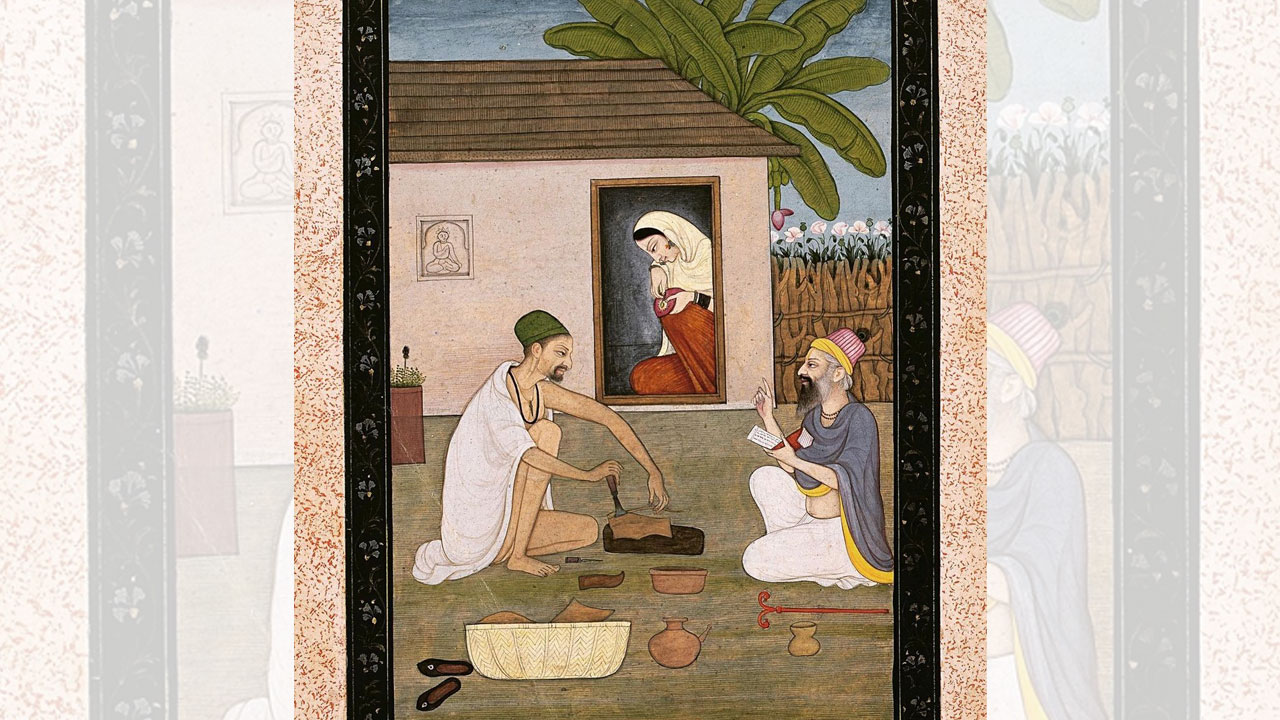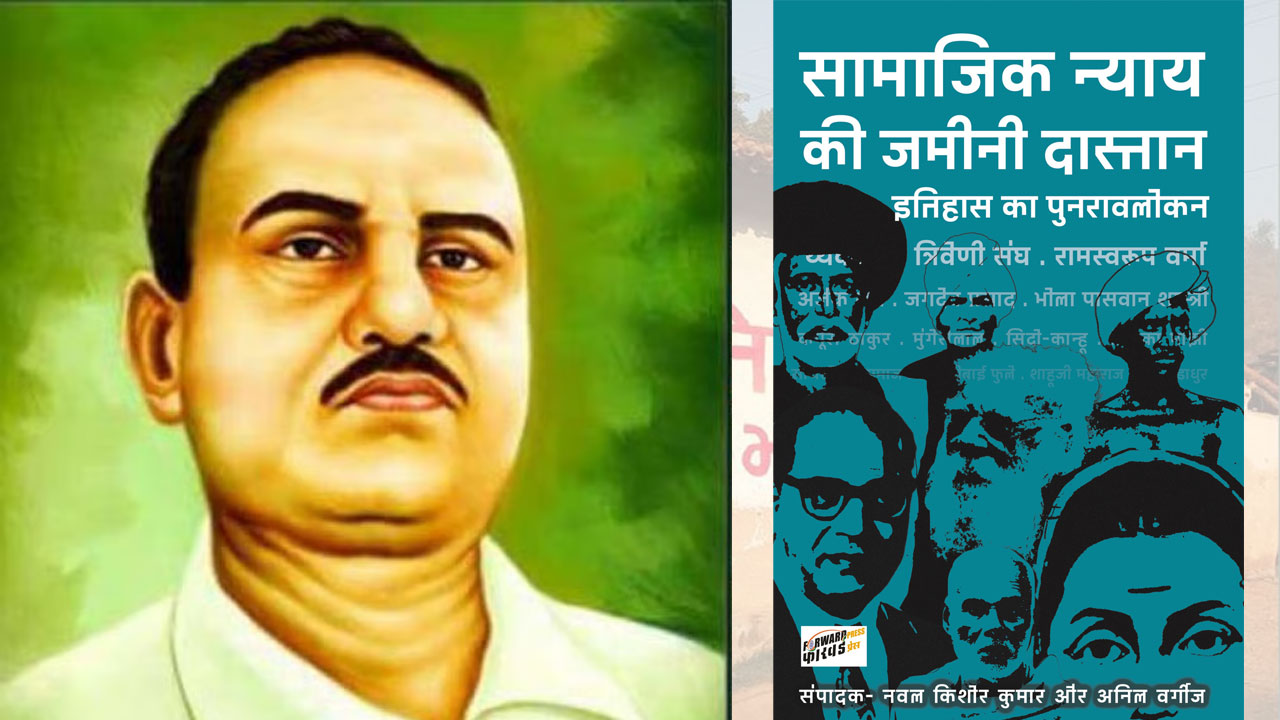यद्यपि औपनिवेशिक राज्य जाति व्यवस्था का आलोचक था परंतु इसके साथ ही वह सामाजिक समूहों को जाति और जनजाति की श्रेणियों में विभाजित करता था और इन्हीं के रूप में उनकी गणना भी करता था। औपनिवेशिक शासन के विरोधी शीर्ष नेतृत्व में गांधी और आंबेडकर शामिल थे। इन दोनों के अछूत प्रथा के संबंध में मुक्तलिफ विचार थे। आंबेडकर, आधुनिकता में अपने दृढ विश्वास के चलते यह कहते थे कि राजनीतिक सुधार के पूर्व सामाजिक सुधार होने चाहिए। उनका मानना था कि आधुनिक नियम किसी भी ऐसे समाज पर लागू नहीं किए जा सकते जो परंपरा से नियंत्रित हो।[1] आंबेडकर के लिए सामाजिक सुधार का अर्थ था अछूतों की ऊँची जातियों से रोजाना के संघर्ष से मुक्ति, कार्यस्थल और समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा और जाति का पूर्ण उन्मूलन। वे सामाजिक बहिष्करण से निपटने के संबंध में कांगे्रस की सोच से असहमत थे। कांग्रेस अध्यक्ष डब्लूसी बैनर्जी ने सन 1892 में पार्टी के इलाहबाद में आयोजित अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो यह कहते हैं कि हम तब तक राजनीतिक सुधार नहीं कर सकते जब तक कि हम हमारी सामाजिक व्यवस्था को नहीं बदल देते। मैं दोनों के बीच कोई संबंध नहीं देखता‘‘।[2]
समाजवादी, सामाजिक बहिष्करण को अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखते थे। उनकी यह मान्यता थी कि समाजवाद के आगाज से जाति स्वमेव अदृश्य हो जाएगी। इस तर्क का आंबेडकर के पास जवाब यह था कि अगर वर्गीय विवेचना में जाति को नजरअंदाज किया गया तो कार्यस्थल जातिगत विभेद के अड्डे बन जाएंगे।[3]
आंबेडकर, जाति के उन्मूलन के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध थे। उन्होंने इसके समर्थन में अपनी लेखनी में कई तर्क दिए, जिनमें से अधिकांश बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित थे। उन्होंने अछूत प्रथा को अपरोक्ष रूप से स्वीकार करने के लिए कांग्रेस पर कटु हमले किए। परंतु आंबेडकर अपने समय की आधुनिकता से प्रभावित थे और इसलिए उन्हें समाज के कुछ तबकों को मताधिकार से वंचित रखने या राजनीतिक सुधार से अलग रखने में कुछ भी गलत नहीं दिखता था। आर्थिक प्रगति का यूरोप-केन्द्रित माडल, उत्पादन के साधनों के आधार पर समाजों और संस्कृतियों को श्रेणीबद्ध करता था। सामाजिक विकासवादियों के विचारों के प्रभाव के चलते जो समाज, सभ्यता के तथाकथित पदक्रम में नीचे के पायदानों पर होते थे, उन्हें अक्सर राजनीतिक और सामाजिक बहिष्करण का सामना करना पड़ता था। सन 1929 में साईमन आयोग के समक्ष अपने बयान में आंबेडकर ने कहा, ‘‘आदिम जनजातियों में अब तक इतनी राजनीतिक समझ विकसित नहीं हो सकी है कि वे उन्हें उपलब्ध राजनीतिक अवसरों का उचित इस्तेमाल कर सकें और वे किसी भी बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदाय के हाथों का खिलौना बनकर, खुद का कुछ भी भला किए बगैर, संतुलन को बिगाड़ सकती हैं।‘‘[4]
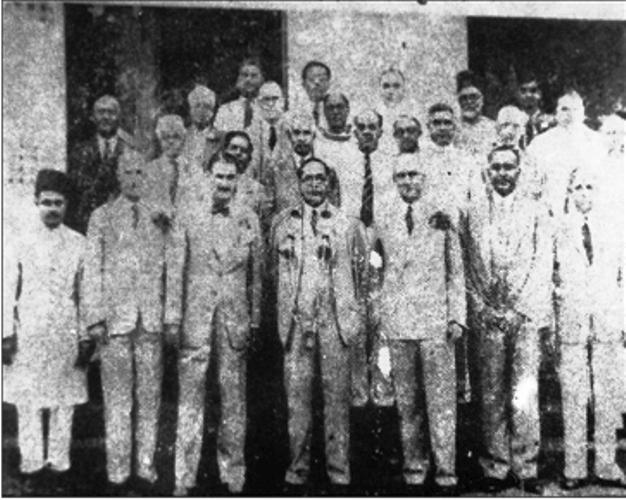
जाति को जनजाति से अलग कर देखने के कारण आंबेडकर ने, अपने अनेक पूर्ववर्तियों की तरह, ‘सभ्यों‘ और ‘असभ्यों‘ के बीच दीवार खड़ी कर दी। इस दृष्टिकोण के चलते जनता के एक बड़े तबके को दमन का सामना करना पड़ा। यह इस तथ्य के बावजूद कि उनमें और स्थापित जातियों में कई सांस्कृतिक और धार्मिक समानताएं थीं।
गांधी के लिए धर्म के बिना राष्ट्र का कोई अस्तित्व नहीं था। उनके शब्दों में, ‘‘मैं नहीं मानता कि धर्म का राजनीति से कोई लेनादेना नहीं है। धर्म से विलग राजनीति केवल एक लाश के समान है, जिसे गाड़ दिया जाना चाहिए।[5] डब्ल्यूडब्ल्यू हंटर (19वीं सदी के उत्तरार्ध व 20वीं सदी के पूर्वार्ध के एक नृवंशविज्ञानी) को उद्धत करते हुए गांधी कहते हैं ‘‘भारत को कभी गरीबों के लिए किसी अलग कानून अथवा मृत्यु, बीमारी और गरीबी की स्थिति में जाति-विनियमित सेवा की जरूरत नहीं थी।[6] हंटर की राय यह थी कि पुरानी संस्थाओं का अध्ययन और पड़ताल कर उन्हें पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। यह गांधी को स्वीकार्य था क्योंकि वे हिन्दू धर्म के समर्थक थे और हिन्दुओं के अन्य धर्मों को अंगीकृत करने के खिलाफ थे। गांधी का सोचना यह था कि अछूत प्रथा, हिन्दुओं का एक आंतरिक मसला है और उन्हें पवित्रता और प्रदूषण के उन विचारों से स्वयं ही मुक्त होना पड़ेगा, जिनके कारण वे अछूतों का स्पर्श नहीं करते और उनके साथ भोजन आदि ग्रहण नहीं करते।
आंबेडकर के लेख ‘द एनिहीलेशन आफ कास्ट‘ के प्रतिउत्तर में उन्होंने जाति का बचाव करते हुए कहा कि जाति एक पैतृक कर्तव्य है और अपने लिए निर्धारित कार्य करने में कुछ भी गलत नहीं है। हिन्दू धर्म के भ्रष्ट हो जाने पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि आंबेडकर, हिन्दू धर्म के प्रसिद्ध संतों की शिक्षा को नजरअंदाज करते हुए ऐसे ग्रंथों का हवाला दे रहे हैं, जो प्रामाणिक नहीं हैं।[7] यहां गांधी चैतन्य, ज्ञानदेव, तुकाराम, तिरूवल्लुवर, रामकृष्ण परमहंस, राजा राममोहन राय, महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोर और विवेकानंद की बात कर रहे थे।[8] वे अछूतों को ‘भंगी‘ और ‘अंत्यज‘ के नाम से पुकारते हैं और आंबेडकर से भी एक कदम आगे बढ़कर यह कहते हैं कि नीची जातियों का हिन्दुकरण किए जाने की आवश्यकता है।

यह स्पष्ट है कि गांधी और आंबेडकर के भाषणों और लेखनी से यह झलकता है कि वे औपनिवेशिक राज्य के आधुनिकीकरण व ‘सेडेंटराईजेशन‘ (किसी घुमंतु आबादी का एक स्थान पर बस जाना) के तत्कालीन वर्चस्वशाली आख्यान से सहमत थे। जहां आंबेडकर एक सांविधिक आयोग का गठन कर आदिवासियों को मताधिकार से वंचित करने के हामी थे, वहीं गांधी भंगियों और अंत्यजों का हिन्दुकरण करना चाहते थे। गांधी इस वैदिक परिकल्पना से सहमत थे कि प्रत्येक व्यक्ति को वही मिलना चाहिए, जिसका वह अपने जन्म के आधार पर अधिकारी है। गांधी की यह सोच, औपनिवेशिक नृवंशविज्ञानियों के नस्ल आधारित सिद्धांतों के अनुरूप थी।[9]
आदिवासियों के बहिष्करण की दो अवधारणायें
सन 1919 के मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत, इंडियन स्टेच्यूटरी कमीशन (साइमन कमीशनद्) गठित किया गया। इस आयोग को इस विषय पर विचार करना था कि भारतीय उपमहाद्वीप, संवैधानिक सुधारों के लिए तैयार है अथवा नहीं और यह भी कि इन सुधारों का देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयोग को देश में शिक्षा और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थिति के संबंध में विस्तृत रपट प्रस्तुत करनी थी। उसे यह भी तय करना था कि देश के नागरिकों को मताधिकार देने की क्या शर्तें हों। आंबेडकर के इस आयोग के समक्ष दिए गए बयान को समझने के लिए पहले हमें उन मानदंडों का अध्ययन करना होगा, जो औपनिवेशिक राज्य ने मताधिकार प्रदान करने हेतु निर्धारित किए थे।

अधिकांश नगरपालिकाओं में मतदाताओं की पात्रता का निर्धारण करने वाले नियम सन 1886 में बनाए गए थे और 1917 तक लगभग अपरिवर्तित रहे। मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी और यह आवश्यक था कि मतदाता संबंधित शहर में रहते हों या व्यापार करते हों या उनकी वहां अचल संपत्ति हो और वे नगरपालिका को कर चुकाते हों। इसके अतिरिक्त नियमों में कुछ वैकल्पिक पात्रताओं का उल्लेख भी था जैसेः[10]
(1) नगरपालिका सीमा के अंदर निर्दिष्ट मूल्य की अचल संपत्ति का मालिकाना हक। अधिकांश मामलों में न्यूनतम मूल्य रू. 200 और कुछ बड़े शहरों के मामले में रू. 300 था।
(2) किराएदारों के मामले में न्यूनतम 1 रू. प्रतिमाह और बड़े शहरों के मामले में रू. 2 प्रतिमाह किराया।
(3) निर्दिष्ट न्यूनतम आय जो सामान्यतः रू. 10 प्रतिमाह और बड़े शहरों में रू. 15 से रू. 25 प्रतिमाह थी।
(4) न्यूनतम निर्दिष्ट आय के साथ या उसके बिना, कुछ शैक्षणिक योग्यताएं। सामान्यतः यह शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी थी परंतु बड़े शहरों में विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक था।
(5) न्यूनतम रू. 25 प्रति वर्ष का भूराजस्व का भुगतान।
सन् 1917 में सभी नगरपालिकाओं के निर्वाचन नियमों को परिवर्तित किया गया। पात्रता के मानदंड पूर्वानुसार ही रखे गए परंतु भूराजस्व को छोड़कर, अन्य मामलों में ‘कट आफ’ बढ़ा दिया गया। अचल संपत्ति, किराए व आय की न्यूनतम सीमा में बढ़ोत्तरी की गई और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को बढ़ा दिया गया। अब 55 नगरपालिकाओं में अचल संपत्ति का न्यूनतम मूल्य रू. 800 हो गया, 57 नगरपालिकाओं में न्यूनतम मासिक किराया रू. 2 कर दिया गया और 45 नगरपालिकाओं में न्यूनतम आय रू. 20 प्रतिमाह कर दी गई। इसके साथ ही, बहु-मतदान की व्यवस्था समाप्त कर दी गई।[11]
सन् 1920 के दशक में साईमन आयोग ने मताधिकार के प्रश्न पर विचार किया। उसने सभी वर्गों के लोगों के विचार सुने। आंबेडकर ने दलितों को मताधिकार देने की तो वकालत की परंतु आदिवासियों को इससे वंचित रखे जाने की बात कही। उनका मानना था कि आदिवासी, मताधिकार पाने के योग्य नहीं हैं। अतः जहां स्टूच्येटरी कमीशन के लिए संपत्ति पर मालिकाना हक, मताधिकार के लिए आवश्यक था वहीं आंबेडकर की दृष्टि में, चूंकि आदिवासी जंगली और असभ्य थे, इसलिए वे मताधिकार पाने के योग्य नहीं थे।
आत्मसात्करण या बहिष्करण?
आदिवासियों की आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के प्रयास 19वीं सदी में ही शुरू हो गए थे परंतु 1920 के दशक में इस दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन आया। यह कहा गया कि उन आदिवासी समुदायों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए, जो स्थानान्तरी कृषि करते हैं[12] और जिनकी विशिष्ट धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं हैं।[13] सन् 1930 का दशक आते-आते राज्य की रणनीति, आदिवासियों को नियंत्रण के घेरे में बांधने की हो गई। राज्य के दृष्टिकोण में बदलाव होता रहा परंतु यह माना जाता रहा कि संथालों जैसी वे जनजातियां, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करना, आधुनिक कानूनों का पालन करना और एक स्थान पर खेती करना प्रारंभ कर दिया है, वे सभ्य तरीके से जीवन जीने की ओर बढ़ रहीं हैं। जीएस घुरिए के अनुसार, ‘‘सेंट्रल प्राविंसिस की वन नीति, वहां उपलब्ध संसाधनों की प्रकृति पर निर्भर करती थी और वहां रहने वालों का इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने में उपयोग करने पर जोर देती थी।‘‘[14] 19वीं सदी के मध्य तक राज्य ने सेन्ट्रल प्राविंसिस में कई ऐसे नियम लागू कर दिए, जिनका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करना था।

कुछ क्षेत्रों को चिन्हित कर उन्हें स्वायत्त क्षेत्र बनाने में राज्य की यह रूचि, सामाजिक वर्गों के संबंध में दृष्टिकोण में बदलाव की सूचक थी। जहां औपनिवेशिक नृवंशविज्ञानियों के लेखन और जनगणना के भारी भरकम आंकड़ों में जाति और जनजाति के बीच अवसीमिय रिश्तों पर जोर दिया गया, वहीं सन् 1920 के दशक के बाद से, सामाजिक समूहों के वर्गीकरण व राज्य के उनके प्रति दृष्टिकोण में अंतर आ गया। सन् 1930 के दशक में कई बुद्धिजीवियों ने अपने लेखन में ‘समावेशीकरण‘ व ‘बहिष्करण‘ के प्रश्न पर विचार किया। जीएस घुरिए, समावेशीकरण के पक्ष में थे और इस संदर्भ में एव्ही ठक्कर उनके समर्थक थे। वेरियर एल्विन जैसे कुछ अन्य लोग, ‘स्वायत्त क्षेत्रों‘ के पक्ष में थे। एल्विन का कहना था कि जनजातियों की जीवनशैली दूसरों से एकदम अलग है। इस सिलसिले में वे बैगाओं की मासूमियत, उनकी ईमानदारी व उनकी ‘स्वतंत्र महिलाओं‘ का उदाहरण देते थे। उनका कहना था कि अगर जनजातियों को हिन्दू समाज का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई तो उनमें अछूत प्रथा व बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का प्रसार हो जाएगा और उनकी एकजुटता समाप्त हो जाएगी। ‘‘एक आदिम व्यक्ति का जीवन बहुत सीधा-सादा और प्रसन्नता से परिपूर्ण होता है। प्राकृतिक सुख उसके जीवन को समृद्ध करते हैं। उनकी गरीबी के बावजूद उनका जीवन अतिसुंदर पहाड़ों के बीच बीतता है…गांवों में उनके बच्चों का जीवन उतना ही सुंदर होता है जितना कि जंगली भैंसे का सींग और उतना ही मनोहर जितना घोड़े का गला‘‘।[15]
जनजातियों के आत्मसात्करण या उन्हें स्वायत्त क्षेत्रों में रखे जाने और गांधी का नीची जातियों के हिन्दू धर्म में आत्मसात्करण की वकालत की प्रतिध्वनी हमें जेएच हटन की ‘कास्ट्स ऑफ इंडिया’ में सुनाई देती है।[16] हटन ने ‘बाहरी जातियों’ का अध्ययन किया और यह पता लगाया कि उन्हें हिन्दू समाज में अधिक स्वीकार्य कैसे बनाया जा सकता है। उन्होंने हिन्दू समाज में पिछड़ी जातियों की स्वीकार्यता के संबंध में निम्न मानदंड प्रस्तावित किए :
- क्या संबंधित जाति या वर्ग की शुद्ध ब्राह्मणों द्वारा सेवा की जा सकती है?
- क्या संबंधित जाति या वर्ग की उन नाईयों, भिश्तियों, दर्जियों इत्यादि द्वारा सेवा की जा सकती है, जो ऊँची जातियों के हिन्दुओं की ऐसी सेवा करते हैं?
- क्या संबंधित जाति के व्यक्ति के स्पर्श या उसके नज़दीक आने से, ऊँची जाति के हिन्दू प्रदूषित होते हैं?
- क्या संबंधित जाति या वर्ग के व्यक्ति के हाथों से उच्च जाति का हिन्दू पीने का पानी ले सकता है?
- क्या संबंधित जाति या वर्ग के सदस्यों द्वारा सड़कों, नावों, कुंओं और स्कूलों जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल प्रतिबंधित है?
- क्या संबंधित वर्ग या जाति के सदस्यों का हिन्दू मंदिरों में प्रवेश वर्जित है?
- क्या सामान्य सामाजिक अंतव्र्यवहार में संबंधित जाति या वर्ग के किसी सुशिक्षित सदस्य के साथ, उसके समकक्ष शैक्षणिक योग्यता वाला उच्च जाति का व्यक्ति समानता का व्यवहार करेगा?
- क्या संबंधित जाति या वर्ग केवल अज्ञानता, अशिक्षा अथवा निर्धनता के कारण पिछड़ा है और अगर इन्हें दूर कर दिया जाए, तो वह किसी प्रकार की सामाजिक अक्षमता का सामना नहीं करेगा?
- क्या संबंधित जाति या वर्ग, अपने पेशे के कारण पिछड़ा हुआ है और अगर वह अपना पेशा बदल ले तो उसे किसी सामाजिक अक्षमता का सामना नहीं करना पड़ेगा?[17]
हंटर यह सब स्वाधीनता के कुछ वर्षों बाद लिख रहे थे, जब संविधानसभा में पिछड़ी जातियों के मुद्दे पर बहस चल रही थी। यह स्पष्ट है कि कोई भी सामाजिक समूह या तो जाति हो सकता है या जनजाति – फिर चाहे वह बहिष्करण का शिकार हो या उसका आत्मसात्करण हो गया हो। जनगणना में जिन सामाजिक समूहों का हाशियाकरण किया जाता है, बाद में भारतीय राज्य उनकी उन्हीं श्रेणियों को स्वीकार कर लेता है। इससे हमें बुद्धिजीवियों की असफलता का अहसास होता है – उन बुद्धिजीवियों की, जिन्होंने जाति और जनजाति की औपनिवेशिक श्रेणियों को स्वीकार कर लिया।

जनगणना ने कई ऐसी नई श्रेणियों का निर्माण किया, जो कि मूलतः तरल व अवसीमिय थी। परंतु इस तथ्य के बावजूद, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर ब्राह्मणवाद और राज्य के प्राधान्य को हाशिए पर पड़े वर्ग चुनौती दे सके, तो इसका कारण जनगणना ही थी। जनगणना ने दलित और जनजातीय पहचान को मज़बूती दी क्योंकि विभिन्न समुदायों के एक वर्ग के रूप में गणना से इन लोगों को पहली बार उनके संख्याबल का अहसास हुआ। इसके साथ ही, यह भी सही है कि धार्मिक श्रेष्ठतावादी समूहों की राजनीति भी जनगणना पर ही आधारित थी। जनगणना ने ही उन्हें बताया कि आबादी में उनकी कितनी बड़ी संख्या है। हिन्दू महासभा और तब्लीग-ए-जमात का सन 1920 के दशक में उभार, जनगणना के परिणामों से भी जुड़ा हुआ था।
सन 1992 में बाबरी मस्ज़िद का ध्वंस और 2002 के गुजरात दंगे – दोनों ही अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की अवधारणा पर आधारित थे। समकालीन सांप्रदायिकता और संप्रदायवाद को समझने के लिए हमें जनगणना में उसकी जड़ें तलाशनी होंगी। जनगणना के कारण भले ही जाति और संप्रदाय की राजनीति में बदलाव आया हो परंतु राजनीति का आख्यान, नस्ल के संबंध में 19वीं सदी की धारणाओं का कैदी बना हुआ है। आज भी, अतीत में उनके साथ हुए अन्याय के आधार पर समुदायों का निर्माण हो रहा है और वे एकजुट होकर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हाल में गुजरात के पाटीदारों और हरियाणा के जाटों ने इसी आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया था।
सन्दर्भ :
[1] बीआर आंबेडकर, ‘एनिहीलेशन आफ कास्ट’, 1 दिसंबर 1944, नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई 2015 तक संशोधित
[2] ’द डाक्टर एंड द सेंट’ (2013): नई दिल्ली, नवायन, पृ 213 में प्रकाशित डब्लूसी बैनर्जी (1882) के भाषण से उद्धत
[3] बीआर आंबेडकर, ‘एनिहीलेशन आफ कास्ट’, (1944½ ’द डाक्टर एंड द सेंट’ (2013): नई दिल्ली, नवायन, पृ 213
[4] उपरोक्त पृष्ठ 249
[5] ‘सिलेक्टिड वर्क्स ऑफ़ एमके गांधी’ संपादक रोनाल्ड डंकन, फेबर एंड फेबर, लंदन, पृ 127
[6] ‘कलेक्टिड वर्क्स ऑफ़ एमके गांधी’ राजकोट में भाषण, 25 सितंबर 1919
[7] ‘एनिहीलेशन आफ कास्ट’ पृष्ठ 326
[8] उपरोक्त, पृष्ठ 328
[9] बी आर आंबेडकर (1944), “रिप्लाई टू महात्मा गाँधी” परिशिष्ट 2, ‘एनिहीलेशन आफ कास्ट’
[10] ‘इंडियन स्टेच्यूटरी कमीशन” (1930) द्वारा पंजाब सरकार के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन, खंड 10, पृष्ठ 135
[11] उपरोक्त
[12] जीएस घूरिये, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ़ इंडिया (1963)
[13] पार्लियामेंटरी डिबेट्स, पांचवी श्रृंखला, खंड 299, 1395-1401, ‘अगर हम इस समय ‘रिंग फेन्स पालिसी‘ (ईस्ट इंडिया कंपनी की सीमाओं की रक्षा करने के लिए बफर जोन विकसित करने की नीति) अपनाते हैं और कई इलाकों को पृथक कर देते हैं तो हम पिछड़े क्षेत्रों को देश की सामान्य नीति के अंतर्गत लाने में देरी करेंगें‘‘ घुरिए (1963) में उद्धृत
[14] उपरोक्त
[15] वेरियर एल्विन, ‘द एबोरिजिनल’ (1943), लन्दन: ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
[16] जेएच हटन, कास्ट इन इंडिया, (1963); ऑक्सफ़ोर्ड: ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में ‘एक्सटीरियर कास्ट्स’
[17] उपरोक्त, 195
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in
फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें
मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया
दलित पैंथर्स : एन ऑथरेटिव हिस्ट्री : लेखक : जेवी पवार