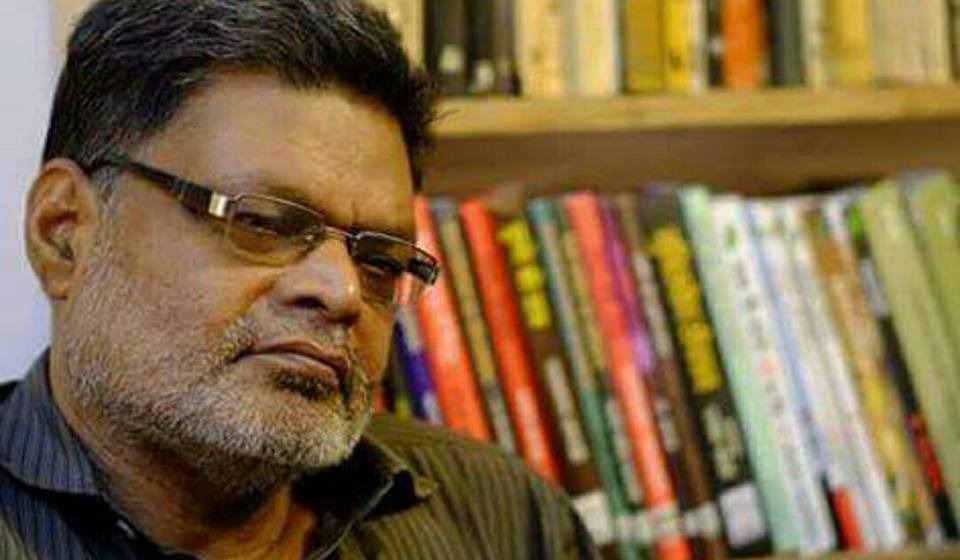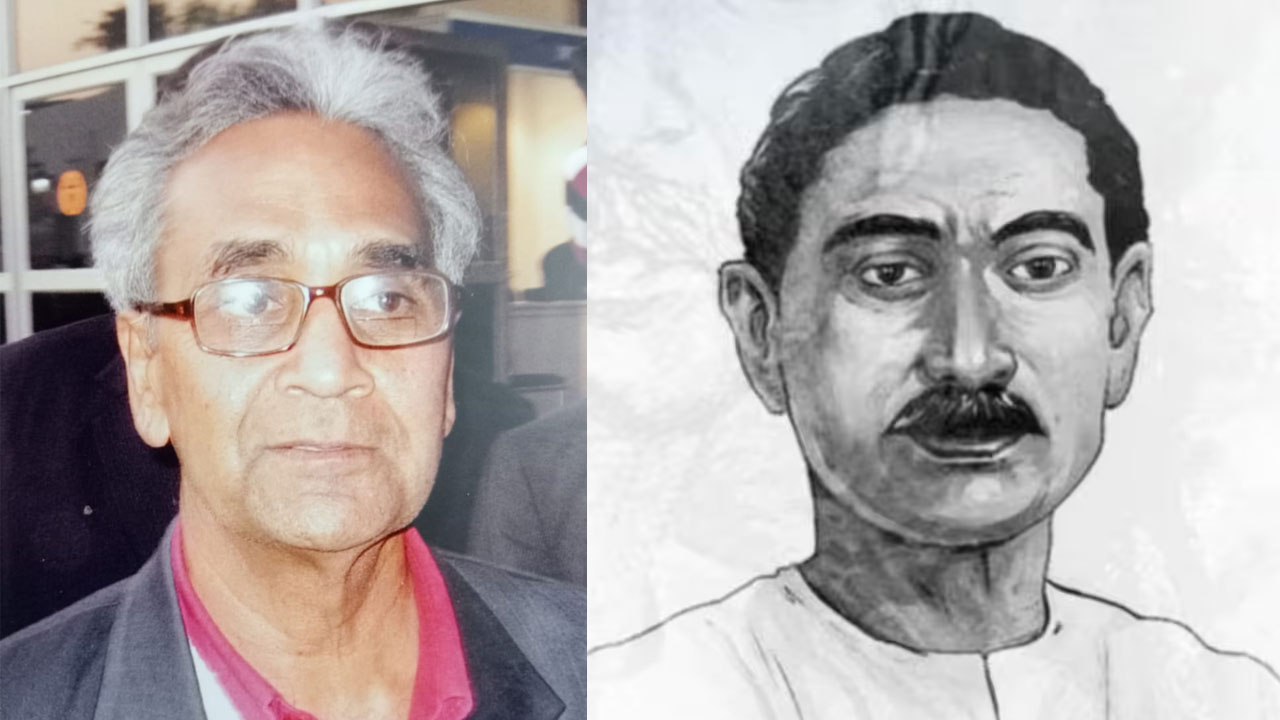लोहा गलाने की तकनीक सबसे पहले आदिम जनजाति ‘असुर’ ने ही दुनिया को सिखायी। इस संबंध मे जानकारी देने वाली एक दिलचस्प किताब ‘ट्रेडिशन एण्ड इनोवेशन इन दी हिस्ट्री ऑफ आयरन मेंकिंग’ है। ‘ट्रेडिशन एण्ड इनोवेशन इन दी हिस्ट्री ऑफ आयरन मेंकिंग’ एक दिलचस्प किताब है। इसमें लोहे के निर्माण और उससे विविध आकारों में ढालने की तकनीक पर विभिन्न लेखों को संपादित किया गया है।

अल्युमिनियम का पता चलने के बाद लोहा दूसरा ऐसा धातु था, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता था। इसे एक सबसे उपयोगी धातु माना जाता था, क्योंकि लगभग सभी उद्योगों में इसका इस्तेमाल होता था। यह विश्वास किया जाता है कि कांस्य युग के अन्त में संयोगवश लोहे की खोज हुई थी। भारत और चीन में लोहे के निर्माण का विकास अलग-अलग हुआ। भारत में 600 ईसापूर्व से ही उच्च गुणवत्ता का स्टील बनाया जाता था। भारत लोहे और स्टील के उत्पादन और धातु के शिल्प कौशल की प्राचीन विरासत के लिए जाना जाता था। यहां बडी संख्या में लौह स्मारक हैं, जो प्राचीन धातु विज्ञान में भारत की विशेषज्ञता को दर्शाते हैं। इसके कुछ उदाहरण के रूप में धार और दिल्ली के लौह स्तम्भों, उड़ीसा में कोर्णाक के लोहे के बीम को देख सकते हैं।
भारत में लौह तकनीक का ज्ञान का इतिहास संभवतः ईसा के 2000 वर्ष पहले तक जाता है। शुरू में यह आमतौर पर माना जाता था कि भारत में लोहा आर्यों के साथ आया। इस तरह की बहुत सारी अटकलें अब खारिज की जा चुकी हैं। इनमें से कुछ की चर्चा नीचे की जा रही है।
1. पहले यह माना जाता था कि हित्तियों का लौह तकनीक के ज्ञान पर एकाधिकार था और उनके साम्राज्य के विध्वंस के साथ ही यह तकनीकी ज्ञान 1200 ईसापूर्व के आस-पास लगभग दुनिया भर में फैला। लेकिन अब यह सभी को पता है दुनिया में बहुत सारे स्थल हैं, जहां धात्विक लोहा 1200 ईसापूर्व से पहले इस्तेमाल होता था। हालांकि कम मात्रा में इस्तेमाल होता था। कुछ शुरूआती संदर्भों में पिटवा लोहे के साथ-साथ ढलवा लोहे का उल्लेख भी मिलता है।
2. ‘अयस” शब्द का ऋग्वेद में कई बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद आर्यों का भारत में सबसे शुरूआती ग्रन्थ है। आमतौर अयस का अर्थ लोहा माना जाता है। लेकिन अयस शब्द का विस्तार से जांच-पड़ताल करने पर यह बात सामने आती है कि यह या तो धातु या तांबे-कांसे की ओर संकेत करता है। खास संदर्भों में इसकी दोनों अर्थों में व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा ठीक-ठीक रूप में इसका अर्थ तांबा-कांस्य है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि लोहा भारत में आर्यों (ऋग्वेद के रचयिता) के साथ आया।
3. धातु विज्ञान, यानी लोहे को गलाने और ढालने (आकार देने) की प्रक्रिया को इतना जटिल माना जाता था कि विभिन्न स्थानों पर इस तकनीक का ज्ञान लोगों को रहा होगा, इसे असंभव सी चीज माना जाता था। लेकिन हाल के शोध यह दिखाते हैं कि लोहा, तांबे और शीशे को गलाने की प्रक्रिया का उप-उत्पाद था। इस चीज ने किसी भी तांबे-कांसे का निर्माण करने वाले समाज में लोहे का उत्पादन सहज सुलभ बना दिया था। लोहे की उपलब्धता विशेषज्ञ और कम गलतियां करने वाले समूहों की तुलना में उन आदिम और कम दक्ष समूहों में ज्यादा थी, जो भूल-गलतियां करते हुए, इस नए पदार्थ का निर्माण कर रहे थे। अतः कुछ परिस्थितियों में जब शीशा फ्लेक्सेस के इस्तेमाल स्वरूप पिघल गया हो, उन खास परिस्थतियों में तांबे में से ऐसा तांबा बचा रह सकता है, जिसमें लोहे की मात्रा अधिक हो और यहां तक की धात्विक लोहा भी बचा रह सकता है।

4. यदि हम ऐतिहासिक कालानुक्रम के प्रमाणों पर निगाह डालें, तो यह चीज सामने आती है कि लोहे का जन्म एक देशज परिघटना है। हाल में मध्य गंगा के मैदानों में सोनभद्र जिले में राजा नल का टीला , मिर्जापुर जिले में मलहार और बंगाल में पांडुराजार धीबी, हाथीगरा, मंगालकोट इत्यादि जैसे कई सारे स्थल मिले हैं, जहां लोहे की उपस्थिति के महत्वपूर्ण आरंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कोई भी इस प्रकार के सभी प्रमाणों की उपेक्षा नहीं कर सकता है। ये प्रमाण बताते हैं कि भारत में बिना किसी विदेशी सहयोग के स्वतंत्र रूप में लौह तकनीकी का ज्ञान विकसित हुआ था। हालांकि यह संभव है कि कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में हो सकता है कि लोहे का प्रचलन पड़ोसी क्षेत्रों के संपर्क से हुआ हो, लेकिन तथ्यों का कोई भी संकलन इस बात का समर्थन नहीं करता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अन्दरूनी हिस्सों में विदेशी लौह तकनीकी प्रसार हुआ था।
साहित्यिक प्रमाण
देशज लौह और स्टील उद्योग से संबंधित साहित्यिक प्रमाणों की भरमार है। लेकिन देशज लौह उद्योग के संबंधित जिन साहित्यिक प्रमाणों तक हमारी सहज पहुंच है, उसका बड़ा हिस्सा यूरोपीय स्रोतों से प्राप्त हुआ है,क्योंकि इस विषय से संबंधित ज्यादात्तर नृ-जातीय-ऐतिहासिक आंकड़े औपनिवेशिक काल की शुरूआत में यूरोपीय पर्यवेक्षकों द्वारा इकट्ठा किए गए थे। इन पर्यवेक्षणों को देखकर यह लगता है कि ज्यादात्तर यूरोपीय प्रमाण वास्तविक तथ्यों को सामने लाने की तुलना में उन पर परदा डालने का काम करते हैं और असल कारीगर उनके दृष्टि से गायब हैं। ये यूरोपीय पर्यवेक्षक मुख्य रूप में लौह उत्पादन की बाह्य रूपरेखा (भट्ठियों की आकृति और आकार, कार्य की पद्धति, उत्पादन इत्यादि) से सरोकार रखते थे, अन्य चीजों की चर्चा चलते-फिरते तरीके से की गई है, जैसे की कारीगरों की चर्चा, ‘आदिवासी’, बर्बर अथवा ‘एक दुबले-पतले प्राणी’ के रूप मे कर दी गई है। भारतीय लोहे के बारे में यूरोपीय इतिहास लेखन में एक अऩ्य तत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके चलते यूरोपीय इतिहासकार देशज लौह तकनीक की परंपरा के महत्व को ठीक से नही समझ पाये और इसकी भूमिका को बहुत कम आंका। वह तत्व इस सच्चाई से जुडा है कि औपनिवेशिक पर्यवेक्षकों की भारत में लौह धातु विज्ञान की अवधारणा कुल मिलाकर अट्ठारहवीं शताब्दी की शुरूआत और लौह तकनीक की बेशमेर प्रक्रिया के आविष्कार के समय के बीच की अवधि को ही अपने सरोकार का मुख्य विषय बनाती है।
इसके उलट उपलब्ध देशज साहित्य भारतीय लौह दस्तकारी की पंरपरा के एक भिन्न परिप्रेक्ष्य को सामने लाता है, हालांकि इस देशज साहित्य की अपनी सीमाएं हैं। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की सीमाओं के बारे में सभी को यह बात ज्ञात है कि ये इतिहासकार, शायद ही वास्तविक कार्य स्थलों की जांच-पड़ताल करते हों, जहां दस्तकार काम करते हैं। ये इतिहासकार लेखागारों और इसी तरह के अन्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, जिनका आमतौर पर ऐतिहासिक शोधों में इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐतिहासिक प्रमाण लौह तकनीक पर कार्य के आरंभिक विचारों की व्याख्या नहीं कर सकते, यह नहीं बता सकते कि दस्तकार की विशिष्ट दस्तकारी संरचना की स्थिति क्या थी, किन कार्य स्थलों पर उनका काम था और वर्कशाप की संरचना कैसी थी।
झारखण्ड का देशज लौह उद्योग
झारखण्ड में धातु विज्ञान की एक लंबी परंपरा रही है, इसके प्रमाण तांबा, स्वर्ण और लोहे को गलाने के पुरातात्विक साक्ष्यों में पाया जाता है। यह इस विशिष्ट उपकरण तकनीक के विकास और फैलाव का केंद्र था। यह माना जाता है कि घुमंतु समूह, जिन्हें असुर के रूप में जाना जाता है, उन्हीं लोगों ने ही लोहे को गलाने की इस कारीगरी को इस क्षेत्र में पहले-पहल शुरू किया। (इससे जुड़ी हुई ध्यान देने की दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय हिमालय क्षेत्र की परंपरागत लौह तकनीक के स्थलों के नाम भी असुर से संबंधित हैं) झारखण्ड से असुरों का कितना पुराना संबंध है, यह ज्ञात नहीं है। यहां पर दो तरह के लोहे को गलाने के वर्कशाप हैं। इन्हीं से झारखण्ड के लौह उद्योग को पहचाना जाता है। घुमंतु लोहारों की खुली चूल्हे वाली भट्ठी और भारी संख्या में छप्पदार भट्ठी । इस तरह हम देखते हैं कि लोहे को गलाने वाली ज्यादात्तर कोथ-साल तरह के वर्कशाप हैं, इसके बाद खम्मार-साल वर्कशाप या लौह शोधन गृह हैं। यहां पर कुछ ऐसे भी समूह थे, जो लोहे को गलाने के काम नहीं करते थे, वे लोहे को विभिन्न रूपों में ढालने में माहिर थे। इन विभिन्न समूहों में उकरणों की तकनीक की भिन्नता भी दिखती है। यह चीज अवधारणाओं में व्यापक विभिन्नता और उनकी कारीगरी की तकनीक से संबंधित उपलब्धियों को अभिव्यक्त करती है। उल्लेखनीय बात यह है कि साधारण साल या लोहे को गलाने की छोटी भट्ठियां और कोथा-साल की तरह के बड़े वर्कशाप के बीच का द्विविभाजन भारत के अन्य हिस्सों में भी मौजूद था।

भारत में लोहे के परंपरागत काम का स्वरूप
भारत में बहुत सारे ऐसे समूह थे, जिनका मुख्य पेशा लोहे को गलाना या इससे संबंधित था, लेकिन हम भारत में लोहे को गलाने की परंपरागत तकनीक को सामने लाने के लिए केवल चार नृ-जातीय समूहों (अगरिया, असुर, बिरजिया और लोहार) को ले रहे हैं। ये चार समूह हमें भारत के परंपरागत लौह तकनीक से अच्छी तरह परिचित कराते हैं।
1. अगरिया लोगों की लोहे को गलाने की तकनीक :
अगरिया एक अनुसूचित जनजाति है, जो मध्य प्रदेश और छतीसगढ़ के मंडाला, दिनधोरी, बिलासपुर और बालाघाट जिलों में रहती है। अगरिया समूह का मुख्य और परंपरागत पेशा लोहे को गलाना था। अगरिया समुदाय का अयस्क भंडारों के काफी निकट निवास रहता है। लौह अयस्कों के निकट रहने का उद्देश्य समय और उर्जा बचाना था। जितने बड़े पैमाने पर भारत में लौह अयस्कों का भण्डार फैला हुआ था, उसके चलते गहराई में खुदाई करने की जरूरत नहीं थी। इन लोगों द्वारा मुख्य रूप से लौह अयस्क का हेमेटाइट या मैगेनेटाइट रूप ही उपयोग में लाया जाता था, जो भारी लाल भूरे रंग के पत्थरों की लैटेरीटिक चट्टानों में पाए जाते थे। इन पत्थरों को छोटे-छोटे टुकडों मे तोड़ लिया जाता था, और चिपचिपी मिट्टी से इनको साफ कर लिया जाता था। वे लोग लौह अयस्क को चारकोल के साथ 1 और 3 के अनुपात में मिलाकर, इस मिश्रण को भट्टी में डाल देते थे। भट्ठी को पूरी तरह से मिश्रण से भर देने के बाद इसमें आग सुलगा देते थे और भट्ठी के मुंह को पूरी तरह बन्द कर दते थे। ड़ेढ घंटे तक निरंतर हवा के झोंकों से भट्ठी को भभकाने के बाद अपशिष्ट पदार्थ के निकास मार्ग से गाढे पिघले तरल पदार्थ का निकलना शुरू होता है, जो इस बात का संकेत देता है कि लोहे के पिघलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जब लावा निकलना बंद हो जाता है, तो धौंकनी हटा ली जाती है। अन्त में लाल अर्द्ध पिघले लोहे के पिण्डों को सडसी की मदद से निकाल लिया जाता है और उसे पिटने लिए ले जाया जाता है। बार-बार इस लौह पिण्ड को पिटने और गर्म करने के बाद, इसका इस्तेमाल औजार और घरेलू उपयोग का सामान बनाने के लिए किया जाता है।
2. असुरों की लोहा गलाने की तकनीक :
हम कह सकते है कि असुरों की लोहा गलाने की तकनीक अतीत की जीवित तकनीक है। असुर बिहार की 30 अनुसूचित जनजातियों में से एक हैं। ये झारखंड के दक्षिणी छोटानागपुर के पठारी इलाकों यथा गुमला, लोहरदग्गा मे पाए जाते हैं। तीन विभिन्न किस्मों के लोहे की इनको पहचान थी। पहले को मैग्नेटाइट कहते है, जिसे असुर पोला कहते थे। दूसरा हेमेटाइट है, जिस आमतौर पर बीची के रूप में जाना जाता है। तीसरा लैटेराइट से प्राप्त हेमेटाइट है, जिस आमतौर पर गोटा नाम से पुकारा जाता है। हरे साल के पेड़ के चारकोल का इस्तेमाल इनके द्वारा किया जाता है। यह चारकोल लोहे को पिघलाने की प्रक्रिया के लिए पर्याप्त होता है। साल का पेड एक अच्छी गुणवत्ता वाला जंगली लकड़ी है।
3. लोहा गलाने वाले बिरजिया :
बिरजिया झारखंड की सबसे आदिम जनजातियों में से एक हैं। वर्तमान समय में बिरजिया लोग अधिकांशतः लोहारदागा, बिशनपुर और राइडीह (गुमला) और पलामु जिले के गुरू पुलिस स्टेशन में पाए जाते हैं। परंपरागत तौर पर बिरजिया लोगों का मुख्य व्यवसाय लोहा गलाना, बेनोरा की खेती करना और टोकरी बुनना है। यह माना जाता है कि यह पहली मानव प्रजाति है, जिसने लौह अयस्क की खोज की और अपनी देशज प्रक्रिया का प्रयोग करके एक अलग तरह का लोहा तैयार किया। इनमें से कुछ आज भी अपने परंपरागत पेशे को अपनाए हुए हैं, लेकिन कच्चे माल की कमी के चलते बिरजिया लोगों ने नए आर्थिक क्रिया-कलापों को अपनाना शुरू कर दिया है। इन लोगो द्वारा लोहे को पिघलाने की भट्ठी के रूप में कोथी (खुली चूल्हा भट्ठी) का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी उंचाई लगभग 2-1/2 फीट तक होती है, जिसमें एक सुराख होता है। इस भट्ठी को लौह अयस्क और चारकोल के मिश्रण से लबालब भर दिया जाता है और एक नलिका के माध्यम से हवा भेजी जाती है। हवा भेजने के लिए एक बेलनाकार धौंकनी को पैरों से चलाया जाता है। पैर से चलाई जाने वाली इस धौकनी को चौऊपा कहते हैं। हवा से 4 से 5 घंटों तक भभकाया जाता है। भट्ठी का तापमान कितना हो, यह चीज विशेषज्ञ कारीगर स्वयं तय करते हैं। अपचयन के बाद धौंकनी को हटा लिया जाता है और भट्ठी के मुंह को खोल दिया जाता है। स्पंज के रूप में एकत्रित पदार्थ ( ब्लूम ) को भट्ठी से निकाल लिया जाता है और उस स्पंजी पदार्थ को पहले हल्के से पीटा जाता है, फिर उस पर कड़ा प्रहार किया जाता है। इस प्रक्रिया में उसे मनचाहे रूपों में ढाला जाता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आधुनिक तकनीक की प्रतियोगिता में यह परंपरा खत्म होने के करीब है।
गुडुलिया लोहर और उनकी लोहा निर्माण की तकनीक
गुडुलिया लोहार राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से और उत्तर प्रदेश में रहते हैं। लोहे का काम ही गुडुलिया लोहारों का मुख्य परंपरागत पेशा है। ये लोग घुमंतु समूह के लोग हैं। बैलगाड़ी ही इनका घर होता है, जिसमें सारी सामग्रियों और साधनों के लादे रहते हैं, जो उनके जीवन के लिए जरूरी हैं। उनके पूर्वज जिस तकनीक का इस्तेमाल करते थे, ठीक उसी तरह की परंपरागत तकनीकी का इस्तेमाल वे आज भी करते हैं। यह तकनीक पिता से पुत्र को स्थानान्तरित होती है। ये लोहे के रद्दी टुकडों का इस्तेमाल करने के विशेषज्ञ हैं। वे छोटा सा गड्ढा खोदते हैं, उसका आग धधकाने की जगह के रूप में इस्तेमाल करते हैं और हाथ से चलने वाले पंखा उत्पाद को भभकाता है। बार-बार गरम करके उस पर प्रहार करने से रद्दी लोहे की गुणवत्ता बढाई जाती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से वे जैसा चाहते है, वैसा उपकरण और औजार बनाते हैं।

आधुनिक युग में परंपरागत लौह निर्माण की स्थिति
परंपरागत लौह निर्माण काम देश के कुछ दूर-दराज के क्षेत्रों में अभी जारी है, जहां उच्च गुणवत्ता के लोहे का उत्पादन कारीगरों द्वारा छोटी भट्ठियों में किया जाता है। लेकिन वर्तमान परिवर्तित होते राजनीतिक-सांस्कृतिक और सामाजिक-पर्यावरणीय बाध्यताओं के चलते परंपरागत लौह निर्माण के काम के पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है,ताकि उपलब्ध तकनीक की वर्तमान आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सके। यह कहा जा रहा है कि कच्चे माल की उपलब्धता के साथ-साथ चारकोल के इस्तेमाल, दोनों दृष्टियों से परंपरागत तकनीक से लौह निर्माण फुजुलखर्जी है। यह भी कहा यह जा रहा है कि चारकोल के इस्तेमाल के चलते जंगलो की कटाई की प्रक्रिया तेज होती है। लेकिन यदि हम परंपरागत तकनीक से लौह निर्माण की प्रक्रिया को ठीक से देखें तो हम पाते हैं कि परंपरागत लौह निर्माण करने वाले समूह उन लौह अयस्कों का उपयोग करते हैं जिनकी उपेक्षा की जाती है या जिनको निम्न स्तर का माना जाता है और आधुनिक स्टील कारखानों द्वारा जिन्हें गलाने योग्य नहीं समझा जाता। परंपरागत काम करने वालों के काम का एक अन्य महत्व यह है कि वे उन छोटी जगहों पर स्थित हैं और अयस्कों के उन छोटे भंडारों का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी उन भौगोलिक स्थानों की सूचियों में नाम दर्ज नहीं होता, जिन्हें आर्थिक तौर पर फायदेमंद खदान क्षेत्रों में गिना जाता है। जिस उत्कृष्टता के साथ परंपरागत लौह उत्पादक उपेक्षित क्षेत्रों से अयस्कों का चुनाव करते हैं, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए यदि हम समग्रता में देखें तो, उनकी तकनीकी उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर आधारित है। जहां तक दूसरे आरोप का संबंध है, की जंगलों के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, जब हम इस संदर्भ में विचार करते हैं तो पाते हैं कि वे जंगलों में गिरे हुए, सूखे पेड़ों का ही चारकोल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर के अगरिया परिवार के लोग जंगलों में जाते हैं और साल के पत्ते इकट्ठा करते हैं। इन पत्तों पर वे खाना खाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संयमपूर्ण इस्तेमाल के प्रति उनका नजरिया कितना प्रकृति संरक्षक है, इसको इस बात से समझा जा सकता है कि प्रति परिवार कितने पत्तों का इस्तेमाल होगा, यह पहले से तय होता है। जब वे पत्तियों तक का भी अंधाधुंध या असावधानी से इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो कैसे हम यह आरोप लगा सकते हैं कि वे पेडों की बर्बादी करते हैं? वे पेडों के प्रति अत्यन्त आदर और सम्मान प्रकट करते हैं। वे मानते हैं कि पेड़ों पर उनके देवी-देवता अथवा पूर्वजों की आत्मा वास करती है, जो लोगों के कल्याण की चिन्ता करते हैं।
पर्यावरण संरक्षण में देशज-अनार्य लौह तकनीक की अहमियत
बिगड़ती पारस्थितिकी के वर्तमान हालातों में परंपरागत तकनीक पर्यावरण को बचाने और इसे प्रदूषण मुक्त बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। परंपरागत तकनीक में उर्जा के स्रोत के रूप में चारकोल(लकड़ी का कोयला) का इस्तेमाल किया जाता है, यह स्थापित सत्य है कि आधुनिक स्टील मिलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ईधनों की तुलना में यह बहुत कम प्रदूषक है। दूसरी बात यह है कि कोयला या अन्य जीवाश्म ईंधन बड़े पैमाने पर कैंसरकारी उप-उत्पाद पैदा करते हैं, जबकि दूसरी और चारकोल प्रदूषणकारी नहीं है, क्योंकि इसमें कम मात्रा में सल्फर पाया जाता है। इन समुदायों द्वारा जिन लौह भट्ठियों का इस्तेमाल किया जाता है, वे छोटी होती हैं, जिसके चलते वे वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। परंपरागत लौह कार्य छोटे पैमाने के घरेलू उद्योग के रूप में होते हैं, जो बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं। इन समुदायों द्वारा जिन संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है, वे संसाधन भी एक विशाल क्षेत्र से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए वे किसी एक क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन को ज्यादा सघन तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इन समुदायों द्वारा जिस अयस्क और ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है,वे पर्यावरण को प्रभावित नहीं करते हैं। इन तथ्यों से इस बात की पुष्टि होती है कि लौह निर्माण के लिए परंपरागत दस्तकारों द्वारा जिस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, वह वर्तमान संदर्भ में पर्यावरण अनुकूल आर्थिक गतिविधि है।
निष्कर्ष :
उपरोक्त तथ्यों से इस बात की पुष्टि होती है कि भारत में परंपरागत लौह तकनीक अच्छी तरह से विकसित थी। लोहे को गलाने की देशज तकनीक आदिवासी दस्तकारों समूहों के बीच पाई जाती थी। धीर-धीरे मुख्य रूप से निम्न कारणों से यह तकनीकी लुप्त होती जा रही हैः
- बाजार में बेहतर उपकरणों और इनके इस्तेमाल की उपलब्धता के चलते परंपरागत तकनीक की पकड़ ढीली पड़ती गई।
- कच्चे माल के अभाव ने इन आदिवासियों को आर्थिक क्रिया-कलापों के नए रास्तों को अपनाने को बाध्य कर दिया।
- लौह निर्माण का काम बहुत ही श्रमसाध्य और समय खपाने वाला था।
- जिस अन्य तत्व ने इस परंपरा के लुप्त होने की प्रक्रिया को तेज करने में अहम भूमिका निभाई, वह था, पश्चिमी तकनीक को अपनाना। भारतीय आदिवासियों को उनके वास स्थानों से खदेड़ दिया गया और एक ऐसी अनजानी दुनियां में उन्हें ठेल दिया गया,जिस दुनिया की कठिन हालातों का सामना करने के लिए वे तैयार नहीं थे। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपनी परंपरागत तकनीकी को खो दिया और अपने अस्तित्व को बनाए रखने लिए जीवन-निर्वाह के ऩए तरीके अपनाने को बाध्य हुए। आज जब हम उनकी लौह तकनीक की अन्तर्निहित संभावनाओं का समझ पा रहे हैं, तो हमें स्वतंत्रता के बाद अपनी औद्योगिक नीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत महसूस होती है।
भोपाल स्थित मानव जाति का इंदिरा गांधी म्यूजियम खत्म होती इस परंपरा को जीवित करने की कोशिश कर रहा है। यह निश्चित तौर पर लोहे को परंपरागत तरीके से गलाने वाले बेरोजगार लोगों का संरक्षण करने में मदद् करेगा और इस प्रकार लौह तकनीक की इस परंपरागत व्यवस्था को बचाने में हम सक्षम होंगे।
स्रोत :
1. सरकार, स्मृतिकुमार, 2002, स्टडिंग इंडियाज इंडिनियस आयरन इंडस्ट्रीजः लूकिंग फार एन अल्टरनेटिव एप्रोच, ट्रेडिशन एण्ड इनोवेशन इन दी हिस्ट्री ऑफ आयरन मेकिंग, गिरिजा पांडे और जनाफ गेइजेरस्टाम( संपादित ), नैंनीतालः पहर, पृ. 205-224
2. त्रिपाठी, विभा, 2002, आयरन टेकनालॉजी इन इंडियाः सर्वाइवल ऑफ एन एनशिएऩ्ट ट्रेडिशन, ट्रेडिशन एण्ड इनोवेशन इन दी हिस्ट्री ऑफ आयरन मेकिंग, गिरिजा पांडे और जनाफ गेइजेरस्टाम( संपादित ), नैंनीतालः पहर, पृ. 225-236
3. नायल, राकेश और निलंजन खाटुआ, 2002, ट्रेडिशनल आयरन मेकिंग, ट्रेडिशन एण्ड इनोवेशन इन दी हिस्ट्री ऑफ आयरन मेकिंग, गिरिजा पांडे और जनाफ गेइजेरस्टाम( संपादित ), नैंनीतालः पहर, पृ.250-257
(अनुवाद : सिद्धार्थ)
महिषासुर से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए ‘महिषासुर: एक जननायक’ शीर्षक किताब देखें। ‘द मार्जिनलाइज्ड प्रकाशन, वर्धा/दिल्ली। मोबाइल : 9968527911. ऑनलाइन आर्डर करने के लिए यहाँ जाएँ: अमेजन, और फ्लिपकार्ट। इस किताब के अंग्रेजी संस्करण भी Amazon,और Flipkart पर उपलब्ध हैं।