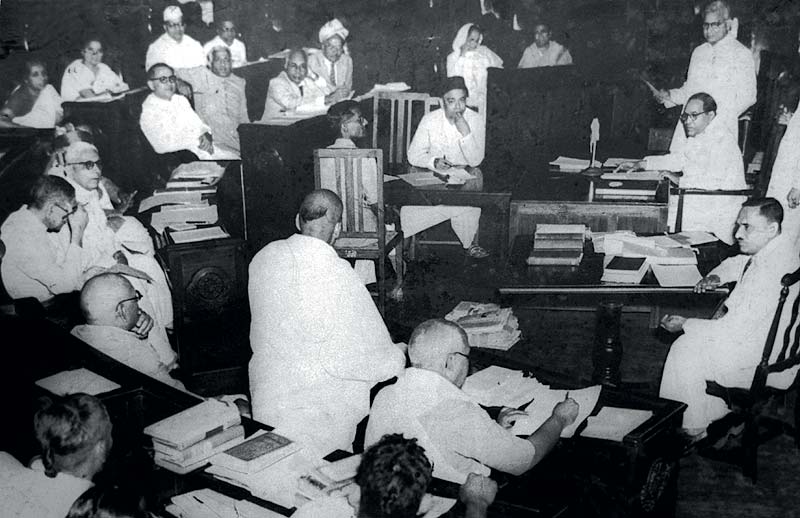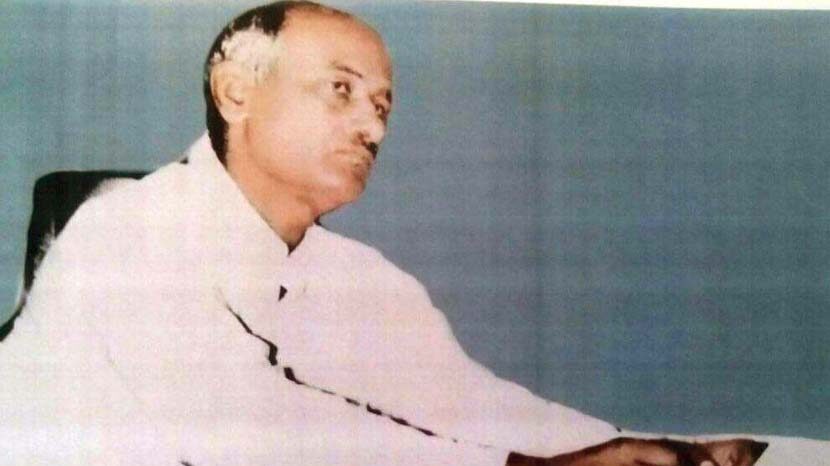(भारत सरकार के नौकरशाहों में जिन चंद लोगों ने अपने को वंचित समाज के हितों के लिए समर्पित कर दिया, उसमें पी.एस. कृष्णन भी शामिल हैं। वे एक तरह से आजादी के बाद के सामाजिक न्याय के जीते-जागते उदाहरण हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने सामाजिक न्याय संबंधी अपने अनुभवों को डॉ. वासंती देवी के साथ साझा किया। वासंती देवी मनोनमनियम सुन्दरनर विश्वविद्यालय, तमिलनाडु की कुलपति रही हैं। संवाद की इस प्रक्रिया में एक विस्तृत किताब सामने आई, जो वस्तुतः आजादी के बाद के सामाजिक न्याय का इतिहास है। फारवर्ड प्रेस की इस किताब का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने की योजना है। हम किताब प्रकाशित करने से पहले इसके कुछ हिस्सों को सिलसिलेवार वेब पाठकों को उपलब्ध करा रहे हैं। आज पढ़ें- जाति का विनाश कैसे हो और नौकरशाह इसमें कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं, के संबंध में पी.एस. कृष्णन के विचार –संपादक)
आज भी राष्ट्र के विकास में जाति-व्यवस्था सबसे बड़ी बाधक
-
वासंती देवी
आजादी के बाद के सामाजिक न्याय का इतिहास : पी.एस. कृष्णन की जुबानी, भाग – 12
वासंती देवी : इस समय जब राष्ट्र आंबेडकर की 125वीं जयंती मना रहा है; तब, मेरे विचार में आपसे यह जानना प्रासंगिक होगा कि जाति व्यवस्था के शिकार व्यक्तियों के संबंध में आपके सरोकार क्या हैं? भारत, भयावह जाति-प्रथा को समाप्त करने में असफल रहा है; जिसे आप हमारी ‘सभ्यतागत कमी’ कहते हैं। इस बारे में आपकी क्या सोच है?
पी.एस. कृष्णन : ऐसे कई कारक हैं, जिनके चलते हम हमारी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व कर सकते हैं। परंतु, हर सभ्यता और संस्कृति की अपनी कमियां और दोष होते हैं। हमारी महान सभ्यता पर भारतीय जाति व्यवस्था और उससे जुड़ी अछूत-प्रथा एक बदनुमा दाग है। इस व्यवस्था ने एक ऐसे तंत्र का निर्माण कर दिया है, जिसके चलते कुछ जातियां और समुदाय, जिन्हें हम एससी-एसटी कहते हैं और कुछ हद तक एसईडीबीसी भी, स्थाई वंचना के शिकार हो गए हैं और इन समुदायों के अतिरिक्त, अन्य वर्गों को समाज और देश के संसाधनों पर लगभग एकाधिकार हासिल हो गया है। इस व्यवस्था के मुख्य लक्ष्य हैं :
- मजदूरों को मजदूर बनाकर रखना और खेतिहर श्रमिकों को यही काम करते रहने के लिए मजबूर करना।
- दलितों को दबाकर रखना और उनकी मुक्ति की कोई राह उन्हें उपलब्ध न होने देना।
- आदिवासियों को दूरदराज के क्षेत्रों में सीमित रखना; सिवाय तब के, जब उनके श्रम की आवश्यकता हो।
- दलितों और आदिवासियों को अलग-थलग रखना; उनके मनोबल को तोड़ना। उन्हें उनके आर्थिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक विकास और आगे बढ़ने के अवसरों से या तो पूर्णतः वंचित रखना या उन्हें ऐसा करने के न्यूनतम अवसर देना।
भारतीय जाति व्यवस्था (दलितों के मामले में अछूत-प्रथा, जिसका अविभाज्य हिस्सा है) आज भी विद्यमान है। उसके घातक परिणाम हम आज भी देख सकते हैं। आज भी दलित व आदिवासी हर क्षेत्र में सामाजिक रूप से अगड़ी जातियों व वर्गों की तुलना में पिछड़े हुए हैं; चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो या शैक्षणिक या फिर आवास, स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ा हुआ कोई पहलू हो। एसईडीबीसी इन दोनों के बीच में हैं। परंतु, वे अगड़ी जातियों की तुलना में एससी-एसटी के अधिक नजदीक हैं। इस व्यवस्था के कारण न केवल एससी-एसटी और एसईडीबीसी के साथ सदियों से अन्याय होता आ रहा है, वरन इससे भारतीय राष्ट्र और समाज की भी अपूरणीय क्षति हो रही है। इसके कारण हम अपने मानव संसाधनों का भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि भारत उतना विकास नहीं कर सका है, जितना वह कर सकता था। और यही कारण है कि बाबा साहब डाॅ. आंबेडकर कहते थे कि ‘जाति, राष्ट्र-विरोधी है।’ यद्यपि, इस व्यवस्था से समाज को होने वाला नुकसान भयावह है और हम सभी के सामने है। परंतु, भारतीय श्रेष्ठि वर्ग ने इस व्यवस्था का उन्मूलन करने में कभी रुचि नहीं दिखाई।

मेरी समझ में ऐसा इसलिए है, क्योंकि भारतीय समाज, भारतीय संस्थाओं और भारतीय राजनीतिक पार्टियों का नेतृत्व आज भी ऐसे लोगों के हाथों में है, जो जाति-प्रथा से लाभान्वित हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। एससी-एसटी व गैर-भूमिस्वामी पिछड़े वर्गों के चंद लोगों को राजनीतिक दलों में जगह मिली है; परंतु पार्टियों में उनकी भूमिका सीमित और कमजोर है। इसका कारण उनकी कोई गलती या उनमें कोई कमी नहीं है। मैं यह जानता हूं कि उनमें से कई अत्यंत प्रतिभाशाली हैं। परंतु, उन्हें कभी उनकी पार्टियों के नेतृत्व में उचित स्थान नहीं मिला।

इस सिलसिले में मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। मैं पहले ही श्री दामोदरन संजीवैय्या के बारे में बता चुका हूं। एक अन्य मेधावी और जमीन से जुड़े दलित नेता, जो मुझे याद पड़ते हैं; वे हैं- बिहार के श्री भोला पासवान शास्त्री। वे एक बुद्धिमान और अत्यंत उदारमना व्यक्ति थे। उन्हें समाज की गहरी समझ थी और उनकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी पर कोई ऊंगली नहीं उठा सकता था। बिहार की राजनीति के एक उथल-पुथल भरे दौर में उन्हें कुछ महीनों के लिए एक गैर-कांग्रेस गठबंधन सरकार का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। उन्हें उनके कद और गुणों के अनुरूप कभी कोई पद नहीं मिल सका। वे मोरारजी देसाई सरकार द्वारा नियुक्त अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। उस दौरान मैं गृह मंत्रालय में एससी व बीसी मामलों का प्रभारी संयुक्त सचिव था। इस हैसियत से मैंने अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीपी) की परिकल्पना प्रस्तुत कर, उसे लागू करने की पहल की। आयोग और मेरे बीच हुई कुछ चर्चाओं में मैंने आयोग को एससीपी के बारे में बताया। आयोग ने इससे प्रभावित होकर इस योजना को लागू करवाने में मंत्रालयों और योजना आयोग से चर्चा कर मेरी मदद की। श्री भोला पासवान शास्त्री का कहना था कि ‘एससीपी होना चाहिए।’ वे देश के उन चंद राष्ट्रीय नेताओं में से थे, जो एससीपी व आदिवासी उप-योजना के महत्व को समझ सके। उनके व एक अत्यंत पिछड़ी जाति से आने वाले राज्यमंत्री श्री धनिकलाल मंडल व श्री योगेन्द्र मकवाना (जो पहले विपक्ष में थे और बाद में इंदिरा गांधी सरकार में गृह राज्यमंत्री बने) का समर्थन और सहयोग, एससीपी को लागू करवाने में काफी मूल्यवान साबित हुआ।

एससी व अन्य वंचित वर्गों के मेधावी, अनुभवी और सत्यनिष्ठ नेताओं के होते हुए भी, राष्ट्रीय पार्टियों और अनेक क्षेत्रीय पार्टियों का असली नेतृत्व अगड़ी जातियों के लोगों के हाथों में रहा और अभी चंद वर्षों से कुछ राज्यों में भू-स्वामी एसईडीबीसी के हाथों में। जो लोग इन वर्गाें से नहीं थे, उन्हें सत्ता के लिए भू-स्वामी जातियों का मुंह ताकना पड़ता था। इन राजनीतिक दलों के नेतृत्व और उन सामाजिक वर्गों, जिन्हें मदद की जरूरत थी; के बीच हितों की टकराहट थी। इन परिस्थितियों के चलते जाति-प्रथा द्वारा देश की तबाही और इस प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता पर बहुत कम ध्यान दिया गया। दुर्भाग्यवश वह वर्ग, जिसे ‘नागरिक समाज‘ कहा जाता है और जिसकी इन दिनों बहुत चर्चा है; उसके अधिकांश सदस्य भी सामाजिक दृष्टि से श्रेष्ठि वर्ग के हैं। यही बात विभिन्न संस्थाओं के प्रमुखों (जिनमें बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाएं, विश्वविद्यालय और मीडिया संस्थान शामिल हैं) के बारे में सही है। आश्चर्य नहीं कि जाति-प्रथा की जकड़न जरा भी कमजोर नहीं पड़ी है। इस स्थिति में परिवर्तन तभी आ सकता है, जब एससी-एसटी और एसईडीबीसी की गैर-भूस्वामी जातियां एकजुट हों और प्रजातांत्रिक तरीके से अपने वैध अधिकारों को पाने के लिए जोरदार आवाज उठाएं। इस एकजुटता से ही जहरीली जाति-प्रथा के अंत की संभावना बन सकती है।
पी.एस. कृष्णन : अछूत-प्रथा, घिनौनी जाति-प्रथा का सबसे घातक पहलू है। इस प्रथा का शिकार केवल वे ही जातियां हैं, जिन्हें 1935 के बाद से एससी कहा जाने लगा है। हमारी सभ्यता व अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है और देश की एक बड़ी आबादी अपने जीवनयापन के लिए खेती पर निर्भर है। खेती और उससे संबद्ध गतिविधियों के लिए खेतिहर श्रमिकों की अनवरत आवश्यकता होती है। परंतु, यह आवश्यकता पूरे साल एक-सी नहीं रहती। हमारे देश में मानसून की वर्षा केवल कुछ महीनों तक होती है। इन महीनों में सबसे ज्यादा संख्या में खेतिहर श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। परंतु, जब उनकी जरूरत नहीं रहती; तब भी उनका उपलब्ध रहना आवश्यक होता है। जिन जातियों को खेतिहर श्रमिक के रूप में काम करने पर मजबूर किया गया, उन्हें हम एससी कहते हैं। साल-दर-साल सदियों तक उनकी उपलब्धता कैसे सुनिश्चित की गई? इसके लिए यह जरूरी था कि उन्हें इस काम से मुक्ति की किसी भी राह से वंचित कर दिया जाए। उन्हें कोई और काम करने का अधिकार ही न हो। और इसीलिए अछूत-प्रथा का आविष्कार किया गया।
अछूत-प्रथा यह सुनिश्चित करती है कि इसकी शिकार जातियों (जो खेतिहर श्रमिकों का मुख्य स्रोत हैं) के सदस्यों को सामाजिक दृष्टि से अलग-थलग रखा जाए। जो व्यक्ति समाज, संगठित राजनीतिक पार्टियों और ‘नागरिक समाज‘ में शीर्ष पर हैं; वे सब ऐसी जातियों से हैं, जिन्हें इस व्यवस्था से लाभ हुआ है और आज भी हो रहा है।
अछूत-प्रथा केवल कुछ मनमाने और सनक भरे नियमों का संकलन नहीं है। इसे केवल यह करो और यह न करो के नियमों का समूह मात्र मानकर सन् 1950 के दशक में इमेन्युअल शेखर ने इसका विरोध किया और इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई। इसके बाद सन् 1950 के दशक के अंत में, दक्षिणी तमिलनाडु के रामनाथपुरम में दंगे हुए। सच यह है कि यह एक अत्यंत धूर्ततापूर्ण और सोच-समझकर निर्मित की गई व्यवस्था है; जिसका मुख्य लक्ष्य खेतिहर श्रमिकों को दूसरे पेशे अपनाने या आगे बढ़ने के सभी अवसरों से वंचित रखना है। आश्चर्य नहीं कि यह आज भी बरकरार है।
यह भी पढ़ें : मेरे संघर्षों के कारण लागू हुआ मंडल कमीशन : पी.एस. कृष्णन
किसी भी अहितकारी या अन्यायपूर्ण प्रथा का उन्मूलन कानून या संविधान के द्वारा करना एक महत्वपूर्ण कदम है। परंतु, इससे वह बुराई समाप्त नहीं हो जाती। इसके लिए पारंपरिक अर्थव्यवस्था और समाज के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन लाना आवश्यक है। उदाहरणार्थ, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक दलित परिवार के पास सिंचित भूमि का कम-से-कम इतना बड़ा टुकड़ा हो, जिससे वह अपना जीवनयापन कर सके और इस जमीन पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा किए जाने को प्र्तिबंधित किया जाना चाहिए। यह मात्र एक उदाहरण है। जाति-प्रथा के शिकार लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए कई तरह के कानूनों और कार्यक्रमों व योजनाओं की आवश्यकता है। इसका रोडमैप मैंने सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नेताओं, कुछ क्षेत्रीय पार्टियों और इन पार्टियों की सरकारों के नेतृत्व को उपलब्ध करवाया है।
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, बल्कि इस दिशा में किसी भी गंभीर प्रयास के लिए, यह जरूरी है कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं की इसके प्रति प्रतिबद्धता हो। यह अब तक नहीं हो सका है और इसके कारणों का वर्णन मैं पीछे कर चुका हूं। अगर इस प्रथा का उन्मूलन किया जाना है, तो इसके लिए जरूरी है कि अछूत-प्रथा के शिकार वर्ग शांतिपूर्ण ढंग से एकजुट हों और बदहाली का जीवन जी रहे अन्य वर्गों के साथ मिलकर अपने अधिकारों के लिए लड़ें। यह प्रक्रिया शुरू तो हुई है; परंतु इसने अब तक अपेक्षित गति और मजबूती हासिल नहीं की है।

अछूत-प्रथा के मूल में है खेतिहर श्रमिकों को खेतिहर श्रमिक ही बनाए रखने का प्रयास। और इसी के चलते उन्हें न तो शैक्षणिक विकास करने का अवसर दिया जाता है और न ही उनके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य व पोषण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। जहां तक छुआछूत जैसी प्रकट प्रथाओं का सवाल है; तो ये भी देश के कुछ हिस्सों में जिंदा हैं। यद्यपि, पिछली डेढ़ सदी में चले सामाजिक आंदोलनों के कारण छुआछूत का प्रचलन कम हुआ है। इसके साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के चलते अछूत-प्रथा ने नए स्वरूप ग्रहण कर लिए हैं। उदाहरणार्थ, गांवों और कस्बों में स्थित छोटे-छोटे होटलों और चाय की दुकानों में दो तरह के बर्तन रखे जाते हैं और अछूतों को अलग बर्तनों में चाय व खाद्य सामग्री परोसी जाती है। शहरी क्षेत्रों और यहां तक कि महानगरों में भी यह प्रथा किसी-न-किसी स्वरूप में जीवित है। मुझे पता है कि आज भी कुछ शहरी इलाकों में दलितों को किराए पर मकान नहीं मिलते। केवल वे ही दलित, सरकारी या अन्य आवासीय परिसरों में मकान ले पाते हैं; जो संगठित क्षेत्र में उच्च स्तर पर कार्यरत हों। दलितों के होटलों को ग्राहक नहीं मिलते। अगर उनमें से कुछ इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते भी हैं, तब भी उन्हें मजबूर होकर अपने होटल इत्यादि बंद कर देने पड़ते हैं।
शहराें और कस्बोें मेें रहने आने वाले एससी असंगठित क्षेत्र में श्रमिक के रूप में काम करने और झुग्गी बस्तियों में निवास करने के लिए मजबूर होते हैं। यही बात उन आदिवासियों के बारे में भी सही है, जो अपना घर-बार छोड़कर काम की तलाश में शहरों में आते हैं। यद्यपि, तुलनात्मक रूप से उनकी संख्या एससी से काफी कम होती है। एसईडीबीसी के कमजोर वर्गों (जिनमें मुस्लिम एसईडीबीसी भी शामिल हैं) का भी कमोबेश यही हाल होता है।
देश में सत्ता के ढांचे (जिसके कुछ लक्षणों का मैंने पहले वर्णन किया है) के चलते अछूत-प्रथा का प्रभाव कम करने और उसका उन्मूलन करने के कार्य को यथेष्ट महत्व नहीं मिल सका। फिर चाहे वह इस प्रथा के सामाजिक और शैक्षणिक प्रभाव की बात हो या उसके द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की। संविधान का अनुच्छेद-17 कहता है कि ‘अस्पृश्यता का अंत किया जाता है…, अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा; जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।’ यह प्रावधान 26 जनवरी, 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही प्रभावी हो गया। परंतु, अछूत-प्रथा का आचरण करने वालों को दंडित करने से संबंधित कानून को अस्तित्व में आने में पांच वर्ष और लगे। अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 (जो 1.6.1955 से लागू हुआ), की कमियां एकदम शुरुआत में ही स्पष्ट हो गई थीं। मैंने इस बारे में अलग से लिखा है कि किस तरह राज्य सरकारों ने इस कानून को मजाक बना दिया और केंद्र सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 में संशोधन कर, उसे अधिक कड़ा बनाने में 20 साल लग गए और ये संशोधन 19 नवंबर 1976 से लागू हुए। तथ्य यह है कि ये संशोधन भी अपर्याप्त हैं।
मुझे कहना होगा कि इस मुद्दे की उपेक्षा के लिए ‘राज्य’ जिम्मेदार नहीं हैं; बल्कि वे लोग जिम्मेदार हैं, जिनका राज्य तंत्र पर नियंत्रण है। दूसरे शब्दों में, वे लोग जो केंद्र और राज्य सरकारों में शीर्ष पदों पर हैं, जो वर्चस्वशाली वर्गों द्वारा नियंत्रित विधानमंडलों के सदस्य हैं और जो हमारी न्याय-प्रणाली के प्रभारी हैं। हमारी न्याय-प्रणाली में अछूत-प्रथा के शिकार व्यक्तियों की संख्या न के बराबर है।
वासंती देवी : हाथ से मैला साफ करने की घृणित प्रथा आज भी जारी है। यह इस तथ्य के बावजूद कि इसे कानून द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। राज्य, नगरीय निकाय प्रशासन और रेलवे इस कानून के सबसे बड़े उल्लंघनकर्ता हैं। एससी को इस आपराधिक अमानवीयकरण से मुक्ति कैसे दिलाई जा सकती है? क्या इस काम को कर रहे लोगों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करवाए बिना यह संभव है?
पी.एस. कृष्णन : हाथ से मैला साफ करने की प्रथा के अस्तित्व में आने और उसके बने रहने का एक प्रमुख कारण यह है कि जाति-प्रथा ने हमारी मानवीय संवेदनाओं को मार दिया है। हाथ से मैला साफ करने की प्रथा इसलिए कायम है, क्योंकि यह काम करने वाले लोग आसानी से और सस्ते में उपलब्ध हैं। वे आसानी से और सस्ते मेें इसलिए उपलब्ध हैं, क्योंकि उनके पास जीवनयापन का कोई और साधन नहीं है और जाति-प्रथा ने इस कार्य को कुछ समुदायों का पारंपरिक पेशा बना दिया है। ये सभी समुदाय एससी हैं। मेरी गणना के अनुसार, जो लोग हाथ से मैला साफ करने के काम से जुड़े हुए हैं; वे देश की कुल एससी आबादी का 10 प्रतिशत हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि 10 प्रतिशत एससी हाथ से मैला साफ करने का काम कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हाथ से मैला साफ करने वाले समुदायों की आबादी, एससी की कुल आबादी का 10 प्रतिशत है। इस तरह, यदि हाथ से मैला साफ करने की प्रथा बनी हुई है; तो उसका कारण पारंपरिक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं हैं। इसे केवल कानून बनाकर समाप्त नहीं किया जा सकता। इस कानून को गंभीरता से लागू किया जाना भी आवश्यक है। इसके साथ-साथ, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हाथ से मैला साफ करना किसी व्यक्ति की मजबूरी न बन जाए। कई देशों में इस तरह की स्वच्छता प्रणालियां हैं, जिसमें हाथ से मैला साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष तकनीकी आदि जैसे जटिल क्षेत्रों में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। परंतु, उसने कभी गंभीरता से यह प्रयास नहीं किया कि ऐसी तकनीकी विकसित की जाए, जिससे बिना हाथ से मैला साफ किए स्वच्छता बनाए रखी जा सके। इसकी तकनीकी बहुत साधारण है। मैंने श्रम मंत्रालय की सफाई और चमड़ा कामगाराें पर कार्यकारी समूह के सदस्य के तौर पर एक नए कानून का मसौदा तैयार किया था; जिसका शीर्षक था- ‘हाथ से मैला साफ करने वाले व अन्य सफाई कर्मी (पूर्ण मुक्ति, समग्र पुनर्वास व कार्य करने की स्थितियों का मानवीकरण) अधिनियम, 2010’। इस मसौदे का कार्यकारी समूह की बैठकों में खंडवार परीक्षण कर इसका अनुमोदन किया गया था। इस मसौदे में तकनीकी के इस्तेमाल के संबंध में निम्न प्रावधान थे :
- सीवर संबंधी सेवाओं का नगर पालिकाओं द्वारा मानवीकरण किया जाएगा और यह काम करने वाले कर्मियों को हर प्रकार के खतरों और गंदगी से मुक्त किया जाएगा। इसके लिए जो कदम उठाए जाएंगे, उनमें शामिल है… इस तरह का यंत्रीकरण, जिसके चलते किसी व्यक्ति को सीवरों, नालियों या मेनहोल में घुसने की जरूरत न पड़े। नालियों व सीवरों से गाद और रुकावटें हटाने के लिए सक्षम यंत्रों का प्रयोग; सीवर लाइनों के संधारण के लिए उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल और सीवरों और नालियों में ठोस व नष्ट न होने वाले पदार्थों का प्रवेश रोकने के लिए स्क्रीनरों का प्रयोग।
- भारत सरकार एक स्वायत्तशासी राष्ट्रीय स्वच्छताकर्मी शोध संस्थान की स्थापना करेगी; जो जल्द-से-जल्द विश्व के विभिन्न हिस्सों में स्वच्छता कर्मियों को खतरों और गंदगी से बचाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधियों का अध्ययन कर, तदानुसार, सीवेज नालियाें व सेप्टिक टैंकों की सफाई की प्रणाली का आधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर पूर्ण यंत्रीकरण करेगी, जिनमें निम्न बिंदु शामिल होंगे :
- उन्नत तकनीकी का प्रयोग कर सीवर लाइनों का निरोधक अनुरक्षण।
- काम करने के स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए रासायनिक डिटेक्टरों का प्रयोग।
- ठोस व नष्ट न होने वाले पदार्थों का प्रवेश रोकने के लिए स्कीनरों का प्रयोग व
- बांस की खपच्ची के स्थान पर यांत्रिक उपकरण का इस्तेमाल।
भारत सरकार राष्ट्रीय स्वच्छता तकनीकी मिशन की स्थापना करेगी; जो आधुनिक प्रविधियों और तकनीकों की पहचान कर और उनका विकास कर उन्हें भारत सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय संस्थाओं और प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और संस्थानों, निजी औद्योगिक व वाणिज्यिक संस्थानों, सफाईकर्मियों और समाज की जानकारी में लाएगी; ताकि उन्हें अपनाया जा सके।
इन प्रावधानों को उस अधिनियम में शामिल नहीं किया गया, जिसे सरकार ने तैयार किया और संसद से स्वीकृत करवाया। मेरे द्वारा तैयार किया गया मसौदे को (जिसे श्रम मंत्रालय के कार्यकारी समूह ने अनुमोदित किया था) सन् 2010 में सरकार को प्रेषित कर दिया गया था। इस मामले में कुछ समय तक कुछ भी नहीं हुआ, क्याेंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व श्रम मंत्रालय, इस कानून को अंतिम रूप देने और उसे संसद में प्रस्तुत करने का काम एक-दूसरे पर टालते रहे। मैं तत्कालीन सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री श्री मुकुल वासनिक के ध्यान में यह तथ्य लाया कि हाथ से मैला साफ करने वाले श्रमिक जिन जातियों से आते हैं, उनके कल्याण की जिम्मेदारी उनके मंत्रालय की है और इसलिए उनके मंत्रालय को ही इस कानून को अंतिम रूप देकर उसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उन्हाेंने मेरे इस सुझाव को स्वीकार किया। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, जिसे इस मंत्रालय ने संसद में प्रस्तुत किया और जिसे सन् 2013 में संसद की स्वीकृति मिली। निश्चित तौर पर इसके पूर्व पारित मैनुअल सफाई कर्मचारियों और शुष्क शौचालयों के निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 से बेहतर है। परंतु, उसमें तकनीकी के प्रयोग संबंधी पहलू का समावेश नहीं है; और साथ ही यह कुछ अन्य समस्याओं के बारे में भी मौन है, जिनका वर्णन नीचे किया गया है।
एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो लोग हाथ से मैला साफ करने का काम कर रहे हैं या उनके परिवारों के सदस्य हैं; उन्हें जीवनयापन के वैकल्पिक साधन (जो स्वच्छता संबंधी कार्यों से एकदम अलग हों) अपनाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसा केवल वर्तमान सफाईकर्मियों और उनके परिवारों के मामले में ही नहीं, बल्कि उन सभी जातियों के मामले में किया जाना चाहिए, जो पारंपरिक रूप से यह काम करते आ रहे हैं। ताकि, जब वर्तमान कर्मियों को मुक्त कराया जाए, तो उनका स्थान अन्य लोग इसलिए न ले सकें; क्योंकि वे उपलब्ध ही न हों। कुल मिलाकर, भारत में हाथ से मैला साफ करने वाले लोग उपलब्ध ही नहीं होने चाहिए। उनकी आपूर्ति लाइन को ही काट दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही पीड़ितों को ऐसे वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, जिनके साथ उस तरह का तिरस्कार व कलंक न जुड़ा हो; जैसा कि हमारे समाज में सफाईकर्मियों से जुड़ा हुआ है। वर्तमान सरकार बड़े पैमाने पर कौशल विकास कार्यक्रम लागू कर रही है। इस कार्यक्रम का फोकस उन जातियों पर होना चाहिए, जो पारंपरिक रूप से हाथ से मैला साफ करने का काम करती आ रही हैं। ताकि, सप्लाई लाइन पूरी तरह से काट दी जाए और समाज और सरकार को मजबूर होकर मानव-संगत तकनीकी व प्रणाली का प्रयोग सफाई कार्य के लिए करना पड़े। वर्तमान में ऐसा नहीं लगता कि हमारा राजनीतिक तंत्र और नागरिक समाज इस मामले में कुछ करने के प्रति गंभीर है।
हाथ से मैला साफ करने वाले कर्मियों से मेरा परिचय और जुड़ाव उन दिनों से है, जब मैं किशोर था। करीब 70 वर्ष पहले, मेरे ध्यान में यह तथ्य आया कि केरल के तिरुअनंतपुरम में चैंगलचुला नामक इलाके में बड़ी संख्या में हाथ से मैला साफ करने वाले लोग निवास करते हैं। मुझे यह भी पता चला कि उच्च जाति के एक व्यक्ति श्री रामकृष्ण पिल्लई, तिरुअनंतपुरम में हाथ से मैला साफ करने वालों को संगठित कर रहे हैं। वे देश और केरल में ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। पेशे से वे दर्जी थे और कांग्रेस-जनों और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वालों के लिए ‘झुब्बा‘ नामक एक वस्त्र बनाया करते थे। यह उत्तर भारत के कुर्ते के जैसा था और इस कारण उन्हें ‘झुब्बा रामकृष्ण पिल्लई‘ भी कहा जाता था। हाथ से मैला साफ करने वालों के लिए काम करने के कारण उन्हें ‘थोट्टी रामकृष्ण पिल्लई‘ की पदवी भी दी गई थी। थोट्टी का अर्थ होता है सफाई-कामगार। इसके कई दशकों बाद, सन् 2007 के आसपास, मैं श्री रामकृष्ण पिल्लई से मिला। तब तक वे बहुत वृद्ध हो चुके थे। मैंने उनसे उनका जीवन परिचय मांगा और औपचारिक रूप से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से भारत सरकार को उन्हें पद्मभूषण प्रदान किए जाने की सिफारिश के साथ भेजा। कोई आश्चर्य नहीं कि नैतिक और सामाजिक दृष्टि से एक असाधारण कार्य करने वाले इस सामान्य व्यक्ति को हमारी व्यवस्था ने कोई मान्यता नहीं दी। न तो नौकरशाहों ने और न ही राजनीतिक नेतृत्व ने उनके योगदान को सराहना देने में रुचि दिखाई।
यह भी पढ़ें : हाथों से मैला कब तक उठाएगा देश?
हाथ से मैला साफ करने वालों और उनकी जातियों के साथ मेरा पहला व्यावहारिक वास्ता तब पड़ा, जब मैं सन् 1958-59 में ओंगोल का सब-कलेक्टर था। मैंने इस बारे में प्रश्न क्रमांक चार के उत्तर में पहले ही बता दिया है। सन् 1978-82 में गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव की हैसियत से मैंने हाथ से मैला साफ करने वालों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम उस समय लागू ‘नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए मशीनरी‘ योजना के भाग के रूप में लागू किया गया था। मेरा तर्क यह था कि अछूत-प्रथा के उन्मूलन के लिए हाथ से मैला साफ करने वालों की मुक्ति और पुनर्वास अपरिहार्य हैं। बाद में इस कार्यक्रम को ‘हाथ से मैला साफ करने वालों की मुक्ति व पुनर्वास‘ नाम से एक अलग केंद्र-प्रवर्तित योजना का दर्जा दे दिया गया। अब इसे ‘हाथ से मैला साफ करने वालों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना‘ के नाम से जाना जाता है।
सन् 1985 में जब मैं लंबी छुट्टी पर था। उस दौरान मैंने आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एन.टी. रामाराव से एससी, एसटी, एसईडीबीसी व विशिष्टतः हाथ से मैला साफ करने वालों के संबंध में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने हाथ से मैला साफ करने वालों की मुक्ति और पुनर्वास के संबंध में मेरे विचारों में काफी दिलचस्पी दिखाई। मैंने उन्हें यह भी बताया कि अगर इसके लिए पूरे राज्य हेतु समग्र योजना बनाई जाए, तो उसके कार्यान्वयन के लिए संभवतः विश्व बैंक से मदद मिल सकती है। उन्हाेंने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी कि मैं हाथ से मैला साफ करने की प्रथा के उन्मूलन और यह काम करने वालों की मुक्ति के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव तैयार करूं। मैंने यह प्रस्ताव तैयार किया, जिसे श्री एन.टी. रामाराव ने विमुक्ति का नाम दिया। परंतु, इसके बाद आए राजनीतिक परिवर्तनों की आंधी में यह प्रस्ताव खो गया।

सन् 1993 के कानून अर्थात मैनुअल सफाई कर्मचारियों और शुष्क शौचालयों के निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम का फोकस हाथ से मैला साफ करने वालों पर नहीं था। यह वैसा ही था, जैसे प्रिंस ऑफ डेनमार्क के बिना हेमलेट। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, इस मामले में बेहतर है कि इसका फोकस हाथ से मैला साफ करने वालों पर है।
हाथ से मैला साफ करने के कार्य से मुक्त किए गए कर्मियों, उनके परिवारों और ऐसे अन्य परिवारों के सदस्यों (जो ऐसी जातियों से हैं, जिनके सदस्य पारंपरिक रूप से यह काम करते आए हैं और जो मुक्त किए गए कर्मियों का स्थान ले सकते हैं) के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। उन्हें इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा सकता है, जिससे वे विभिन्न पेशों को अपना सकें। इसके अलावा उनके लिए स्वरोजगार की व्यवस्था भी की जा सकती है। उनमें से कई को बड़े शहरों और शहरी क्षेत्रों में स्थित दूध प्रदाय करने वाले बूथों में काम दिया जा सकता है। सभी लोगों को हाथ से मैला साफ करने के काम से मुक्त किए गए कामगारों या ऐसी जातियों के लोगों (जो पारंपरिक रूप से यह काम करते हैं) के हाथों से ही दूध मिलना चाहिए। जहां ये बूथ सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित हैं; वहां यह आसानी से किया जा सकता है। जो बूथ निजी या सहकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं, उनके मामले में कानून बनाकर या उन्हें राजी कर यह हो सकता है। इसी तरह, रेलवे में जो लोग चाय या पानी प्रदाय करते हैं; वे इसी श्रेणी के होने चाहिए। हाथ से मैला साफ करने की व्यवस्था को बनाए रखने का जो पाप रेलवे ने किया है, उसके प्रायश्चित स्वरूप उसे इन्हीं श्रेणियों के व्यक्तियों को खाना पकाने और उसे यात्रियों तक पहुंचाने का काम देना चाहिए। उन्हें इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बड़े रेलवे स्टेशनों पर, जहां खानपान व अन्य सेवाएं ठेके पर दी जाती हैं; ठेके की शर्तों में यह शामिल होना चाहिए कि ठेकेदार इन श्रेणियों के व्यक्तियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिलवाने के बाद, खाना पकाने और परोसने का काम देंगे। यह आरक्षण नहीं है। यह अछूत-प्रथा से उस स्तर पर मुकाबला करने का प्रयास है, जिस स्तर पर वह सबसे अधिक मजबूत और व्यापक है। इन सभी उपायों का वर्णन मैंने अधिनियम के अपने मसौदे में किया था, जिसमें हर श्रेणी के नियोक्ताओं के उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए थे। परंतु, सरकार द्वारा जो अधिनियम अंततः लागू किया गया; उसमें ये प्रावधान नहीं हैं। आज हमारे समक्ष जो महत्वपूर्ण कार्य है, वह है- यह सुनिश्चित करना कि सन् 2013 में लागू किए गए अधिनियम का ठीक से क्रियान्वयन हो और जल्द-से-जल्द विधायिका द्वारा इसमें उपयुक्त संशोधन किए जाएं। मैं इस पहलू पर और अधिक विस्तृत चर्चा एससी व एससी के लिए विशेष घटक योजना पर मेरी आगामी पुस्तकों मेें करूंगा।
(क्रमश: जारी)
(कॉपी संपादन : प्रेम बरेलवी/एफपी डेस्क)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in
फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें
मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया