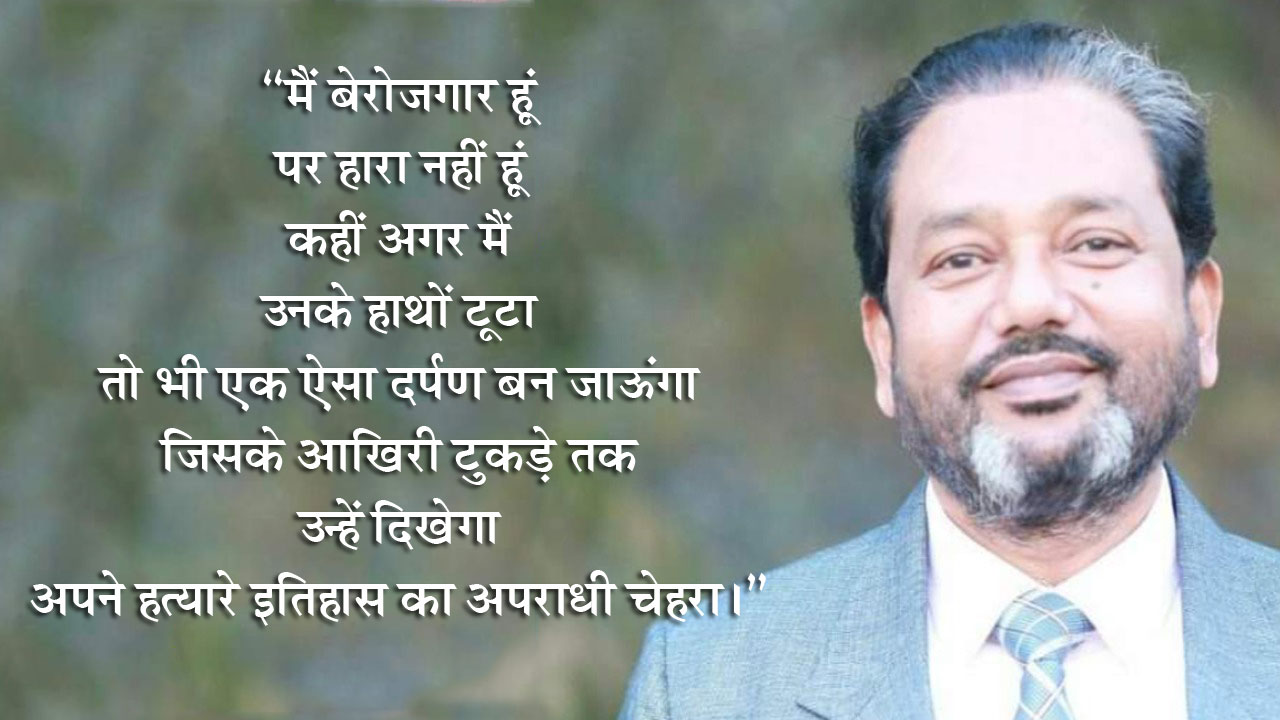जन-विकल्प
अशोक की धम्म नीति पर देशी-विदेशी विद्वानों ने बहुत अध्ययन-मनन किया है और उसकी गिनती दुनिया के महानतम शासकों में की गयी है। कुछ मामलों में वह ख़ास जरूर था; लेकिन यह आखिर क्यों हुआ कि उसके बाद मौर्य साम्राज्य लड़खड़ा गया? अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं लुढ़कती देखी गयी हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। निश्चय ही अशोक द्वारा उठाये गए कदम में कुछ दोष थे। इसके कारणों का विश्लेषण जिस तरह होना चाहिए था, उस तरह नहीं हो सका। उस पुराने जमाने में उसने राज्य के आदर्श को बौद्ध धम्म में केंद्रित कर दिया। उसने राज्य-विस्तार की योजनाएं नहीं बनायीं और कलिंग के बाद कोई युद्ध नहीं किया। यह सब सच है। लेकिन सच यह भी है कि अब और कोई युद्ध करना दिख भी नहीं रहा था। इसलिए उसने शांति की नीति अपनायी, जो शायद एक कूटनीतिक चाल अधिक थी। उत्तर-पश्चिम से लेकर दक्षिण के थोड़े-से इलाके को छोड़ कर सुदूर इलाकों तक मौर्य साम्राज्य का परचम लहरा रहा था। कलिंग अब इसमें शामिल था। उसके ज़माने में संचार के जो साधन थे, वह इस तरह के नहीं थे कि पूरे साम्राज्य पर पाटलिपुत्र से नियंत्रण किया जा सके। इस उद्देश्य से यदि उसने शांति की नीति अपनाई तो यह एक अपने किस्म की राजनीति ही थी। लेकिन प्रतीत होता है यह इतना भर नहीं था, या यह बिलकुल नहीं था। धम्म उसकी व्यक्तिगत सनक थी, जिसके लिए उसने राज्य को खत्म होने दिया। इतिहासकार रोमिला थापर कहती हैं “अशोक निस्संदेह बौद्ध मत की ओर आकर्षित हुआ था और बौद्ध सिद्धांतों पर आचरण भी करने लगा था। लेकिन उसके समय का बौद्ध मत मात्र एक धार्मिक विश्वास नहीं था, अपितु अनेक स्तरों पर वह एक सामाजिक और बौद्धिक आंदोलन भी था, जिसने समाज के अनेक पक्षों को प्रभावित किया था। ऐसी स्थिति में किसी भी कुशल राजनेता को इस आंदोलन के संपर्क में आना ही पड़ता।”
रोमिला आधुनिक दुनिया के जनतन्त्रात्मक उपकरणों से राजतन्त्र के एक ऐसे राजा का आकलन करना चाहती हैं, जो अपनी प्रवृत्ति में अंत तक तानाशाह बना रहा। वह यह भूल गयीं कि वह पुरानी दुनिया के किसी गणतंत्र के राजा अथवा प्रमुख का आकलन नहीं कर रही हैं। अशोक को जनता से हमदर्दी की बहुत दरकार नहीं थी। धम्म उसकी व्यक्तिगत मुक्ति का एक सोपान था। इससे उसके आचरण में आये बदलावों से जनता को कुछ फायदे हुए होंगे, लेकिन उसकी सनक से पूरे साम्राज्य, पूरी राजनीति को जो नुकसान हुआ, उसका बोझ अंततः जनता को ही ढोना पड़ा। उसके होते ही साम्राज्य में कमजोरी के लक्षण स्पष्ट होने लगे थे। तक्षशिला के विद्रोह को उसने स्वयं दबाया था और कलिंग ने उसके दांत खट्टे कर दिए थे। अन्य स्थानीय शक्तियां बार-बार सिर उठाती थीं और सीमा पार भी यवन और अन्य शक्तियां निरंतर सक्रिय थीं। इन्हीं स्थितियों में 36 साल शासन करने के उपरांत 232 ईसापूर्व में वह मर गया। जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ, उसकी मौत सम्राट के तौर पर हुई। उसने किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान ने अशोक के आखिरी समय का जो वर्णन किया है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि वह विक्षिप्त हो चुका था। उस वर्णन के अनुसार अशोक ने एक बड़ी राशि बौद्ध संघ को दान देने की ठान ली थी। संभव है कुछ अतिशयोक्ति हो, लेकिन कहते है यह राशि एक सौ करोड़ थी। उसने 96 करोड़ तो दान कर दिए थे, लेकिन चार करोड़ की राशि शेष थी। अशोक जब आखिरी दिनों में आया और उसे अनुभव होने लगा कि अपनी प्रतिज्ञा पूरी किये बिना ही मैं ‘निर्वाण’ प्राप्त कर जाऊंगा तो उसने अपने राज्य को ही दान कर दिया। यह हास्यास्पद स्थिति ही थी। लेकिन उसके मनोविज्ञान का विश्लेषण किया जाए तो इसके कुछ और अर्थ निकल सकते हैं। क्या उसने अपने साथ ही राज्य के विलोप की बात सोच ली थी? और क्या उसने यह सोच लिया था कि बौद्ध-संघ जनता के कल्याण और राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल लेगा? यदि यह उसकी सोच थी, तब यह विक्षिप्त व्यक्ति की सोच ही समझी जा सकती है। उसे अपनी कमाई तो दान देने का पूरा हक था, किन्तु प्रजा की गाढ़ी कमाई की राशि इस तरह दान करने पर उसे सोचना चाहिए था। क्या बुद्ध और उनके धम्म से उसने यही शिक्षा ग्रहण की थी? उसके पूर्व भी कुछ राजा बुद्ध और बौद्ध धर्म से प्रभावित रहे, लेकिन उन सब ने इस तरह की अदूरदर्शिता नहीं दिखलाई। आश्चर्य है इस काल पर काम करने वाले इतिहासकारों ने इस तरह के प्रश्न क्यों नहीं उठाये।

साम्राज्य के महादान की कथा किसी को भी अविश्वसनीय लग सकती है। लेकिन यदि हम इस कथा पर विश्वास करें तो यह उसके उत्तराधिकार की कहानी से भी जुड़ जाती है। बिन्दुसार की मृत्यु के बाद अमात्यों ने हस्तक्षेप करके जिस तरह अशोक को राजा बनाया था, एकबार फिर वैसा ही हुआ। एक बार फिर अमात्यों की चली। कहते हैं अमात्यों ने चार करोड़ रुपये इकठ्ठा किये और उसे संघ को देकर बंधक बने राज्य को मुक्त किया। अशोक के उत्तराधिकारियों का चित्र साफ-साफ़ नहीं दीखता। कई पत्नियां थीं, तो पुत्र भी कई होंगे, जो उन दिनों कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन पुराणों और बौद्ध ग्रंथों के आधार पर एक उलझी-सी तस्वीर बनती है। उसका एक बेटा तीवर था, जिसका उसके अभिलेखों में उल्लेख है। इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री का अनुमान है वह उनके जीवनकाल में ही मर गया था। पुत्र महेंद्र को उसने अपने जीवन काल में ही भिक्षु बना दिया था। पुत्र कुणाल की चर्चा सभी ग्रंथों में मिलती है, जो एक कथा के अनुसार अपनी विमाता तिष्यरक्षिता द्वारा अँधा कर दिया गया था। संभवतः इसी कारण उसके राजा बनने पर किसी ने विचार नहीं किया। जो जानकारी मिलती है, उसके अनुसार अशोक के बाद मगध साम्राज्य कई भागों में विभक्त हो गया। जैसे पाटलिपुत्र पर दसरथ सत्ता पर काबिज होता है, लेकिन उज्जैन पर सम्पदि और कश्मीर पर इसी वंश का जालौक स्वतंत्र शासक बन जाता है। ये सब मौर्य ही थे और कहा जा सकता है कि पूरे भारत में मौर्य शासन ही था, लेकिन पाटलिपुत्र की सत्ता सिमट गयी थी। उत्तर-पश्चिम के बड़े हिस्से पर यवन ताकतें कब्ज़ा जमा चुकी होती हैं। इस तरह कहा जाना चाहिए कि अशोक अपने साथ मौर्य साम्राज्य के शौर्य को भी लेता गया। जिस साम्राज्य को महापद्मनंद और चन्द्रगुप्त ने ऊंचाइयों पर पहुँचाया और जिसे बिन्दुसार ने सम्भाल कर रखा, उसे अशोक ने व्यक्तिगत सनक में विनष्ट कर दिया। उसके हज़ारों स्तम्भ उसके प्रचार स्तम्भ बन कर रह गए। उसने सोचा था इन स्तम्भों के आधार पर ही उसकी छवि बनेगी। वह कुछ गलत भी नहीं था। लम्बे समय तक इसी आधार पर उसे महान कहा जाता रहा। लेकिन अब समय आ गया है जब हमें अशोक के बारे में गंभीर हो कर निर्णय लेना चाहिए। महानता की चादर काफी दागदार है।
अशोक के बाद भी कोई सैंतालीस वर्षों तक पाटलिपुत्र और देश के बड़े हिस्सों में मौर्य शासन रहा। लेकिन अब पहले जैसी चमक नहीं थी। उज्जैन का मौर्य राजा सम्पदि जैन धर्म अपना चुका था और कश्मीर का जालौक वैदिक धर्म में रूचि ले रहा था। इससे यह भी अर्थ निकलता है कि जनता के प्रभावशाली हिस्से पर जिस मत का प्रभाव होता था, राजा उससे एकात्मता प्रदर्शित करता था। इससे उसे जनता पर प्रभाव रखने में सुविधा होती होगी। यह विचारणीय है कि उज्जैन और कश्मीर के शासक जब जैन और वैदिक धर्म की तरफ अभिमुख हो जाते हैं, तब भी पाटलिपुत्र का शासक बौद्ध ही क्यों बना रहता है। अशोक ने बौद्ध संघों को जो दान दिए उसके प्रभाव पाटलिपुत्र के इर्द-गिर्द घनीभूत थे। पाटलिपुत्र स्थित कुक्कट-विहार इतना संपन्न और मजबूत हो गया था कि बाद में पुष्यमित्र शुंग को इसे तबाह करने में विफलता ही हाथ लगी। इस तरह किसी विचार या धर्म का इतना अधिक राजनीतिकरण अंततः उसके लिए भी नुकसानदायक ही सिद्ध होता है। बौद्ध धर्म की तार्किकता और संघों के विवेक में बहुत अंतर आया। संघों और विहारों में इतना धन इकठ्ठा हो गया कि वहाँ अपराध स्वाभाविक तौर पर बढ़ने लगे। अनुदान और सहूलियतें किसी विचार को जिस तरह भ्रष्ट करती हैं, बौद्धधर्म इसका उदाहरण बन गया।
यह भी पढ़ें – पियदसि लाजा मागधे : मगध का प्रियदर्शी राजा
अशोक के बाद के सैंतालीस वर्षों में किस राजा ने कितने समय तक शासन किया, इस पर इतिहासकार एक मत नहीं हैं। दसरथ और उसके बेटे वृहदरथ या वृहद्रथ की चर्चा मगध के शासक के रूप में होती है। यह वृहदरथ ही था जिसके सेनापति ने धोखे से उसकी हत्या कर दी और सत्ता अपने हाथों में ले ली। हुआ यह कि सेनापति पुष्यमित्र ने अपने राजा वृहद्रथ को सेना के निरीक्षण के लिए आमंत्रित किया। उत्तर-पश्चिम में यवनों की गतिविधियों को देखते हुए सेना को सतर्क रखना आवश्यक था। राजा वृहद्रथ जब सेना का निरीक्षण कर रहा था अचानक से पुष्यमित्र ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। निश्चित ही उसने सेना को इसके लिए विश्वास में लिया होगा। यह घटना 185 ईसापूर्व में हुई और इसके साथ ही 137 वर्षों तक भारत भूमि पर राज करने वाले इस राजवंश का हमेशा के लिए अंत हो गया। पाटलिपुत्र की राजनीति भी फिर कभी मौर्यों के गौरव को नहीं छू सकी।

मध्य प्रदेश के सतना जिले के भरहुत स्तूप में बुद्ध की खंडित मूर्ति
पुष्यमित्र शुंग कौन था? इसपर कम ही चर्चा हुई है। सामान्य तौर पर इसे ब्राह्मण माना गया है, लेकिन दिव्यावदान के अनुसार यह मौर्य कुल का ही था। लेकिन इसकी संभावना कम ही है। पुष्यमित्र-वृहदरथ संघर्ष निश्चित रूप से मौर्यों का गृहयुद्ध नहीं था। पुष्यमित्र अनजाने या जाने एक बड़ी लड़ाई का नेतृत्व कर रहा था। वह महत्वाकांक्षी और कुटिल प्रवृति का था इसमें कोई शक नहीं। वह संभवतः उस पतंजलि का शिष्य रहा था, जो योगसूत्र और पाणिनि के अष्टाध्यायी का भाष्यकार था। निश्चित ही वह विद्वान था, लेकिन यह भी तय है कि वह बौद्धों से नफरत करता था। हर विद्वान संत भी नहीं होता। विद्वान व्यक्ति की कुटिलता सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक घातक होती है। उसके बुरे नतीजे बहुआयामी होते हैं। उसके शिष्य पुष्यमित्र में भी बौद्धों से नफरत का यह भाव था, जिसकी सूचना बौद्ध ग्रंथ ही देते हैं। पुष्यमित्र अपने गुरु पतंजलि से वैचारिक स्तर पर प्रशिक्षित हुआ हो इसकी पूरी संभावना है। लेकिन इतने पर भी यह दो या अधिक से अधिक कुछ लोगों के एक समूह, जिसे हम गिरोह कह सकते हैं का मामला है। अधिक से अधिक इसे सैन्य-क्रांति कह सकते हैं। इसके लिए किसी पूरी जाति या सम्प्रदाय को जिम्मेदार बनाना उचित नहीं है। हमारे ज़माने में इंदिरा गाँधी की हत्या उनके सरकारी आवास पर सुरक्षा प्रहरियों द्वारा की गयी थी। कुछ इसी तरह की घटना पुष्यमित्र द्वारा की गयी थी। इसके लिए हम किसी पूरे संप्रदाय को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते।
अनेक इतिहासकारों ने पुष्यमित्र शुंग की परिघटना को इस नजरिये से देखा है मानो वह बौद्धधर्म के विरुद्ध एक ब्राह्मण विद्रोह या क्रांति थी। लेकिन जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, इस दृष्टिकोण में बहुत बल नहीं है। यह ठीक है कि मौर्य और उसके पूर्व के नन्द राजा वैदिक ब्राह्मण धर्म में यकीन नहीं करते थे और उनके झुकाव परिव्राजकों से जुड़े पंथ की ओर थे। इन परिव्राजक पंथ में बौद्ध, जैन और आजीवक सम्प्रदाय के लोग थे। ये लोग वेदों में यकीन नहीं करते थे और लगभग निरीश्वरवादी थे। परलोक में कम ध्यान रखने के कारण आचरण की शुद्धता और सामाजिक मेलजोल की भावना पर जोर देते थे। लेकिन जो लोग यह सोचते हैं यह केवल गैरब्राह्मणों का पंथ था, तो वे गलती पर हैं। नन्द या मौर्य राजाओं ने कभी भी ब्राह्मणों को हाशिये पर नहीं रखा। बौद्ध धर्म में भी अनेक ब्राह्मण हमेशा रहे। बुद्ध के समय तो सारिपुत्त और मौद्गल्यायन थे ही, बाद के दिनों में भी अनेक ब्राह्मणों के इस पंथ में होने की जानकारी मिलती है। अश्वघोष, वसुबन्धु,नागसेन आदि बौद्धों के बड़े दार्शनिक ब्राह्मण कुलों से आये। नन्द और मौर्य राजवंशों के अनेक विश्वसनीय अधिकारी ब्राह्मण रहे। धननंद का मंत्री राक्षस, जिसे लेकर संस्कृत नाटक मुद्राराक्षस लिखा गया है, ब्राह्मण था। अशोक का बौद्ध गुरु तिस्स मोग्लिपुत्त ब्राह्मण परिवार से आता था। स्वयं वृहदरथ ने जब पुष्यमित्र शुंग को सेनापति रखा था, विश्वास के तहत ही। इसलिए पुष्यमित्र का कार्य एक धोखा था, कोई जन-क्रांति नहीं थी। हर व्यक्ति में राजा बनने की अभिलाषा हो सकती है। और जिस किसी में यह अभिलाषा संघनित होने लगती है, उसे पागल बना देती है। महापद्मनंद, अशोक आदि सब ऐसे ही राजा बने थे। पुष्यमित्र अकेला नहीं था।
हाँ, कोई भी राजा जब राजसत्ता में आता है, खास कर अचानक, जैसे पुष्यमित्र आया था, तो वह अपनी और अपने कृत्यों की हिफाजत के लिए धर्म का सहारा जरूर लेता है। आधुनिक ज़माने में भी यही होता है। राजनेता अपनी सुविधा के लिए धर्म या जाति का सहारा लेते रहते हैं। पुष्यमित्र ने यही किया था। उसके प्रति उसके समकालीन और परवर्ती जो विवरण हैं उसमे उसे अच्छा नहीं माना गया है। केवल बौद्ध-ग्रन्थ ही नहीं, अन्य हिन्दू और यहां तक की ब्राह्मण विवरणों ने भी उसके कृत्य को महिमामंडित नहीं किया है। वाणभट्ट के हर्षचरित में जब वह कई राजाओं के कपटपूर्ण कृत्यों का वर्णन करता है तब उसी क्रम में पुष्यमित्र को रखता है। वह उसे कपटी सेनापति कहता है। पुष्यमित्र के कृत्यों पर आधुनिक ज़माने के कुछ इतिहासकारों ने अनावश्यक बल दिया। उसे प्रतीक बना कर दरअसल वह इस ज़माने की हिन्दू और ब्राह्मण-राजनीति कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो पुष्यमित्र के कार्य को एक राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में रखा। यह सब इतिहास के साथ खिलवाड़ के अलावा और कुछ नहीं है।
पुष्यमित्र निश्चय ही भयभीत था। पाटलिपुत्र में उसने अपनी राजधानी नहीं रखी। उसने अपनी राजधानी विदिशा में बनाया। निश्चय ही उसने बौद्धों के खात्मे के लिए सब कुछ किया। इसका एक कारण उसका पतंजलि के इशारे पर चलना हो सकता है। मगध के बौद्धों ने निश्चय ही उसका विरोध किया होगा क्योंकि दोनों के सामूहिक स्वार्थ टकराते थे। इसलिए संभव है उसने बौद्ध विरोधी रुख बनाये रखा। इसके लिए उसे वैदिक-ब्राह्मण संस्कृति के उन्नयन के लिए प्रयास करना था, ये सब काम उसने किये। लम्बे समय तक वेद-निरपेक्ष शासन रहने से वर्ण-व्यवस्था पर जोर नहीं दिया गया था। यह कमजोर हो चुकी थी और गाल बजाने वाले पण्डे-पुरोहितों के लिए समाज में कोई जगह नहीं रह गयी थी। जब कोई जातिवाद या संप्रदायवाद प्रभावी होता है तब उसका असली लाभ इसी तलछट तबके को होता है। इसलिए अपनी महत्ता से ये अभिभूत हो समर्थन में खड़े हो जाते हैं। इस तबके का समर्थन हासिल करने के लिए पुष्यमित्र ने वह सब किया, जो वह कर सकता था। कहते हैं बौद्ध विद्वानों की हत्या के लिए उसने इनाम घोषित कर रखे थे। मार्क्सवादियों की हत्या के लिए तो इस ज़माने की जनतन्त्रात्मक सरकारें भी यह कार्य करती हैं। लेकिन इन सब के साथ उसने अनेक हिन्दू ग्रंथों का सम्पादन करवाया। ‘मनुस्मृति’ आज जिस रूप में है, उसका स्वरुप शायद इसी दौरान मिला। अन्य हिन्दू ग्रंथों की भी रचना हुई ,और इस तरह उसने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि बौद्धों का जमाना गया। इस पर अधिक जोर देने के लिए उसने दो बार अश्वमेध यज्ञ किये, जो बीते जमाने की चीज हो गयी थी। हर दकियानूस राजा या राजनेता पुरानी बातों के पुनरुद्धार की बात करता है। इससे समाज की प्रतिगामी ताकतों को बल मिलता है और नए ख्यालों को रोकना संभव होता है। इस रूप में पुष्यमित्र प्रतिगामी सोच पर चल रहा था। उसने समाज की स्वाभाविक धारा को पलटने, उसे पुराने ढर्रे पर ले जाने की पूरी कोशिश की। इन कोशिशों का एक नतीजा तो यह निकला कि समाज के उत्पादक तबके में नैराश्य आया। शिल्पियों और किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा और इनकी भावना को आगे के समय में वणिक तबके ने आगे बढ़ाया। इस विषय पर हम आगे बात करेंगे।
पुष्यमित्र शुंग हमेशा बौद्ध विरोधी बना रहा,ऐसी बात नहीं थी। जैसा कि मैंने कहा अपने शासन के लिए एक समर्थक वर्ग सृजित करने के लिए राजा जाति और धर्म का सहारा लेते थे। उनका असल मकसद राज करना होता था। बड़ी संख्या में अशोक के स्तूपों को विनष्ट करने वाले पुष्यमित्र को जब लग गया कि उसका शासन स्थिर हो गया है, तब उसने भरहुत और साँची के बौद्ध चैत्यों का पुनरुद्धार भी किया। ये दोनों वर्तमान मध्यप्रदेश में हैं। भरहुत सतना जिले में है और साँची रायसेन जिले में। साँची का चैत्य महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहां बुद्ध के धातु-अवशेष रखे गए हैं। भरहुत में सारिपुत्त और मौद्गल्यायन के अवशेष रखे गए हैं।
(संपादन : नवल)