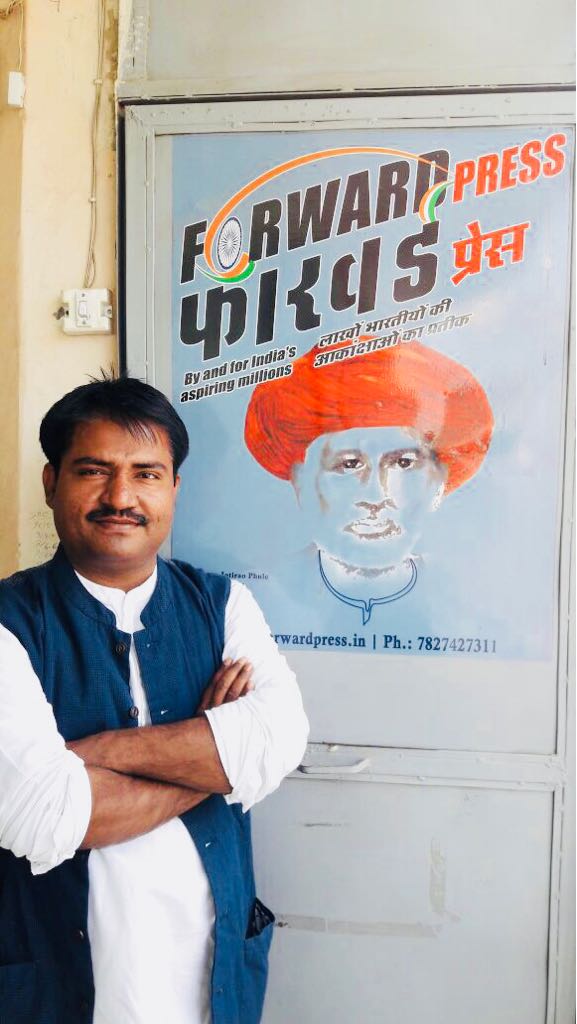पुस्तक समीक्षा
गोंड संस्कृति व परंपराओं से शेष भारत लगभग अपरिचित है। इसकी एक वजह भाषागत विभिन्नता भी है। लंबे समय से भारत में एक बहस चल रहा है कि कौन यहाँ का मूल समुदाय है और कौन नहीं। आर्य-अनार्य के बीच के संघर्ष में भारत के मूल आदिवासी समुदायों का इतिहास, परंपरा और संस्कृति पूर्ण रूप से तहस नहस हो गई। ऐसी संस्कृतियों का कोई लिखित इतिहास नहीं बचा। लेकिन यह सब आज तक आदिवासी समुदायों के बीच उनके लोक-कला, संगीत, नृत्य, वाद्य यंत्र, कहानी, कला, इत्यादि में मौखिक इतिहास के रूप में जीवित है। अपनी संस्कृति, परंपराओं को बचाने को संघर्षरत है मध्य भारत का गोंड़ समुदाय। इस किताब में लेखिका उषाकिरण आत्राम और उनके जीवनसाथी रहे सुन्हेरसिंह ताराम ने गोंड समुदाय के बीच अति महत्वपूर्ण माने जाने वाले ऐसे ही एक ऐसे गढ़ “कचारगढ़” के इतिहास और सांस्कृतिक परंपराओं को लिपिबद्ध किया है, जिसके सन्दर्भ में इसके पूर्व कोई आधिकारिक रचना नहीं थी।
यह किताब कई सवाल करती है तथा एक अनजान पठार से पाठको को परिचित करवाती है। मसलन, उस संस्कृति का क्या हुआ जो यहां के मूलनिवासियों का था और आर्यों ने जिसे तहस-नहस कर दिया? यह किताब इस सवाल का जवाब खोजने में अध्येताओं, शोधार्थियों और इतिहास के प्रति अनुराग रखने वालों की मदद कर सकती है।
सुन्हेरसिंह ताराम गोंडवाना दर्शन के संपादक रहे। गोंड संस्कृति और भाषा के लिए आजीवन काम करने वाले ताराम का निधन 7 नवंबर, 2018 को हो गया। उनके निधन के बाद यह पहली पुस्तक है जो प्रकाशित हुई है। इस किताब के केंद्र में कचारगढ़ है। कचारगढ़ गोंड समाज के लोगों के लिए सबसे बड़ा धार्मिक स्थल क्यों है और इससे जुड़ा इतिहास क्या है, यही जानकारी यह किताब देती है। यह किताब हिंदी में है, शायद इसके पीछे दोनों लेखकों का उद्देश्य यही रहा होगा कि गोंड संस्कृति के मौलिक विमर्श के बारे में वे भी जानें व समझें जो गोंड़ी भाषा नहीं जानते हैं।

इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हिंदी में होने के बावजूद गोंडी शब्दों को उनके उसी रूप में शामिल किया गया है। अनेक शब्द तो ऐसे हैं, जिनका इस्तेमाल हिन्दी प्रदेशों में होता आया है। इसके अलावा कई प्रसंग भी हैं जो शेष भारत में किसी दूसरे रूप में सुने-पढ़े जाते हैं। यह किताब कुछ रहस्यों के भेद भी खोलती है। इन्हीं रहस्यों में से एक है जंबू द्वीप और शंभूशेक-गौरा का रहस्य। इसी क्रम में यह किताब उस सच का संकेत देती है जिसके आधार पर भारत में गणना की शुरुआत हुई। जो गणित में रूचि रखते हैं, उनके लिए यह जानना और भी रोचक हो सकता है कि वस्तुओं के गिनने की प्रक्रिया का आविष्कार गोंड समाज के लोगों ने किया। इस आविष्कार को ऐबकस से भी पुराना माना जाना चाहिए।
किताब में बताया गया है कि कली कंकाली के 33 बालकों को आदर्श मानव बनाने के लिए [लिंगो व जंगो द्वारा] सात सगा शाखाओं की सामाजिक संरचना और पांच सगा शाखाओं के मुखिया की व्यवस्था की गई। इसके लिए सावरी पेड़ के फूल की पत्तियों का उपयोग किया गया। इस फूल में 12 पत्तियां रहती हैं। इसी के आधार पर तय किया गया। 1 से 1 देव, 2 से 2 देव और इसी तरह 12 से 12 देव। इसे गिनने की प्रक्रिया की शुरुआत की संज्ञा दी जा सकती है।
यह किताब हिन्दू मान्यताओं पर बड़े सवाल खड़े करती है। जैसे कि जिसे आर्य जंबू द्वीप कहते अघाते नहीं हैं, वह दरअसल यहां के मूलनिवासियों का शंभूद्वीप है जिसपर शंभू का राज था। आर्यों ने शंभू यानी शंकर का मिथक इसी के आधार पर गढ़ा होगा। इसकी संभावना इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि शंभू के साथ जो महिला गोंड संस्कृति की लोक-कथाओं में सामने आती है, उसके नाम गौरा, गौरी और पार्वती हैं।
आपने हिंदू धर्म के संस्कारों में रेवा खंड का जिक्र सुना होगा। यह किताब आपको इसका रहस्य भी बताती है। असल में यह देश तब रेवाखंड के नाम से जाना जाता था। इस आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि आर्य जब आए तब उन्होंने पहले तो लूट-खसोट किया होगा। लेकिन बाद में उन्हें वन-संपदा से परिपूर्ण इस देश ने उन्हें बसने के लिए प्रेरित किया होगा। तब उन्होंने यहां के मूलनिवासियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की होगी। इस क्रम में उन्होंने मूलनिवासियों के नायकों का पुनर्पाठ अपने तरीके से किया तथा उनके शब्दों, परंपराओं और जीवन शैली को अपनाने की कोशिश की होगी। कालांतर में आर्यों ने सभी पर अपना कब्जा किया होगा।
जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह किताब कचारगढ़ पर केंद्रित है, जहां जाने का विचार 1980 में किया गया। सह लेखक सुन्हेरसिंह ताराम के मुताबिक, उनके अलावा बी. एल. कोर्राम, के. बी. मर्सकोला और मोतीरावण कंगाली इस यात्रा में शामिल थे। वहां की गुफा में पारी कुपार लिंगों से संबंधित स्थान की पुष्टि होने के बाद 1984 में जत्रा (धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजन) की शुरुआत हुई। हालांकि तब केवल 5 लोग ही इस जत्रा में शामिल हुए। परंतु, अब यहां हर साल बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है और लोग गोंड संस्कृति और परंपराओं के संबंध में विचार-विमर्श करते हैं।
यह भी पढ़ें – महिषासुर विमर्श : गोंड आदिवासी दर्शन और बहुजन संस्कृति
हालांकि यह किताब विस्तृत गोंड संस्कृति और परंपरा के एक सीमित आयाम को ही सामने लाती है। यह किताब लेखकों, अध्येताओं व शोधार्थियों के लिए आधार ग्रंथ बन जाती यदि इसमें गोंडी पूनेम दर्शन का और विस्तार होता। साथ ही गोंड तीज-त्यौहारों का उल्लेख भी होता तो इसकी उपयोगिता और सार्थक होती।
बहरहाल, यह किताब उन अध्येताओं के लिए उपयोगी साबित होगी जो गोंड भाषा नहीं जानते हैं। दोनों लेखकों ने अनेकानेक गोंड भाषा के शब्दों का अनुवाद हिंदी में किया है। परंपराओं और मान्यताओं की प्रस्तुति एक कथावाचक के जैसे की गई है जो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि घर के बड़े-बुजुर्ग कहानियां सुनाते हैं। इसलिए इस किताब में रोचकता भी है। इन सबसे बढ़कर इस किताब में वे सूत्र सूचनाएं हैं जिनके आधार शोधार्थी भारतीय संस्कृति से जुड़े मूल सवालों पर शोध कर सकते हैं। इनमें छठे परिशिष्ट में उल्लेखित उन प्रकाशित किताबों की सूची है जो गोंडी भाषा और संस्कृति से संबंधित हैं। इसके अलावा तीसरे परिशिष्ट में गोंडवाना महासभा अधिवेशन के आयोजनों की जानकारी है जो वर्ष 1930 से शुरू हुई। इसी में गोंड महासभा का संविधान का उल्लेख है। इसके एक नियम के मुताबिक आदिवासी गोंड प्रकृति को देवी-देवता मानने वाले, नि:सर्ग को अपना आराध्य मानने वाले अहिन्दू हैं।
समीक्षित पुस्तक : गोंडवाना में कचारगढ़ पवित्र भूमि
लेखकद्वय : उषाकिरण आत्राम व गोंडवाना रत्न सुन्हेरसिंह ताराम
प्रकाशक : वैभव प्रकाशन, रायपुर (छत्तीसगढ़)
कुल पृष्ठ : 120
मूल्य : 100 रुपए
(संपादन : गोल्डी/सिद्धार्थ)