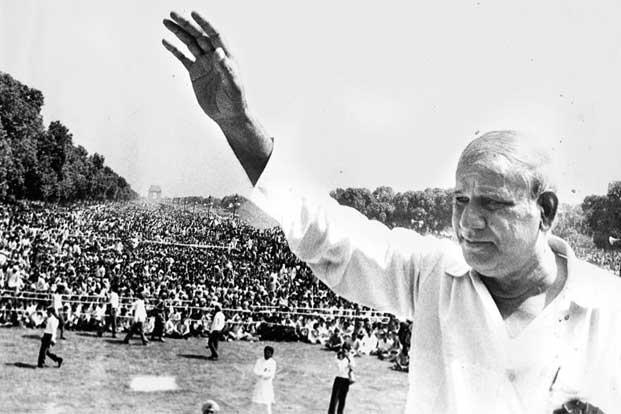सामान्य तौर पर जब हम फिल्म और फिल्म में महिला पात्रों पर चर्चा करते हैं तो हम निश्चित तौर पर बहुत कम फिल्में ही ऐसी पाते हैं, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि उनमें महिला पात्रों के साथ फिल्मकार ने न्याय किया है। अधिकांश फीचर फिल्मों में महिलाएं केवल “फिलर” के रूप में ही उपयोग की जाती हैं। यहां तक कि नायिका प्रधान फिल्मों में भी महिला पात्रों की भूमिका इस रूप में होती है कि उन्हें भारत का पुरूष समाज आसानी से निगल सके। लेकिन यह सुखद है कि इस तरह का दोहरा चरित्र फीचर फिल्मों तक ही सीमित है। फीचर फिल्मों के इतर हाल के वर्षों में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में नये प्रयोग हुए हैं। इन्हें नेट फ्लिक्स और यूट्यूब जैसे मंचों ने लोकप्रियता दी है। इन मंचों के जरिए युवा अनेकानेक प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही एक युवा फिल्मकार हैं निरंजन कुजूर। इनकी एक फिल्म “दीबी दुरगा” बहुत खास है। खास इसलिए कि इस में आदिवासी महिलाओं के जीवन के तमाम आयाम अपने-आप सामने आते हैं।
करीब पांच मिनट की इस फिल्म/म्यूजिक वीडियो पर चर्चा से पहले यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि जातिगत व नस्लगत भेदभाव के जितने मानदंड पुरूषों के लिए हैं, उससे अधिक महिलाओं के लिए होते हैं। मसलन, महिला चाहे वह उच्च जाति की हो या आदिवासी-दलित-ओबीसी परिवार की, उन्हें हर हाल में सहना ही पड़ता है। लेकिन हम अपनी ही दुख में इतने भींगे होते हैं कि अन्य किसी के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। हम यह कभी महसूस ही नहीं कर पाते हैं कि सुदूर जंगलों में रहने वाली आदिवासी स्त्रियां किस तरह के दुख झेलती हैं और यह भी कि नवउदावादी अर्थव्यवस्था ने उनके जीवन में किस तरह का जहर घोला है।
इस फिल्म के कहानीकार और निर्देशक निरंजन कुजूर हैं। केंद्रीय आदिवासी महिला पात्र की भूमिका में पोईरानी बासकी ने अभिनय से प्रभावित किया है। जबकि पारंपरिक दसईं गीत काे गाया है श्रीमंती हेम्ब्रम ने। फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसका वीडियो है जिसे स्टैंले मुद्दा ने रिकार्ड किया है। जबकि साउंड की रिकार्डिंग मंजूल टोप्पो ने की है।

फिल्म में पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले की आदिवासी स्त्रियों की जनजातीय दिनचर्या को बेहद बारीकी से दर्शाया गया है। फिल्म निर्देशक निरंजन कुजूर द्वारा निर्देशित इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना मिल चुकी है। इतना ही नहीं, वर्ष 2019 में इसे बांगलादेश की राजधानी ढाका में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित भी किया गया। वहीं वर्ष 2019 में भोपाल में आयोजित प्रथम आदिवासी फिल्म महोत्सव के अलावा इसे इसी वर्ष मलेशिया में आयोजित विश्व आदिवासी फिल्म महोत्सव में भी चयनित किया गया।
फिल्म “दीबी दुरगा” की स्टोरी लाइन सचमुच अनोखी है। मतलब यह कि वीडियो में नजर आने वाला दृश्य कुछ और आवाज कुछ और। दोनों में प्रत्यक्ष तौर पर कोई संबंध नहीं। फिल्म शुरू ही होती है एक अधेड़ उम्र की महिला के नींद खुलने से। शुरू का यह दृश्य हिंदी साहित्य में सौंदर्य के तत्व तलाशने वालों के लिए एक नजीर है। आंखें मींचती हुई हुर्ह एक स्त्री की तस्वीर दर्पण में किस तरीके का इफेक्ट पैदा कर सकती है, यह इस फिल्म में देखा जा सकता है। इसके पहले कि आगे फिल्म के अगले हिस्से की बात करें, यह जानना बेहद दिलचस्प है कि फिल्म की अवधि एक गीत की अवधि के बराबर है। मतलब फिल्म की शुरुआत ही गीत से होती है और अंत भी गीत के साथ ही। जैसे वीडियो और ऑडियो नदी के दो किनारे हों, जो चलते तो साथ-साथ हैं परंतु मिलते कभी नहीं हैं।
संथाली बोली में यह गीत “दसईं गीत” है। इस गीत में आदिवासी महिला अपनी दो बेटियों दीबी और दुरगा को याद करती है जो अब उसके पास नहीं है। गीत से यह तो स्पष्ट नहीं होता है कि दोनों कहां गयीं हैं? क्या वह जंगल में गुम हो गयी हैं या फिर शहरों से आने वाली हवाओं ने उनका शिकार कर लिया है। फिल्म के हर फ्रेम में नजर आने वाली महिला भी नहीं जानती है। लेकिन वह उम्मीद करती है कि उसकी बेटियां अच्छा जीवन देखने-समझने गयी हैं। गीत में वह इसकी भी अभिव्यक्ति करती है कि जो सुख उसने स्वयं नहीं हासिल किये हैं, उन्हें वे यानी उसकी बेटियां जरूर हासिल करे।

इस छोटी सी फिल्म में निर्देशक ने न केवल पितृसत्ता पर करारी चोट की है बल्कि इस विडम्बना पूर्ण सत्य को भी उद्घाटित किया है कि जिस आदिवासी संस्कृति में महिलाओं को श्रम की दृष्टि से सशक्त और स्वतंत्र माना जाता है, वहां भी वे न केवल पितृसत्ता की शिकार हैं बल्कि उनके साथ होने वाले जुल्म और अत्याचार के प्रति भी कोई आवाज नहीं उठती। यहां स्वरुप रानी की कविता की ये पंक्तिया बेहद सटीक जान पड़ती हैं :
अरे हाँ !
अपनी जिंदगी को मैंने
जिया कब?
घर में पुरुष अहंकार
एक गाल पे थप्पड़ मारता है
तो गली में वर्ण आधिपत्य
दूसरे गाल पर चोट करता है।
इस वीडियो में केवल महिला है जो अपनी बेटियों को दिन भर खोजती है, पुकारती है, उनके बारे में सोच-सोच कर रोती है। किन्तु किसी से कुछ नहीं कहती। उसका ये रुदन भी केवल गीत के माध्यम से ही दीखता है। फिल्म में कहीं उसे रोते हुए नहीं देखा जा सकता। फिल्म में पिता को कहीं भी चिंतित नहीं दिखाया गया। पति-पत्नी के बीच किसी प्रकार का संवाद भी नहीं है। वह सबके पास होते हुए भी अकेली है। एकदम निपट अकेली। जंगल से लकड़ियां लेकर लौटते हुए रास्तें में एक टीले पर बैठ वह अपने एकाकीपन की पराकाष्टा को प्राप्त कर लेती है जब उसके सामने पहाड़ सी ऊंची चुनौतियां हैं और अनंत तक विस्तृत आसमान। कुछ देर विचार मग्न हो उठती है और घर की ओर चल पड़ती है। मानों उस जंगल और घर के बीच यही ‘टीला’ उसका अपना है।
दरअसल फिल्म के जरिए निरंजन कुजूर ने आदिवासी इलाकों में होने वाली चाइल्ड ट्रैफिकिंग को दिखाने की कोशिश की है। मसलन, फिल्म की नायिका अपनी दो बेटियों के साथ दो अन्य बच्चियों आइनोम और काजल को भी याद करती है। उनके लिए भी वह सुखद कामनाएं कर रही है। फिल्म की खूबसूरती भी यही है कि जहां एक ओर वह अपनी बेटियों के लिए सुखद जीवन की कामना कर रही है, अपने दैनिक जीवन में हाड़तोड़ मेहनत कर रही है। इनारा यानी कुंए से पानी भरने से लेकर देर रात बिस्तर पर पति के जबरिया हमले को झेलने के बाद खुद को नींद के हवाले करने के पहले तक के हर दृश्य को बड़ी ही खूबसूरती से निरंजन ने दिखाया है।
यहाँ संताली कवयित्री निर्मला पुतुल की कविता की पंक्तिया बेहद प्रासंगिक लग रही हैं :
मैं इलाके की उन गुम हो गई
लड़कियों को ढूंढना चाहती हूँ।
समझना चाहती हूँ उनके जीवन
और दिनचर्या का गणित।
देखना चाहती हूँ उनके भीतर
कितना बचा है झारखण्ड।
कितनी बची है उनकी भाषा में
संताल परगना … और …
गाँव, घर वापस लौटने की
गुंजाइश बची है, उनकी आँखों में
या नहीं।
देखना चाहती हूँ मैं।
दरअसल इस फिल्म में दर्शायी गई कहानी किसी एक ग्रामीण आदिवासी इलाके की स्त्रियों की कहानी नहीं है, बल्कि ये फिल्म बहुत संक्षेप में उन सब दलित, उपेक्षित, आदिवासी, अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों या इलाकों में होने वाली ‘चाइल्ड ट्रैफिकिंग’ (बाल देह व्यापार) बलात्कार और न जाने कितने ही खौफनाक अपराधों को सामने लाती है। इन्हें न तो पुलिस के थानों में दर्ज किया जाता है और न ही सरकार नामक कोई व्यवस्था हस्तक्षेप करती दिखती है।
(संपादन : नवल)