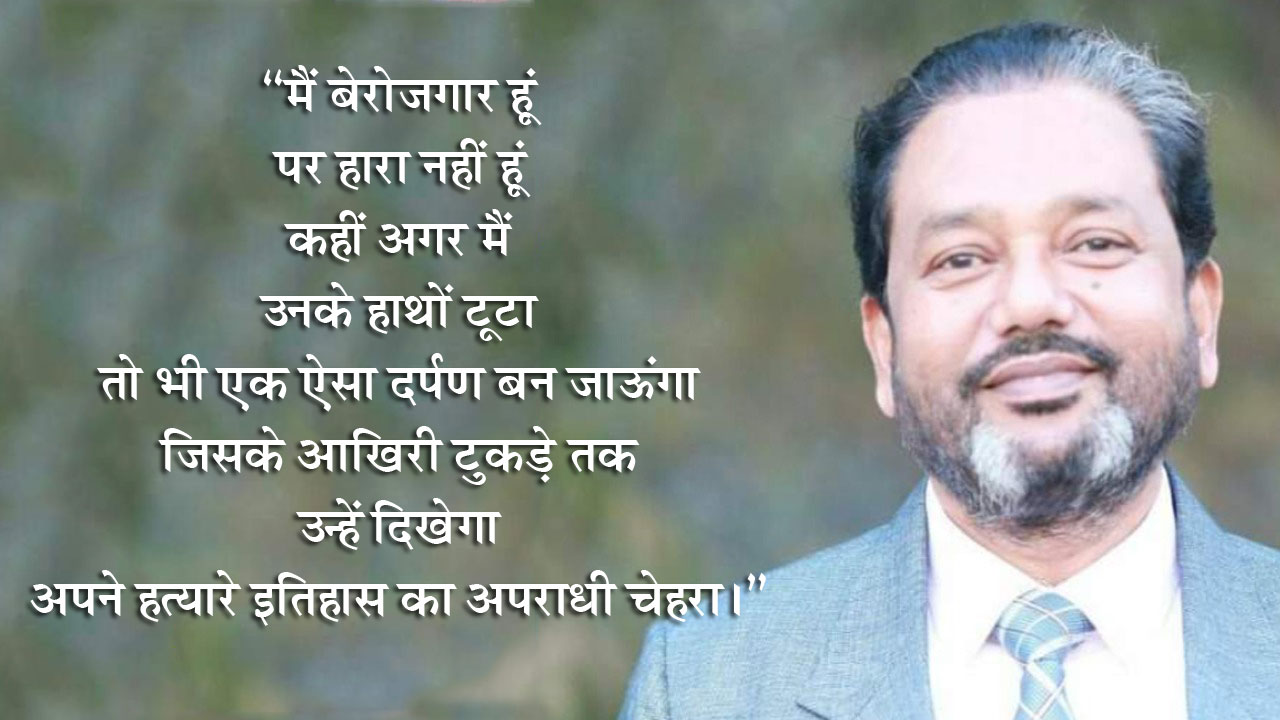दूसरा भाग
उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ से ही भारत की शूद्र जातियों में उच्च जातियों से अपनी उत्पत्ति खोजने की कवायद शुरु हो गई थी। आदि हिन्दू, आदि द्रविड़ और मूलनिवासी आन्दोलन के भी पहले उनमें ब्राह्मण और क्षत्रिय से अपनी उत्पत्ति के आन्दोलन शुरु हो गए थे। हिन्दू समाज की बहुत सी शूद्र और अतिशूद्र जातियों ने अपनी नई अस्मिता के लिए अपने ब्राह्मण और क्षत्रिय गोत्र ढूंढ़ लिए थे। बंगाल में चण्डाल अपना नामकरण नमोशूद्र कर रहे थे, और अपने को ब्राह्मण गोत्र का मान रहे थे। उत्तर प्रदेश में अहीर और चमार जातियों ने भी अपनी मूल उत्पत्ति क्षत्रिय और ब्राह्मण से खोज ली थी, और उसका इतिहास भी उन्होंने लिख डाला था। इसका एक बड़ा कारण ब्राह्मणों के वे शास्त्र भी हैं, जिनमें अनुलोम-प्रतिलोम वर्णसंकर के रूप में शूद्र-अतिशूद्र जातियों की उत्पत्ति का मिथ्या विधान रचा गया है। इसलिए, काशीप्रसाद जायसवालजी की कलवार जाति के द्विजातीयकरण के पक्ष में दी गई सम्मति को समझना होगा।
वर्ष 1927 में कलवार जातीय सभा का अधिवेशन जबलपुर में हुआ था। उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा कलवार जाति की उत्पत्ति के संबंध में निर्णय लेने का था। मोतिहारी, बिहार अधिवेशन में जायसवालजी ने वैश्य उत्पत्ति के पक्ष में अपनी सहमति दी थी, जिसके कारण स्वजातीय लोगों में तनाव पैदा हो गया था[1], क्योंकि वे क्षत्रिय से नीचे पदक्रम में जाने को तैयार नहीं थे। इस विवाद के बारे में जिज्ञासुजी की निम्न टिप्पणी से पता चलता है, जो उन्होंने ‘कलवार केसरी’ (आश्विन शुक्ल, संवत 1981, अर्थात जुलाई 1924) में लिखी थी –
“भगवन! जब से आपने मोतिहारी के भाषण में कहा है कि हम लोग वैश्य हैं, जहां तक ज्ञात हुआ है, तभी से जाति में एक ऐसा दल बन गया, जो अपने को वैश्य ही होना चाहता है। वैश्वत्व के विचार लोगों में पहले से भी थे, पर आपके भाषण उनको उत्तेजना अवश्य मिली और वे हिम्मत करके खुल्लम-खुल्ला अपने पक्ष का समर्थन करने लगे हैं। आपसे यह भी छिपा नहीं है कि जाति में एक बहुत बड़ा भाग ऐसा भी है, जो अन्त तक अपने को क्षत्रिय ही कहने पर तुला हुआ है। गत वर्ष की महासभा में जाति इसी झगड़े में पड़कर दो भिन्न-भिन्न दलों में विभक्त हुआ चाहती थी। पर बहुत यत्न से छह महीने का समय देकर जाति को दो दलों में विभक्त होने से बचाया गया। अब आगामी वर्ष के सम्मेलन में फिर वही प्रश्न सामने हैं। आपने कृपा करके जो व्यवस्था दिलाई, उससे यह सिद्ध हो गया है कि यह जाति उत्पत्ति से क्षत्रिय है और वैश्यवृत्ति द्वारा अपना निर्वाह करती है। अब आप कृपा करके अपनी निज की स्पष्ट सम्मति भी प्रकाशित कर दीजिए कि क्या इस जाति को अपनी उतपत्ति को बलवान मानकर क्षत्रिय नाम से अपना परिचय देना चाहिए अथवा कर्म को प्रधनता देकर अपने को वैश्य कहना चाहिए। जाति के लाखों मनुष्य आपके श्रीमुख की ओर टकटकी लगाए निहार रहे हैं, अतएव आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप कृपा करके जो पक्ष श्रेयष्कर हो, उसकी घोषणा कर दीजिए। आप जैसे सर्वविद् विद्वान से और अधिक क्या निवेदन किया जाए।”[2]

इस विवाद का शमन 1927 के जबलपुर सम्मेलन में हुआ, जिसके वे सभापति बनाए गए थे। इस सम्मेलन में उनकी सहमति से कलवार जाति-संगठन का नामकरण ‘अखिल भारतीय हैहय क्षत्रिय महासभा’ के रूप में हुआ। जिज्ञासुजी ने रांची के व्याख्यान में कहा था कि हैहय क्षत्रियों का संघर्ष भृगुओं के साथ हुआ था, और भृगु वंशीय परशुराम ने 21 बार हैहय क्षत्रियों का नाश किया था। इस पर जिज्ञासुजी के अनुसार, जायसवालजी ने हैहय क्षत्रियों को महाप्रतापी और तेजस्वी बताया था। लेकिन इस सम्मेलन में जायसवालजी ने जो व्याख्यान दिया था, उसमें वे जाति के उन्मूलन का पक्ष लेते हैं। इस दृष्टि से यह व्याख्यान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उन्होंने जाति की प्रशंसा नहीं की, बल्कि उसे निरर्थक बताया है। वे कलवार जाति के द्विजातीयकरण का भी समर्थन नहीं करते हैं। उनका जोर इस बात था कि अब वह दिन दूर नहीं, जब जाति की सभाओं की जरूरत न रह जायेगी। उन्होंने कहा कि जाति की संस्था उठा देने के कानून बन रहे हैं, और वे ऐसे कानूनों के पक्ष में हैं।[3] हिन्दू शास्त्रों में कहा गया है कि जाति को ईश्वर ने बनाया है। किन्तु जायसवालजी ने जोर देकर कहा कि जाति मनुष्यकृत है, ईश्वरकृत नहीं।[4] उनका कहना था कि मनुष्य ने जाति बनाई है, और वह जब उसकी जरूरत न समझे, उसे खत्म कर सकता है। उनका विश्वास था कि सभी देशों में आरंभ में जातियां होती हैं, जापान में जातियां थीं, अरब में जातियां थीं, पर सभ्यता और ज्ञान के प्रसार के साथ वहां जातियां टूट गईं। किन्तु उन्हें इस बात का दुख था कि ‘भारत में हिन्दुओं ने बहुत बातों में उन्नति की, पर जाति अभी तक नहीं तोड़ी।’[5]
यह भी पढ़ें : काशीप्रसाद जायसवाल को जैसा मैंने पढ़ा (पहला भाग)
उन्होंने भारत को एक बीमार देश कहा, जिसने जातियों को बनाए रखा हुआ है। इसलिए उन्होंने जोर देकर कहा कि ‘जब तक जातियां हैं, तभी तक जाति-सभाओं की सार्थकता है।’ वे आशावादी थे, और मानते थे कि जातियां जल्दी समाप्त हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने जाति-भाइयों को अपने संबोधन में कहा था कि ‘हम लोग जाति को अमर मानने की भूल कभी न करें। हमें जाति और जातीय सभाओं को अस्थाई मानकर उनकी सेवा करें।’[6]
उन्होंने अपने जाति-भाइयों की इस समस्या के संबंध में कि उनकी उत्पत्ति किस वर्ण से हुई है, और वे स्वयं को क्षत्रिय कहें या वैश्य, बहुत ही रोचक बात कही: ‘भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों को क्षत्रियों से निकला बतलाया और ब्राह्मणों ने अपने को ब्रह्मा के मुख से। न ब्राह्मणों की यह उत्पत्ति दूसरों ने मानी, और न दूसरों की उत्पत्ति ब्राह्मणों ने मानी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बाहर और उपर हब्शी, यूनानी, यहूदी, चीनी, जापानी निकले, जिनसे साबित हुआ कि पुरुष सूक्त की कही मनुष्य जाति का चातुर्यवर्ण बेचारा नर समुद्र का कूपमण्डूप ही ठहरा।’[7] जायसवालजी ने वर्ण-मोह से ग्रस्त व्यक्ति को कुंए के मेढक की संज्ञा दी, जो सदा कुंए के अंधेरे में रहता है, और बाहर की दुनिया को नहीं जानता। उनका विचार था कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से वर्णाश्रम अर्थात्, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति हुई है, तो भारत के बाहर के देशों में जो इनसे भी उच्च और श्रेष् मनुष्य- यहूदी, यूनानी, चीनी, जापानी जाति रहती है, उसकी उत्पत्ति तो किसी वर्ण से नहीं हुई। फिर क्या वे नीच हैं? इस आधार पर वे वर्ण की आवश्यकता को नकार रहे थे।
इसके बाद, जायसवालजी ने चातुर्यवर्ण की व्यवस्था को वर्ण के आधार पर ही निरर्थक साबित करते हुए यह महत्वपूर्ण बात कही-
‘चातुर्यवर्ण का इतिहास ऐसा नहीं है कि उसको नितांत अटल समझा जाए। पतंजलि-व्याकरण-भाष्यकार ने, जो चन्द्रगुप्त के मौर्य वंश के बाद और पुष्यमित्र शुंग के राज्य में कोई 130 वर्ष विक्रम संवत से पहले हुए, लिखा है कि उनके समय में ब्राह्मण गोरे रंग वाले और चमकते भूरे केश वाले, अर्थात अंग्रेजों के समान रंग वाले होते थे; गौररू पिंगलरू कपिलेश:। पर, ये चिह्न अब बहुत कम मिलते हैं। इसी तरह एक ब्राह्मण ग्रन्थ ने वैश्यों को श्वेत और क्षत्रियों को लाल, अर्थात् जैसे अंग्रेजों में लाल रंग वाले वेल्श होते हैं, कहा है, पर ये चिह्न अब नहीं मिलते। अश्वघोष नामक बड़े ब्राह्मण पंडित ने जो पाटलिपुत्र के आसपास का रहने वाला था, शक संवत के आसपास हुआ, कहा कि वर्ण की बात थोथी है, क्योंकि उसके देखने में शूद्र ब्राह्मणों के समान दिख पड़े। ऐसी अवस्था में चातुर्यवर्ण को एक पक्का सिद्धांत मानना और उसे एक पक्की चीज मान उत्पत्ति खोजना बिल्कुल व्यर्थ परिश्रम है। ईश्वर का नियम है कि मनुष्य मात्र, जो एक जगह में रहें एक हैं, फिर किसी चयन से कोई उन्हें चार कोटियों या कोठरियों में विभक्त नहीं कर सकता, वे एक ही होंगे।’
इतना स्पष्ट है कि जायसवालजी कलवार जाति की उत्पत्ति खोजने अथवा जाति के द्विजातीयकरण के पक्ष में नहीं थे। कलवार जाति को वैश्य या क्षत्रिय वर्ण से जोड़ने का कार्य जायसवालजी ने किया था, जैसाकि जिज्ञासुजी का मत है, वरन, जायसवालजी ने सम्मेलन में यह मत व्यक्त किया था कि ‘ऐसी दशा होते हुए भी यदि हिन्दू जाति की कोई उपजाति ढूंढ़े और उत्पत्ति कायम करे, तो वह उत्पत्ति नाम मात्र की है। ऐसी उत्पत्ति सभी की है और यदि उस कोटि की उत्पत्ति का विवरण आप चाहते हैं, तो उसे मेरे मित्र बाबू नारायण चन्द्र शाह ने अपनी किताब में दिया है। और उससे भी अच्छा विवरण व्यवस्थापत्र में, जिसे सोमवंशीय क्षत्रिय सभा अलवर ने छापा है, दिया हुआ है। इसका पोषण महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्राी ने, जो हिन्दुस्तान के सबसे बड़े ऐतिहासिक पंडित हैं, किया है। इसका अभिप्राय यह है कि जन्म से हम क्षत्रिय और कर्म से वैश्य हमारा उत्पत्ति-इतिहास है।’[8] मतलब साफ है कि जायसवालजी ने अन्य विद्वानों के मतों के आधार पर अपना अभिप्राय व्यक्त किया था, कलवार जाति की उत्पत्ति की खोज नहीं की थी। उन्होंने रायबहादुर हीरालाल साहब के इस मत को भी स्वीकार किया कि मध्यकाल में कलवार जाति के बहुत से राजा हुए हैं, पर इस अवसर पर उन्होंने महत्वपूर्ण बात यह कही कि ‘बीती ताहि बिसारि दे, आगे की सुध् लेय’।[9] अतीत रहा होगा शानदार, पर वर्तमान शानदार नहीं है। उन्होंने कहा कि जरूरत शिक्षित होकर वर्तमान को सुधारने की है। शिक्षा भी कौन सी? अंग्रेजी की, संस्कृत की नहीं। देखिए वे कितनी महत्वपूर्ण बात कहते हैं-
‘उन्नति की जड़ शिक्षा है और शिक्षाओं में राज-शिक्षा का आदर सब देश, सब काल में अधिक रहा हैं, और रहेगा। इसमें जो चुकता है, पिछड़ता है। मुसलमानी राज्य में कायस्थों ने मध्य हिन्दुस्तान में और ब्राह्मणों ने बंगाल में राज-भाषा और राज-शिक्षा को पकड़ा, जिससे आज भी वे आगे हैं। जो अंग्रेजी शिक्षा का आज तिरस्कार करेगा, पिछड़ा ही रहेगा, और पददलित रहेगा। अंग्रेजी शिक्षा वस्तुतः यूरोपीय शिक्षा है। जैसाकि एक बार महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्राी ने संस्कृत शिक्षा के तारतम्य में कहा है, अंग्रेजी आंख खोलने वाली है और संस्कृत शिक्षा आंख मूंदने वाली है। संस्कृत उतने ही जानने की जरूरत है कि शास्त्र दूसरे के द्वारा न जानना पड़े। पर उसे साम्प्रत मरहलों (आज के मसलों) को तय करने वाला कोई न समझे। जो विद्या 10 हजार या 5 हजार वर्ष पहले ठीक थी, वह आज काम नहीं दे सकती। दुनिया आगे चलती है, आप भी आगे चलें।’[10]
काशीप्रसाद जायसवाल ने एक और महत्वपूर्ण बात यह कही कि जाति के लोग अलग छात्रावास और अलग स्कूल-कालेज खोलने की भूल न करें। उनका मत था कि जो सबके लिए संस्थाएं मौजूद हैं, उनसे ही काम लेना चाहिए, नही तो कट कर अलग होने के बुरे परिणाम भी होंगे, और व्यर्थ का खर्चा भी होगा।[11] अगर हम डाॅ. आंबेडकर के विचारों से तुलना करें, तो तरक्की के लिए अंग्रेजी भाषा सीखने के विचार दोनों के समान हैं, परन्तु अलग छात्रावास और स्कूल-कालेज खोलने के विचार में भिन्नता नजर आती है। डाॅ. आंबेडकर ने अछूतों के लिए न केवल अलग छात्रावास खोले थे, वरन् दलित वर्गों की शैक्षणिक उन्नति के लिए कालेजों की स्थापना भी की थी, जो आज भी दलित वर्गों की शिक्षा के महान केन्द्र हैं। अलग संस्थाएं कायम करने के संबंध में, आंबेडकर और जायसवाल के विचारों की भिन्नता का कारण अस्पृश्यता थी, जिसके कारण दलित वर्गों का न केवल हिन्दुओं के स्कूलों में प्रवेश वर्जित था, बल्कि सरकारी स्कूलों में भी सवर्ण हिन्दू उनके प्रवेश में बाधाएं डालते थे। इसलिए उनकी शैक्षणिक उन्नति के लिए अलग स्कूलों और छात्रावासों की आवश्यकता थी। किन्तु कलवार जाति अछूत जाति नहीं थी, और सार्वजनिक स्कूल-कालेजों में उनके प्रवेश पर हिन्दुओं को आपत्ति नहीं थी।
काशीप्रसाद जायसवाल ने अपने व्याख्यान में बिरादरी के लोगों को कुरीतियां छोड़कर कुछ सुरीतियांअपनाने की सलाह दी, जिसमें पंच-पंचायत की आज्ञा मानना, जाति-भाई की सेवा करना, अमीर-गरीब भाई को बराबर समझना, पंचों के सामने विवाह या नियोग करना, दहेज न लेना, और नौकरी न करके छोटा-मोटा रोजगार करना मुख्य थीं। उन्होंने द्विज बनने के फेर में न पड़ने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा करना घृणित काम करना है।[12] उन्होंने अन्त में बिरादरी के लोगों से दो वचन भरवाए: पहला, यह कि सब वर्गों के जाति-भाई परस्पर कच्ची रसोई खाना शुरु कर दें, और दूसरा यह कि ‘आप सब वर्गों के जाति-भाई परस्पर बेटी-विवाह आरम्भ कर दें, इसमें आनाकानी न करें।’ इसे उन्होंने जाति-उन्नति का अच्छा अवसर बताया।[13]
जायसवाल का इतिहास–बोध
क्या काशीप्रसाद जायसवाल के इतिहास-बोध की पृष्ठभूमि में उनका हिन्दू दृष्टिकोण है? प्रोफेसर डा. रतनलाल ने ‘काशीप्रसाद जायसवाल संचयन’, (खण्ड-2) की भूमिका में लिखा है कि जायसवाल की शब्दावली ज्यादातर हिन्दू परम्पराओं से आती है। उनके मुहावरे, प्रेरणाएं और दृष्टान्त सब हिन्दू-शास्त्राीय ग्रन्थों से लिए गए हैं। वे आर्य-हिन्दू में कोई अंतर नहीं करते और राम उनके आदर्श नायक हैं।[14] इसका कारण यह है कि जायसवाल जिस नवजागरण काल में हुए, वह काल हिन्दुत्व के उत्थान का काल भी था। मैथिलीशरण गुप्त, रवीन्द्रनाथ टैगोर, महावीरप्रसाद द्विवेदी, रामचन्द्र शुक्ल, अयोध्यासिंह ‘हरिऔध’, राय कृष्णदास उनके समकालीन ही नहीं, उनके संगी-साथी भी थे। इन मित्रों के बीच उनका उठना-बैठना था। ये लोग, जो सभी द्विजातीय संस्कारों से ग्रस्त थे, जब मिलते होंगे, तो शायद ही जाति-व्यवस्था और अमीरी-गरीबी पर परस्पर चर्चा करते होंगे! जायसवाल धनाढ्य व्यापारी पिता के पुत्र थे। जब वे विलायत पढ़ने गए थे, तो अपना रसोइया साथ लेकर गए थे, और विलायत में किराए के फ्लैट में रहे थे। इससे उनकी संपन्नता को समझा जा सकता है। उन्हें हिन्दुत्व से जोड़ने के लिए ये मुख्य कारक हो सकते हैं। इसके बावजूद, उनकी सोच संकीर्णता के दायरे में नहीं गई थी। वे हिन्दू धर्म से प्रभावित नहीं थे, बल्कि उसमें पैदा हुए थे। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि जायसवालजी विलायत में कुछ क्रान्तिकारियों के सम्पर्क में भी आए थे, और यह भी सब जानते हैं कि वे राहुल की विचारधारा के सम्पर्क में भी आजीवन रहे थे। संभवतः इस प्रभाव ने उनके विचारक और लेखक को संकीर्ण होने से रोका हो। धर्म, दर्शन और इतिहास पर उनका अध्ययन और ज्ञान निस्सन्देह विशाल था। पर, उनकी इस विचार-यात्रा में हमें उनका समाजवादी चिन्तन भी दृष्टिगोचर होता है।
जायसवालजी ने ‘पाटलिपुत्र’ में, जिसके वे संपादक थे, सात किश्तों में ‘हिन्दू-राज्यशास्त्र’ एक लेखमाला लिखी थी। पहला लेख ‘पाटलिपुत्र’ में 15 अगस्त 1914 को और अन्तिम सातवां लेख 17 सितम्बर 1914 के अंक में छपा था। पहले लेख में उन्होंने लिखा – “प्राचीन समाज में सबसे महत्वपूर्ण तंत्र समिति-तंत्र था। समिति को बहुत सी संस्थाओं की माता कह सकते हैं। वेदों के समय जनसमूह को ‘विश:’ कहते थे। ये विश जनों में विभक्त थे। ये जन जब सार्वजनिक बातों पर विचार करने के लिए एकत्र होते थे, तो उसे समिति कहते थे। समिति से बहुत छोटी कोई 10-15 विशों की एक दूसरी संस्था थी, जिसे सभा के नाम से पुकारते थे। जन (विश) शुरू में पांच थे, जो समिष्ट रूप से ‘पंचजनाः’ कहलाते थे। पंचजनाः के समिति-तंत्र की सुध् ‘पंचायत’ के नाम से अब तक चली आ रही है। पंचायती प्रथा यहां इतनी ही पुरानी है, जितनी कि हमारी हिन्दू जाति है या यों कहिए कि वह वेद सी अनादि है।”[15] यहां वेद को अनादि बताना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ‘पंचायत’ को अनादि बताना महत्वपूर्ण है, जिससे वेदपूर्व जनजातीय समाज की समिति-तन्त्र का पता चलता है। दूसरे लेख में, जो गणतन्त्र पर है, लिखा है: “बौद्ध धर्म के जोर पकड़ने के पहले गणों का पुराना नाम संघ था। बुद्ध भगवान ने लिच्छवी (जिसे मनुस्मृति में निच्छवी कहा है) गणराज्य की संस्था के अनुकरण पर अपना भिक्षु संघ बनाया था। संघ शब्द बौद्ध भिक्षुओं के तन्त्र का द्योतक हो जाने पर, संघ तंत्र का नाम गणतंत्र रक्खा गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में संघवृत नामक अध्याय में इन्हीं गणतंत्रों का वर्णन है। पतंजलि के समय तक ‘संघ’ मुख्यतः गणतंत्र के ही अर्थ में समझा जाता था।”[16]
जायसवाल ने लिखा कि बुद्ध के समय में गोरखपुर, बस्ती और मुजफ्फरपुर के उत्तर मल्ल, लिच्छवी आदि के गणतंत्र थे, जो संसारोपरत बुद्धदेव को बहुत प्रिय थे। काठियावाड़ गुजरात में यादवों का तंत्र बहुत पुराना था, जिन्हें वे स्वराज्य या स्वराष्ट्र कहते थे।[17] सुराष्ट्र और सूरत नाम इन्हीं से निकले हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र, बौद्धसूत्र और महाभारत के गणों के विषय में सात बातें बताईं- (1) गणमात्र शासक समझे जाते थे, इससे सबके सब ‘राजनरू’ कहलाते थे। इनके सिक्कों पर किसी एक आदमी का नाम नहीं, वरन गणमात्र का नाम होता था। (2) गणों के लोग मुखिया होते थे। राजकार्य ये ही लोग करते थे। किसी-किसी गण में कुछ कुल होते थे, जिनके लोग राजा की उपाधि धारण करते थे। ये तंत्र कुलीन थे। (3) गणों का राज्यकोष भरा रहता था। (4) गणमात्र में बराबरी थी, कोई उंचा-नीचा न था। (5) राज्य के सारे मन्त्र (मसले) गणमात्र की समिति और परिषदों में निश्चित होते थे। बुद्ध ने कहा था कि जब तक वृज्जी समितियों की बैठकें बराबर जारी रखेंगे, तब तक वे अजेय रहेंगे। (6) कानून और न्याय का प्रबंध बहुत अच्छा रहा करता था। और, (7) अपना बल बढ़ाने को कई गण मिलकर संघात (संधि) बना लेते थे, जो दुर्भेद्ध समझे जाते थे।[18]
लेकिन जायसवाल के अनुसार, “यहां के राजनीतिज्ञों को ये छोटे-छोटे तंत्र पसन्द न आए। ये वीर तो थे, पर छोटे होने के कारण निर्बल थे। कौटिल्य ने इनकी निर्बलता सिकन्दर के सामने देखी। इसलिए एक के बाद दूसरे ये तंत्र, जिन्हें ग्रीक लोगों ने ‘स्वतंत्र अभिजन’ लिखा है, अपना और देश का स्वातन्त्रय गवां बैठे। इसलिए कौटिल्य ने उनके निराकरण करने और उनकी भूमि साम्राज्य में मिला लेने की नीति निर्धारित की। इस नीति के तहत धीरे-धीरे इनका लोप हो गया, पर विक्रम से कोई 300 वर्ष पीछे तक मालवों का तंत्र बना हुआ था।”[19]
हालांकि ये तंत्र भी अलग-अलग स्वतंत्र अभिजन थे, इसलिए ये भी अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रख सके। जायसवाल ने तीसरे लेख में राजा के चुनाव, चौथे लेख में हिन्दू राजा की उच्छृखलता पर रुकावटें, पांचवें लेख में हिन्दू राजा के कर्तव्य और अधिकार का वर्णन किया है। छठे लेख में उन्होंने हिन्दू जाति के बारे में कतिपय यूरोपीय विद्वानों के मतों का खंडन किया है कि हिन्दू जाति पारमार्थिक पशुओं का झुंड न थी। वे राजनीतिक लोक थे। इस लेख में उन्होंने हिन्दुओं की राजनीतिक उन्नति की सीमा पर विचार किया है। उन्होंने लिखा कि हिन्दू राज्यशास्त्र के विचारों में बहुत कुछ उन्नति हुई, किन्तु कारणवश बहुत कुछ बाकी रह गया। ग्रीक लोग गणतंत्र के आगे न बढ़ सके और यहां राजतंत्र और उससे बढ़कर साम्राज्य (एकराट्) की स्थापना हुई। नन्दों और मौर्यों ने जो राज्य स्थापित किया, वह ब्रिटिश भारत से भी बड़ा था। उन्होंने कहा कि चीन में पहला साम्राज्य भारत के साम्राज्य के नक्शे पर स्थापित किया गया।[20]
जायसवाल ने इसी लेख में लिखा कि यहां तक तो सब अच्छा ही अच्छा चित्र है, पर अंधेरी जगह भी निगाह डालना होगा। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के समय से कुछ पहले हिन्दू साम्राज्य टूटकर छोटे-छोटे राज्य हो गए। इसका कारण, उनके अनुसार, यह था: ‘अधिकतर हिन्दू राजनीतिक बातों और अधिकारों से दूर रखे गए थे। जब शूद्रों की संस्था चलाई गई, उस समय तक तो वह राजनीतिक आवश्यकता थी। गंगा-यमुना के किनारे जो अनार्य जाति रहती थी, वह शूद्र के नाम से प्रचलित थी।’[21] जायसवाल यहां बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि शूद्र जाति अनार्य जाति थी। उन्होंने आगे वायु पुराण के हवाले से बताया कि शूद्र एक स्वतंत्र जाति है, वर्ण नहीं। उनके अनुसार, शूद्र शब्द फारस के आर्यों के वेद में नहीं पाया जाता, न किसी संस्कृत धातु से निकला है। उनका मत है कि शूद्र भारत की आदिम जाति गंगा-यमुना तटस्थ देश के स्वामी थे।[22]
शूद्रों का अलगाव कैसे हुआ और उनका पतन कैसे हुआ? इस विषय में भी जायसवाल ने अपनी अलग ही स्थापना दी है। उन्होंने लिखा: ‘इनसे (शूद्रों से) हम लोगों ने बहुत सी बातें सीखीं और ये ऐसे प्रबल थे कि जो हम लोगों के साथ बस गए थे, उनसे भी हमारे पूर्व पुरुष इतना सन्देह रखते थे कि उन्हें दूध तक न दूहने देते थे। डरा करते कि कहीं विष मिलाकर बैर न चुकावें। ग्राम में भी वे बाहर रखे जाते थे कि रात को स्वप्नावस्था में सर्वहत्या न कर डालें। अर्थशास्त्र तक में लिखा है कि शूद्रों को इकट्ठा न बसने दें, नहीं तो इनसे भय रहेगा। अस्तु, शुरू में यह स्वाभाविक था। पर, समय बीत जाने पर इस स्थिति में परिवर्तन न किया गया।’[23] जायसवाल के अनुसार इसका प्रभाव वैश्य वर्ग पर भी पड़ा। उन्होंने लिखा कि इसका बुरा परिणाम यह हुआ कि अपने वैश्य भी राज्यप्रबन्ध में स्वत्वहीन शूद्र तुल्य कर डाले गए।[24] उनका मत था कि जिस तरह ग्रीक का पतन, हेलट लोगों के कारण, जो ग्रीक के शूद्र थे, हुआ और अपने गुलामों के कारण रोमन नीचे गिरे, उसी तरह वैश्य भी गिरे। उनके अनुसार, ‘यहां अधिकांश प्रजा शूद्र और शूद्रकल्प वैश्य थी, फिर अधिकार कौन मांगता और जाति का राजनैतिक नवजन्म कौन करता?’[25]
जायसवालजी का यह मत सही था कि यहां अधिकांश जनता शूद्र थी, इसलिए अधिकार कौन मांगता? और, जिस तरह यूरोप में, जैसाकि उन्होंने लिखा है, ईसाई धर्म ने मनुष्यमात्र की सदृश्यता की घोषणा कर दी थी, वैसी सदृश्यता की घोषणा हिन्दू धर्म ने नहीं की थी। पर, ‘मरे को कब तक रोइए’, जायसवालजी ने लिखा, ‘अंग्रेजी झंडे के नीचे हिन्दू जाति अपनी चिता के भस्म से फिर उठेगी।’ किन्तु, चिता के भस्म से कोई उठा है? हिन्दू जाति तो मरी ही नहीं थी। वह अंग्रेजी झंडे के नीचे भी अपने पुनरुत्थान के कार्य को तेजी से आगे बढ़ा रही थी। अंग्रेजी झंडे के नीचे दलित वर्ग को अधिकार देने के प्रश्न पर हिन्दू जाति ने जिस तरह घमासान मचाया था, वह पूरी दुनिया ने देखा था, और जायसवालजी ने जरूर देखा होगा।
[1] काशीप्रसाद जायसवाल संचयन, खंड 1, पूष्ठ 37
[2] वही, पृष्ठ 36
[3] वही, पृष्ठ 192
[4] वही
[5] वही
[6] वही, पृष्ठ 193
[7] वही
[8] वही, पृष्ठ 194
[9] वही
[10] वही
[11] वही, पृष्ठ 195
[12] वही
[13] वही, पृष्ठ 196
[14] वही, पृष्ठ 20
[15] वही, पृष्ठ 140
[16] वही, पृष्ठ 141
[17] कृष्ण इसी तंत्र के नायकों में थे, इसी कारण राजा नहीं कहला सके और इसलिए कदाचित शिशुपाल ने राजाओं की सभा में उनका कार्ययोग नापसंद किया
[18] काशीप्रसाद जायसवाल संस्कार (खंड-2), पृष्ठ 142-143
[19] वही, पृष्ठ 143
[20] वही, पृष्ठ 155
[21] वही, पृष्ठ 158
[22] वही, पृष्ठ 157
[23] वही
[24] वही
[25] वही
(संपादन : नवल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in
फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें
मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया