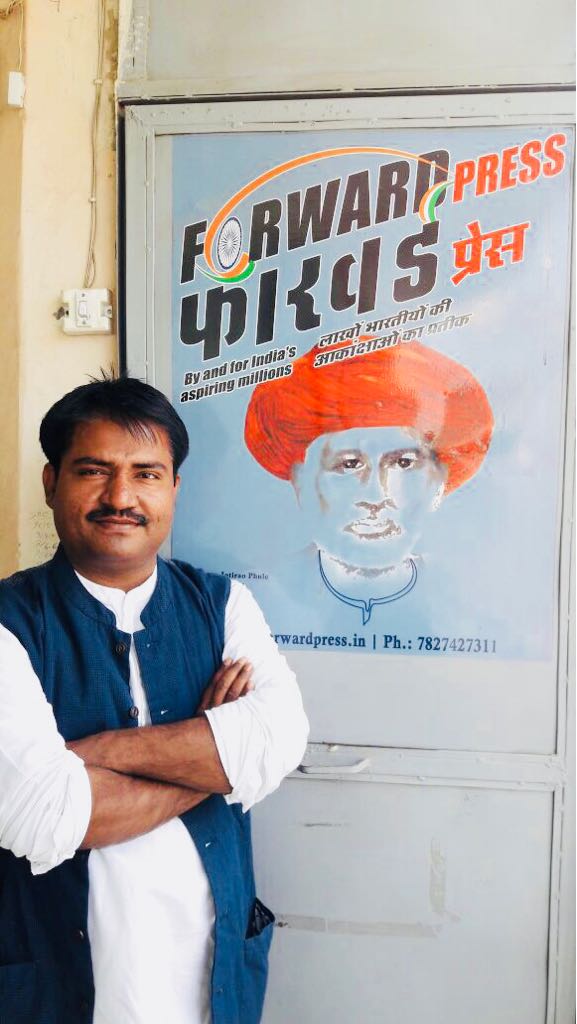[दलित साहित्य अब अनेक स्तरों पर मुख्यधारा के साहित्य के साथ मुठभेड़ कर रहा है। समालोचना के क्षेत्र मेंअनेक आवाजें इसके भीतर से भी उठी हैं और विमर्श का विस्तार हुआ है। यहां तक कि दलित साहित्य के नामकरण पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही, देश में मौजूदा सामाजिक-राजनीतिक परिवेश में दलित साहित्य की दिशा कैसी हो, इन बातों को लेकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. राजेश पासवान ने फारवर्ड प्रेस से खास बातचीत की। प्रस्तुत है इसका पहला भाग]
मुख्यधारा के साहित्य की जब बात होती है तब उसके शिल्प और सौंदर्य को लेकर अक्सर कहा जाता है कि दलित साहित्य में यह पक्ष कमजोर नजर आता है? इसे आप किस रूप में देखते हैं?
साहित्य की परिभाषा में सबके हित का भाव निहित होता है। यह तो सही है कि हर साहित्य का एक एक कलात्मक पक्ष होता है, जिसके मुख्य अवयवों में शिल्प, विंब, विधान आदि शामिल हैं। इसका सामाजिक पक्ष यह कि इसमें सबके हित का भाव है। तो अगर हम दोनों पक्षों को मिलाकर कहें तो जहां एक ओर कलात्मक पक्ष साहित्य के सौंदर्य में वृद्धि करता है, तो दूसरी ओर उसका सामाजिक पक्ष साहित्य को संपूर्णता में व्याख्यायित करता है। फिर हम मुख्यधारा का साहित्य कहें या हिंदी साहित्य कहें या दलित साहित्य की बात कहें। दलित साहित्य अपने संवेदना के स्तर पर साहित्य के उसी भाव को पुष्ट करता है कि साहित्य में सबका हित निहित है। दलित समाज है, स्त्रियां हैं, ट्रांसजेंडर हैं, अल्पसंख्यक और आदिवासी भी हैं। ये सभी समाज का हिस्सा हैं।
जैसा कि कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण होता है तो इसका मतलब जो समाज में है वह साहित्य में भी दिखना चाहिए। दर्पण की यही खासियत होती है कि जो सामने है उसमें वही नजर आएगा। समाज में जब दलित हैं, स्त्रियां हैं, अल्पसंख्यक हैं बाकी अन्य जो लोग हैं तो उनकी तस्वीर भी साहित्य में दिखनी चाहिए। इस वजह से साहित्य में उनकी उपस्थिति बहुत जरूरी है।
जहां तक हम कलात्मक सौंदर्य वाली बात करते हैं तो कलात्मक सौंदर्य एक सौंदर्य बोधहै, जो हर व्यक्ति का अपना अलग-अलग होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि समाज में किसी को गोरे लोग पसंद आते हैं, किसी को काले रंग के लोग पसंद आते हैं। समाज में ‘ब्लैक इज ब्यूटीफुल’ वाला विचार भी रहा है। तो ये जो सौंदर्य का सारा विचार है, सबके लिए अलग-अलग रहा है। इसको ऐसे भी समझें कि किसी को शाकाहारी भोजन अच्छा लगता है तो किसी को मांसाहारी अच्छा लगता है।
इसलिए कोई एक स्थायी सौंदर्य, समान रूप से सबके लिए नहीं होता है। जैसे मैं एक उदाहरण से कहूं— शरण कुमार लिंबाले अपनी आत्मकथा में एक जगह लिखते हैं कि जब वे पढ़ने जाते थे तो उन्हें क्लास के बाहर बैठाया जाता था। क्लास के बाहर जहां बाकी बच्चे अपना चप्पल उतार कर जाते थे। वे वहीं से बैठकर पढ़ते थे। उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है कि जो उनके गांव के प्रधान की लड़की थी, उसका चप्पल उन्हें बहुत सुंदर लगता था। तो यह उनका सौंदर्यबोध है क्योंकि वह बाहर बैठते हैं तो उस परिवेश में जो चीज सुंदर है, वह उनके लिए सुंदर है। वे यह नहीं कह सकते कि कक्षा के अंदर कौन सी चीज सुंदर है क्योंकि कक्षा के अंदर जाने का उनका अधिकार नहीं था। वे अंदर नहीं जा सकते थे। तो इसी वजह से दलित साहित्य का जो सौंदर्य शास्त्र है, वह दलित समाज के व्यक्तियों की जहां तक पहुंच है, उनके दायरे में जो आनेवाली चीजें हैं, उनके जीवन-व्यवहार का जो हिस्सा हैं – उनका सौंदर्य बोध भी उसी में से निकलेगा। ना कि कहीं और से निकलेगा। किसी और का अनुभव उनका अनुभव नहीं बन सकता, क्योंकि यह सहानुभूति और स्वानुभूति वाला मसला है कि किसी को वही चीज अच्छी लगेगी जो उसके पहुंच में हो। या जो उसकी संवेदनाओं को अधिक प्रभावित करती हो।

मुख्य धारा के साहित्य के सौंदर्य शास्त्र में या जो हिंदी साहित्य का सौंदर्य शास्त्र माना जाता है, जिसमें रस, अलंकार, छंद और विंब-विधान आदि चीजों की जो वकालत की जाती है, और दलित साहित्य का जो अपना सौंदर्य शास्त्र है, हमें लगता है कि दोनों के अपने निकस अलग हैं, उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। दोनों का परिवेश अलग है। इस वजह से दोनों का सौंदर्य शास्त्र भी अलग होगा। और यह एक अलग सौंदर्य-शास्त्र की भी लोगों ने बात भी की है। लिखा भी है। दलित साहित्य के सौंदर्य-शास्त्र पर कई लोगों ने पुस्तकें लिखी हैं। अब यह देखने का काम पाठकों का है कि उसे कौन सी चीजें पसंद आती हैं या किसे वह वास्तविक मानता है, क्योंकि साहित्य के साथ-साथ एक स्वाभाविकता का भी प्रश्न आता है कि साहित्य में हम जो बात कर रहे हैं, जो लिख रहे हों, वह कितना स्वाभाविक है। और अक्सर जो दलित साहित्य के बारे में आता है कि सहानुभूति या स्वानुभूति का साहित्य है तो स्वानुभूति कहीं भी अधिक बेहतर होती है सहानुभूति से। कई बार दूसरे माध्यमों से जो अनुभव प्राप्त करते हैं और खुद जो अनुभव करते हैं– उसमें अपना अनुभव ज्यादा प्रामाणिक होता है।
दलित साहित्यकारों ने जिस अनुभव के आधार पर अपने साहित्य और निकस बनाए हैं, वे अधिक वास्तविक लगते हैं, वनिस्पत किसी और के द्वारा बनाए गए या कह सकते हैं कि शास्त्रीय विधानों द्वारा बनाए गए निकस से। यह एक बात मुझे सही लगती है।
अभी तक जो हम दलित साहित्य की बात करते हैं तो आत्मकथा की विधा सबसे महत्वपूर्ण नजर आती है। जैसा कि आपने भी शरण कुमार लिंबाले की आत्मकथा जिक्र किया या फिर हम ओमप्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा ‘जूठन’ की हम बात कर लें या तुलसीराम जी की ‘मुर्दहिया’ की बात कर लें तो आत्मकथाओं का ये दौर जो है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? दूसरा यह कि अब हम क्या कुछ बदलाव की गुंजाइश दिखती है?
हां, एकदम बदलाव की गुंजाइश की दिखती है। मैंने दलित आत्मकथाओं पर 1997 में एम.फिल किया था। उस समय ओमप्रकाश वाल्मीकि की ‘जूठन’ प्रकाशित हुई थी। ‘दलित आत्मव्यक्ति और जूठन’ विषय पर मैंने एम.फिल किया था। तो उसमें कई सारे निष्कर्ष मैंने निकाले थे। जैसे एक निष्कर्ष यह भी था कि जो आत्मकथाएं हैं, वह दलित समाज के इतिहास के शिलालेख की तरह हैं। जैसे अगर कोई इतिहास लिखा जाता है तो देखा जाता है कि इसमें इससे संबंधित अतीत में क्या घटनाएं घटित हुई हैं। तो यह एक जीवंत इतिहास लेखन की तरह हैं, क्योंकि आत्मकथाएं प्रामाणिक हैं। दलित समाज का कोई लिखित इतिहास इस तरह नहीं मिलता। जो भी मिलता है मौखिक ही मिलता है। हमारे बुजुर्गों ने अगली पीढ़ी को जो कहा, वह ऐसे ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती जाती है। दलित समाज के ऊपर बहुत कम लिखा गया है। इसलिए ये आत्मकथाएं अपनी प्रामाणिकता में एक जीवंत इतिहास का काम करती हैं। और मुझे लगता है कि इनके अध्ययन का दायरा सिर्फ दलित साहित्य नहीं बल्कि मनुष्य जाति के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। उन्हें भी यह देखना चाहिए कि दलित समाज की आत्मकथाएं जिस दौर में लिखी जा रही हैं, उस दौर का समाज विज्ञान क्या है। उस दौर का शिक्षा स्तर क्या है। आर्थिक स्तर क्या है। हम मानव विकास सूचकांकों कीबात करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि जिस दौर में आत्मकथाएं लिखी जा रही हैं, उस समय दलितों का मानव विकास सूचकांक क्या है। उसमें उनकी अपनी जीवन-शैली क्या है, खान-पान और रहन-सहन क्या है। शिक्षा का स्तर क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है। नौकरियों में किस तरह से व्यवहार हो रहा है। तो इन सबकी प्रामाणिक रूप से जांच-पड़ताल के लिए आत्मकथाएं एक जीवंत और प्रामाणिक दस्तावेज लगती है। इनकी सच्चाई से कोई इंकार नहीं कर सकता, क्योंकि लिखने वाले भी आज मौजूद हैं और उस तरह की घटनाएं रोज अखबारों में और विभिन्न माध्यमों में देखने-सुनने को मिल जाती हैं। किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में दलितों का उत्पीड़न होता है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है।
मुझे लगता है कि आत्मकथाएं आने वाले भविष्य के लिए दलित इतिहास लिखने में सहायक साबित होंगीं। जहां तक बात आप कर सकते हैं भविष्य के लिए तो मुझे इसमें यह जरूर लगता है कि आत्मकथाओं के लेखन में कुछ घटनाओं से बचा जा सकता था। मतलब यह कि इन आत्मकथाओं में यथार्थ तो कटु यथार्थ की तरह बयान किए गए हैं, फिर भी कुछ ऐसे यथार्थ हैं जिन्हें नजरअंदाज किया जा सकता था। मुझे लगता है कि दलित युवाओं को मनोबल तोड़ने का या कम करने का काम भी कभी-कभार आत्मकथाएं करती हैं। हम एकदम यह मानने के लिए तैयार हैं कि दलित समाज के ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार किए गए हैं। जबरन उन्हें गुलाम बनाया गया। जबरन उनकी स्त्रियों के साथ अमानवीय काम हुए हैं, लेकिन वह सब कहीं न कहीं एक दुखद अध्याय है। और एक तरीके से कह सकते हैं कि संकेत रूप में जिक्र करना चाहिए था। उनका बहुत विस्तार में जो आत्मकथाओं में जो उल्लेख है, खासकर दलित स्त्रियों के बारे में, वहां थोड़ा बचा जा सकता था। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि जब हम एक आदर्श बनाते हैं, तो मनोबल बढ़ाने वाले भी कुछ चीजें साहित्य में डालते हैं। यह तो समझना ही होगा कि वह संघर्ष सबके लिए है। ये चीजें आत्मकथाओं में होनी चाहिए थी। दूसरी एक और बात कि इन आत्मकथाओं का फायदा दलित समज को हुआ है। समाज में संघर्ष तो सबसे अधिक दलिताें ने किया है। लेकिन इन आत्मकथाकारों का संघर्ष और संघर्ष के बाद इन सभी आत्मकथाकारों ने सम्मानजनक पदों को प्राप्त किया है। कोई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है या अन्य लोग समाज में अच्छे पदाधिकारी बने हैं, या ऊंचा ओहदा पर गए हैं। तो जो बाकी समाज संघर्ष करता है, उसे लगता है कि हां मैं भी ऐसा कर सकता हूं। ये जो घटनाएं मेरे साथ हुई हैं – गरीबी, अपमान और वंचना जो हमारे साथ हुई है – इसको झेलते हुए भी मैं कुलपति तक बन सकता हूं। मैं अधिकारी भी बन सकता हूं। मैं विश्वविद्यालय का प्रोफेसर भी बन सकता हूं। तो एक तरह से आज की पीढ़ी का हौसला बढ़ाने का काम ये आत्मकथाएं करती हैं। ऐसा मुझे लगता है।
एक बात यह भी कि संघर्ष के साथ-साथ आत्मकथाएं जब लोग लिखते हैं, तब वे सम्मानजनक पद या उपलब्धि को प्राप्त कर चुके होते हैं। इस संघर्ष में बहुत सारे लोग टूटकर बिखर जाते हैं। बिखरे हुए लोगों ने आत्मकथाएं नहीं लिखी हैं। जो लोग सफल हैं, सफल लोगों की आत्मकथाएं दूसरे संघर्षशील लोगों के लिए प्रेरणा देने का काम करती हैं। इस अर्थ में आत्मकथाएं सफल हैं। ऐसा मुझे लगता है।
क्रमश: जारी
(संपादन : समीक्षा / अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in
फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें
मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया
बहुजन साहित्य की प्रस्तावना
दलित पैंथर्स : एन ऑथरेटिव हिस्ट्री : लेखक : जेवी पवार
महिषासुर एक जननायक’
महिषासुर : मिथक व परंपराए
जाति के प्रश्न पर कबीर
चिंतन के जन सरोकार