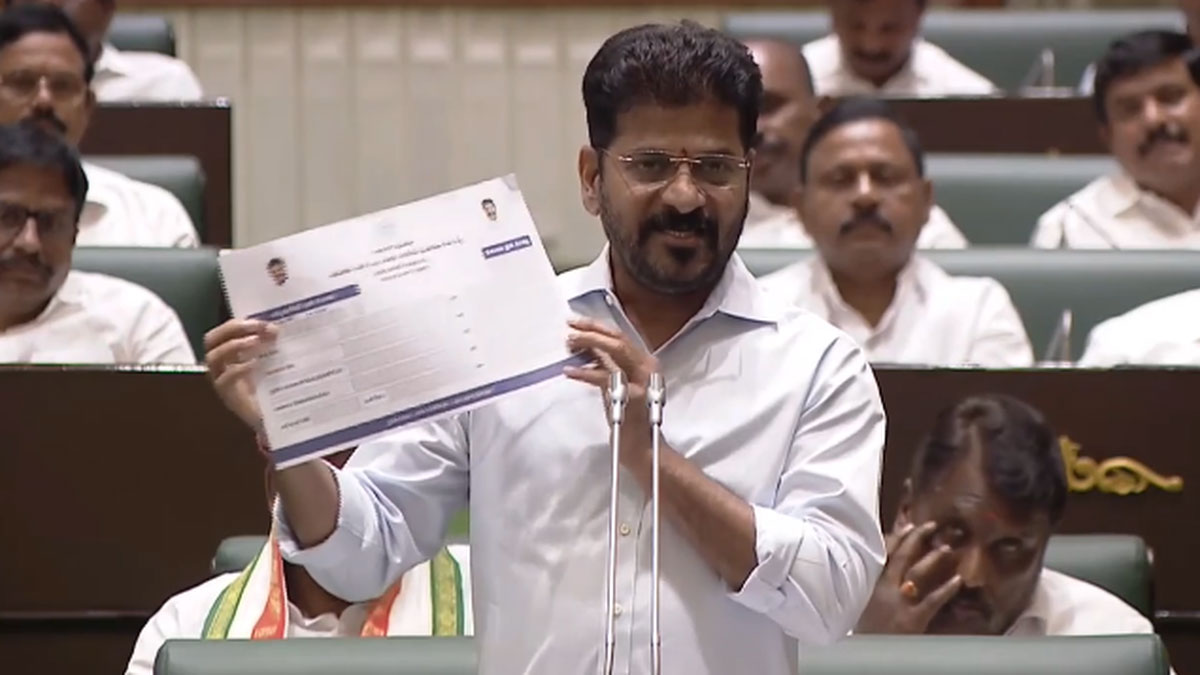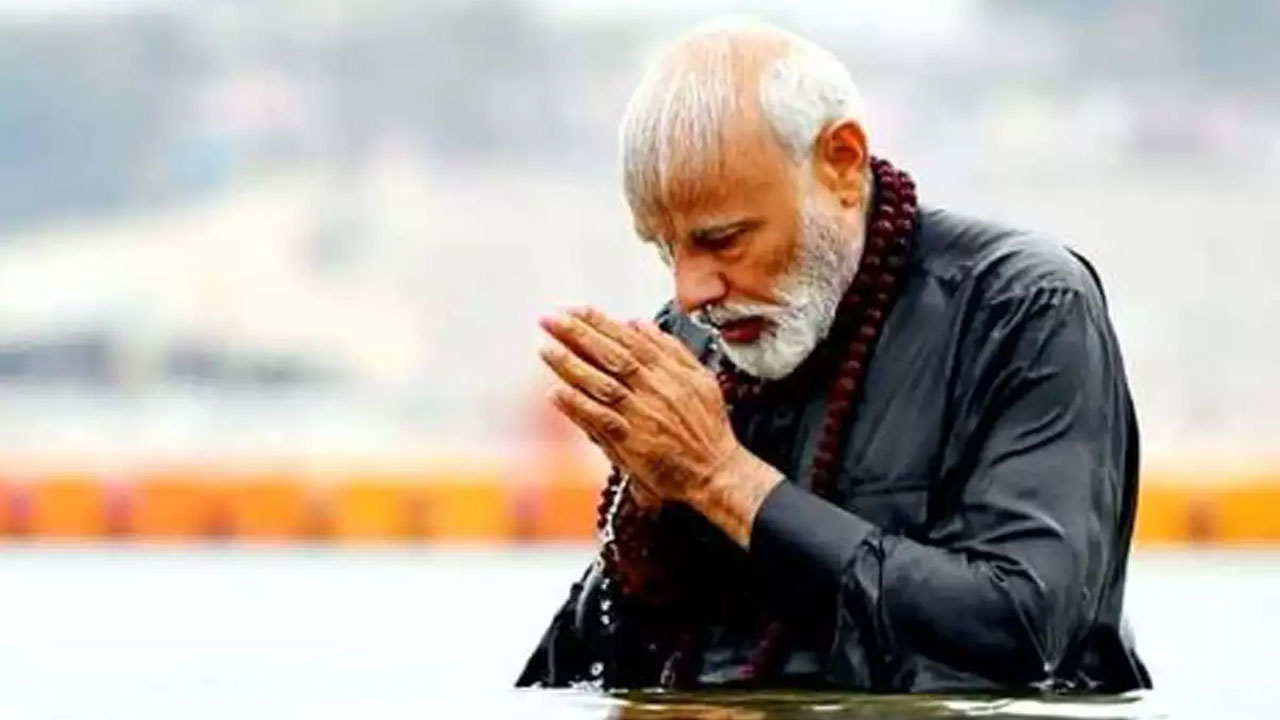जम्हूरियत में विपक्षी दलों का मजबूत होना जरूरी है और समाज के कमजोर तबकों के लिए उनको अपेक्षाकृत ज्यादा संवेदनशील और मुखर होना चाहिए। मगर, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें इसकी कमी महसूस हो रही है। लगता है कि विपक्ष हमलावर सांप्रदायिकता के सामने ‘किंकिर्तब्यविमूढ़’ है। अगर ऐसा नहीं होता तो देश की राजधानी दिल्ली में एनआरसी, सीएए के खिलाफ शांतिपूर्ण और लंबे आंदोलन को, जिस तरह पूर्व नियोजित सांप्रदायिक दंगों के जरिए सत्ता पक्ष ने कुचला, उसे लेकर दिल्ली सरकार अथवा अन्य विपक्षी दलों द्वारा जमीनी तौर पर, हस्तक्षेप करके रोकने का कोई प्रयास नहीं हुआ। जाहिर है कि कहीं भी कोई दंगा–फसाद हो या प्राकृतिक आपदा, उनमें जान–माल, इज्जत–आबरू का ज्यादा नुकसान तो गरीब पसमांदा तबकों का ही होता है।
इसी तरह देश के कई भाजपा शासित राज्यों में 2014 के बाद से ही गोरक्षा, घर वापसी, लव जिहाद, मंदिर–मस्जिद के नाम पर हमारे लोगों की मॉबलिंचिंग हो रही है। क्या ऐसे में सिर्फ ‘ट्वीट’ करना और संसद में सवाल उठाना ही काफी है? 2017 तक मैं भी जद(यू) के सदस्य के रूप में राज्यसभा में था। इस दौरान हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, बिहार जहां भी इस तरह की घटनाएं हुईं, उसके बाद, घटनास्थल पर जाकर पीड़ित लोगों से मिला। लौटकर संसद में भी मजबूती से सवाल उठाया। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि विपक्षी पार्टियों के प्रमुखों की बात तो छोड़ दीजिए। मुस्लिम सांसद भी इस इंतजार में बैठे ही रहे कि उनकी पार्टी का निर्देश होगा तब पीड़ितों से मिलने जाएंगे। अलबत्ता इक्का–दुक्का सांसदों ने अखबारी सूचनाओं के आधार पर संसद में जरूर इस सवाल को उठाया। यह अच्छी बात है कि जब दलितों की हत्या–बलात्कार की घटना हो या अन्य किसी की हत्या या पुलिस जुल्म हो, इसमें कई पार्टियों के प्रमुखों तक पीड़ितों से मिलने पहुंच जाते हैं। वे कई मामलों में उनकी आर्थिक मदद भी करते हैं। मगर, दुख तो तब होता है जब मुसलमानों के साथ ऐसी दर्दनाक घटनाएं होती हैं तो, उनकी मातमपूर्सी के लिए भी कोई नहीं आता।
हम यह समझ रहे हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि कुछ लोगों को डर है कि अगर वे इस तबके के पक्ष में खड़ा होंगे तो ‘हिंदू’ उनसे नाराज हो जाएंगे। मगर, आम हिंदू समाज का मानष (तासीर ) ऐसा हरगिज नहीं है। अगर ऐसा होता तो सत्ता पक्ष द्वारा जिस तरह की नफ़रती कारवाईयां पिछले 8 साल से चलाई जा रही हैं, उससे एकबारगी पूरा देश जल उठता। जरूरत इस बात की है कि विपक्ष हर तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ और सामाजिक न्याय के लिए मजबूती से खड़ा हो जाए। प्रेम और भाईचारा स्थायी और नैसर्गिक है। नफ़रत तो बनावटी और अस्थायी होता है।
यह कैसी विडंबना है कि दंगाइयों, मॉबलिंचिंग और बलात्कार करनेवालों के पक्ष में तो भाजपा के नेता मजबूती से खड़े हो जाते हैं, ऐसे लोगों को माला पहनाया जाता है, पार्टी तथा सरकार में तरक्की दी जाती है। क्या ऐसा इसलिए नहीं है कि हमारे लोग सांप्रदायिकता की मुखालफत के नाम पर सेक्युलर पार्टियों के पक्ष में वोट डालते हैं? तो क्या हमारा यही गुनाह है? हम पीड़ित पक्ष के लोग जिन नेताओं–पार्टियों को वोट देते हैं, वह हमारे पक्ष में मजबूती से खड़ा क्यों नहीं होते?

क्या यह सही नहीं है कि वामपंथी पार्टियों को छोड़ बाकी विपक्षी दलों के नेता अपनी जुबान पर ‘सेक्युलर’ शब्द लाने से भी परहेज करने लगे हैं? क्या यह शब्द भारत के संविधान की रूह नहीं है? संविधान की किताब में रहते हुए भी अगर यह शब्द निष्प्रभावी हो जाए तो क्या व्यवहारिक रूप में अपना देश धर्म आधारित राज्य नहीं हो जाएगा? क्या मौजूदा हुक्मरान पार्टी के लोगों द्वारा देश को धर्म आधारित राज्य बनाने की खुलेआम घोषणा नहीं की जा रही है? क्या जम्हूरियत और सेक्ल्युरिज्म के सारे सतूनों (खंभों) को एक–एक कर तोड़ा नहीं जा रहा है? क्या यह सच्चाई नहीं है कि विपक्ष इसको बचाने के लिए अकेले अथवा मिल–जुलकर कोई संघर्ष खड़ा करने में अभी तक विफल रहा है?
क्या विपक्ष ने कभी इस पर गौर किया है कि आक्रामक सांप्रदायिकता और चौतरफा कारपोरेट लूट और कब्जा अभियान को रोकने में आप लोग क्यों विफल हो रहे हैं? हमारा मानना है कि समतामूलक समाज बनाने और सामाजिक न्याय की लड़ाई को छोड़कर आप लोग ऐसे लोगों के मान मनौव्वल और मनुहार में लग जाते है, जहां से अभी कुछ भी हासिल होनेवाला नहीं है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि देश के बहुजनों की ताकत पर विपक्षी दलों का भरोसा कमजोर हो गया है, बगैर किसी वैचारिक प्रतिबद्धता के, सियासी जोड़–तोड़ के जरिए, सत्ता में फिर से जाने तथा अपनी पार्टी को बचाने की चिंता, देश पर भी भारी पड़ रही है? क्या विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा है कि उनकी सरकारों को किस तरह गिराया जा रहा है? पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। विपक्ष के दिग्गज नेताओं को जेल भेजने का डर दिखाकर परेशान किया जा रहा है।
एनडीए सरकार की गरीब विरोधी एवं एकाधिकार पूंजीवाद समर्थक नीतियों के बरअक्स विपक्षी दल कोई मजबूत एजेंडा लेकर मैदान में क्यों नहीं उतर पा रहे हैं? विपक्ष सिर्फ उनकी नीतियों के खिलाफ मौखिक प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा हैं। कहीं विपक्ष को ऐसा तो नहीं लगता है कि एक दिन देश की जनता मौजूदा हुकूमत की नीतियों से तंग आकर खुद–ब–खुद विपक्ष दलों को सत्ता में बिठा देगी? आठ साल हो गए। ‘नोटबंदी, कोरोना महामारी और कमरतोड़ महंगाई के बीच रिकार्डतोड़ बेरोजगारी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, दस्तकार, छोटे उद्योग–धंधे वाले खुदकुशी कर रहे हैं। देश के जल–जंगल, जमीन, बालू, कोयला, खनिज आदि प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूट हो रही है। दूसरी तरफ दो–चार लोगों का शुमार दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपतियों में हो रही है। मगर, इस को लेकर सरकार को खुली चुनौती देने वाला कोई नहीं है। हमारे देश में 85 करोड़ लोग ‘लाभार्थी’ के नाम पर ‘याचक’ की श्रेणी में धकेल दिए गए हैं।
तीन बड़े जन–आंदोलन
बची–खुची खेती–किसानी को एकाधिकार पूंजीपतियों के हवाले करने हेतु सरकार ने जिन तीन काले कृषि कानूनों को बनाया, उसके खिलाफ किसानों ने शांतिपूर्ण ढंग से करीब एक साल तक ऐतिहासिक आंदोलन चलाकर, इन कानूनों को वापस करा दिया। इसी तरह एनआरसी, सीएए के खिलाफ शांतिपूर्ण लंबे ऐतिहासिक आंदोलन में मुस्लिम महिलाओं ने भारी संख्या में शिरकत कर फौरी तौर पर इसे रुकवा दिया है। मगर, स्थायी तौर पर इस को खत्म करने के लिए विपक्ष की क्या तैयारी और रणनीति है? उपरोक्त दोनों तबकों के जन आंदोलनों से पहले 2 अप्रैल, 2018 को दलित समाज के लोगों ने अपने बूते एक दिवसीय शांतिपूर्ण ‘भारत बंद’ के जरिए संसद से पारित अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1998 में संशोधन को वापस करा दिया। किसी पार्टी के आह्वान पर यह बंद और आंदोलन नहीं हुए थे।
यह भी पढ़ें – ‘हम पसमांदा हैं और अब पेशमांदा होना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी’
सेना में चार साल की भर्ती हेतु ‘अग्निपथ योजना’ को लेकर छात्र–नौजवानों के गुस्से का जिस तरह विस्फोट हुआ तथा उपरोक्त सभी बड़े आंदोलनों को सुसंगत और संगठित रूप में आगे बढ़ाने के लिए विपक्ष ने क्या प्रयास किया? ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर और गरीब परिवारों के युवाओं की स्थायी तौर पर सेना में भर्ती होकर सरकारी नौकरी पाने की अंतिम इच्छा भी क्या खत्म नहीं कर दी गई है? क्या तेजी के साथ निजीकरण की प्रक्रिया चलाकर सभी धर्मों के दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को पढ़ने तथा सरकारी नौकरी में जाने के रास्ते सदा के लिए बंद नहीं किए जा रहे हैं? ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की मांग क्या विपक्षी दलों का केंद्रीय मुद्दा नहीं होना चाहिए?
हमने देखा है कि 2014 के बाद विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव में भी विपक्षी दल अपने मूल जनाधार और बुनियादी मुद्दों को छोड़कर ज्यादातर इधर–उधर की ही बातें करते रहे। यही नहीं कोई छह–आठ महीने पहले ये बिना किसी तैयारी के चुनाव मैदान में उतर जाते हैं, जिसका नतीजा भी देश ने देखा है। कुछ तो भाजपा के डर से पूरे चुनाव घर में ही बैठे रह गए। इसका खामियाजा न सिर्फ उपरोक्त पार्टियों को भुगतना पड़ा है, बल्कि उनके वोटरों का मनोबल भी इससे टूटा है। सांप्रदायिकता के उभार के चलते आज जिस तरह की स्थिति है, 1946-47 और 1948 में तो इस से भी खतरनाक स्थिति रही होगी। मगर तब महात्मा गांधी कहां डरे? बल्कि इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान तक दे दी। यही नहीं वह हमेशा ‘अंतिम जन’ के लिए लड़ते– काम करते रहे।
दलित मुसलमानों–ईसाइयों का सवाल
क्या विपक्षी दल यह जानते हैं कि गांधी से लेकर डॉ. अंबेडकर, डॉ. राममनोहर लोहिया, मार्क्सवादी चिंतक राहुल सांकृत्यायन तक सभी ने यह माना है कि धर्म बदलने से इंसान की सामाजिक स्थिति नहीं बदलती है। मुसलमानों और ईसाइयों में भी अस्पृश्य(अछूत ) हैं। जब कायदे से कोई सवाल उठ जाता है तो वह बात बौद्धिक विमर्श में भी चली जाती है। इसका असर राजनीति में भी होता है। 1998 से शुरू हुए पसमांदा तहरीक के बाद ही यूपीए सरकार ने सच्चर कमिटी और रंगनाथ मिश्र आयोग का गठन किया। लेकिन, राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में उसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। रंगनाथ मिश्र आयोग का ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ ही यह था कि अन्य धर्मों में दलित की पहचान और उसके उत्थान के लिए उपाय का सुझाव देना इस आयोग का काम होगा।
इस आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा है कि ‘दलित मुसलमान और दलित ईसाइयों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है’। यह भेदभाव फौरन समाप्त किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ‘एक्जीक्यूटिव ऑर्डर’ से यह काम कर सकती है। इसके लिए संविधान संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। इस आयोग ने इस तबके के लिए जगह–जगह ‘नवोदय विद्यालय’ की तर्ज पर स्कूल खोलने जैसी सिफारिशें भी की हैं। सच्चर कमेटी ने भी दलित मुसलमान और दलित ईसाइयों को ‘शिड्यूल कास्ट’ का दर्जा देने की सिफारिश की है। उसने एक ‘ इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन’ बनाने की भी सिफारिश की है। उसने यह भी कहा है कि मुसलमानों के एक बड़े हिस्से की हालत हिंदू दलितों से भी ज्यादा खराब है। उसने दस्तकार बिरादरियों की हालत सुधारने के लिए भी कई उपाय सुझाए हैं। मगर यूपीए सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हमारे संगठन की शुरू से यह मांग रही है कि दलित मुसलमानों और दलित ईसाईयों को एससी का दर्जा देने तथा छुटे हुए कबीलों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का का कोटा भी बढ़ाया जाना चाहिए। यह न सिर्फ न्यायसंगत होगा, बल्कि ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि भाजपा को दलित–आदिवासियों को हमारे खिलाफ खड़ा करने का मौका नहीं मिल सके।
हम विपक्षी दलों को याद दिलाना चाहते हैं कि नरसिंह राव सरकार के समय मदर टेरेसा दलित ईसाइयों के लिए अनुसूचित जाति के दर्जें की मांग को लेकर दिल्ली में राजघाट के महात्मा गांधी समाधि पर एक दिन लिए उपवास पर भी बैठी थीं। उस समय इसे लेकर भाजपा के लोगों ने इस संत महिला के खिलाफ क्या–क्या बुरा नहीं बोला। यहां यह भी बता देना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी से लेकर वामपंथी दलों, जनता दल(यू), राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मरहूम राम विलास पासवान जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मरहूम वाईएसआर ने भी समय–समय पर हमारी मांगों का समर्थन किया था। नीतीश कुमार ने तो एनडीए में होने के बावजूद एक सांसद के रूप में इस सवाल को लोकसभा में उठाया था। इसे लेकर भाजपा संसदीय दल के नेता बी. के. मल्होत्रा से उनकी बकझक भी हो गयी थी। बाद में भाजपा के मुखपत्र ‘पांचजन्य’ ने नीतीश जी के खिलाफ कवर स्टोरी छापी थी। लालू जी और मुलायम सिंह जी तथा वाईएसआर साहब के मुख्यमंत्रीत्व काल में तो बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश विधानसभाओं ने भी, दलित मुस्लिम, दलित ईसाई को एससी का दर्जा देने के लिए, अपने विधानसभा से प्रस्ताव पारित करा कर, तत्कालीन केंद्र सरकार को भेजा था। पर इन पार्टियों ने इससे आगे बढ़कर कुछ नहीं किया।
जहां तक पसमांदा तबकों की राजनीतिक सशक्तिकरण की बात है तो इक्का–दुक्का मामले को छोड़ विपक्षी दलों ने मुसलमानों की कुल आबादी में 80 फीसदी पसमांदा आबादी को किसी तरह का राजनितिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया और न इनके सवालों को अपनी राजनीति का केंद्र बिंदु बनाया। इसके उलट ये ‘पसमांदा’ शब्द तक अपनी जुबान पर लाने से परहेज करते रहे हैं। पहले से यह तबका अपना राजनीतिक बहिष्कार झेल ही रहा था कि भाजपा के शासनकाल में आर्थिक बहिष्कार भी झेलने लगा है। मुर्गा–मुर्गी, सब्जी–फल बेचने से लेकर भीख मांगने तक इनकी पिटाई की जा रही है। मुसलमान होने के नाते इस दौर में जो लोग भी मारे–काटे, लुटे–जलाए जा रहे हैं, उनमें अधिकांश तो पसमांदा मुसलमान ही हैं। पसमांदा मुसलमान मुल्क की सियासी पार्टियों–सरकारों से मजहब की बुनियाद पर कुछ नहीं मांग रहे हैं। बल्कि हर क्षेत्र में उनके साथ मजहब के नाम पर जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करने की मांग कर रहे हैं।
आखिर क्या कारण है कि इस सब के बावजूद नरेंद्र मोदी इस तबके से अचानक हमदर्दी जताने लगे हैं? क्या इसका कारण ‘सेक्युलर और सामाजिक न्याय की विचारधारा’ की पार्टियों द्वारा पसमांदा तबके को नजरअंदाज करना नहीं है? एआईएमआईएम प्रमुख असददुदीन औवैसी जब से हैदराबाद से निकल बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल में अपना पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं तबसे उनकी जुबान से भी पसमांदा शब्द सुनने को मिलने लगा है। पहले तो वह यह शब्द सुनकर भड़क जाते थे। ये दोनों पसमांदा तबके को यह समझाने में लगे हैं कि देखो, आप जिसको वोट देते हो वह तो तुम्हारा नाम भी नहीं लेता है। संभव है कुछ नासमझ और लालची लोग इनके बहकावे में आ जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि इनके इस प्रचार अभियान से पसमांदा तबके में विपक्ष के प्रति उदासीनता पैदा हो जाए।
उपरोक्त परिस्थितियों से अवगत कराने का मकसद यही है कि विपक्ष अपनी भूमिका को समझे। यह न केवल पसमांदा समाज के उत्थान का विषय है बल्कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की चुनौती भी है। इस मसले पर बिंदुवार चर्चा करने की आवश्यकता है। आशा है आप हमारी बात को समझेंगे और पसमांदा–बहुजन दावेदारी के सवाल पर मुखर होकर काम करेंगे।
- पसमांदा केवल वोट बैंक नहीं है, वह सामाजिक न्याय और समता की लड़ाई का हिस्सा है। यह हमारा संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक दायित्व है कि उन्हें राजनीति की मुख्यधारा में लाकर सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलवाने का प्रयास करें।
- दलितों और अति पिछड़ों की तरह पसमांदा भी गरीब, उपेक्षित, पिछड़ा है। इसके एक हिस्से की हालत तो हिंदू दलितों से भी खराब है। विपक्ष डरे नहीं, पसमांदा शब्द उर्दू–फारसी का जरूर है, लेकिन यह ‘रिलीजन’ और ‘कास्ट’ न्यूट्रल है। इस नाम का न कोई धर्म है न कोई जाति। यह जमात (वर्ग) सूचक शब्द है और भारतीय संविधान के दायरे में भी है।
- पसमांदा अगर हर तरह से सशक्त होता है, तो मुसलमानों में मौजूद तंगनजरी और रूढ़िवादिता कम होगी। पसमांदा को यदि लगेगा कि उसे भी आगे बढ़ने और साथ चलने के अवसर मिल रहे हैं तो उसका अलगावपन कम होगा। भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो धारणाएं बन रही है, वे खंडित होंगी। भारत दुनिया में एक मॉडल बनेगा कि वह कैसे अपने अल्पसंख्यकों और कमजोर तबकों को साथ लेकर चल रहा है और दूसरे भी चल सकते हैं।
- मौजूदा हुकूमत राष्ट्रीय परिसंपत्तियों और प्राकृतिक संसाधनों को चंद कारपोरेट घरानों के हवाले कर रही है। अगर इस लूटी गई दौलत को फिर से वापस लाने की योजना के साथ विपक्षी दल आगे आएंगे तो, एक समय निजी बैंकों तथा कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के वक्त जैसा जनसमर्थन बना था उससे बड़ा जनउभार खड़ा हो जाएगा।
- मौजूदा केंद्र सरकार ने तो राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना कराने से मना कर दिया है। दलित मुसलमानों–ईसाईयों को एससी का दर्जा नहीं देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी लिख कर दे दिया है। अगर विपक्षी दल अभी से इस बात की घोषणा कर देंगे कि केंद्र की सत्ता में आने पर वह राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक आर्थिक जनगणना कराएंगे तथा एससी का कोटा बढ़ाकर उसमें दलित मुसलमानों–ईसाइयों को शामिल करेंगे, तो यह उनका एक ऐतिहासिक कदम होगा।
- भाजपा की तरह अगर सिर्फ ‘टोकनिज्म’ नहीं कर विपक्षी दल, वास्तविक रूप में पसमांदा– अतिपिछड़े हिंदू–मुस्लिम समाज को, सत्ता–प्रशासन में उनकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व दे देंगे तो, भाजपा की ‘फूट डालो राज करो’ की नीति धराशायी हो जाएगी।
- सेना में ‘अग्निपथ योजना’ किसान–मजदूरों के बेटों को स्थाई नौकरी से वंचित करने के लिए है। सीएए, एनआरसी कानून पसमांदा मुसलमानों और दूसरे गरीब लोगों का वोटिंग राइट छीनने के लिए है। सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा अभियान जम्हूरियत का गला घोटने के लिए है। मजदूर वर्ग के सभी हिमायती कानूनों को बदलना पूंजीपतियों के पक्ष में है। कानून बना कर किसानों की जमीन छीनने का प्रयास उन्हें मजदूर बनाने के लिए है। सरकार के खिलाफ बोलने–लिखने पर रोक लगाना तानाशाही है। देखना है, विपक्ष एकजुट होकर इस तानाशाही का मुकाबला किस तरह करता है।
(संपादन : नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in
फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें
मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया