इसके पहले आपने पढ़ा : भगत सिंह की दृष्टि में सांप्रदायिक दंगों का इलाज
भगत सिंह के दस्तावेज़ों के अनुसार, सितंबर, 1928 के ‘किरती’ में ‘एक निर्वासित’ एम.ए. नामक एक छद्म नाम के लेखक का एक बहुत ही विचारोत्तेजक लेख प्रकाशित हुआ था। भगत सिंह और उनके साथियों ने इस लेख पर गहराई से विचार किया और उसे अपने विचारों के अनुकूल माना। शायद इसीलिए इस लेख को भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज़ों में शामिल किया गया। दस्तावेज़ के संपादकों ने इस लेख को लाला हरदयाल की रचना बताया है। इस लेख का शीर्षक है– ‘वर्ग-रुचि का आंदोलनों पर असर’।[1] भगत सिंह की राजनीतिक विचारधारा के केंद्र में वर्ग-संघर्ष एक प्रमुख सिद्धांत रहा है। इसलिए मैंने अपने ‘भगत सिंह-मूल्यांकन’ शृंखला के इस अंतिम अध्ययन में वर्ग-संघर्ष को केंद्र में रखा है। चर्चा करने से पूर्व लाला हरदयाल के लेख से एक अंश देखते हैं, जो हालांकि लंबा है, पर महत्वपूर्ण है–
“प्रश्न उठता है कि यह अजीब हालत पैदा ही किस तरह हो गई? क्या कारण है कि जो लोग खेती करते, कपड़ा बुनते, नालियां साफ़ करते, या आटा पीसते हैं, उनकी आमदनी उन लोगों से कई गुना कम है, जो केवल लेक्चर देते हैं या मुक़दमों पर बहस करते हैं, जो न्याय करते या हुकूमत करते हैं, जो केवल दुआ करते या कुछ भी नहीं करते? क्या कभी किसी ने सोचकर देखा है कि भगवान के हर बंदे और समाज के लिए खेती-बाड़ी, कारीगरी, दस्तकारी आदि करने वाले ‘क़ानून’ या ‘सरकार’, मज़हब या साहूकार या केवल ज़मींदार (वे लोग जो ज़मीनों के मालिक तो बन बैठे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते) से ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर क्या कारण है कि उस आदमी को, जो कि कुछ घंटे कुर्सी पर बैठकर कुछ आदमियों को जेल में भेज देता है, गेहूं बोने वाले किसान और जूते गांठने वाले मोची से कई गुना अधिक तनख्वाह दी जाती है? एक राजा या मजिस्ट्रेट या साहूकार ही मेहनतकश लोगों से कौन-सा अच्छा, लाभदायक और ज़रूरी काम करता है? अनेक लोग सारा दिन एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाकर काम करते हुए भी अपनी ज़रूरी चीज़ें प्राप्त नहीं कर सकते। क्या वजह है कि एक आदमी बैठा पंखा खींचता है और एक अंदर पड़ा – भले ही वह हिंदू, मुसलमान या ईसाई हो – खर्राटे मारता है। इसे ही पंखा खींचने पर क्यों नहीं लगाया जाता? वह लोग, जो अनाज, दूध, मेवे, सब्ज़ी पैदा नहीं करते, बल्कि इन चीज़ों को इस्तेमाल करते और खाते हैं, वास्तव में तो वही बेचारे किसान की मेहनत का लाभ उठाते हैं। इस बात को समझने के लिए किसी फ़िलॉसफ़ी की ज़रूरत नहीं है। वे लोग जो रोटी पैदा नहीं करते, और न रूई कातकर, बुनकर कपड़ा तैयार करते हैं, और फिर भी रोटी खाते और कपड़ा पहनते हैं, तब इसका यही अर्थ है कि वे अपना हिस्सा ग़रीब मेहनतकशों की मेहनत में से ले लेते हैं, जोकि रोटी पैदा करते हैं, कपड़े तैयार करते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि खेती करने वाले उस मेहनतकश किसान को इन मुफ़्तखोर लोगों की तरह अच्छी ख़ुराक भी नहीं मिलती, तो दिल में ख़याल आता है कि इस व्यवस्था में ज़रूर कहीं न कहीं धोखा है, ग़लती है, ज़ुल्म है। लेकिन यह मसला ‘सर्व-दर्शन-संग्रह’ आदि शास्त्रों की सोलह प्रकार की फ़िलॉसफ़ी पढ़ने से हल नहीं हो सकता। सेहत और ज़िंदगी के सवाल को छोड़कर आज हम एक बहुत बड़ा सवाल पूछना चाहते हैं कि दुनिया में ये जो दो पार्टियां हैं– एक ओर अमीर, विद्वान, सुस्त और हरामखोर; दूसरी तरफ़ ग़रीब, मेहनतकश, ज़ाहिल अनपढ़ लोग, जोकि दुनिया की दौलत पैदा करते हैं, तो यह दूसरा पक्ष किस तरह अस्तित्व में आया? दुनिया के तमाम आंदोलन, जो इस सच्चे सवाल को ओझल करते हैं, केवल बेहूदा, फ़िज़ूल और ख़तरनाक हैं, फिर भले ही मजलिसी हों, भले ही मज़हबी हों, या भाईचारे वाले, आर्थिक हों या राजनीतिक, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय।”[2]
निस्संदेह, लाला हरदयाल ने मेहनतकश लोगों की ग़रीबी और मुफ़्तखोर अमीरों का जो ख़ाका प्रस्तुत किया है, वह भारतीय समाज व्यवस्था का विद्रूप है। वह सही प्रश्न उठाते हैं कि क्या कारण है कि जो लोग खेती करते, कपड़ा बुनते, नालियां साफ़ करते, या आटा पीसते हैं, उनकी आमदनी उन लोगों से कई गुना कम है, जो केवल लेक्चर देते हैं या मुक़दमों पर बहस करते हैं, जो न्याय करते या हुकूमत करते हैं, जो केवल दुआ करते या कुछ भी नहीं करते? लेकिन लाला हरदयाल इसका कारण पूंजीवाद में खोजते हैं। भगत सिंह की दृष्टि में भी पूंजीवाद ही इसका कारण था। असल में पश्चिमी समाजवादी दार्शनिकों को पढ़कर अपनी समझ विकसित करने वाले विचारक, चाहे वे लाला हरदयाल हों, या भगत सिंह और उनके साथी, या जवाहरलाल नेहरू हों, या कोई और, भारतीय समाज-व्यवस्था में मौजूद आर्थिक असमानताओं को तब तक नहीं समझ सकते, जब तक कि वे ब्राह्मणवाद का अध्ययन नहीं करेंगे। वे समस्या तो पकड़ लेते हैं, पर उसका कारण नहीं जान पाते, इसलिए उसका निदान भी उनकी समझ से बाहर होता है। लाला हरदयाल इसका कारण पूंजीवाद को मानते हुए लिखते हैं–
“पिछले इतिहास से यदि कोई शिक्षा मिलती है, तो वह यह कि अमीर वर्ग को दौलत ही सबसे अधिक प्यारी चीज़ है। उसको मज़हब और देशभक्ति से ज़्यादा ज़ायदाद और व्यक्तिगत स्वार्थों से प्रेम है। देशभक्ति और मज़हब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन वह भी अमीर वर्ग को दौलत की चेटक (इंद्रजाल) से आज़ाद कराने में निष्फल साबित हुई है। दुनिया में आज तक ऐसा ही होता आया है और जब तक बड़े-छोटे अमीर तबक़े ही ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक ऐसा ही होता चला जाएगा।”[3]
लेकिन ये बड़े-छोटे अमीर तबक़े ख़त्म कैसे होंगे? इस प्रश्न का हल लाला हरदयाल ने नहीं सुझाया। समाजवादियों की तरह लालाजी भी इसी मत के थे कि वर्ग सिर्फ़ दो ही होते हैं– अमीर और ग़रीब। वह लिखते हैं–
“दुनिया में दोनों ही क़ौमें मौजूद हैं– अमीर और ग़रीब। इनमें कोई प्यार और हमदर्दी नहीं है। वह तो एक-दूसरे के पक्ष के विचार समझने में भी असमर्थ हैं। साधारण लोग तो कम-समझी की वजह से दूसरों के ख़याल और काम के बारे में नहीं समझ सकते और समझदार लोगों को जमाती बंटवारा दूसरों को समझने से वंचित रखता है। इससे हम देखते हैं कि जमाती बंटवारे के अलावा हालात भी अमीरों को ग़रीबों की असली हालत से परिचित नहीं होने देते। मनुष्य के विचार आमतौर पर उसके तज़ुर्बे पर निर्भर हुआ करते हैं और अमीर लोगों को ग़रीबों की हालत का कुछ भी तज़ुर्बा नहीं।”[4]
लालाजी अभी भी समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पाए। उन्हें यह तो पता था कि अमीरों और ग़रीबों में प्यार तथा हमदर्दी नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, इसका वह वास्तविक कारण नहीं जान सके। असल में उनका सिद्धांत और दृष्टिकोण वर्गीय था, जबकि भारत की समस्या जातीय है। इसलिए उनका ध्यान ब्राह्मण-धर्म के उस सिद्धांत की ओर नहीं गया, जो इस समस्या की जड़ में है। अगर वह अमीर-ग़रीब की समस्या का कारण ब्राह्मण-धर्म में तलाश करते, तो वह उन्हें वर्ण-व्यवस्था में मिल जाता। हालांकि भगत सिंह ने ‘अछूत समस्या’ पर अपने लेख में इस कारण को पकड़ा था, पर सिर्फ़ अछूत-मामले में। उन्होंने लिखा है कि हमारे पूर्वज आर्यों ने इन्हें नीच कहकर अलग किया और फिर उनमें पूर्वजन्म का दर्शन थोप दिया, ताकि वे विद्रोह न कर सकें।[5] लेकिन भगत सिंह यह नहीं देख सके कि इसी दर्शन ने अमीरी और ग़रीबी को भी पैदा किया है और अमीरों को ग़रीबों के प्रति संवेदनहीन बनाया है। भारत की बहुसंख्यक ग़रीब आबादी जिस शूद्र-अतिशूद्र वर्ग से आती है, उसकी अछूत, नीच और ग़रीब स्थिति वर्ण-व्यवस्था के कारण ही है, जिसमें ये शिक्षा और स्वतंत्र जीविका आदि के समस्त अधिकारों से वंचित वर्ग हैं। इस व्यवस्था को आज भी ब्राह्मण अपने पूर्वजों की आदर्श और परिपूर्ण व्यवस्था मानते हैं, और विश्वास करते हैं कि उनके पूर्वजों को अनंत काल तक देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। ब्राह्मणों ने इन वर्गों की अछूत, नीच और ग़रीब स्थिति को अनंत काल तक बनाए रखने के लिए उन पर पूर्वजन्म के कर्मफल को थोपा, और तमाम मनगढ़ंत और हास्यास्पद कहानियां लिखकर और उन कहानियों को कथा-सत्संगों में प्रचारित कराके उनके मनों में इस धारणा को मज़बूत कर दिया कि वे अपने पूर्वजन्म में किए गए पापों के कारण ही इस जन्म में अछूत, नीच, और गरीब बने हुए हैं; उनसे यह भी कहा गया कि उनके लिए वर्ण-व्यवस्था में जो कर्म और कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, वे उनके अनुसार इस जीवन में आचरण करें, तो अगले जन्म में उच्च कुल में पैदा होंगे। इस दर्शन के तहत जब किसी का अछूत होना, नीच होना और ग़रीब होना उसके पूर्वजन्म के पापों का फल है, तो कोई भी उच्च वर्ण का व्यक्ति उसके प्रति अपनी सहानुभूति और संवेदना क्यों व्यक्त करेगा? इसी दर्शन ने ब्राह्मणों, ठाकुरों और बनियों को ग़रीबों के प्रति कठोर, निर्दयी और निष्ठुर बनाया और उन्हें अलगाववादी बनाया। दलितों और शूद्रों की अलग बस्तियां इसी अलगाव के कारण अस्तित्व में आईं, जिनमें द्विज वर्णों के लोग जाना भी पसंद नहीं करते।
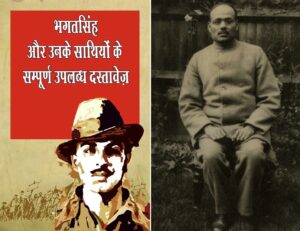
सवाल है कि इन पीड़ित वर्गों ने विद्रोह क्यों नहीं किया? इसका एकमात्र कारण पूर्वजन्म के कर्मफल की धारणा ही नहीं है, बल्कि वे उपाय भी हैं, जो मनु ने समाज-व्यवस्था को संरक्षित करने के लिए किए थे। डॉ. आंबेडकर ने एक जगह लिखा है कि विद्रोह के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं– पहली, अन्याय का बोध होना; दूसरी, यह जानने की क्षमता कि कोई अन्याय से पीड़ित है; और तीसरी, हथियारों का होना। मनु ने विद्रोह को रोकने के लिए ये तीनों ही स्थितियां समाप्त कर दीं। उसने अपनी कानून-व्यवस्था में शूद्रों को आगे बढ़ने के अवसर देने पर रोक लगाईं, शिक्षा का अधिकार देने पर रोक लगाई, और हथियार रखने के अधिकार पर रोक लगाई। दूसरी ओर, उसने पीड़ितों के विद्रोह को दबाने के लिए द्विजों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें आगे बढ़ने, शिक्षा प्राप्त करने, हथियार रखने के सारे अधिकार दिए। इस प्रकार शक्ति और हिंसा के इस्तेमाल से विद्रोह को दबाकर समाज-व्यवस्था को सुरक्षित रखने का यह एकमात्र उपाय मनु ने किया था।[6] इसी व्यवस्था ने एक बड़ी आबादी को अछूत, नीच और ग़रीब बनाकर रखा, और उनके प्रति शेष समाज को निष्ठुर बनाया।
ऐसा क्या कारण था कि भारतीय समाज-व्यवस्था को जितनी गहराई से पेरियार रामासामी नायकर और डॉ. आंबेडकर जैसे दलित-बहुजन विचारकों ने समझा, उतनी गहराई से न तिलक, न गांधी, न भगत सिंह और न उनके साथी और न लाला हरदयाल जैसे राष्ट्रवादी चिंतक समझ सके? इसका एक ही कारण था कि ये वर्ण-व्यवस्था और ब्राह्मण-दर्शन से पीड़ित वर्ग नहीं थे, बल्कि लाभान्वित वर्ग थे। वे अस्पृश्य नहीं थे और न अधिकार-वंचित थे, इसलिए वे अछूतों के प्रति संवेदनशील तो हो सकते थे, पर उनके सामाजिक स्तर की पीड़ा का अहसास नहीं कर सकते थे, जो उन्हें समस्या के मूल में ले जाने के लिए प्रेरित करता। संक्षेप में वे समाज में निम्न वर्गों के विद्रोह को दबाने वाले वर्गों से आते थे।
लाला हरदयाल आगे एक और दिलचस्प बात लिखते हैं–
“मैं आज यह साबित करना चाहता हूं कि पिछले तीस सालों से (यानी 19वीं सदी के तीन दशकों में) जो शैक्षणिक और राजनीतिक लहरें उठीं, उनसे हिंदुस्तान के आम लोगों ने बहुत कम लाभ उठाया, क्योंकि ऊंचे दर्जे के कहे जाने वाले लोग ही इन लहरों को उठाते थे। इसलिए इनके आदर्श भी इनके जमाती रंग में रंगे रहते हैं। हर एक लहर, इस लहर के उठाने वाले लोगों का असली निचोड़ हुआ करती है। निचले दर्जे के सुधारक लोग ग़रीब किसानों और मज़दूरों के अंदर घुसकर इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। वे अपनी जमात के दुःख और तकलीफ़ें ही समझ सकते हैं। उनका आदर्श ही उनके वर्गगत तंग दायरे में चला जाता है। वह इस काम को, जोकि इन दोनों जमातों को अलग-अलग करता है, लांघ नहीं सकते।”
इसके बाद वह लिखते हैं–
“मैं यह लेख केवल इसलिए लिख रहा हूं कि किसान और मज़दूर ही हमारे प्यार के हक़दार हैं। अंग्रेज़ी अदब से परिचित लोग कार्लाइल के प्रसिद्ध उसूल को कई बार पढ़ चुके होंगे कि ‘मैं केवल दो ही आदमियों की इज़्ज़त और उनसे मुहब्बत करता हूं, किसी तीसरे की नहीं।’ मैं एक क़दम और आगे बढ़ता हूं और कहता हूं कि मैं केवल एक आदमी को ही प्यार और इज़्ज़त की निगाह से देखता हूं, किसी दूसरे को नहीं और वह है ग़रीब मज़दूर (किरती), जो दुनिया की दौलत पैदा करता है?”[7]
लेकिन सवाल यह है कि भारत में दौलत पैदा करने वाले ये किरती यानी मज़दूर पूंजीवाद के ख़िलाफ़ संगठित क्यों नहीं हो सके और बग़ावत क्यों नहीं कर सके? इस सवाल पर समाजवादी चिंतक विचार नहीं करते। इस सवाल का उत्तर भारत के ब्राह्मणवाद में है, जिसका दूसरा नाम मनु की समाज-व्यवस्था है। जैसा कि कहा गया, भारत के समाजवादी उच्च और निम्न, अमीर और ग़रीब तथा मालिक और मज़दूर ये दो वर्ग मानते और जानते हैं, हालांकि ऐसी कोई हठधर्मिता कार्ल मार्क्स में नहीं थी। मार्क्स ने एक तीसरे ‘मध्यवर्ग’ को भी स्वीकार किया था। सामाजिक स्तर के हिसाब से मध्यवर्ग में भी कई वर्ग हैं। सच तो यह है कि भारतीय समाज आरंभ से ही वर्गीय समाज रहा है, पर सामंतवाद और ब्राह्मणवाद ने इसे एक कठोर जातिवादी समाज बना दिया। यह जातिवाद ही भारतीय समाज की वर्गीय एकता में बाधा बना हुआ है। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के बारे में लिखा था– “कांग्रेस सर्वहारा संगठन नहीं है। इसलिए वह ज़मींदारों और पूंजीपतियों को अपने संगठन से निकाल नहीं सकता। यदि कांग्रेस को दक्षिण और वाम दृष्टि से देखा जाए, तो उसमें एक दक्षिणपंथी किनारा है, एक वामपंथी अल्पमत है और विशाल मध्यवर्ती जनसमूह है, जो वाम-मध्य के सन्निकट है। गांधीवादी समूह इसी मध्यवर्ती वाम-मध्य का अंग है। राजनीतिक दृष्टि से यह प्रमुख रूप से वाम है; सामाजिक दृष्टि से इसके वामपंथी रुझान हैं, लेकिन प्रधानत: यह मध्य है। किसानों के मामले में, यह किसानों के पक्ष में है।”[8] लेकिन यह समूह सामाजिक और राजनीतिक किसी भी दृष्टि से ब्राह्मणवाद के विरुद्ध कभी नहीं रहा, और इस आधार पर वह अछूतों के वैधानिक अधिकारों के पक्ष में भी कभी नहीं रहा।
कांग्रेस और उसके नेताओं– गांधी-नेहरू आदि के बारे में एक आकलन डॉ. आंबेडकर का भी था। उन्होंने लिखा है– “शासक वर्ग के सदस्य इस तथ्य से हमेशा सचेत रहते हैं कि वे शासक वर्ग से हैं, और शासन करना ही उनका लक्ष्य है। तिलक यह कभी नहीं भूल सके कि वह ब्राह्मण हैं और शासक वर्ग के हैं। ठीक यही बात जवाहरलाल नेहरू और उनकी बहन विजय लक्ष्मी के बारे में कही जा सकती है। नेहरू को समाजवादी और जातिवाद में विश्वास न करने वाला माना जाता है, पर पट्टाभिसीतारमैया ने ‘लाइफ ऑफ़ पंडित जवाहर लाल नेहरू’ की भूमिका में लिखा है कि नेहरू ब्राह्मण होने पर गर्व करते थे। इसी तरह 1940 में जब दिल्ली में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा गया कि जनगणना में जाति का उल्लेख न किया जाए तो विजय लक्ष्मी ने यह कहकर उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था कि उन्हें ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आता कि वह अपने ब्राह्मण-रक्त पर गर्व न करें। वल्लभभाई पटेल भी इसी विचार के हैं कि वह शासक जाति से हैं। ये नेता (गांधी, नेहरू, तिलक, पटेल आदि) केवल इसी भावना से ग्रस्त नहीं थे कि वे शासक वर्ग से हैं, बल्कि इस विचार से भी ग्रस्त थे कि दास वर्ग के लोग तिरस्कार करने योग्य हैं, उन्हें दास बने रहना चाहिए और उन्हें कभी शासन करने की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। तिलक ने शोलापुर में कहा था कि “मैं नहीं समझता कि तेली, तंबोली, धोबी आदि निम्न वर्गों के लोग विधान सभाओं में जाकर क्या करेंगे? वास्तव में उन्हें ऐसे नीच विचार सार्वजानिक मंचों पर प्रकट करने में न लज्जा आती थी और न पश्चाताप होता था।”[9]
लाला हरदयाल किसानों और मज़दूरों को ही एकमात्र ग़रीब वर्ग समझते थे, लेकिन उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था कि इस वर्ग में यह जानने की चेतना क्यों पैदा नहीं हुई कि वे क्यों ग़रीब हैं? वह यह तो कहते हैं कि जो लहरें उठीं, वे मध्यवर्ग से उठीं, और उनमें किसान-मज़दूरों की भागीदारी नहीं थी। लेकिन क्या उनकी ‘ग़दर पार्टी’ में किसान-मज़दूर थे? क्या भगत सिंह की नौजवान सभा में गरीब, मज़दूर, और अछूत थे? भारत में किसान-मज़दूर और निम्न वर्गों से कोई पार्टी बनी थी, तो वह सिर्फ़ डॉ. आंबेडकर की ‘इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी’ थी, जिसने क़ायदे से ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी थी। लेकिन इसे अछूतों की पार्टी कहा गया और गैर-अछूत किसानों और मज़दूरों ने इस पार्टी को अपना समर्थन नहीं दिया। डॉ. आंबेडकर ने इस पार्टी का गठन वर्ग-चेतना और वर्ग-हितों के आधार पर किया था। उन्होंने 1938 में दलित वर्गों के कामगारों को संबोधित करते हुए कहा था कि इस देश के श्रमिकों के दो शत्रु हैं, एक ब्राह्मणवाद और दूसरा पूंजीवाद। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को नकारता है, इसलिए श्रमिक वर्ग संगठित नहीं हो पाते। इसलिए ब्राह्मणवाद से लड़े बिना पूंजीवाद से नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि ब्राह्मणवाद श्रमिक वर्ग की एकता में बाधक है।[10] एक अन्य सभा में, जो खोती-प्रथा, ईनामदार-प्रथा और ज़मींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार से क़ानून बनाने की मांग करने के संबंध में हुई थी, डॉ. आंबेडकर ने कहा था, “किसानों और मज़दूरों को अपनी ग़रीबी के कारण जानना ज़रूरी हैं, जो उन्हें अमीरों और शोषकों में मिलेंगे।”[11] एक अन्य भाषण में, जो उन्होंने ट्रेड यूनियनों को राजनीति में प्रवेश करने के संबंध में दिया था, उसमें कहा था–“श्रमिक वर्ग में एकता पैदा करने के लिए उन्हें यह बताया जाना ज़रूरी है कि जो अधिकार वे दूसरे मज़दूरों को देने के लिए तैयार नहीं हैं, उसके लिए उनका दावा ग़लत है। एकता पैदा करने का सही तरीक़ा यह है कि जो मज़दूर सामाजिक भेदभाव मानता है, वह सिद्धांत रूप में ग़लत है और मज़दूरों की एकता के लिए बाधक है। दूसरे शब्दों में, यदि हमें मज़दूरों को एक श्रेणी में संगठित करना है, तो मज़दूरों में मौजूद ब्राह्मणवाद को जड़ से नष्ट करना होगा।”[12]
लाला हरदयाल ने अपने लेख में आंदोलनात्मक लहरों को तीन हिस्सों में बांटा है– राजनीतिक, शैक्षिक और धार्मिक। राजनीतिक लहर से उनका मतलब कांग्रेस की राजनीति से था, जो कौंसिल और असेंबली में हिंदुस्तानियों की सीटें बढ़ाने के लिए चली थी। लाला हरदयाल ने इस लहर को मध्यवर्ग को लाभ पहुंचाने वाली कहकर उसका विरोध किया था। यथा–
“इन लहरों की क़ामयाबी से मध्यम दर्जे के लोगों को ही लाभ पहुंचता है। उन्होंने कभी बेगार, प्लेग आदि मर्ज़ों के विरुद्ध बंदोबस्त करने की कोशिश नहीं की। न कभी लगान, नमक-टैक्स, आबियाना कम करवाने या लोगों की शिक्षा का ठीक प्रबंध किया है, हालांकि यही ज़रूरी सवाल हैं, जिनके हल हो जाने से जनता को लाभ हो सकता है। बेचारे मज़दूर या किसान को सिविल सर्विस या पंजाब कौंसिल से क्या लाभ है? वह इज़्ज़त नहीं चाहता, पदवी नहीं चाहता। हां, वह रोटी, आरोग्यता और आज़ादी ज़रूर चाहता है।”[13]
आपने देखा? लाला हरदयाल का कितना दकियानूसी चिंतन है? ये भी उच्चता की ग्रंथि से उसी तरह ग्रस्त थे, जिस तरह तिलक ग्रस्त थे, जिन्होंने कहा था कि तेली-तंबोली विधानसभाओं में जाकर क्या करेंगे? ये कह रहे हैं कि मज़दूर या किसान सिविल सर्विस या कौंसिलों में जाकर क्या करेंगे? लाला हरदयाल चाहते थे कि मज़दूर और किसान का बेटा भी मज़दूर और किसान ही बनकर जिए। वह पढ़-लिखकर शासन और प्रशासन में कोई भूमिका न निभाए। वह यही चाहते थे कि शासन और प्रशासन में उच्च जातियों का ही प्रभुत्व और वर्चस्व बना रहे, उसमें किसान और मज़दूर प्रवेश न करे। इसलिए लाला हरदयाल यह नहीं सोच सके कि अगर किसान और मजदूर कौंसिलों में नहीं जाएंगे, तो वहां उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? क्या वही अमीर, ज़मींदार और उच्च जातियों के लोग कौंसिलों में किसानों और मज़दूरों का भी प्रतिनिधित्व करेंगे, जो उनके जन्मजात शोषक हैं? अगर किसान और मज़दूर वर्गों के लोग कौंसिलों में नहीं जायेंगे, तो वे अपनी आवाज़ कैसे उठाएंगे? वे अपने हित में क़ानून कैसे बनाएंगे? अगर किसान और मज़दूर वर्ग के लोग सिविल सर्विस में नहीं जायेंगे, शासन-प्रशासन में अपनी भूमिका नहीं निभायेंगे, तो वे अपने वर्गों पर होने वाले अन्याय को कैसे दूर करेंगे? अगर अन्याय और शोषण करने वाले वर्गों के लोग ही शासक और प्रशासक बने रहेंगे, तो कभी भी समाज में परिवर्तन नहीं आएगा, यथास्थिति ही क़ायम रहेगी। एक तरफ़ लाला हरदयाल कांग्रेस की राजनीति पर यह आरोप लगाते हैं, हालांकि सही लगाते हैं कि वह मध्य वर्ग के हितों के लिए काम करती है, और दूसरी तरफ़ स्वयं किसानों और मज़दूरों को राजनीति में आने का विरोध करते हैं। क्या उनकी यह सोच किसानों और मज़दूरों के हित में थी?
शैक्षणिक लहरों के बारे में लाला हरदयाल ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है–
“शैक्षणिक लहरों के लिए तो हमारी बहुत-सी ताक़त ख़र्च हुई और बहुत से नेक मर्द और औरतों की ज़िदगियां इनके लिए वक्फ़ हो गईं। लेकिन परिणाम यहां भी निराशा भरा हो गया है, क्योंकि इससे भी मध्यम वर्ग को ही कुछ लाभ पहुंच सका है। हमारे बहुत से नेताओं ने शहरों में अलग-अलग क़ौमों, बिरादरियों और सभाओं की ओर से स्कूल-कॉलेज खोल दिए, लेकिन क्या हम पूछ सकते हैं कि उन देशभक्तों के दिलों में स्कूल-कॉलेज खोलने का ख़याल किस तरह पैदा हुआ? और क्यों उन्होंने अपने इस बड़े काम को गांवों में नहीं किया, जिससे ख़र्च तो कम होता, और लाभ अधिक पहुंचता।
“समाज के शैक्षणिक अड्डे केवल इसलिए क़ायम हुए कि मध्यम दर्जे के लोगों के बाल-बच्चे अच्छी तरह कमा सकें। यही वर्ग-रुचि काम कर रही है। दक्षिण के देशभक्तों ने शिक्षा के लिए बहुत क़ुर्बानियां दीं, लेकिन किनकी शिक्षा के लिए? फर्गुसन कॉलेज ने मध्यम वर्ग के लिए हज़ारों नौजवानों को शिक्षा दी। रोजी कमाने और उन्नति करने योग्य बनाया, लेकिन किसानों के लिए इसने क्या किया? इस कालेज में से जितने वकील और प्रोफ़ेसर निकलते हैं, वे बेचारे किसानों के सिरों पर यूं ही ख़ाली बैठे मौज़ मारते हैं। वे भी किसानों का लहू पीने वाली जमात में शामिल हैं।
“स्त्री-शिक्षा का शोर भी मध्यम वर्ग के लोगों का ही मसला है। हमारी कन्या-पाठशालाओं में किसानों की कितनी लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं? असल में गांवों में तो यह सवाल ही नहीं है, क्योंकि वहां तो मर्द भी अनपढ़ हैं। यह सवाल तो तालीमयाफ़्ता नौजवानों के लिए पढ़ी हुई लड़कियों की ज़रूरत से ही पैदा हुआ कि लड़कियों को भी शिक्षा दी जाए। इससे मध्यम वर्ग के लोगों के घर अधिक ख़ुशहाल और आराम वाले बन गए। … उन लोगों के आराम और तरक्क़ी से किसानों और मज़दूरों को कोई लाभ नहीं पहुंच सकता। यदि ये शैक्षणिक लहरें आम लोगों की बेहतरी के लिए जारी की गई होतीं, तो सबसे पहले गांवों में स्कूल खोले जाते, क्योंकि किसी भी मुल्क़ के आम लोगों में प्रारंभिक शिक्षा के बिना जागृति नहीं आ सकती।”[14]
ऐसा प्रतीत होता है कि लाला हरदयाल को किसान-मजदूर की केवल रट लगी हुई थी। उन्हें किसान-मज़दूरों के सामाजिक यथार्थ का ज्ञान नहीं था। वे गांवों के सामाजिक यथार्थ से भी परिचित नज़र नहीं आते। वे मध्यवर्ग के शैक्षणिक लाभ के विरुद्ध थे, और चाहते थे कि प्राथमिक स्तर पर स्कूल खोलने का कार्य गांवों में होना चाहिए था। निश्चित रूप से गांवों में शैक्षणिक विकास ज़रूरी था, जो भारत में स्वतंत्रता मिलने के बाद, स्वदेशी सरकारों ने भी नहीं किया। भारत के गांव आज भी शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। आज भी गांवों में प्राथमिक स्कूलों की भौतिक स्थिति अत्यंत ख़राब और दयनीय है। लाला जी ने यह सवाल सही उठाया कि देशभक्तों ने शहरों में स्कूल-कॉलेज खोले, जिनसे मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचा; और उन्होंने गांवों में स्कूल नहीं खोले। इसका कारण या तो लालाजी जान नहीं सके या जान-बूझकर उस कारण पर गए नहीं। वह कारण जातिवाद है। इसी जातिवाद ने भारत के उन देशभक्तों ने, जो शासक भी थे, स्वतंत्रता के बाद भी गांवों में शैक्षणिक विकास नहीं होने दिया। गांवों में जिन किसान-मज़दूरों की बात लालाजी करते हैं, उनमें कोई भी उच्च जाति का नहीं था। वे सभी निम्न जातियों के, निम्न वर्गीय लोग थे, जिन्हें पढ़ा-लिखा कर बाबू-वकील बनाकर शासक वर्ग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारता? गांवों में स्कूल खोले जाने के विरुद्ध उच्च जातियों के लोग इसलिए भी थे, क्योंकि उनमें अछूतों को भी प्रवेश देना पड़ता। अगर वे ऐसा करते, तो सवर्ण जातियों के लोग विरोध करते, क्योंकि उनके बच्चे अछूत बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे। यह तो बात रही, उन स्कूलों की, जो लालाजी के मुताबिक़ देशभक्तों और अलग-अलग बिरादरियों की सभाओं द्वारा खोले गए थे। लेकिन सरकार द्वारा खोले गए स्कूलों का लाभ भी उच्च जातियों को मिला था, क्योंकि उनमें भी अछूतों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। हालांकि, यह भेदभाव अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से नहीं था, बल्कि सवर्णों की तरफ़ से था। एक तो उन स्कूलों में सभी शिक्षक ब्राह्मण थे, जो अछूतों की छाया से भी बचते थे, और दूसरे, गांव के सवर्ण हिंदू अछूतों की शिक्षा के ख़िलाफ़ थे। जिस वर्ष लाला हरदयाल ने यह लेख लिखा, उसके सात साल बाद की, यानी 1935 की घटना है। बंबई सरकार ने सरकारी स्कूलों में अछूत बच्चों को प्रवेश दिए जाने का आदेश जारी किया था। इससे खुश होकर गुजरात के कविठा गांव के अछूतों ने गांव के सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजने का निश्चय किया। तभी वहां के सवर्ण हिंदुओं ने अछूतों को हुक्म दिया कि वे अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए जोर न दें। लेकिन अछूतों ने इस हुक्म की परवाह नहीं की और अपने चार बच्चों का स्कूल में दाख़िला करा दिया। अगले ही दिन सवर्णों ने अपने बच्चे स्कूल से निकाल लिए। इसके कुछ समय बाद गांव के सवर्ण हिंदुओं ने, जिनमें सवर्ण महिलाएं भी शामिल थीं, अछूतों के घरों पर हमला कर दिया। उनके घरों को तोड़-फोड़ के बर्बाद कर दिया, जो भी अछूत स्त्री-पुरुष घर में मिला, उनकी लाठियों से बेरहमी से पिटाई की। हिंदुओं के आतंक से पीड़ित अछूतों को गांव छोड़ना पड़ा।[15]
लालाजी का यह कहना कि मध्यम वर्ग के हज़ारों नौजवान शिक्षा पाकर किसानों के लिए कुछ नहीं करते और वे किसानों का लहू पीने वाली जमात में शामिल हो जाते हैं, ग़लत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शिक्षित होकर भी किसान और मज़दूर-विरोधी विचारधारा रखता है, तो यह शिक्षा का नहीं, उसके संस्कारों का दोष है, जो उसके सामंती परिवेश ने उसे दिए हैं। इसमें संदेह नहीं कि हिंदुओं में, और ख़ास तौर से ब्राह्मणों और अन्य उच्च जातियों में, आधुनिक शिक्षा कोई वैचारिक परिवर्तन नहीं ला सकी। देश के महानतम ब्राह्मण और सवर्ण नेता, जैसे तिलक, नेहरू, गांधी, मालवीय, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, हेडगेवार, सावरकर, आदि सभी अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त थे, लेकिन इसके बावजूद इनमें से किसी भी नेता ने अपने रूढ़िवादी विचारधारा का त्याग नहीं किया था। ये सभी अपने उच्च वर्ण की श्रेष्ठता-बोध से ग्रस्त थे, जो वास्तव में एक व्याधि है, जिससे वे अंग्रेज़ी शिक्षा पाकर भी मुक्त नहीं हुए थे। लेकिन इसके विपरीत उसी अंग्रेज़ी शिक्षा ने जोतीराव फुले, डॉ. आंबेडकर, पेरियार रामासामी नायकर आदि बहुत से निम्न वर्गों के व्यक्तियों के आगे एक नई दुनिया खोल दी थी, और उनका समग्र रूपांतरण हो गया था। इन्हीं लोगों ने भारत की समस्या को ठीक से समझा और इन्हीं लोगों ने किसानों और मज़दूरों की आवाज़ उठाई, क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि सामंती और ब्राह्मणवादी नहीं थी, बल्कि निम्न वर्गीय परिवेश की थी।
मध्यवर्ग उच्च जातियों से बना है, इसमें संदेह नहीं; इसलिए जैसाकि डॉ. आंबेडकर का मानना था कि यह वर्ग देश का नेतृत्व करने के लिए योग्य नहीं है। “सही नेतृत्व के लिए जिस आदर्शवाद और स्वतंत्र विचार की आवश्यकता होती है, वह सिर्फ मज़दूर वर्ग में ही संभव है। कुलीन उच्च वर्ग में आदर्शवाद हो सकता है, लेकिन स्वतंत्र विचारधारा नहीं हो सकती। मध्यवर्ग अवसरवादी होता है, उसमें न कोई आदर्श होता है और न स्वतंत्र विचारधारा होती है। लेकिन श्रमिक वर्ग में आदर्शवाद और स्वतंत्र विचारधारा दोनों संभव हैं। उसमें नई समाज-व्यवस्था के लिए भूख होती है। यही भूख उनकी आशा है, जो श्रमिक वर्ग को जीवित रखती है। यह वह जिजीविषा है, जिसके लिए वह संघर्ष में उतरता है और एकजुट रहता है। श्रमिक वर्ग का नेतृत्व ही भारत और भारतीयों को स्वाधीनता और नई समाज-व्यवस्था दे सकता है।”[16]
डॉ. आंबेडकर ने यह बात 1943 में कही थी, हालांकि वह इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के गठन के समय से समाजवादियों से – कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध, जो पूंजीपतियों, ज़मींदारों और ब्राह्मणों की पार्टी थी, और जिससे किसानों, मज़दूरों और निम्न वर्गों के हित में काम करने की कोई उम्मीद नहीं थी – समाजवादी मोर्चा बनाने का आह्वान करते आ रहे थे, लेकिन चूंकि कम्युनिस्ट और समाजवादी राजनीति भी ब्राह्मणों और उच्च जातियों के हाथों में थी, इसलिए वे कांग्रेस के साथ ही अपने आपको जोड़े रहे। परिणाम वही हुआ, पूंजीपति, नवाब, राजे-महाराजे, ज़मींदार और ब्राह्मण ही स्वतंत्र भारत के शासक बने। और इन शासकों ने सत्ता की बागडोर हाथ में आते ही, भारत में राजनीतिक लोकतंत्र तो क़ायम किया, पर भारतीय समाज को हिंदू समाज ही बनाकर रखा, उसे लोकतांत्रिक समाज नहीं बनने दिया।
संदर्भ :
[1] सत्यम, भगतसिंह और उनके साथियों के संपूर्ण उपलब्ध दस्तावेज़, राहुल फाउंडेशन, लखनऊ, संस्करण 2014, परिशिष्ट सात, पृष्ठ 526 (यह लेख जगमोहन सिंह और चमन लाल द्वारा संपादित ‘भगतसिंह और उनके साथियों के दस्तावेज़’ राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2010 में पृष्ठ 217 पर है)
[2] वही, पृष्ठ 527-528
[3] वही, पृष्ठ 529
[4] वही, पृष्ठ 529-530
[5] वही, देखिए, अछूत समस्या, पृष्ठ 268
[6] डा. बाबासाहेब आंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, वाल्यूम 12, संस्करण 1993, देखिए, प्रिजर्वेशन ऑफ़ सोशल आर्डर, पृष्ठ 727-28
[7] सत्यम, उपरोक्त, पृष्ठ 530-531
[8] जवाहरलाल नेहरू, दि यूनिटी ऑफ़ इंडिया, पृष्ठ 121-22, साभार, कृष्णकांत मिश्र, समाजवादी चिंतन का इतिहास, भाग तीन, ग्रंथ शिल्पी, दिल्ली, 2002, पृष्ठ 297
[9] डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, वाल्यूम 9, 1990, देखिए, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू दि अनटचेबिल्स, पृष्ठ 208-209
[10] सोर्स मटेरियल ऑन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एंड दि मूवमेंट ऑफ़ अनटचेबिल्स, वाल्यूम 1, 1982, पृष्ठ 165
[11] डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, वाल्यूम 17, पार्ट 3, 2000, पृष्ठ 170
[12] वही, पृष्ठ 173
[13] सत्यम, उपरोक्त, पृष्ठ 533
[14] वही, पृष्ठ 534-535
[15] डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, वाल्यूम 5, 1989, देखिए, अनटचेबिल्स एंड लॉलेसनेस, पृष्ठ 41-43
[16] वही, वाल्यूम 10, संस्करण 1991, देखिए, व्हाई इंडियन लेबर इज डिटरमाइंड टू विन द वार, पृष्ठ 43
(संपादन : नवल/अनिल)





