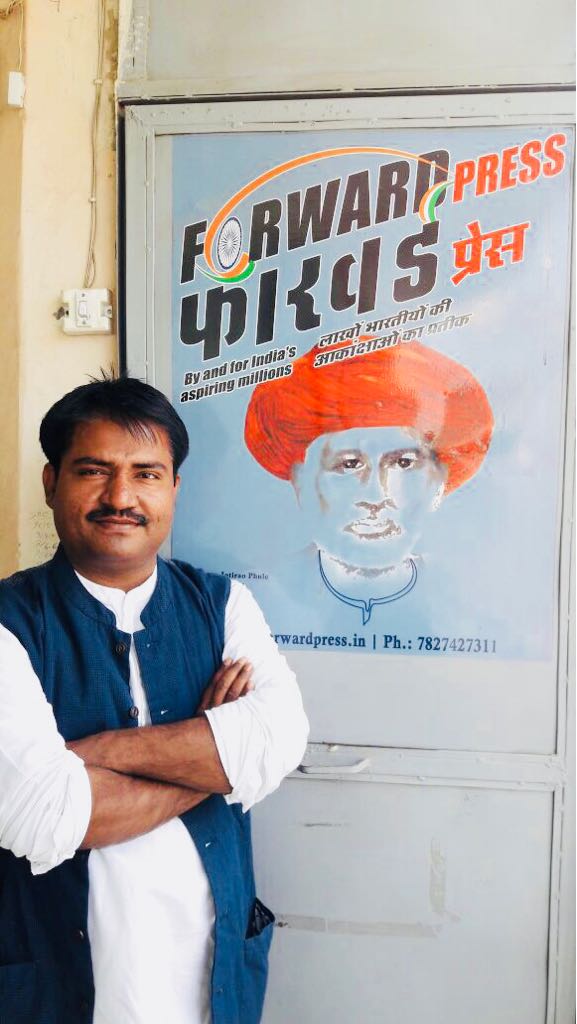साहित्यिक विधाओं में गजलाें का सृजन भी शामिल है। हालांकि इसे एक खास धर्म अथवा भाषा-भाषियों तक सीमित मान लिया जाता है। लेकिन आंबेडकरवादी मूल्यों के आधार पर गजलों के माध्यम से ब्राह्मणवादी परंपराओं को चुनौती देना बी.आर. विप्लवी की खासियत रही है। बीते 15 नवंबर, 2024 को वे दिल्ली में थे। इस मौके पर उन्होंने अपने जीवन और दलित साहित्य (खासकर गजलों के सृजन से संबंधित) के बारे में नवल किशोर कुमार से बातचीत की। प्रस्तुत है इस बातचीत के संपादित अंश का अंतिम भाग
पहले भाग से आगे
यदि हम दलित साहित्यकारों की बात करें तो आपको सबसे ज्यादा किन्होंने प्रभावित किया?
देखिए क्रांतिकारी दो तरह के लोग रहे। एक वे, जिन्होंने अपने लेखन से ज़्यादा बड़ा परिवर्तन लाया। साधारण भाषा में ही लिखा, लेकिन परिवर्तन किया। इसलिए पुरोधा तो उनको ही कहेंगे। जैसे ललई सिंह यादव और चंद्रिकाप्रसाद जिज्ञासु जैसे नायकों ने अपनी भाषा को सहज रखा और तथ्यों को अधिक से अधिक संप्रेषित किया। यह उन्होंने बाबासाहब की प्रेरणा से किया। ये बाबासाहब से प्रत्यक्ष मिलने वाले लोग थे। बाद के दौर में लिखने वालों में श्यौराज सिंह ‘बेचैन’ पसंद आए। उनकी आत्मकथा है– ‘मेरा बचपन मेरे कंधों पर’, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं मां के सामने उसका वाचन करता था। ऐसे कारुणिक भावों वाले प्रसंग थे कि उन्हें हुए पढ़ते हुए हम मां-बेटे रो पड़ते थे। श्यौराज सिंह बेचैन की आत्मकथा में उनकी मां कहती हैं कि “चलो एक बात अच्छो है। यह खाय के हम सब मरि जाएंगे। कोई रोवनहारो ना बचौगो।”
उनका यह कथन पढ़कर एकदम से रोना आता है कि… क्या कथा है, सब बीमार पड़े हुए हैं ज़हरीली चीज़ खाकर। सबको उल्टी-दस्त हो रही है।
मुझे डॉ. धर्मवीर ने भी प्रभावित किया है। मैं तो कहूंगा कि मुझे इन सभी लोगों के लेखन ने प्रभावित किया है और इन सभी ने मुझे प्रभावित किया।
श्यौराज सिंह बेचैन से दोस्ती हो गई। आज भी उनके घर आना-जाना होता रहता है। कंवल भारती जी से मेल-मुलाकात उतनी अनौपचारिक नहीं है, औपचारिक है। लेकिन उनको भी मैं बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि वे बड़ा काम करते हैं और लगातार करते हैं। उनके खरी-खरी लिखने से कुछ लोग बिदक जाते हैं। लेकिन उन्हें जो अच्छा लगता है, वही लिखते हैं।
देखिए कोई भी सच्चा लेखक किसी खूंटे से नहीं बंधा होता है। उसका अपना स्वतंत्र विचार होता है। अब दलित साहित्य में कोई कुछ भी लिख दे और यदि यह मान लिया जाय कि दलित साहित्य है तो हम बस मानते ही चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा होगा तो हमारा लेखक होना बेकार है। जो तार्किक होगा, जो प्रासंगिक होगा, जिससे सबका भला होने वाला होगा, हम उसी की बात कहेंगे।
आज दलित साहित्य की जो स्थिति है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
इस समय दलित साहित्य काफ़ी समृद्ध हो गया है। पहले यह देखिए कि इसका प्रस्थान बिंदु कहां है। इसका जन्म कैसे हुआ है? वह यातनाओं की कोख से जन्मा है। एक पीढ़ी ने जो सहा है, उसने उसे लिखा। अब आज की पीढ़ी के लिए वह बात नहीं है। वह दूसरे रूप में आ गई है। तो आज की पीढ़ी नए तरह से लिख रही है। अभी तक तो जो पिछली पीढ़ी ने लिखा है, उसने दलित साहित्य को काफी समृद्ध कर दिया है। बहुत सारी बातें कविताओं के ज़रिए आईं। नाटक में काम हुआ। कहानी में काम हुआ। कहीं कम, कहीं ज्यादा। सबसे ज्यादा आत्मकथाओं ने शोर मचाया-सार्थक आवाज़ उठाई, क्योंकि वह बिल्कुल जीती-जागती मिसाल थीं। लोगों ने उसको जीया है और एकदम से, बिल्कुल, गवाह बन करके खड़े हैं। कहीं आप काट ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें काल्पनिक चीज़ें नहीं हैं। कहानी में घटनाएं कहीं और की हो सकती। कहानीकार पृष्ठभूमि कहीं और से लेता है, पात्र कहीं और से लेता है। मिला-जुला कर लिखता है। लेकिन आत्मकथा में लेखक तो खुद ही जिम्मेदार है। झूठ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा आत्मकथाएं प्रभावित करती रही हैं। श्यौराज सिंह बेचैन की आत्मकथा का सात-आठ भाषाओं में अनुवाद हो गया। इस तरह दलित साहित्य अभी तक काफी समृद्ध हुआ है। लेकिन अभी आगे जो साहित्य है, उसको अपनी ओज और दिशा बदलनी होगी और यह बदल भी रहा है। इसकी वजह यह कि जो यातना है, उसका रूप बदल गया है। अब रूप बदल गया तो इस बदले रूप को पकड़ना पड़ेगा। इतना ज़्यादा लिखा जाना चाहिए कि वह सब तक पहुंचे। वेद, पुराण या जितने भी पाखंडी साहित्य हैं, वर्चस्ववादी जानते हैं कि ये झूठ हैं और वे कहते भी हैं कि हां है, लेकिन, वह आस्था का सवाल है। तो उन्होंने लिख दिया एक झूठ और वही फैल गया चारों ओर। और दलित-बहुजन सच को भी उस मात्रा में नहीं बोल पा रहे हैं। उस आवेग में नहीं ला पा रहे हैं। इसलिए यह एक जिम्मेदारी है, जो आज दलित-बहुजन पीढ़ी लिख सकती है। अभी देखिए कि अयोध्या में राम मंदिर बना। लोगों ने आलोचना की कि राम तो मिथक है। उसका कोई इतिहास नहीं है। वर्चस्ववादियों ने भी कहा कि राम का संबंध आस्था से है, इतिहास से नहीं है। और देखिए कि बुद्ध जिनका संबंध इतिहास से है, वह किनारे कर दिए गए। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी बात को किस मात्रा में, किस आवेग से, कितने लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए दलित साहित्य पर विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। या फिर आप चाहे इसे बहुजन साहित्य कहिए।

क्या आप भी आत्मकथा लिखने का विचार रखते हैं? यदि हां तो वह ग़ज़ल के रूप में होगी या गद्य के रूप में?
जहां तक मेरी आत्मकथा का सवाल है, वह मेरे दिमाग़ में है। जो मैंने संस्मरण बताए, उससे भी आपको लगा होगा कि आत्मकथा लिखी ही जानी चाहिए। देखता हूं कि कब तक लिख पाता हूं। लेकिन उसका रूप गद्य ही होगा। वजह यह कि गद्य सब तक पहुंचता है, सबकी समझ में आता है। ग़ज़ल को सभी लोग समझ नहीं पाते।
आपकी एक कृति का शीर्षक है– ‘तश्नगी का रास्ता’। तश्नगी का मतलब तो तृष्णा है। इससे आपका अभिप्राय क्या है?
देखिए तिश्नगी का मतलब तृष्णा है। इसको समझने के पहले यह देखें कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। लोग कहते हैं कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, पूछिए तो बहुत लोग नहीं बताएंगे। उनका ज्ञान था कि दुख के कारण क्या हैं? उन्होंने 12 प्रकार की दुख उपजाने वाली कड़ियां बताईं, जो केवल एक अविद्या के द्वारा पैदा होती हैं। इस अविद्या से आपका संस्कार बनता है। संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप बनता है। नाम-रूप से षडआयतन, षडआयतन से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से स्पर्श, स्पर्श से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति या जन्म, जाति से जरा-मरण-रोग-शोक-दौरमनस्य पैदा होते हैं। ऐसी बारह कड़ियां हैं। उसमें एक कड़ी है तण्हा (तृष्णा)। नाम-रूप से षडआयतन बनता है। इसे छह आयतन कहते हैं। इस तरह से आते-आते वह जरा-मरण तक जाता है। अब जरा-मरण को रोकने की जो विधि है, उसको कहते हैं अनुलोम-विलोम। एक अनुलोम कारण है और एक निवारण है उसका दुख निरोध। तो इस प्रकार एक ‘तण्हा’ शब्द है, जिसमें जाएंगे तो पाएंगे कि अलग विषय है। इसलिए बीच में मैं उसको छोड़ दे रहा हूं। …प्रतीत्य-समुत्पाद है। उसपर बहुत किताबें हैं। वह बहुत बड़ा विषय है। एक पूरी फिलॉस्फी है। भगवान बुद्ध ने कहा कि इन सब चीजों को जब आदमी देखता है, उससे इंटरैक्शन होता है, उससे पाने की तृष्णा पैदा होती है। इस तरह पाने की प्यास जगती है तो वह दुख का कारण है। अब देखिए कि तण्हा शब्द जो है, पाली का प्राकृत है। इसका सबसे मूल पैशाची है। लोग समझते हैं कि यह पिशाचों की भाषा है। पिशाच का मतलब जिसकी नाक बेढंगी हो, जिसके दांत बड़े-बड़े हों, आंखें बड़ी-बड़ी हों, ऐसा रूप बना दिया। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। ये यहां के जो मूल निवासी हैं, उनकी भाषा है पैशाची। तो तण्हा वहां से है, वह बन गया तृष्ना और यही शब्द फारसी में तिश्नगी हो गया। फिर उर्दू ने एडाप्ट कर लिया उसको। उर्दू में तिश्नगी और तश्नगी दोनो चलता है। तृष्ना से तृष्णा हो गया। ‘तिश्नगी का रास्ता’ नाम मैंने इसलिए उसका रखा कि मुझे समझ में आया कि इस जीवन में तृष्णा ही तृष्णा है। और जो भी रास्ता है तृष्ण की तरफ लेकर जा रहा है। हम हमेशा चाहते हैं कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए या फिर ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला। इसलिए इसका नाम ‘तश्नगी का रास्ता’ रखा। और एक ग़ज़ल संग्रह जो 2004 में इसके बाद प्रकाशित हुआ, उसका नाम है– ‘सुबह की उम्मीद’। ‘सुबह की उम्मीद यूं रोशन रही, इस भरोसे रात काली कट गई’। सुबह की उम्मीद का मतलब है कि आगे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें उससे उम्मीद है कि सुबह होगी, कभी न कभी। रात ही थोड़े रहेगी। यह लड़ाई जो लड़ी जा रही है, उसका फलाफल अच्छा होने वाला है। इसलिए हमें रुकना नहीं है, लड़ाई को छोड़ना नहीं है।
दलित साहित्य के विकास में समालोचना की भूमिका होनी चाहिए, वह कैसी है?
दलित साहित्य में समालोचना विधा को बहुत आगे जाना चाहिए। वहां तक अभी नहीं गई है। और समालोचना किसी भी साहित्य में, किसी भी विधा में उसका महत्वपूर्ण अंग इसलिए है क्योंकि इससे सुधार की गुंजाइशें बनती हैं। कोशिश यह होनी चाहिए कि स्वयं में सुधार व मुख्यधारा में आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, आगे बढ़े। जब तक समालोचना नहीं होती तब तक जिसे नीर-क्षीर विवेक कहा जाता है, वह नहीं होगा। एक समालोचक की दृष्टि यह होनी चाहिए है कि उसको किसी से प्रेम नहीं है, किसी से घृणा नहीं है। जो सच है, जो तर्कपूर्ण है, उसके बारे में विश्लेषण करें। देखिए दलित साहित्य की खासियत यही है और उसे बनाए रखना चाहिए कि वह तर्कसंगत है और सच के करीब है। अगर उसमें भी भावनावश चीजें आती गई या केवल काल्पनिक चीजें जो कि संभव नहीं है, तो निरर्थक होती जाएगी। इनसे हमें परहेज करना चाहिए। समालोचना यह रास्ता दिखाती है। और बहुत से लोग समालोचना को समझते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जबकि इसकी बहुत जरूरत है। दलित साहित्य में समालोचना को अभी और आगे जाना है। अभी यह बहुत सीमित है। इसलिए आप देख रहे हैं कि दलित साहित्य में एक जो अच्छी खासी धारा चल रही थी, अब उसके छोटे-छोटे पॉकेट बन गए हैं और बहुत सारी अनियंत्रित चीजें आने लगी हैं। कोई कुछ भी लिख रहा है तो उसका नाम दलित साहित्य दे दे रहा है। हर साहित्य का एक पैरामीटर होता है। दलित साहित्य का भी अपना एक पैरामीटर है। अगर कोई डॉ. आंबेडकर और बुद्ध की विरासत को संभालने वाले साहित्य के पैरामीटर से जब बाहर होगा तो वह दलित साहित्य कहां रह जाएगा। इसकी तीन कसौटियां हैं– समता, स्वतंत्रता और बंधुता। इन तीनों से जो विचलित होगा, दलित साहित्य कैसे कहा जा सकेगा।
एक झगड़ा बहुजन साहित्य का भी है। कोई दलित साहित्य कहता है तो कोई बहुजन साहित्य। जबकि दलित साहित्य और बहुजन साहित्य, दोनों तो एक ही साहित्य है। नाम को लेकर बहुत से झगड़े आपने देखे होंगे। मैं कहता हूं कि यह सोच ही गलत है कि यदि कोई बहुजन साहित्य कहे, पिछड़ा साहित्य कहे या कि दलित साहित्य कहे। मैंने ऊपर में तीन पैरामीटर की बात कही। देखना होगा कि इनसे आपका कितना लगाव है और आप इसे कितना आगे बढ़ाते हैं, और यह कि कितना विचलन है। इसी चीज को मापना ही समालोचना का काम है।
समस्या यह आती है कि कोई दलित साहित्य है या नहीं है, इसका निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि रचनाकार किस जाति का है। यदि रचनाकार दलित है तो यह सीधे-सीधे मान लिया जाता है कि उसकी रचना दलित साहित्य के खांचे में फिट बैठ जाएगी। कई बार ऐसा होता है यदि उसकी रचनाएं जैसाकि आपने बताया समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के पैरामीटर से अलग हटती नजर आती हैं तब भी माना जाता है कि वह दलित साहित्य है, क्योंकि रचनाकार दलित जाति का है।
हां, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि काट-छांट की जानी चाहिए। बस मान लेने से नहीं होगा कि कुछ भी लिख दिया तो दलित साहित्य हो गया। जबतक बुद्ध के जो पैरामीटर हैं, और डॉ. आंबेडकर के पैरामीटर हैं, जिनकी घोषणा हमने स्वयं की है, का यदि उल्लंघन होता है तो उसे दलित साहित्य नहीं माना जाएगा। यही देखना तो समालोचकों का काम है। टिप्पणीकार हैं, समालोचक हैं, उनका यही काम है।
एक लड़ाई यहां आकर केंद्रित हो जाती है कि कबीर दलित थे कि नहीं थे।
बकवास है। मेरी राय में कबीर को आप गैर-दलित साहित्य और दलित साहित्य में कह कर उनकी टांग नहीं खींच सकते हैं। आप बहुजन साहित्य कह दें या दलित साहित्य कह दें, चाहे जो भी कह दें, कबीर बिल्कुल एक हमारी परंपरा के आदि कवि हैं। उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। इसलिए वे कहां, किस परिवार में पैदा हुए, दलित थे या नहीं थे, कोई मायने नहीं रखता। वस्तुत: वे इसी धारा के कवि हैं और उनकी रचनाएं समता, स्वतंत्रता और बंधुता के तीनों पैरामीटर को पूरा करती हैं। इसलिए वह दलित-बहुजन साहित्य के पुरोधा साहित्यकार हैं। हम इसको बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हैं कि कबीर – जिन्होंने तीनों मानकों को अपने केंद्र में रखा – के जन्म को इस तरह से उधेड़ा जाए।
कबीर को लेकर डॉ. धर्मवीर की जो टिप्पणियां हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है?
डॉ. धर्मवीर ने तो मुझसे एक बार यह भी कहा था कि बुद्ध तो क्षत्रिय थे, उनकी चर्चा आप क्यों करते हैं। तब मैंने उनसे कहा कि बुद्ध क्षत्रिय थे या नहीं, ये कैसे साबित होगा। क्या आप इसे साबित कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा कि मैं ऐसी आदिवासी कौम से हूं, जहां पांच बहने थीं, वे भाइयों से ब्याही गईं। तो… हम क्या बताएं कि हमारी जाति क्या है, हमारा धर्म क्या है। हम तो उसी में पैदा हुए। भाई बहन में शादी होती थी। उसी में पैदा हुए। आप जाति खोदोगे तो बड़े पचड़े हैं उसमें। अब मान लें कि जाति प्रमाणपत्र मिल रहा है। अब कबीर का जाति प्रमाणपत्र खोजेंगे तो यह दिक्कत की बात है न। बुद्ध का जाति प्रमाणपत्र खोजेंगे तो यह दिक्कत की बात है। आस्था से पहले मुख्य चीज है विचारधारा। दलित साहित्य के बारे में कहते हैं कि दलित ही लिख सकता है। दलित के द्वारा दलितों के लिए साहित्य। एक समय तक ठीक बात थी। वह इसलिए कि दलित ने भोगा हुआ है, इसलिए वह सही से लिखेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। इसलिए कहा कि दलित होना जरूरी है। अब कल एक स्त्री ने जो कहा, वह मेरे दिल को छू गई। क्या बात कही उसने। उसने कहा कि होटलों में शेफ पुरुष ही क्यों होते हैं? वैसे यह तो खुशी की बात है कि चलो पुरुष भी किचन में काम कर रहे हैं। लेकिन उसने कहा कि नहीं, स्त्री जब रजस्वला होती है तब वह तीन दिनों तक अछूत मानी जाती है। इससे बचने के लिए पुरुषों ने होटलों में शेफ का काम किया है। देखिए यह बात केवल एक स्त्री ही महसूस कर सकती है। अगर हम कहें कि स्त्री स्त्री के दर्द को सही से जानेगी तो इसमें गलत कुछ नहीं है। स्त्री साहित्य के लिए स्त्री होना अगर जरूरी कहें तो 99 फीसद तो ठीक बात है। ऐसा ही दलित साहित्य के बारे में है। लेकिन हम अपने पुरोधाओं की जाति औऱ वंश खोजेंगे तो अनुलोम-विलोम का चक्कर है। लेकिन अगर कोई समता, स्वतंत्रता और बंधुता को आधार बनाकर लिख रहा है तो दलित ही है, यह भी तो माना जा सकता है।
पुरुषोत्तम अग्रवाल ने जो कबीर का वर्गीकरण करने की कोशिश की है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे?
यह सब दिमागी फितरत है। अपने को मशहूर करने के लिए लोग नये तरीके की चीजें गढ़ देते हैं ताकि वो लाइमलाइट में आ जाएं। कबीर तो बहुत सिंपल आदमी थे। सबके यहां बैठने वाला आदमी, बहुत मस्तमौला आदमी। इसलिए उनके बारे में यह तो नहीं कहा जा सकता कि वे बनिया थे, तेली थे, कुम्हार थे, चमार थे, रैदसिया थे। कबीर की जाति क्यों देखते हैं, उनका काम देखिए, जिससे सबका भला हो रहा है। उनके साहित्य में जो अमृत बरस रहा है, उनकी वाणी में वो देखो। उस अमृत में भीगो न कि उनकी जाति-पाति खोजो। जाति खोजने से क्या होगा। मान लें कि आप कबीर को दलित साहित्य में नहीं रखते हैं तो इससे कबीर को क्या परेशानी हो जाएगी? कुछ भी नहीं। तुम्हें परेशानी होगी। तुम उन्हें कैसे समझते हो, यह तुम्हारा मैटर है। कबीर को जो कहना था, कह दिया। तो ये पुरुषोत्तम अग्रवाल जो ज्ञान बांट रहे हैं, ऐसे ज्ञान बांटनेवालों से मैं कतई सहमत नहीं हूं। ऐसे-ऐसे पुरुषोत्तम अग्रवाल बहुत से हैं। दलितों में भी बहुत से हैं। उसको क्या कहिएगा। हर कौम में दो-चार प्रतिशत लोग ऐसे होते ही हैं।
समाप्त
(संपादन : राजन/अनिल, लिप्यांतरण : समीक्षा)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in