‘कुशवाहा रामप्रकाश’ उन लोगों के बीच एक चर्चित कविता है जो दिनेश कुशवाह को जानते हैं और उनकी कविताओं से प्रेम करते हैं। उनका काव्य संग्रह ‘इसी काया में मोक्ष’ आया तो था 2007 में, मगर यह कविता उससे पहले से सुनी-सुनाई जा रही थी। बीस वर्षों के बाद भी यह कविता ताज़ा मालूम पड़ती है। आज दिनेश जी जब भी बनारस में कविता सुना रहे होते हैं तो लोगों की मांग होती है कि ‘कुशवाहा रामप्रकाश’ ज़रूर सुनाइए! (जैसे बनारस में आग्रह किया जाता था केदारनाथ सिंह से कि ‘बनारस’ कविता सुनाइए!) कई बार स्वयं रामप्रकाश कुशवाहा पाठ के समय उपस्थित रहे हैं।
डॉ. रामप्रकाश कुशवाहा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के हिंदी विभाग के विद्यार्थी रहे और दिनेश जी के समकालीन वरिष्ठ! दोनों एक ही समय में परिसर में मौजूद थे। बाद में रामप्रकाश जी उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक और प्राचार्य हुए।
एक कुशवाहा ने एक कुशवाहा पर यह कविता लिखी है। बहुत आत्मीयता और अधिकार के साथ यह कविता शुरू होकर आगे बढ़ती है। ऊपरी तौर पर हास्य की सामग्री दिखने वाली इसकी काव्य-वस्तु अपने अंतःकरण में सामाजिक पीड़ा भरे हुए है। यह पीड़ा कोई हाय-हाय नहीं मचाती बल्कि धीमे-धीमे धिक्कारती जाती है पीड़ा-दाताओं को! पाठ होते हुए भी देखा गया है कि श्रोताओं को थोड़ी हंसी आ ही जाती है। स्वयं दिनेश जी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाते हैं। रामप्रकाश जी को भी आनंद आता है। शैली के इसी रूप ने इस कविता को संजीवनी दी है। हाहाकार और चीत्कार होने पर शायद यह कविता अपने सामाजिक दर्द को उस प्रभावशीलता के साथ व्यक्त नहीं कर पाती।
कविता शुरू होती है इसी सूचना से कि हमने एक दूसरे की ‘टाइटल’ देखी–
“हमने एक दूसरे के पीछे
एक जैसी पूंछ देखी और शरमाये
पर हमारे पास शर्म से लाल गाल नहीं
टभकते दुःख थे
जिन्होंने हमें मित्र बना दिया।”
‘पूंछ’ एक जैसी थी, मतलब जाति एक थी। घाघ थे नहीं कि शरमाते नहीं, इसलिए शरमाए! लगा होगा कि विश्वविद्यालय में आकर जाति के आधार पर दोस्ती करना ठीक नहीं होगा! शिक्षा जाति-भेद को मिटाती है। सभी बराबर हैं। कुशवाहा की दोस्ती कुशवाहा से कोई अच्छी बात नहीं होगी! यह तो जातिवाद कहलाएगा! लेकिन जल्दी ही जान लिया कि महत्त्वपूर्ण आधार ‘पूंछ’ नहीं है, बल्कि ‘टभकते दुख’ हैं। इन दुखों ने उनकी मित्रता की शुरुआत की। हिंदी के किसी दूसरे कवि ने शायद ही इस तरह की ‘पूंछ’ की चर्चा की होगी! दिनेश जी ने इस बात को रखा है कि ज्ञान के केंद्र विश्वविद्यालय का माहौल भी जाति के प्रश्नों से अछूता नहीं है!
कविता आगे बढ़ती है इस बात के साथ कि रामप्रकाश जी की ऊंचाई छह फुट तीन इंच की है–
“जिस दिन वे कहते मेरा सारा दोष
मेरी छः फुट तीन इंच की ऊंचाई में है
उस दिन वे ज़रूर एक कविता लिखते।
एक दिन उन्होंने एक बड़े दर्पण में
डॉ. रामप्रकाश कुशवाहा को देखा
और आश्चर्य से भर गए कि
उन्होंने इस ऊंट से पढ़ने और
लिखने का इतना अधिक काम लिया।”
प्रकृति ने अधिक ऊंचाई दी और ज़माने ने इतना टोका कि यह विशेषता दोष बन गई। जिस दुर्लभता को गुण बनना था वह दोष की तरह मन-मस्तिष्क पर मढ़ दिया गया। इस दोष-दर्शन के स्रोत कहीं तो होंगे! कोई तो होगा जो उन्हें बताता होगा कि ज्यादा लंबाई गुण नहीं, दोष है। दिनेश जी उन लोगों की चर्चा नहीं करते मगर संकेत छोड़ते हैं कि मानसिक दुर्बलता प्रदान करनेवाली शक्तियां हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। अपनी विशिष्टता को दोष की तरह महसूस करने पर रामप्रकाश जी एक कविता लिखते। ज़ाहिर-सी बात है कि उस कविता के मूल में व्यक्तित्व में समाया दुख ही होगा। दिनेश जी ने खामोशी के साथ इस बात को उजागर किया है कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समाज से आए हुए लोग उचित उत्साह-वर्द्धन के अभाव में निराशा के शिकार होते हैं। विश्वविद्यालय का परिवेश आज भी पिछड़े समाज के अनुकूल नहीं हो सका है। आज से चालीस साल पहले तो यह जड़ता और भी गहरी थी।
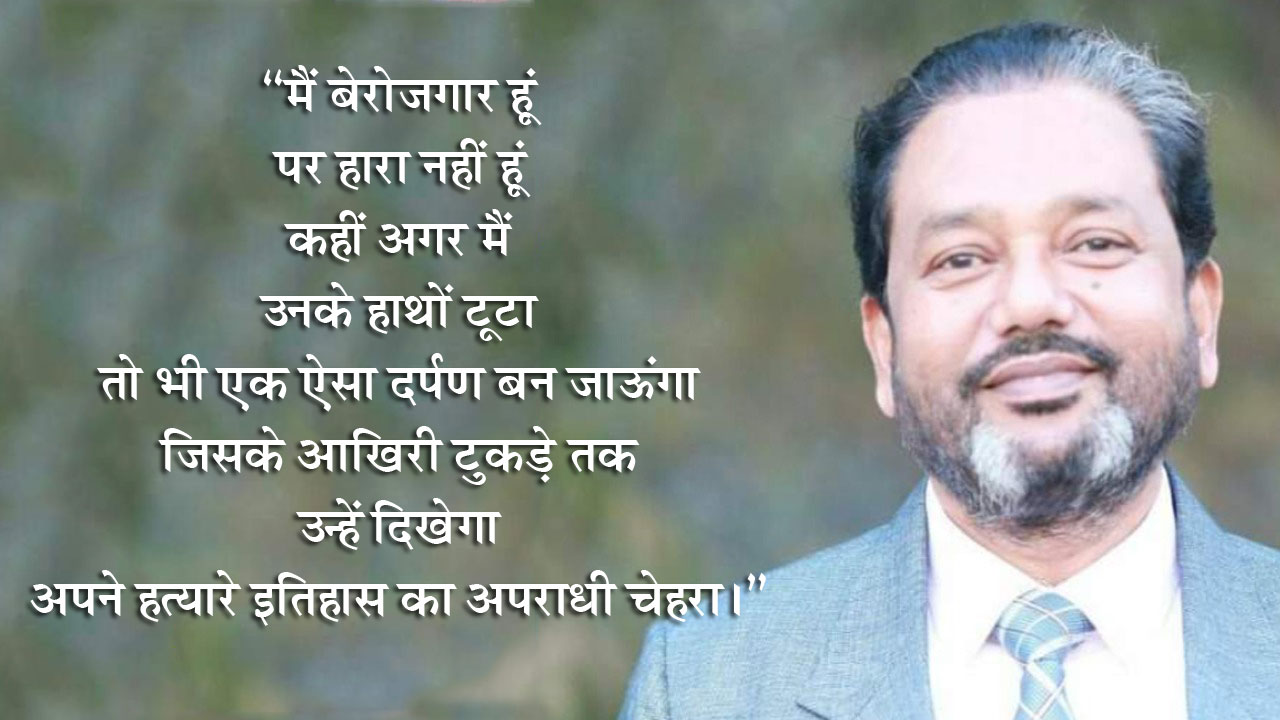
एक दिन वह भी आया जब पीएचडी पूरी हुई और रामप्रकाश कुशवाहा ‘डॉ.’ की उपाधि से अलंकृत हुए। इतनी बड़ी उपाधि भी अपनी ‘ऊंचाई’ के अनुकूल उनके मन-मस्तिष्क को आत्मविश्वास और आत्मगौरव प्रदान नहीं कर सकी। वे अचंभे में जीते रहे कि उन्होंने इतना पढ़-लिख कैसे लिया! वे अपनी ‘ऊंचाई’ को ‘ऊंट’ कहकर हास्यास्पद छवि गढ़ते हैं। वे कुछ इस तरह नहीं कह पाते कि ‘उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारु दो-चार खड़े।’
प्रकृति ने विशिष्टता दी और प्रवृत्ति ने ज्ञान! मगर सामाजिक विन्यास की आतंरिक और प्रकट चोट विश्वविद्यालय परिसर और ज्ञानियों के परिवेश में मिलती रही। जो कुछ अर्जित किया था वह मानो सलीब की तरह ढोने को वे अभिशप्त थे। अर्जित ज्ञान से राह खुलनी चाहिए थी मगर वह ज्ञान राह क्या खोलता स्वयं भार बन गया – ‘जिसे वे सलीब की तरह कंधे पर ढोते’। वे अपने ‘ज्ञान’ के साथ निकलते और चाहते कि इसे कहीं सम्मानजनक जगह मिले! मगर अनुभव की कड़वाहट बढ़ती ही जाती थी। उन्हें लगा ही नहीं कि उनके पढ़-लिख लेने के बाद उनका महत्त्व कहीं से बढ़ा है। ज्ञानियों की दुनिया उन्हें ‘समुद्री डाकू’ की तरह लगती–
“उन्हें अक्सर कोलंबस की आत्मा का ख़्याल आता
वे ज्ञान के लुटेरों को सदी का समुद्री डाकू
और उनके अड्डे को अमरीका कहते।
वे नौकरियों के लिए जाते
और वापस कर दिये जाते
आकर ईसा की तरह बुदबुदाते
उन्हें क्षमा करना प्रभु!
वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं।”
यह वह दौर था जब दुनिया दो ध्रुवीय थी। समाजवादी रास्ते में पूंजीवादी अमेरिका बाधक था। वहीं से यह रूपक लिया गया है। विश्वविद्यालय के परिवेश में मिलनेवाले ज्ञानियों की जातिवादिता और स्वार्थपरता को आज भी कहां ख़त्म किया जा सका है। वे एक अड्डे की तरह का व्यवहार करने को अभ्यस्त हैं। तब यह माहौल और ज्यादा गहरा था। फलतः रामप्रकाश जी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते और असफल करार दिये जाते! चयन करनेवाला अच्छी तरह से जान रहा होता है कि वह किस ‘कुलशील’ का चयन कर रहा है। ‘अज्ञातकुलशील’ के लिए तो कोई जगह हो ही नहीं सकती। ‘ज्ञान’ की जगह ‘कुलशील’ को चयन का आधार बनाया जाना किसी से छिपा नहीं है। मगर जीवट किसान समाज से विश्वविद्यालय आकर पढ़ाई पूरी करनेवाला सदियों तक संघर्ष और प्रतीक्षा करने को तैयार है। वह किसी पैगंबरी भाव से सहनशीलता रखता है और इस बात को मानने के लिए तैयार है कि सामाजिक जड़ता तुरंत नहीं टूटेगी! समय लगेगा! इन गुनहगारों को दोषी मानकर अंतिम संघर्ष नहीं किया जा सकता है। यह संघर्ष लंबा चलेगा!
संघर्ष की इन प्रक्रियाओं को दिनेश जी दोनों तरह से चिह्नित करते हैं। वे आक्रोशित सामाजिक पक्ष को भी रखते हैं और धैर्य-धारी संघर्ष को भी–
“मैं जब भी गुर्राता वे ख़ूब जानते हैं
वे कहते शांत हो बंधु!
सारे निर्णायकों की आत्मा मर चुकी है
और उनकी लाशें कुटेव कर रही हैं
पर यूं ही नहीं रहेगा सब दिन
एक दिन बदलेगा
और मौसम जब बदलता है
तो चूहे के बिल में भी बदलता है
उसका घर छोड़कर भागता है सांप।”
एक कुशवाहा व्यवस्था पर गुर्रा रहा है और दूसरा शांत रहने की सलाह दे रहा है। वह समझा रहा है कि इन मृत निर्णायकों से भला क्या उम्मीद करना! जब तक यह ‘मौसम’ रहेगा यही सब होता रहेगा। किसान ‘मौसम’ बदलने की प्रतीक्षा करता है, वह जानता है कि विपरीत ‘मौसम’ में ज्यादा कुछ संभव नहीं है। उसे पूरा विश्वास है कि माहौल बदलेगा तब ये ‘सांप’ भाग जाएंगे।
दिनेश जी ने कविता के शीर्षक में पहले ‘कुशवाहा’ शब्द रखा है, तब ‘रामप्रकाश’। कवि का आग्रह है कि यह कविता ‘रामप्रकाश’ व्यक्ति को आधार ज़रूर बना रही है, मगर इसका आशय ‘कुशवाहा’ शब्द में निहित उस उत्पीड़ित समाज से है, जिसकी नई पीढ़ी गांव की खेती-बारी से चलकर पढ़ने-लिखने शहर को पहुंची है। यह उत्पीड़ित समाज केवल ‘कुशवाहा’ जाति का समाज नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों का समाज है जिसकी पहली-दूसरी पीढ़ी शिक्षा की नई रौशनी से प्रकाशित होने के लिए संघर्ष कर रही है। शिक्षा की नई शक्ति से वह अपने को लैस करना चाहती है ताकि अपने समय में सम्मानपूर्वक जी सके! पृष्ठभूमि के तौर पर जाति और जन्म की सामाजिक पूंजी (सोशल कैपिटल) से जो जितना कमज़ोर है उसे इस तरह के संघर्ष से उतना गुजरना पड़ता है। यह कविता हर नई पीढ़ी से इसरार करती है कि हार मानकर बैठो नहीं, टूटने से डरो नहीं–
“मैं बेरोजगार हूं
पर हारा नहीं हूं
कहीं अगर मैं
उनके हाथों टूटा
तो भी एक ऐसा दर्पण बन जाऊंगा
जिसके आख़िरी टुकड़े तक
उन्हें दिखेगा
अपने हत्यारे इतिहास का अपराधी चेहरा।”
उत्पीड़ित समुदाय के लोग इस बात के प्रमाण बन जाते हैं कि हत्यारों के इतिहास में अपराधियों के चेहरे किस प्रकार के थे। ये अपराधी ‘गुनाहों का देवता’ होते हैं जो देवता बनकर प्रत्यक्षतः पूजित होते हैं और वस्तुतः बद्दुआओं से घिरे होते हैं। जो ‘इतिहास में अभागे’ हैं वे इन देवताओं के इतिहास के असली लेखक हो सकते हैं। इन अपराधियों के विरुद्ध कहते-सुनते-लिखते हुए एक लंबा दौर गुज़रा है। अपराधियों के चेहरे बेनकाब होते रहे हैं। यह अलग बात है कि ये ‘देवता’ गुनाह करने के लिए अलग-अलग नकाब लगाते रहे हैं। व्याख्या करते हुए रामप्रकाश जी कहते हैं कि यह देश कृष्ण-काव्य के ब्रजमंडल की तरह समृद्ध है, मगर सबको मक्खन खाने का अधिकार नहीं मिल पाया है। सदाचारों का प्रचार करनेवाले वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि कदाचारों पर बहस हो! वे चाहते हैं कि कदाचार का कारोबार भीतर-भीतर चलता रहे और ऊपर से सदाचार की हरियाली लहलहाती हुई दिखती रहे! जो ‘इतिहास में अभागे’ लोग हैं वे इन कदाचारों को देवताओं की लीला समझकर चुप रहें–
“ब्रजमंडल जैसा है समूचा भारतवर्ष
जहां सब कुछ सुलभ है
पर मक्खन कुछ लोग ही खा रहे हैं
सदाचार ही नहीं
कदाचारों की भी लीलाभूमि है यह देश”
रामप्रकाश जी ने भी उस उम्र में प्रेम किया था जब प्रायः सभी लोग करते हैं। अब वे मानते हैं कि यह भावना काल की तरह विस्तृत होती है। हालांकि सच यही था कि उनकी पुरानी प्रेमिकाएं अब उनसे दुआ-सलाम का भी रिश्ता नहीं निभाती थीं। क्या निष्कर्ष निकाल सकते थे रामप्रकाश जी! सो निष्कर्ष निकाला कि उनका अपना प्रेम तो कालिक विस्तार रखता है, मगर प्रेमिकाओं का प्रेम दिलचस्प झूठ के सिवाय और कुछ नहीं माना जा सकता है। वे सोचते थे कि उन तमाम जगहों पर शिलापट्ट लगवा दूं जहां-जहां प्रेम किया था। वे अपने प्रेम की सच्चाई के प्रति आज भी आश्वस्त हैं।
बेरोजगारी और उपेक्षा के कठोर अनुभवों के बावजूद उनका मानवीय मन अपनी कोमलता को खो नहीं देता है। उत्पीड़न से गुजर कर भी अपनी मनुष्यता की रक्षा कर पाना इन धैर्य-धारियों से कोई सीखे। उपेक्षाओं ने उन्हें तोड़ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर अपने मन की कोमलता को उन्होंने बचाए रखा। इस कोमलता के साथ उन्होंने अपने अर्जित ‘ज्ञान’ की भी लगातार रक्षा की। उन्होंने न पढ़ना-लिखना छोड़ा और न ही प्रेम करना–
“हालांकि एक ज्ञानवृद्ध नीरस आचार्य की तरह
दिखने के बावज़ूद वे प्रेम के नाम पर
किशोरियों की तरह शरमाते
जैसे सामने वाले से नैना मिलाते ही
उनका छाप-तिलक सब छिन जाएगा।”
दिनेश जी ने क्रमशः उस विराट् मनुष्यता को इस कविता में उभारा है, जिसे विपरीत परिस्थिति में सामान्य मनुष्य प्रायः अपने भीतर बचा नहीं पाता है। मगर दिनेश जी की तो मानो प्रतिज्ञा है कि ‘इतिहास में अभागे’ लोगों के व्यक्तित्व-कृतित्व और श्रेय को अपनी कविताओं में रेखांकित करेंगे! वे बताएंगे कि इन लोगों को मामूली न समझा जाए! इन पर हंसने की नहीं, सोचने की ज़रूरत है। इनकी उपेक्षा करके मनुष्य की असली तस्वीर से वंचित रह जाएंगे! यथा–
“बीच बाज़ार खड़ी अट्टालिकाओं को वे
मध्यकालीन मायाहाट कहते
जहां त्रिपुर सुंदरियों का काम सिर्फ नैन मटकाना है
निरर्थक गप्पबाज़ उन्हें कालनेमि लगते”
ऊपर चार पंक्तियों में पहचान है उन लोगों की जो ब्रजमंडल का मक्खन खा रहे हैं, जो कदाचारों की लीला में लिप्त हैं। और नीचे की पंक्तियां उनकी पहचान हैं जो ‘इतिहास में अभागे’ तो हैं मगर वर्तमान में डटे हैं अपने संघर्ष और मनुष्यता के साथ! देखें–
“उन्हें सिर उठाकर बांग देता मुर्गा
बहुत पसंद था
साष्टांग दंडवत करते आदमी को देखकर
उन्हें हंसी आ जाती थी।”
वे चाहते थे कि आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, भोर का स्वागत किया जाना चाहिए। सबको बताया जाना चाहिए कि भोर हो रही है, अब जाग जाओ! ‘साष्टांग दंडवत’ उनके काम बिल्कुल नहीं आता जो ‘इतिहास में अभागे’ हैं। दिनेश जी बताते हैं कि ‘धरती से नेह’ रखकर और भाषा से प्यार करते हुए जो जीवन जिया जाता है उसमें अपराजेयता होती है– ‘हृदयेन अपराजितः’। कुछ बातें और भी उल्लेखनीय है कि ‘नंगे पैर चलने ने’ उन्हें धरती से जोड़कर रखा। ‘दो बार सोचने की आदत’ ने पुनर्विचार और धैर्य की प्रवृत्ति दी ताकि क्रमिक संघर्ष किया जा सके! ‘चिरकुट आदमी’ और ‘प्रचंड मूर्ख’ में उन्हें गुंजाइश दिखती थी कि हो सकता है कि यह मेरी-जैसी पृष्ठभूमि से आया हो और कहीं इसने धैर्य खो तो नहीं दिया हो!
दिनेश कुशवाह की काव्य-भाषा अपने समय की श्रेष्ठ काव्य-भाषा है। सहज योग्यता से युक्त उनकी काव्य-भाषा प्रायः कृत्रिमता का शिकार नहीं होती है। हजारीप्रसाद द्विवेदी ने सूर की काव्य-भाषा के बारे में कहा है कि उसमें अलंकार ऐसे प्रयुक्त होते हैं मानो वे हाथ जोड़कर खड़े हों कि जैसे मन करे वैसे प्रयोग कर लो! उसी प्रकार दिनेश जी की कविताओं में काव्य-भाषा के न जाने कितने पक्ष सहज ढंग से रचे-बसे हैं! दिनेश कुशवाह की काव्य-भाषा विस्तृत विश्लेषण की मांग करती है।
‘कुशवाहा रामप्रकाश’ को केवल एक व्यक्ति पर लिखी गई कविता के रूप में ही पढ़कर काम पूरा नहीं हो सकता है। यह केवल ‘कुशवाहा’ की कविता के रूप में भी नहीं पढ़ी जा सकती है। इन दोनों रूपों के बाद उस रूप तक इस कविता के अध्ययन को पहुंचाना होगा, जहां इस कविता का सामाजिक विस्तार खुलता है। यह कविता उन तमाम उत्पीड़ितों की व्यथा-वाणी है जिनकी पहली-दूसरी पीढ़ी खेती-बारी से गुज़रते हुए उच्च शिक्षा की दुनिया तक पहुंची है और अपने लिए सम्मानजनक और न्यायपूर्ण जगह की तलाश कर रही है। यह कविता व्यक्ति से शुरू होकर जाति तक पहुंचती है और फिर पूरे समाज के स्याह पक्ष को जिस विश्वास से प्रकट करती है वह करुण रस के उस रूप से सिक्त है, जिसमें शोक की भूमिका बहुत भीतर से काम कर रही है।
(संपादन : राजन/नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in





