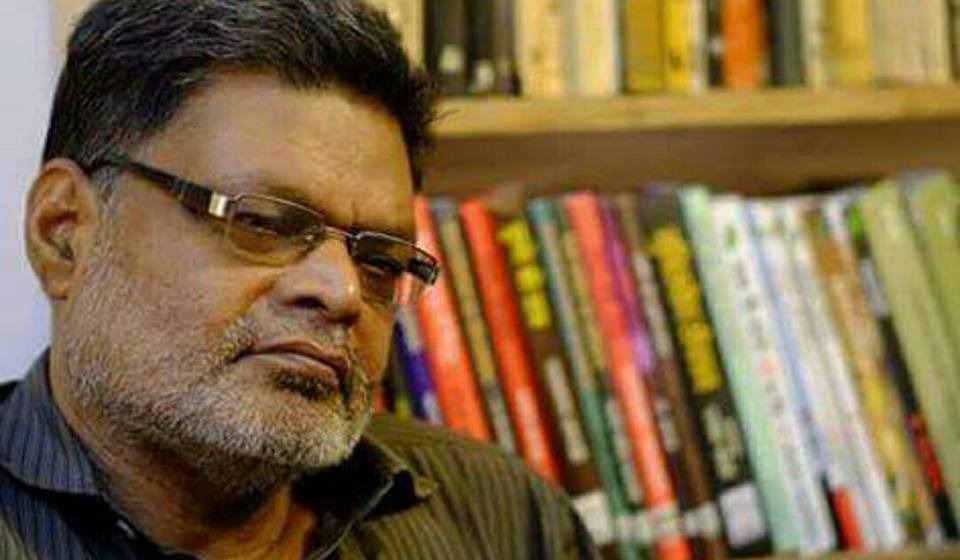ओबीसी साहित्य के नाम पर दिल्ली के दयाल सिंह कॉलेज में सेमिनार होने पर विरोध तो होने की आशंका थी ही, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि यह विरोध दलितों के एक लघु समूह की ओर से हुआ। आशंका थी कि ब्राह्मणवादी लोग इसका विरोध करेंगे क्योंकि दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य के बाद अब अगर ओबीसी साहित्य भी रूप ले लेता है, तो अभी तक जिसे मुख्य धारा का साहित्य कहा जाता रहा है, उसका पाठक कौन बचेगा? इनकी तो दुकान ही बंद होने का खतरा मँडराने लगेगा। खैर, अधिकतर चर्चा सोशल मीडिया पर हुई और उस पर ओबीसी साहित्य के कई समर्थकों ने विचार भी रखे, लेकिन अनावश्यक विरोधी बन गए लोगों की तरफ से एक आग्रह लगातार जारी है कि अलग से ओबीसी साहित्य की ज़रूरत नहीं है।
 ओबीसी साहित्य पर प्रतिक्रिया में कुछ जल्दबाजी की जा रही है। इसे दलित साहित्य के विरोध में माना जा रहा है, जबकि यह शुरू से ही स्पष्ट किया जाता रहा है कि दलित साहित्य और ओबीसी साहित्य में बहुत कुछ तो कॉमन होगा ही। आदिवासी साहित्य के साथ मिलकर ये तीनों धाराएँ ब्राह्मणवादी साहित्य को हाशिए पर डालने की क्षमता रखती हैं, इसलिए इसका स्वागत होना चाहिए।
ओबीसी साहित्य पर प्रतिक्रिया में कुछ जल्दबाजी की जा रही है। इसे दलित साहित्य के विरोध में माना जा रहा है, जबकि यह शुरू से ही स्पष्ट किया जाता रहा है कि दलित साहित्य और ओबीसी साहित्य में बहुत कुछ तो कॉमन होगा ही। आदिवासी साहित्य के साथ मिलकर ये तीनों धाराएँ ब्राह्मणवादी साहित्य को हाशिए पर डालने की क्षमता रखती हैं, इसलिए इसका स्वागत होना चाहिए।
मैंने ओबीसी साहित्य के पक्ष में कई तर्क दिए हैं। एक तर्क ये भी दिया है कि मान लीजिए कोई एक दलित टाइम्स नाम का अखबार या दलित-दहलीज नाम की पत्रिका छप रही है, अच्छी-खासी फल-फूल भी रही है, तो भी एक ओबीसी टाइम्स अखबार या ओबीसी-अलंकार पत्रिका आ भी जाएगी तो कौन-सा पहाड़ टूट पड़ेगा।
विरोध का एक तर्क यह भी है कि ओबीसी तो ब्राह्मणवाद के वाहक हैं, और दलितों पर अत्याचार करने में ब्राह्मणों के सहयोगी हैं या उनसे आगे हैं। मेरा कहना यह है कि मार खा-खाकर मंदिरों में जाने की कोशिश करने वाले दलित क्या ब्राह्मणवाद के वाहक नहीं हैं। दलितों पर अत्याचार की घटनाओं में सवर्णों के साथ ओबीसी भी मिल जाते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, उन लोगों में कुछ न कुछ दलित भी शामिल रहते हैं, जो अपने ही समुदाय के लोगों पर हमला करने-करवाने में साथ देते हैं। दूसरी बात, अगर आप मानते हैं कि ओबीसी कई मायनों में दलितों से एकदम भिन्न हैं जो कि सही भी है, तब तो उनके अलग साहित्य की बात और भी स्वाभाविक है।
सच्चाई तो यह है कि ब्राह्मणवाद के वाहक अगर ओबीसी पाए जाते हैं, तो उसके विरोध में भी बड़ी संख्या में ओबीसी रहे हैं और हैं। यह ओबीसी साहित्य ही तो है, जिसमें सुदामा के पैर धोने की बात को तमाम लोग नकारने लगे हैं। गीता के बारे में भी यह समझने लगे हैं कि ये कृष्ण की बोली या लिखी नहीं है। वो व्यास की करतूत है। उसी में पशुपालन को वैश्य कर्म बताया गया। यह बात उजागर जहाँ की गई है वो भी तो ओबीसी साहित्य है कि गीता को कृष्ण ने नहीं लिखा। गीता तो वेदव्यास ने लिखी, और उसकी मार्केटिंग कृष्ण के नाम पर कर डाली।
एक और उदाहरण देता हूँ। किसी सरकारी विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपना संघ बनाते हैं। ठीक ही है, बनाना भी चाहिए। अब अगर तृतीय श्रेणी वाले कर्मचारी भी अपना संघ बनाएँ तो मैनेजमेंट पर ज्यादा दबाव पड़ेगा। इनका विरोध मैनेजमेंट करे तो समझ में आता है, चतुर्थ श्रेणी संघ विरोध करे, ये समझ से परे है। संघ तो तृतीय श्रेणी कर्मचारी भी बनाएँ, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी बनाएँ। कोशिश यह होनी चाहिए कि एक वृहद कर्मचारी महासंघ भी बने जिसमें सारे कर्मचारी संघ भी शामिल हों। ऐसी जिद करना कि तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ न बने, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ से ही वे संतुष्ट हो जाएँ, ये उचित नहीं है। कहीं न कहीं, उनकी बात को तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ में पर्याप्त जगह नहीं मिल रही होगी, तभी तो वो अलग संघ बना रहे हैं।
ओबीसी साहित्य के नाम पर चिढ़ने वालों से एक सवाल भी है। कई या सभी सवर्ण जातियों और दलित जातियों की तरह ओबीसी जातियों की अनेक अलग-अलग पत्रिकाएँ सालों से निकल रही हैं। यादवों की कई पत्रिकाएँ हैं; कुर्मी, कुशवाहा, साहू, बढ़ई, कुम्हार, पासी और अनेक जातियाँ अपनी अलग-अलग पत्रिकाएँ निकालती हैं। इनमें जो भी, जैसा भी लिखा जा रहा है, वो ओबीसी साहित्य ही तो हैं। बहुत कुछ ऐसा है, जो ये जातियाँ लिखना चाहती हैं, लेकिन उन्हें किसी भी पत्रिका में जगह नहीं मिलती, इसीलिए वे अलग पत्रिका निकालते हैं। क्या किसी ने इन पत्रिकाओं में लिखे जा रहे ओबीसी साहित्य का विरोध किया? जब इन पर आपत्ति नहीं की गई, तो अब अगर ये सारी ओबीसी जातियाँ मिलकर कुछ अधिक सारगर्भित, अधिक तार्किक और अधिक विचारशील लेखन करके ब्राह्मणवाद को खत्म करना चाहती हैं तो क्या आपत्ति है! जो ब्राह्मणवाद के पोषक होंगे, वो तो इस ओर वैसे ही नहीं आएंगे। ओबीसी साहित्य की धारा में तो वही बहेंगे जो समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं। ये साहित्य इन जातीय पत्रिकाओं से बहुत बेहतर ही होगा।
सोशल मीडिया पर भी ही कई सामाजिक न्याय के समूह काम कर रहे हैं। कई दलितों के ग्रुप हैं, कई ओबीसी के ग्रुप हैं और कई सालों से चले आ रहे हैं। थो़ड़े-बहुत मतभेदों के साथ सब चलते रहते हैं और ठीक काम कर रहे हैं। इनमें भी जो लिखा जा रहा है, वह भी तो ओबीसी साहित्य ही तो है। अब अगर वह मुद्रित रूप में भी प्रकट हो तो ये कोई बहुत बड़ी घटना तो नहीं है।
 मेरा मानना तो यह है कि ओबीसी समाज मौजूदा व्यवस्था में मिसफिट ही है। न वह ब्राह्मण है, न क्षत्रिय हैं, न वैश्य और न शूद्र। क्षत्रिय उसे कोई मानने को तैयार नहीं है, और सत्ता में रहने, धन संचय करने का अधिकार रहने, और अस्पृश्यता का शिकार न होने के कारण ओबीसी अपने को शूद्र मानने को तैयार नहीं है। फिर वर्तमान में शूद्र शब्द दलित के पर्याय के रूप में प्रचलित रहा, इसलिए भी ओबीसी अपने को शूद्र नहीं मानता। वेद व्यास की गीता में पशुपालन को वैश्य कर्म कहा गया है। ऐसे में ओबीसी इस ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था में मिसफिट है। ब्राह्मणवादी वर्ण-व्यवस्था के विश्वविद्यालय में ओबीसी नाम के स्टूडेंट का दाखिला तो जबरन कर दिया लेकिन उसके लिए न कोई कोर्स अलॉट है और न ही कोई कक्षा। कभी वह यहाँ बैठता है तो कभी वहाँ। यह ओबीसी नाम का स्टूडेंट अगर अपना अलग ही विश्वविद्यालय खोल ले तो ब्राह्मण यूनिवर्सिटी की समस्या तो समझ में आती है, पर अन्य किसी की आपत्ति समझ से परे है।
मेरा मानना तो यह है कि ओबीसी समाज मौजूदा व्यवस्था में मिसफिट ही है। न वह ब्राह्मण है, न क्षत्रिय हैं, न वैश्य और न शूद्र। क्षत्रिय उसे कोई मानने को तैयार नहीं है, और सत्ता में रहने, धन संचय करने का अधिकार रहने, और अस्पृश्यता का शिकार न होने के कारण ओबीसी अपने को शूद्र मानने को तैयार नहीं है। फिर वर्तमान में शूद्र शब्द दलित के पर्याय के रूप में प्रचलित रहा, इसलिए भी ओबीसी अपने को शूद्र नहीं मानता। वेद व्यास की गीता में पशुपालन को वैश्य कर्म कहा गया है। ऐसे में ओबीसी इस ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था में मिसफिट है। ब्राह्मणवादी वर्ण-व्यवस्था के विश्वविद्यालय में ओबीसी नाम के स्टूडेंट का दाखिला तो जबरन कर दिया लेकिन उसके लिए न कोई कोर्स अलॉट है और न ही कोई कक्षा। कभी वह यहाँ बैठता है तो कभी वहाँ। यह ओबीसी नाम का स्टूडेंट अगर अपना अलग ही विश्वविद्यालय खोल ले तो ब्राह्मण यूनिवर्सिटी की समस्या तो समझ में आती है, पर अन्य किसी की आपत्ति समझ से परे है।
एक मुद्दा अभिव्यक्ति के अवसर का भी है। अगर कहीं एक माइक लगा है, एक मंच लगा है। उस पर कितने लोगों को बोलने का समय मिलेगा और कितना मिलेगा! अधिकतर लोग तो श्रोता ही बनकर रह जाएँगे। बोलने का अवसर तो सबको चाहिए और ये अवसर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ऐसे में कुछ और मंच तैयार हों, तो अधिक लोगों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलेगा।
ओबीसी के कुछ मुद्दे अलग हैं और वे इनको उजागर करना चाहते हैं तो ओबीसी साहित्य के जरिए ही ढंग से हो सकेगा। उदाहरण के लिए, कई ओबीसी परिवारो में ब्राह्मणवाद पोषित होता है लेकिन कई युवा अपने परिवारों में इसका विरोध भी करते हैं। उनकी क्या स्थिति होती है, ये सब ओबीसी साहित्य में ही तो सामने आएगा। ब्राह्मणवादी पाखंड का कई युवा विरोध करते हैं, और उनके परिवार में उनकी कुछ बातें मान भी ली जाती हैं और कई बार डाँट-डपटकर चुप भी कर दिया जाता है। विद्रोही युवा ओबीसी लोकतंत्रवादी भी हों तो वो पूरे परिवार पर अपनी बात थोप नहीं सकता। अगर पत्नी पूजा करती है, पति नहीं करता तो अब पति क्या पत्नी को जबरन रोके! रोके तो लोकंतंत्र और महिला विरोधी कहलाएगा और न रोके तो सवाल उठता है कि पहले अपना घर तो ठीक कर लो। ऐसे ओबीसी युवाओं की दास्तान और विडंबना ओबीसी साहित्य ही तो सामने लाएगा।
एक सच्चाई यह भी है कि सामाजिक न्याय का हर चिंतन इस बहाने ओबीसी को बाईपास करके सीधे दलित तक ही पहुंच जाता है, कि दलित अधिक पीड़ित हैं। दलितों के अधिक पीड़ित होने की बात सही है, पर ओबीसी की भी अपनी दिक्कतें हैं, अपने सरोकार हैं। उन पर भी चर्चा हो, उन पर भी साहित्य हो तो किसी को क्यों आपत्ति है। रही अधिक पीड़ित होने की बात तो सर्वाधिक पीड़ित तो आदिवासी समाज है जिसके जीने का ही अधिकार खत्म किया जा रहा है। जल, जंगल, जमीन से उसे महरूम किया जा रहा है। तो क्या इस वजह से दलित साहित्य ने अपने को आदिवासी साहित्य में ही समाहित करके रखा है क्या? सही तो यह है कि सामाजिक न्याय का चिंतन आदिवासियों तक भी पर्याप्त रूप में नहीं पहुँच पा रहा है।
ओबीसी साहित्य सेमिनार का सुर तो कहीं से भी दलित विरोधी रहा ही नहीं। सबके निशाने पर ब्राह्मणवाद ही रहा, लेकिन इस बहाने बहुत सारे ओबीसी एक साथ बैठे जरूर, जो अन्यथा नहीं बैठते या केवल अपने जातीय सम्मेलनों में केवल अपनी जाति के लोगों के साथ ही बैठते हैं।
एक तरफ ओबीसी में चेतना के अभाव की बात की जाती है और उनकी कई कमियाँ गिनाईं जाती हैं। इस बात से सहमत होकर अगर ओबीसी को जाग्रत किया जाए तो ये तो ठीक ही है न! लेकिन यह होगा कैसे? इसके लिए ओबीसी के बीच जाकर बात करनी होगी, उनकी सभाएँ बुलानी होंगी, इस बारे में लिखना पड़ेगा। और, अगर यही सब करते हैं तो आपको आपत्ति होती है। आखिर व्यापक ओबीसी वर्ग में चेतना उनसे अलग से संवाद किए बिना कैसे संभव हो सकती है!