(एफपीबुक ‘बहुजन साहित्य की प्रस्तावना’ के बहाने)
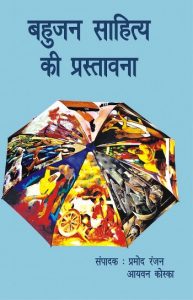 वेब संस्करण की घोषणा हो चुकी थी। वह समयानुसार काम भी करने लगा था। बावजूद इसके ‘फारवर्ड प्रेस’ द्वारा जून 2016 के बाद ‘प्रिंट संस्करण’ के बंद होने की घोषणा मन में आशंका पैदा करने वाली थी। ऐसे में ‘एफपी बुक्स’ की पहली खेप का आगमन बड़ा ही आह्लादकारी है। अपनी प्रतिबद्धता और वायदे पर खरा उतरने के लिए फारवर्ड प्रेस (अब एफपी बुक्स) के संपादक-द्वय आयवन कोस्का और प्रमोद रंजन चिर प्रशंसा के पात्र हैं। पत्रिका अपनी रीति-नीति में आरंभ से ही स्पष्ट रही है। हिंदी में बहुजन साहित्य की अवधारणा को बीच-बहस उतारने तथा तत्संबंधी प्रश्नों को लेकर उत्तेजक एवं महत्त्वपूर्ण बहसों की शुरुआत का श्रेय इसी पत्रिका को जाता है। तीन पुस्तकों की शृंखला में एक का शीर्षक ‘बहुजन साहित्य की प्रस्तावना’ है। पुस्तक-सामग्री का अधिकांश हिस्सा इसी पत्रिका के विभिन्न अंकों में प्रकाशित हो चुका है। बावजूद इसके विषयगत आलेखों को एक स्थान पर ले आना समीचीन था। यह कार्य समय रहते हुआ, इसके लिए भी संपादक द्वय प्रशंसा के पात्र हैं। पुस्तकाकार रचना पत्रिका के कलेवर से कहीं अधिक प्रभावी, आकर्षक तथा दूरगामी महत्त्व रखती है। यदि ‘एफपी बुक्स’की शृंखला पांच वर्ष भी सफलतापूर्वक चली; और प्रकाशकगण इन पुस्तकाकार संस्करणों की, पत्रिका-संस्करण की अपेक्षा आधी प्रतियां भी बेचने में सफल रहे तो यह न केवल बहुजन साहित्य की सैद्धांतिकी विकसित करने में मददगार होगी, बल्कि तब तक ब्राह्मणवाद को चुनौती देने में सक्षम समानांतर जनसंस्कृति के पक्ष में पुख्ता सोच तैयार हो चुकी होगी।
वेब संस्करण की घोषणा हो चुकी थी। वह समयानुसार काम भी करने लगा था। बावजूद इसके ‘फारवर्ड प्रेस’ द्वारा जून 2016 के बाद ‘प्रिंट संस्करण’ के बंद होने की घोषणा मन में आशंका पैदा करने वाली थी। ऐसे में ‘एफपी बुक्स’ की पहली खेप का आगमन बड़ा ही आह्लादकारी है। अपनी प्रतिबद्धता और वायदे पर खरा उतरने के लिए फारवर्ड प्रेस (अब एफपी बुक्स) के संपादक-द्वय आयवन कोस्का और प्रमोद रंजन चिर प्रशंसा के पात्र हैं। पत्रिका अपनी रीति-नीति में आरंभ से ही स्पष्ट रही है। हिंदी में बहुजन साहित्य की अवधारणा को बीच-बहस उतारने तथा तत्संबंधी प्रश्नों को लेकर उत्तेजक एवं महत्त्वपूर्ण बहसों की शुरुआत का श्रेय इसी पत्रिका को जाता है। तीन पुस्तकों की शृंखला में एक का शीर्षक ‘बहुजन साहित्य की प्रस्तावना’ है। पुस्तक-सामग्री का अधिकांश हिस्सा इसी पत्रिका के विभिन्न अंकों में प्रकाशित हो चुका है। बावजूद इसके विषयगत आलेखों को एक स्थान पर ले आना समीचीन था। यह कार्य समय रहते हुआ, इसके लिए भी संपादक द्वय प्रशंसा के पात्र हैं। पुस्तकाकार रचना पत्रिका के कलेवर से कहीं अधिक प्रभावी, आकर्षक तथा दूरगामी महत्त्व रखती है। यदि ‘एफपी बुक्स’की शृंखला पांच वर्ष भी सफलतापूर्वक चली; और प्रकाशकगण इन पुस्तकाकार संस्करणों की, पत्रिका-संस्करण की अपेक्षा आधी प्रतियां भी बेचने में सफल रहे तो यह न केवल बहुजन साहित्य की सैद्धांतिकी विकसित करने में मददगार होगी, बल्कि तब तक ब्राह्मणवाद को चुनौती देने में सक्षम समानांतर जनसंस्कृति के पक्ष में पुख्ता सोच तैयार हो चुकी होगी।
पुस्तक में लेखों को तीन खंडों में संयोजित किया गया है—ओबीसी साहित्य विमर्श, आदिवासी साहित्य विमर्श तथा बहुजन साहित्य विमर्श। उनके माध्यम से हम ‘ओबीसी साहित्य विमर्श’ से ‘बहुजन साहित्य विमर्श’ तक की यात्रा को भी समझ सकते हैं। हालांकि वह अभी अपने आरंभिक पड़ाव पर ही है। पुस्तक की सामग्री विचारोत्तेजक है। विशेषकर कंवल भारती, प्रेम कुमार मणि के लेख, जो सोचने को विवश करते हैं। यहां दो आलेखों का संदर्भ प्रासंगिक है। पहला सुप्रिसिद्ध भाषाविद् डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह का आलेख। ‘ओबीसी’ साहित्यकारों के बारे में उनका अध्ययन विशद् है। वे इस धारा के प्रथम प्रस्तावक माने जाते हैं। ब्राह्मणवादियों के लिए जाति का मुद्दा ईश्वर और धर्म से कहीं ज्यादा महत्त्वपूर्ण रहा है। इसलिए ईश्वर और धर्म के नाम पर अलग-अलग मत रखने वाले ब्राह्मणवादियों में जाति के नाम पर अटूट एकता दिखती है। पिछले ढाई-तीन हजार वर्षों में धर्म ने तरह-तरह के बदलाव देखे हैं। इस कारण इसे जीवन-शैली भी माना जाता है। लेकिन इस बीच जाति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लोगों की अशिक्षा का लाभ उठा, संस्कृति की मनमानी व्याख्या करते आए ब्राह्मण पहले भी शिखर पर थे, आज भी शिखर पर हैं। इस मनुवादी षड्यंत्र को डॉ। राजेंद्र प्रसाद सिंह गंभीरता से सामने लाते हैं। अपने लेख के माध्यम से वे बहुजन साहित्य की आवश्यकता को भी रेखांकित करते हैं। दूसरा आलेख वरिष्ठ लेखक-समालोचक डॉ. चौथीराम यादव का है, जिसमें वे पिछड़े वर्ग के लेखकों के अवदान की याद दिलाते हैं। दोनों विद्वान दलित साहित्य के विकास में पिछड़ी जातियों के साहित्यकारों की भूमिका को चिह्नित करते हैं। यह चिह्नन तथाकथित मुख्यधारा के साहित्य के समानांतर अपनी पहचान बना चुके दलित साहित्यकारों को यथारूप स्वीकार नहीं है। स्वीकार हो भी क्यों! जिस समय जातीय असमानता का सर्वाधिक शिकार रहे दलित-लेखक साहित्य की समानांतर धारा को स्थापित करने के लिए सतत संघर्ष कर रहे थे, पिछड़े वर्ग के लेखक विचित्र-से ऊहापोह में थे। द्विज लेखक उन्हें ईमानदारी से स्वीकारने को तैयार नहीं थे; और दलितों के साथ जाना उन्हें स्वयं अस्वीकार था। अपनी प्रतिभा, लगन और निरंतर संघर्ष द्वारा दलित लेखकों ने तथाकथित मुख्यधारा के साहित्य के समानांतर परिवर्तनकामी साहित्य को खड़ा करने में सफलता प्राप्त की है। अपनी उपलब्धि पर गर्व करने का अधिकार उन्हें है। इसीलिए कबीर, फुले, पेरियार आदि जो दलित साहित्य में पहले से ही सम्मानित स्थान रखते हैं, को ‘ओबीसी’ के नाम पर झटक लेना उन्हें स्वीकार नहीं है। कमोबेश यही मानसिकता आदिवासी पृष्ठभूमि के साहित्यकारों की भी है। बात सही है। दलित साहित्य दमन के विरुद्ध चेतना का साहित्य है। इसमें उन वर्गों की चेतना अभिव्यक्त होती है, जिन्हें इतिहास के दौर में सर्वाधिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। पुस्तक के कुछ लेखों में बहुजन साहित्य को लेकर स्वागत का भाव है, तो कुछ को पढ़कर लगता है कि दलित साहित्यकार बहुजन साहित्य की धारा में पूरी तरह समाहित होने की बजाए उसमें बड़े भाई की भूमिका को बनाए रखना चाहते हैं। साहित्य में बहुजन विमर्श की नवागंतुक धारा ,जो अभी केवल प्रस्तावना तक सीमित है, जिसकी रूपरेखा तक अस्पष्ट है—को लेकर स्थापित साहित्यकारों का दुराव अस्वाभाविक नहीं है।
अच्छी बात यह है कि ‘ओबीसी साहित्य’ को लेकर दलित और आदिवासी साहित्यकारों के जितने भी किंतु-परंतु हैं, ‘बहुजन साहित्य’ के अपेक्षाकृत बड़े कैनवास में उनका समाधान दिखने लगता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जैसे-जैसे बहुजन साहित्य की रूपरेखा स्पष्ट होगी, एक-दूसरे के प्रति समझ में इजाफा होगा—अंतर्विरोधों का समाहार स्वतः होता जाएगा। हालांकि बहुजन साहित्यकारों के कुछ घटकों के समक्ष पहचान का जो संकट अभी है, वह आगे भी बना रह सकता है। दरअसल बहुजन साहित्यकारों में जिन घटकों के सम्मिलन की परिकल्पना हम करते हैं, उनमें दलित, स्त्री-अस्मितावादी, आदिवासी साहित्य-धारा काफी परिपक्व हो चुकी है। जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के साहित्य को लेकर इन्हीं जातियों के साहित्यकार किंतु-परंतु में उलझे हुए हैं। बहुजन साहित्य के एक अन्य घटक आदिमजाति साहित्य के समक्ष भी यही दुविधा बनी हुई है।
यह सच है कि दलित साहित्यकार जिन्हें अपना मूल प्रेरणास्रोत मानते हैं, उनमें से कई पिछड़ी जातियों से आए हैं। यह भी सच है कि दलितों पर अतीत में जो अत्याचार हुए, उनमें चाहे-अनचाहे पिछड़ी जातियों का भी हाथ रहा है। मगर अतीत की अप्रिय घटनाओं के आधार पर मन में गांठ पाल लेने से अच्छा है, भविष्य पर ध्यान दिया जाए। जातिवाद की पृष्ठभूमि की समझ इस संकल्प को आसान बना सकती है। ‘मनुस्मृति’ को मुख्यतः धर्म-ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ को लेकर यह अधूरी समझ है। वह केवल सामाजिक ऊंच-नीच को बढ़ावा देने वाली कृति ग्रंथ नहीं है, असल में वह समस्त संसाधनों पर मुट्ठी-भर लोगों के एकाधिकार की जन्मदाता है। वह ब्राह्मणों को पृथ्वी के समस्त संसाधनों का स्वामी घोषित करती है(सर्वं स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किझ्ज्जिगतीगतम्—मनु। 1/100)। उस दौर में जब अर्थव्यवस्था खेती और पशु-संपदा पर आधारित थी। एक ओर संसार को माया कहना, उसे प्रपंचमय बताना, उससे दूर भागने का उपदेश देना और दूसरी तरफ समस्त संसाधन ब्राह्मणों के नाम घोषित करना—उस व्यवस्था के विरोधाभासों को दर्शाता है। जिसके कारण समाज सहस्राब्दियों तक कमजोर और देश बरसों-बरस गुलाम बना रहा। यह काम सोची-समझी नीति के तहत हुआ। इस तरह किया गया कि ब्राह्मण संपूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक विमर्श तथा जीवन की समस्त गतिविधियों का केंद्र बना रहे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मनुस्मृति की आलोचना आर्थिक वैषम्य को बढ़ावा देने वाले ग्रंथ के रूप में क्यों नहीं की गई? दरअसल ‘मनुस्मृति’ आलोचना की शुरूआत उन वर्गो की ओर से हुई जो कम से कम में गुजारा करने, संतोष को परम धन मानते आए थे। जिनके लिए सामाजिक समानता आर्थिक समानता से अधिक मूल्यवान थी। उन्हें लगता था कि सामाजिक समानता का लक्ष्य प्राप्त होने के उपरांत आर्थिक समानता का मार्ग स्वत: प्रशस्त हो जाएगा।
 बहरहाल, मनु का नाम लेकर किसी अनाम-धूर्त्त ब्राह्मण द्वारा लिखी गई उस पुस्तक के माध्यम से न्याय भावना का गला घोटते हुए समस्त संसाधनों को ब्राह्मणों के नाम कर दिया गया। उस स्थिति में बाकी वर्गों को उनका आश्रित होना ही था। ‘मनुवादी व्यवस्था’ क्षत्रियों को दूसरे स्थान पर रख उन्हें संसाधनों की रखवाली का काम सौंपती है। क्षत्रियों का काम शक्ति-प्रबंधन से जुड़ा है। जिसके पास शक्ति है उसे निर्णय लेने का सलीका न हो तो भी समाज उसकी बातों को आदेश की तरह लेता है। क्षत्रियों ने भी अपने हित को देखते हुए मनुस्मृति के विधान कि ब्राह्मण समस्त संपदा का स्वामी और वे संरक्षक हैं, का अतिक्रमण करना आरंभ कर दिया था। यह विरोध आमने-सामने का नहीं था। मनुस्मृति से कमोबेश दोनों के स्वार्थ जुड़े थे। इसलिए प्रकट में दोनों ही उसका गुणगान करते थे। किंतु आंतरिक स्तर पर संघर्ष हमेशा बना रहता था। कुछ ऐसी घटनाएं भी रहीं जो उस संघर्ष को एकदम धरातल पर ले आती हैं। परशुराम-सहस्रार्जुन युद्ध, विश्वामित्र-वशिष्ठ जैसे संघर्षों की लंबी गाथा है। महाभारत से लेकर देवासुर संग्रामों तक, जिन्हें ब्राह्मण धर्मयुद्ध कहकर प्रचारित करते रहे हैं, वास्तव में संपत्ति और संसाधनों के बंटवारे की खातिर हुए युद्ध थे। महाभारत के कौरव-पांडव परस्पर चचेरे भाई थे, जबकि देवता, दानव, दैत्य आदि तो एक ही पिता की संतान थे। उनकी माएं जरूर अलग-अलग थीं। इतिहास लेखन से बचने वाले ब्राह्मणों ने, निहित स्वार्थ के लिए संपत्ति के बंटवारे की खातिर हुए संघर्षों का जानबूझकर मिथकीकरण किया है। परिणामस्वरूप इतिहास का सच समय की गहरी परतों में विलीन होता चला गया। यहां समुद्र मंथन की प्रतीक कथा का भी संज्ञान ले सकते हैं। उसमें असुरों को वासुकि नाग के फन की ओर खड़ा किया जाता है। देवता पूंछ संभालते हैं। नाग का फन न केवल भारी होता है। बल्कि सारा विष उसी ओर रहता है। इस तरह असुरों को आरंभ से ही कठिन चुनौती के लिए तैयार किया जाता रहा है। वे गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार करते आए हैं। समय के साथ आवश्यकताएं बढ़ीं तो हर नई जरूरत के नाम पर एक नई जाति समाज से जुड़ती चली गई। उन जातियों का न तो अपने श्रम पर अधिकार था, न ही श्रमोत्पाद पर। नतीजा यह हुआ कि अपने श्रम-कौशल पर पूरे समाज का भरण-पोषण करने वाले बहुजन, अल्पसंख्यक अभिजनों के बंधुआ बनकर रह गए। दासत्वबोध उनके स्वभाव का अभिन्न हिस्सा बन गया। गिरबी दिमाग या तो नियति को कोसता; अथवा ‘स्वामी-सर्वेसर्वा’(बॉस इज आलवेज राइट) की भावना के साथ गर्दन झुकाए काम करता रहता था। मार्क्स ने यही बातें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से कही हैं। इसलिए ब्राह्मणवादियों को वामपंथ और मार्क्स फूटी आंख नहीं सुहाते।
बहरहाल, मनु का नाम लेकर किसी अनाम-धूर्त्त ब्राह्मण द्वारा लिखी गई उस पुस्तक के माध्यम से न्याय भावना का गला घोटते हुए समस्त संसाधनों को ब्राह्मणों के नाम कर दिया गया। उस स्थिति में बाकी वर्गों को उनका आश्रित होना ही था। ‘मनुवादी व्यवस्था’ क्षत्रियों को दूसरे स्थान पर रख उन्हें संसाधनों की रखवाली का काम सौंपती है। क्षत्रियों का काम शक्ति-प्रबंधन से जुड़ा है। जिसके पास शक्ति है उसे निर्णय लेने का सलीका न हो तो भी समाज उसकी बातों को आदेश की तरह लेता है। क्षत्रियों ने भी अपने हित को देखते हुए मनुस्मृति के विधान कि ब्राह्मण समस्त संपदा का स्वामी और वे संरक्षक हैं, का अतिक्रमण करना आरंभ कर दिया था। यह विरोध आमने-सामने का नहीं था। मनुस्मृति से कमोबेश दोनों के स्वार्थ जुड़े थे। इसलिए प्रकट में दोनों ही उसका गुणगान करते थे। किंतु आंतरिक स्तर पर संघर्ष हमेशा बना रहता था। कुछ ऐसी घटनाएं भी रहीं जो उस संघर्ष को एकदम धरातल पर ले आती हैं। परशुराम-सहस्रार्जुन युद्ध, विश्वामित्र-वशिष्ठ जैसे संघर्षों की लंबी गाथा है। महाभारत से लेकर देवासुर संग्रामों तक, जिन्हें ब्राह्मण धर्मयुद्ध कहकर प्रचारित करते रहे हैं, वास्तव में संपत्ति और संसाधनों के बंटवारे की खातिर हुए युद्ध थे। महाभारत के कौरव-पांडव परस्पर चचेरे भाई थे, जबकि देवता, दानव, दैत्य आदि तो एक ही पिता की संतान थे। उनकी माएं जरूर अलग-अलग थीं। इतिहास लेखन से बचने वाले ब्राह्मणों ने, निहित स्वार्थ के लिए संपत्ति के बंटवारे की खातिर हुए संघर्षों का जानबूझकर मिथकीकरण किया है। परिणामस्वरूप इतिहास का सच समय की गहरी परतों में विलीन होता चला गया। यहां समुद्र मंथन की प्रतीक कथा का भी संज्ञान ले सकते हैं। उसमें असुरों को वासुकि नाग के फन की ओर खड़ा किया जाता है। देवता पूंछ संभालते हैं। नाग का फन न केवल भारी होता है। बल्कि सारा विष उसी ओर रहता है। इस तरह असुरों को आरंभ से ही कठिन चुनौती के लिए तैयार किया जाता रहा है। वे गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार करते आए हैं। समय के साथ आवश्यकताएं बढ़ीं तो हर नई जरूरत के नाम पर एक नई जाति समाज से जुड़ती चली गई। उन जातियों का न तो अपने श्रम पर अधिकार था, न ही श्रमोत्पाद पर। नतीजा यह हुआ कि अपने श्रम-कौशल पर पूरे समाज का भरण-पोषण करने वाले बहुजन, अल्पसंख्यक अभिजनों के बंधुआ बनकर रह गए। दासत्वबोध उनके स्वभाव का अभिन्न हिस्सा बन गया। गिरबी दिमाग या तो नियति को कोसता; अथवा ‘स्वामी-सर्वेसर्वा’(बॉस इज आलवेज राइट) की भावना के साथ गर्दन झुकाए काम करता रहता था। मार्क्स ने यही बातें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से कही हैं। इसलिए ब्राह्मणवादियों को वामपंथ और मार्क्स फूटी आंख नहीं सुहाते।
आगे चलकर कर्मकांडों में वृद्धि हुई। यायावर ऋषियों के स्थान पर परंपराबद्ध पुरोहित वर्ग छाने लगा। जब तक कर्मकांड आश्रम-केंद्रित रहे, वर्ण-व्यवस्था में कम ही सही, अंतरण की संभावना बनी रही। सत्यकाम जाबाल, मतंग, कर्दम, महीदास, रैक्व, विश्वामित्र आदि ने अपनी प्रतिभा के आधार पर उच्च वर्गों में अंतरण किया। यहां गिनाए गए नामों में पहले पांच ऋषि शूद्र वर्ग से आए थे। ब्राह्मण-ग्रंथों में उनके नाम इसलिए बचे रहे क्योंकि वे मानसिक रूप से ब्राह्मणवादी व्यवस्था को अपनाकर उसके प्रवक्ता बन चुके थे। अजित केशकंबलि, कौत्स, पूर्ण कस्सप, मक्खलि गोसाल भी शूद्र और अपने समय के प्रखरतम दार्शनिक थे। वे ब्राह्मणों के बौद्धिक वर्चस्व को चुनौती देते थे। वेदों को ‘धूर्त्त-भांड और निशाचरों’ की कृति बताकर उनका मखौल उड़ाते थे। इसलिए उनके नाम ब्राह्मण-ग्रंथों से पूरी तरह गायब हैं। सिवाय कौत्स के। कौत्स को वे नहीं मिटा पाए। क्योंकि स्वयं यास्क ने ‘निरुक्त’ के पंद्रहवें अध्याय में उसका उल्लेख किया है। पाणिनी शिष्य, अपने समय का महान वैयाकरणाचार्य कौत्स वैदिक ऋचाओं को ‘निरर्थक’ मानता था, ‘यदि तर्कपूर्ण ढंग से विश्लेषण किया जाए, तो वैदिक ऋचाएं अर्थविहीन काव्य हैं’(निरुक्त पंद्रहवां अध्याय)। कालांतर में यज्ञादि कर्मकांड आश्रमों से निकलकर गृहस्थों की जीवनचर्या का हिस्सा बनने लगे तब स्वार्थी और कूपमंडूक पुरोहित वर्ग ने जन्म लिया। उससे पहले यज्ञादि कर्मकांड मुख्यतः ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों तक सीमित थे। पुरोहित वर्ग द्वारा उनका विस्तार समाज के दूसरे वर्गों तक होने लगा। अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए उसने निकृष्ट समझे जाने वाले कार्यों में लगी जातियों को अस्पृश्य घोषित कर दिया। खुद को ऊंचा दिखाने के लिए ब्राह्मण पुरोहितों ने अस्पृश्यों से दूरी बनानी शुरू कर दी। अस्पृश्य होने के कारण ब्राह्मण उनके घरों में प्रवेश नहीं कर सकता था। परिणामस्वरूप अस्पृश्य कही जाने वाली जातियों से काम कराने की जिम्मेदारी निम्न और मंझोली जातियों पर आ गई। वे स्वयं ब्राह्मणवाद की शिकार थीं। परंतु परिवर्तनकारी चेतना के अभाव में वे अपने शोषकों को ही अपना पालक और मुक्तिदाता मान बैठी थीं। धीरे-धीरे यही उनका संस्कार बनता गया। जब यह व्यवस्था जम गई और ब्राह्मणों का काम आसानी से होने लगा, तब उन्होंने खुद को अस्पृश्यों की छाया से भी दूर रखना शुरू कर दिया। लेकिन यह लोक चलन, यानी महज दिखावे के लिए था। पर्दे के पीछे जारकर्म चलता ही रहता था। आगे चलकर इसी ने सैकड़ों मिश्रित वर्णों और जातियों को जन्म दिया। जातीय उत्पीड़न का निरंतर शिकार रहे अछूतों ने भी कालांतर में अस्पृश्यता को अपनी नियति मान लिया। समय-समय पर जन्मे महापुरुषों ने उनकी चेतना को जगाने की कोशिश भी। परंतु आमूल परिवर्तनकारी दौर सभ्यता के इतिहास में कभी नहीं आ सका।
व्यवस्था के प्रति नासमझी उसकी मनमानियों को बढ़ावा देकर उन्हें चिर-जीवी बनाती है। निरंकुशता लंबी चले तो लोग हालात से समझौता कर उनके आगे समर्पण कर देते हैं। मुक्ति की चाहत जगे भी तो व्यवस्था से अनुकूलित मानस पहले उन्हीं हथियारों को आजमाता है, जो उसकी दुर्दशा का कारण रहे हैं। पाब्लो फ्रेरा के अनुसार उत्पीड़न के कारणों की अपर्याप्त समझ की वजह से, ‘उत्पीड़ित अपनी मुक्ति उत्पीड़क की भूमिका में आने देखता है’(उत्पीड़ितों का शिक्षाशास्त्र)। जाहिर है, दुर्दशा के कारणों के प्रति आधी-अधूरी समझ परिवर्तनकामी आंदोलनों को उनके लक्ष्यों से दूर रखती है। लोग अपनी दुरावस्था के कारणों को समझ न सकें, इसमें धर्म की बड़ी भूमिका होती है। जैसे विकट विपन्नता के लिए आर्थिक असमानता और संसाधनों पर कुछ लोगों के एकाधिकार के बजाय पूर्व जन्म के कर्मों को दोषी ठहराना, स्वर्ग-नर्क की अभिकल्पना, पूजा-पाखंड को संस्कार और माला फेरने, नाम रटने को ज्ञान-साधना की संज्ञा देना आदि। ये सब ब्राह्मणों के वर्चस्ववादी षड्यंत्र का हथियार बने हैं। दुरावस्था के कारणों की आधी-अधूरी समझ ने कई जनांदोलनों को भटकाया है। उदाहरण के लिए वर्ण-व्यवस्था से त्रस्त लोगों ने मुक्ति की चाहत में मनु को गालियां दीं, मनुस्मृति को जलाया, असमानता थोपने के लिए हिंदू धर्म को कोसा, परंतु उन लोगों से दूरी बनाए रहे, जो भिन्न जातीय स्तर पर होने के बावजूद उसके उतने ही शिकार थे, जितने वे। न ही संसाधनों पर एकाधिकार के तथाकथित धर्म-विधान को उन्होंने सीधी चुनौती दी। जबकि क्षत्रियों ने, जैसा कि हमने पहले भी संकेत किया है, इस व्यवस्था को वहीं तक स्वीकारा जहां तक उनके वर्गीय हित सधते हों। कभी बातचीत तो कभी संघर्ष के माध्यम से वे ब्राह्मणों के एकाधिकार को निरंतर चुनौती देते रहे। अपने बौद्धिक चातुर्य के भरोसे शूद्रों का ही एक वर्ग संसाधनों में हिस्सेदारी कर, तथाकथित सवर्ण समूहों का हिस्सा बन गया। जाति-व्यवस्था के रहस्य को समझने के लिए उसकी चर्चा यहां प्रासंगिक है
समय के साथ समाज की जरूरतें बढ़ती गईं। लगातार चुनौतियों से गुजरते हुए उनके शिल्प में सुधार हुआ। अपने उत्पाद को अधिक दाम पर बेचने की समझ भी पैदा हुई। आजीवक कर्मकांडों का निषेध करते थे। बुद्ध ने भी उसी नीति को आगे बढ़ाया था। उसके फलस्वरूप जाति-संबंधी बंधन शिथिल पड़ने लगे। यज्ञ-बलियों में कमी से पशुधन की बचत हुई तो समृद्धि रफ्तार पकड़ने लगी। आजीवकों और बुद्ध के प्रभाव से जाति-प्रथा कमजोर पड़ रही थी। सामाजिक आचार-विचार और शुचिता संबंधी नियम भी ढीले पड़े थे। फलस्वरूप विभिन्न जाति-समुदायों के लोग एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे। शिल्पकारों ने भी संगठन की ताकत को समझा और सामूहिक पद्धति को अपनाया। अपने श्रम-कौशल द्वारा आजीविका चलाने के कारण वे आजीवक कहलाते थे। वही उनका धर्म था। मक्खलि गोसाल, पूर्ण कस्सप, अजित केशकंबलि उनके मार्गदर्शक और आचार्य थे। बौद्ध धर्म के उदय के बाद आजीवकों का एक हिस्सा उसकी ओर आकर्षित हुआ था, लेकिन संगठन और व्यापार के प्रति उनकी निष्ठा ज्यों की त्यों बनी रही। अपने श्रम-कौशल के बल पर शिल्पकार समूहों ने सफलता की ऐसी कहानी लिखी कि कुछ ही अर्से में उसका व्यापार दूर-दराज के देशों तक फैल गया। उनकी प्रगति को ग्रहण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगा।
ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि अपनी शिल्पकला और व्यापार-कौशल से समस्त विश्व को चकित कर देने वाले उन शिल्पकार संगठनों ने राज्य की सत्ता को कभी चुनौती दी हो। अथवा अपनी महत्त्वाकांक्षाओं के कारण राज्य के लिए खतरा बने हों। बावजूद इसके चाणक्य को शिल्पकार संगठनों से आपत्ति थी। वह मजबूत केंद्र का समर्थक था। नहीं चाहता था कि राज्य के समानांतर यहां तक कि उसके आसपास भी दूसरी कोई सत्ता हो। राजभवनों में पलने वाले षड्यंत्रों के बारे में उसे पूरी जानकारी थी। लेकिन राज्य की अर्थव्यवस्था में शिल्पकार संगठनों का योगदान इतना अधिक था कि उनके विरुद्ध सीधी कार्रवाही का साहस चाणक्य में भी नहीं था। उसने शिल्पकार समूहों की निगरानी करना शुरू कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि आजीवक समुदाय, जिसकी संख्या कभी बुद्ध के शिष्यों से भी अधिक थी; तथा जिसके स्थापक मक्खलि गोशाल तथा पूर्ण कस्सप को महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध से पहले ही बुद्धत्व प्राप्त हो चुका था—धीरे-धीरे बिखरने लगा। इससे उस वर्ग को लाभ पहुंचा जिसका उत्पादन में सीधा योगदान न था, जो केवल लाभार्जन की कामना के साथ व्यापार करता था। अवसर अनुकूल देख उसने भेंट-पूजा, दानादि देकर पुरोहितों और अधिकारियों को खुश करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप वे राज्य के कृपापात्र कहलाने लगे। बुद्ध के समय व्यापारिक संगठनों में काम मिल-जुलकर किया जाता था। धीरे-धीरे वैश्य ‘श्रेष्ठि’ संगठन का पर्याय बनने लगे। विशेष अवसरों पर उन्हें राज्य की ओर से आमंत्रित किया जाने लगा। भे ट-सौगात के बदले राज्य की ओर से निर्बाध व्यापार की सुविधा मिलने लगी। परिणाम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दलाल-तंत्र के रूप में सामने आया। जिससे व्यापार के नाम पर उन वस्तुओं के मूल्य-निर्धारण का अधिकार मिल गया, जिसके निर्माण में किसी दूसरे के श्रम-कौशल का योगदान था। धर्म के क्षेत्र में यह काम बहुत पहले शुरू हो चुका था। वहां ‘भक्त’ और ‘भगवान’ के बीच ‘मध्यस्थ’ की भूमिका पुरोहित निभाता था। श्रेष्ठि वर्ग को बढ़ावा मिलने से शिल्पकार समूह अर्थव्यवस्था के केंद्र से हटने लगे। उत्पादों की बिक्री के लिए श्रेष्ठि-वर्ग पर उनकी निर्भरता बढ़ती चली गई। यह काम मनुस्मृति लिखे जाने के आसपास या उससे कुछ ही समय पहले हुआ। दूसरे शब्दों में जब तक देश की राजनीतिक शक्ति विकेंद्रित थी, अर्थसत्ता भी विकेंद्रित रही। सत्ता के उस केंद्रीकरण के दौर में ही महाभारत को उसका वर्तमान रूप मिला। गीता की रचना हुई। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को समर्थन देते हुए ब्राह्मणों ने पुरुष सूक्त की रचना की। स्मृति-ग्रंथ, गीता, पुराणादि वर्ण व्यवस्था समर्थित ग्रंथों की रचना इसी दौर में संपन्न हुई। याद दिला दें कि वर्ण-विभाजन का विचार आर्य अपने पैत्रिक देश पर्शिया से साथ लाए थे। वहां समाज को चार वर्णों) में बांटा गया था। उनके नाम थेᅳ‘अथर्वा’ या पुजारी(Athravas or Priest), रथेस्थस्स या योद्धा(Rathaesthas or Warrior) वास्त्रय श्युआंत्स(Vastrya Fshuyants) अथवा उपार्जक तथा हाउटिस(Huitis or Manual Workers) यानी मेहनतकश मजदूर। भारत में आकर ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बन कहलाने लगे।
शिल्पकार संगठन स्वयं को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखते थे। बावजूद इसके राज्य के समानांतर हैसियत वाले शिल्पकार वर्गों के आर्थिक संगठनों का भय ब्राह्मणों के दिमाग में इतना था कि उन्होंने ‘मनुस्मृति’ के सहारे शूद्र शिल्पकर्मियों से उनके सारे संसाधन, उनके आर्थिक अधिकार छीन लिए। शूद्रों के लिए निर्धारित किया गया कि उनका काम केवल सेवा करना है। अपने लिए कुछ अपेक्षा करना नहीं। वे अपने अवदान के बदले कोई अपेक्षा न रखें। इसके लिए गीता के माध्यम से निष्काम कर्म की अवधारणा को प्रचारित किया। उन्हें बताया गया कि केवल कर्म पर उनका अधिकार है। फल पर नहीं। शूद्रों से यहां तक कहा गया कि यदि उनमें धन-संचय का सामर्थ्य है, तो भी वैसी धृष्टता न करें। इसके बावजूद यदि कोई शूद्र धनार्जन में सफल हो जाए तो ब्राह्मण को अधिकार दिया गया कि वह शूद्र द्वारा अर्जित धन को उसके मालिक (जमींदार/सामंत/सम्राट आदि) की मदद से छीन ले। तरफा दबाव का नतीजा यह हुआ कि शूद्रों की सेवाएं मुफ्त हो गईं। बेगार लेने के लिए शूद्र को जीवित रखना था, इसलिए विशेष अवसरों यानी शादी-विवाह, पर्व-उत्सवों तथा नई फसल के अवसर पर उनको भेंट-सौगात दी जाने लगी, जिसका स्वरूप भीखनुमा होता था। शूद्र इस छलनीति को समझ न पाए इसके लिए उसके पढ़ने-लिखने पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन यह पाबंदी केवल वैदिक साहित्य को तर्कसम्मत ढंग से पढ़ने, अपने विवेक के अनुसार उसका अर्थ निकालने की थी। ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से अध्ययन-अध्यापन करने पर नहीं। महीदास, सत्यकाम जाबाल शूद्र होकर भी वेदपाठी कहलाए गए, क्योंकि वे ब्राह्मणवाद के श्रेष्ठत्व को स्वीकार कर, उसके आगे समर्पित हो चुके थे।
 इस विस्तृत वर्णन का एक ही उद्देश्य है, बहुजन वर्ग की आंतरिक एकता के सूत्रों की खोज करना। ‘बहुजन साहित्य की प्रस्तावना’ से बहुजन साहित्य की सैद्धांतिकी का आधार स्पष्ट नहीं होता। यह कार्य भविष्य पर छोड़ दिया गया है। यदि यह मान लिया जाए कि बहुजन समूह मेहनतकश जातियों और शिल्पकार समूहों का बेहद सक्रिय और कर्मशील समूह रहा है तो उससे न केवल बहुजन साहित्य की अवधारणा स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है, बल्कि उसके सहारे हम इतिहास के कई बिखरे सूत्रों को भी सहेज सकते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि वर्ण-व्यवस्था द्वारा संसाधनों से वंचित कर दिए जाने के बावजूद शिल्पकार समूह पूरी तरह हताश नहीं हुए थे। बल्कि अपने श्रम, शिल्प-कौशल तथा संगठन सामर्थ्य के दम उन्होंने खुद को इतना सुदृढ़ और व्यापक बना लिया था कि राज्य के लिए उनकी उपेक्षा कर पाना पूर्णतः असंभव था। समानकर्मा शिल्पकारों द्वारा संगठन बनाना उन दिनों सामान्य प्रक्रिया थी। लोग अलग-अलग काम करने के बजाए संगठित व्यापार ज्यादा पसंद करते थे। काष्ठकार, धातुकर्मी, स्वर्णकार, चर्मकार, पत्थर-तराश, हाथी-दांत के आभूषण-निर्माता, जलयंत्र निर्माता, बांसकर्मी, कास्सकार(पीतलकर्मी), बुनकर, कुंभकार, स्वर्णकार, तैलिक, रंगरेज, टोकरी बनाने वाले, अनाज व्यापारी, मत्स्यपालक, किसान, छापाकार, मालाकार, कसाई, नाई, पशुपालक, व्यापारी और व्यापारिक काफिले, दुरुह मार्गों पर व्यापारिक काफिलों की रक्षा करने वाले सैनिक, चोर-लुटेरे, महाजन—बुद्धकालीन भारत में 27 प्रकार के सहयोगी संगठनों का उल्लेख जातक कथाओं के जरिये प्राप्त होता है। इसका उल्लेख डॉ. रमेश मजूमदार ने ‘कोऑपरेटिव्स लाइफ इन एन्शियंट इंडिया’ में विस्तार से किया है। उन दिनों वे आजीवक कहलाते थे। ब्राह्मण धर्म में उनकी कोई आस्था न थी। बाद के दिनों में उन्हें शूद्र घोषित कर दिया गया। चाणक्य ने तो क्षत्रियों के संघ का भी उल्लेख किया है। ये संगठन अपने आप में पूर्णतः स्वायत्त थे। उनके आंतरिक मामलों में दखल देने का अधिकार राज्य को भी नहीं था। चूंकि वे राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थे, इसलिए राजा भी उनके साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाते थे। वे अपनी आजीविका को ही अपना धर्म, अपना ईश्वर मानने वाले थे। जिस दौर के भारत को ‘सोने की चिड़िया’ के रूप में याद किया जाता है, वह इन संगठनों का सबसे सक्रिय कार्यकाल था। इससे हम राज्य की अर्थव्यवस्था में उनके महती योगदान का अनुमान लगा सकते हैं।
इस विस्तृत वर्णन का एक ही उद्देश्य है, बहुजन वर्ग की आंतरिक एकता के सूत्रों की खोज करना। ‘बहुजन साहित्य की प्रस्तावना’ से बहुजन साहित्य की सैद्धांतिकी का आधार स्पष्ट नहीं होता। यह कार्य भविष्य पर छोड़ दिया गया है। यदि यह मान लिया जाए कि बहुजन समूह मेहनतकश जातियों और शिल्पकार समूहों का बेहद सक्रिय और कर्मशील समूह रहा है तो उससे न केवल बहुजन साहित्य की अवधारणा स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है, बल्कि उसके सहारे हम इतिहास के कई बिखरे सूत्रों को भी सहेज सकते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि वर्ण-व्यवस्था द्वारा संसाधनों से वंचित कर दिए जाने के बावजूद शिल्पकार समूह पूरी तरह हताश नहीं हुए थे। बल्कि अपने श्रम, शिल्प-कौशल तथा संगठन सामर्थ्य के दम उन्होंने खुद को इतना सुदृढ़ और व्यापक बना लिया था कि राज्य के लिए उनकी उपेक्षा कर पाना पूर्णतः असंभव था। समानकर्मा शिल्पकारों द्वारा संगठन बनाना उन दिनों सामान्य प्रक्रिया थी। लोग अलग-अलग काम करने के बजाए संगठित व्यापार ज्यादा पसंद करते थे। काष्ठकार, धातुकर्मी, स्वर्णकार, चर्मकार, पत्थर-तराश, हाथी-दांत के आभूषण-निर्माता, जलयंत्र निर्माता, बांसकर्मी, कास्सकार(पीतलकर्मी), बुनकर, कुंभकार, स्वर्णकार, तैलिक, रंगरेज, टोकरी बनाने वाले, अनाज व्यापारी, मत्स्यपालक, किसान, छापाकार, मालाकार, कसाई, नाई, पशुपालक, व्यापारी और व्यापारिक काफिले, दुरुह मार्गों पर व्यापारिक काफिलों की रक्षा करने वाले सैनिक, चोर-लुटेरे, महाजन—बुद्धकालीन भारत में 27 प्रकार के सहयोगी संगठनों का उल्लेख जातक कथाओं के जरिये प्राप्त होता है। इसका उल्लेख डॉ. रमेश मजूमदार ने ‘कोऑपरेटिव्स लाइफ इन एन्शियंट इंडिया’ में विस्तार से किया है। उन दिनों वे आजीवक कहलाते थे। ब्राह्मण धर्म में उनकी कोई आस्था न थी। बाद के दिनों में उन्हें शूद्र घोषित कर दिया गया। चाणक्य ने तो क्षत्रियों के संघ का भी उल्लेख किया है। ये संगठन अपने आप में पूर्णतः स्वायत्त थे। उनके आंतरिक मामलों में दखल देने का अधिकार राज्य को भी नहीं था। चूंकि वे राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थे, इसलिए राजा भी उनके साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाते थे। वे अपनी आजीविका को ही अपना धर्म, अपना ईश्वर मानने वाले थे। जिस दौर के भारत को ‘सोने की चिड़िया’ के रूप में याद किया जाता है, वह इन संगठनों का सबसे सक्रिय कार्यकाल था। इससे हम राज्य की अर्थव्यवस्था में उनके महती योगदान का अनुमान लगा सकते हैं।
उपर्युक्त वर्णन से कुछ बातें साफ हो जाती हैं। पहली, संगठन एकता की ताकत। दूसरी, समान-धर्मा संगठनों के साथ एकता की जरूरत, तीसरी धार्मिक मिथ्याडंबरों के बजाय तर्कसम्मत ढंग से निर्णय लेने की कला और चौथी, चुनौतियों से भागने की बजाय परिस्थितियों के साथ संघर्ष करते हुए रास्ता निकालने की कोशिश करना। जाति-आधारित विषमता आज की समस्या नहीं है। सहस्राब्दियों से वह अस्तित्व में है। उसके विरोध में समय-समय पर आंदोलन छेड़े गए हैं। परंतु समस्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई है। इसका पहला कारण तो यही है कि जोतिबा फुले से पहले जाति-विरोधी आंदोलनों की बागडोर मुख्यतः सवर्णों के हाथों में रही है। हालांकि मध्यकाल में कबीर, रैदास जैसे संत कवि शूद्र या अतिशूद्र जातियों से आए थे। जाति के विरोध में संत कवियों ने लगातार लिखा भी। परंतु वे संतोष को परमधन मानने वाले, दैन्य का महिमामंडन करने वाले संत थे। हालांकि रैदास ने ‘बेगमपुरा’ तथा कबीर ने ‘अमरपुरी’ के रूप में समानता पर आधारित समाज की कल्पना की थी। तो भी आर्थिक असमानता और संसाधनों पर द्विज वर्गों के एकाधिकार को लेकर उन्हें बहुत ज्यादा शिकायत न थी। उसे लेकर उनका दृष्टिकोण नियतिवादी था। बावजूद इसके संतकवियों का अपने समाज पर प्रभाव था। अपनी सीमाओं के भीतर उन्होंने ब्राह्मणवाद पर जोरदार प्रहार किया था। संतकवियों की समाज में बढ़ती प्रतिष्ठा को देख द्विज वर्गों के कवि भी उनकी ओर आकर्पित हुए। वे अपने साथ वर्गीय संस्कार भी लाए थे। उन्होंने संत-कवियों की मौलिक अध्यात्म चेतना का धार्मिकीकरण किया। परिणामस्वरूप संतकाव्य की क्रांतिधर्मिता भक्तिकाव्य में सिमटने लगी। तुलसी के आते-आते तो सबकुछ परंपरावादी हो गया। जाति और वर्ण पुनः प्रधान हो गए। उन्नीसवीं शताब्दी तक राजनीति पर धर्म का प्रभाव बना रहा। चूकि धर्म की नींव जाति-व्यवस्था पर टिकी थी, इसलिए जाति के बहिष्कार को लेकर कोई बड़ा आंदोलन उनीसवीं शती से पहले के इतिहास से नदारद है।
जाति और हिंदू धर्म के गठजोड़ को इससे भी समझा जा सकता है कि बौद्ध धर्म से लेकर संत कवियों, सुधारवादी आंदोलनों, ज्योतिराव फुले और डॉ. आंबेडकर सहित जिसने भी जाति के पर कतरने की कोशिश की—प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में उसने धर्म पर भी प्रहार किया। यह आवश्यक था। क्योंकि हिंदू धर्म और जाति-व्यवसथा में नाभि-नाल का संबंध है। दोनों एक-दूसरे को बल प्रदान करते हैं। जाति पर सवाल उठाया जाता है तो धर्म आड़े आ जाता है और धर्म पर सवाल उठाते ही जाति बीच में अड़ जाती है। बुद्ध ने जाति का बहिष्कार किया था, लेकिन उनके बाद बौद्ध धर्म की बागडोर उन लोगों के हाथ में आ गई जो जन्मना सवर्ण थे। उन्हें बुद्ध के धर्म से कोई परेशानी न थी। परेशानी उनके जाति-विरोध से थी। सो उन्होंने धर्म को सहारा लिया। अपना जीवन और समय उन्हें दिया। परंतु जाति के सवाल पर वे सब ठेठ परंपरावादी निकले। अवसर मिलते ही उन्होंने बौद्ध दर्शन के क्रांतिकारी विचारों को धीरे-धीरे जाति-धर्म की ब्राह्मणवादी व्यवस्था से जोड़ने का काम शुरू कर दिया। बुद्ध को अवतार घोषित कहना, यह कहना कि ‘बुद्ध या तो ब्राह्मण के घर जन्म लेते हैं, अथवा क्षत्रिय के’, ब्राह्मणवादियों की तर्कसम्मत निष्कर्षों से पलायन की मानसिकता को दर्शाता है। बौद्ध लेखकों ने प्रथम शास्ता के निर्वाण प्राप्ति के तुरंत बाद अपनी जातिवादी मानसिकता को थोपना आरंभ कर दिया था। इसके लिए उन्होंने बुद्ध को भी नहीं बख्शा, जो आजीवन संघ और समानता का उपदेश देते रहते थे। असल में वह बुद्ध के जीवन-दर्शन की पश्चगामी व्याख्या थी। उन संगठनों की एक कमी खुद को केवल और केवल व्यवसाय तक सीमित रहना था। ज्ञान की शक्ति से अनभिज्ञ रहना तथा ज्ञानार्जन को ब्राह्मणों का विशेषाधिकार मानकर उसकी ओर से उदासीन बन जाना भी, उनकी कमजोरी थी। महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉ.अंबेडकर सफल रहे तो इसलिए कि उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बौद्धिक क्षेत्र में चुनौती दी थी। दोनों ने जीवन के आर्थिक पक्ष पर जोर दिया। उसके फलस्वरूप सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर समानता की मांग होने लगी।
बहुजन साहित्य की अवधारणा विकसित करने में समाज के पुराने अनुभव बहुत काम के सिद्ध हो सकते हैं। क्योंकि जो-जो बंधु बहुजन साहित्य को तथाकथित मुख्य धारा के साहित्य के समानांतर देखना चाहते हैं, उनसे सबसे पहले यही सवाल होगा इसकी मूल अवधारणा या सैद्धांतिकी को लेकर उनकी अपना सोच क्या है? उसमें जाति की क्या भूमिका होगी? क्या जाति का सहारा लेकर शुरू हुआ आंदोलन उसके बिना चार कदम भी चल पाएगा? यदि ऐसा नहीं हो सकता तो बाकी साहित्य और बहुजन साहित्य में क्या अंतर होगा? इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि जाति भारतीय समाज की एक कटु सचाई है। मजबूरी में ही सही, बहुजन साहित्यकारों को इस आंदोलन से जोड़ने का तुरंतिया आधार जाति ही है। बावजूद इसके वैकल्पिक साहित्य और संस्कृति की आधारशिला रखने के लिए जाति जैसी विष-बेलि पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उससे व्यक्ति की बड़ी और स्थायी पहचान नहीं बनती। मार्क्स के दर्शन में जब ‘सर्वहारा’ का नाम लेते हैं तो बेमेलकारी औद्योगिक अर्थव्यवस्था में उपेक्षित, तिरष्कृत, चारों तरफ से छले गए, शोषित व्यक्ति की तस्वीर हमारे मनस् में उभरने लगती है। जाति की मार उससे कहीं ज्यादा घातक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी सर्वहारा को यह अधिकार देती है कि वह पूंजी के दम पर अपनी स्थिति बदलकर पूंजीवादी तबके में शामिल हो सके। जाति न केवल व्यक्ति, बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी इस अधिकार से वंचित रखती है। इसलिए जाति की बैशाखी के सहारे बड़ा और परिवर्तनकारी आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। इस मामले में ‘बहुजन’ सार्थक शब्द है। इससे लोकतंत्र की ध्वनि निकलती है। इसलिए बहुजन साहित्य के नाम पर ऐसा साहित्य स्वीकार्य हो सकता है, जो लोगों में लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति चेतना जगाए।
 वैसे भी साहित्यपन की कसौटी रचना में अंतर्निहित सर्वहित का भाव है। यह मनुष्य की सीमा है कि सिक्के के दूसरे पक्ष को देखने के लिए पहले को आंखों से ओझल करना ही पड़ता है। ऐसे में उदारमना लेखक केवल इतना कर सकता है कि लिखते समय अपनी सोच का दायरा यथासंभव व्यापक रख सके। इस दृष्टि से देखें तो हिंदी का अधिकांश साहित्य ब्राह्मणवादियों द्वारा ब्राह्मणवाद के समर्थन में लिखा गया साहित्य है। वह एक प्रकार का स्तुति-लेखन है, जो येन-केन-प्रकारेण द्विज-हितों का पोषण करता है। संख्याबल के आधार पर ब्राह्मणवाद से लाभान्वित लोगों की संख्या कुल जनसंख्या के पांचवे हिस्से भी कम हैं। जाहिर है, जिसे साहित्य की मुख्यधारा कहा जाता है, वह अल्पसंख्यकों सत्तानशीनों द्वारा अल्पसंख्यक अभिजनों की स्वार्थ-सिद्धि के निमित्त किया गया लेखन है। सामाजिक स्तरीकरण को शास्त्रीय स्वरूप प्रदान करने में उसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। तुलसी, सूर, वाल्मीकि, कालीदास आदि इस धारा के प्रतिनिधि रचनाकार कहे जा सकते हैं। कहने को उनके साहित्य में स्त्री, अल्पसंख्यक, दलित, गरीब-अमीर सब आते हैं। परंतु उनका उपयोग द्विज चरित्रों के महिमा-मंडन के लिए किया जाता है, ताकि सामाजिक भेदभाव वाली व्यवस्था के प्रति लोगों का मूक समर्थन बना रहे। इस प्रकार वे आसमानताकारी व्यवस्था को खाद-पानी देने का काम करते हैं, ताकि वह निर्बंध फल-फूल सके। ब्राह्मणवादी कह सकते हैं कि जब उनके साहित्य में स्त्री, अल्पसंख्यक, दलित, गरीब-अमीर सब हैं, तब साहित्य की नई धारा की जरूरत और उसका औचित्य क्या है? वे यह भी कह सकते हैं भारत में उसके समानांतर क्या उसके दूर-दूर तक कोई ऐसी साहित्य धारा नजर नहीं आती जो उसको चुनौती देने में सक्षम हो, तो उससे मुख्यधारा का साहित्य मानने में गुरेज क्यों हो? उन्हें समझाने के लिए, बशर्ते वे समझना चाहें तो कहा जा सकता है कि किसी रचना के साहित्य होने की पहली शर्त यह है कि वह हाशिया नहीं छोड़ती। यदि कुछ हाशिये पर है तो उसे प्राथमिकता के साथ केंद्र में लाकर विमर्श में सम्मिलित करने की कोशिश करती है। यदि वे अपने साहित्य को मुख्यधारा का साहित्य मानते हैं तो इसका यह अर्थ भी है कि साहित्य में उनके चाहे-अनचाहे ऐसी धाराएं भी मौजूद हैं, जो उपेक्षित या हाशिये की हैं। और ऐसा होने से उन्हें कोई शिकायत भी नहीं है। यदि कभी बराबर में लाने की कोशिश हुई भी तो उपकार भाव से। मानो वही उनके तारणहार हों। यह सोच ही ब्राह्मणवादी ग्रंथों को साहित्य के गौरव से बेदखल करने के लिए पर्याप्त है। बीती दो सहस्राब्दियों के बीच। ब्राह्मणवादी साहित्य द्वारा विरोधी विचारधाराओं से समन्वय या संवाद की संभावना तो दूर, उसकी कोशिश तो उन्हें नकारने और मिटाने की रही है।
वैसे भी साहित्यपन की कसौटी रचना में अंतर्निहित सर्वहित का भाव है। यह मनुष्य की सीमा है कि सिक्के के दूसरे पक्ष को देखने के लिए पहले को आंखों से ओझल करना ही पड़ता है। ऐसे में उदारमना लेखक केवल इतना कर सकता है कि लिखते समय अपनी सोच का दायरा यथासंभव व्यापक रख सके। इस दृष्टि से देखें तो हिंदी का अधिकांश साहित्य ब्राह्मणवादियों द्वारा ब्राह्मणवाद के समर्थन में लिखा गया साहित्य है। वह एक प्रकार का स्तुति-लेखन है, जो येन-केन-प्रकारेण द्विज-हितों का पोषण करता है। संख्याबल के आधार पर ब्राह्मणवाद से लाभान्वित लोगों की संख्या कुल जनसंख्या के पांचवे हिस्से भी कम हैं। जाहिर है, जिसे साहित्य की मुख्यधारा कहा जाता है, वह अल्पसंख्यकों सत्तानशीनों द्वारा अल्पसंख्यक अभिजनों की स्वार्थ-सिद्धि के निमित्त किया गया लेखन है। सामाजिक स्तरीकरण को शास्त्रीय स्वरूप प्रदान करने में उसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। तुलसी, सूर, वाल्मीकि, कालीदास आदि इस धारा के प्रतिनिधि रचनाकार कहे जा सकते हैं। कहने को उनके साहित्य में स्त्री, अल्पसंख्यक, दलित, गरीब-अमीर सब आते हैं। परंतु उनका उपयोग द्विज चरित्रों के महिमा-मंडन के लिए किया जाता है, ताकि सामाजिक भेदभाव वाली व्यवस्था के प्रति लोगों का मूक समर्थन बना रहे। इस प्रकार वे आसमानताकारी व्यवस्था को खाद-पानी देने का काम करते हैं, ताकि वह निर्बंध फल-फूल सके। ब्राह्मणवादी कह सकते हैं कि जब उनके साहित्य में स्त्री, अल्पसंख्यक, दलित, गरीब-अमीर सब हैं, तब साहित्य की नई धारा की जरूरत और उसका औचित्य क्या है? वे यह भी कह सकते हैं भारत में उसके समानांतर क्या उसके दूर-दूर तक कोई ऐसी साहित्य धारा नजर नहीं आती जो उसको चुनौती देने में सक्षम हो, तो उससे मुख्यधारा का साहित्य मानने में गुरेज क्यों हो? उन्हें समझाने के लिए, बशर्ते वे समझना चाहें तो कहा जा सकता है कि किसी रचना के साहित्य होने की पहली शर्त यह है कि वह हाशिया नहीं छोड़ती। यदि कुछ हाशिये पर है तो उसे प्राथमिकता के साथ केंद्र में लाकर विमर्श में सम्मिलित करने की कोशिश करती है। यदि वे अपने साहित्य को मुख्यधारा का साहित्य मानते हैं तो इसका यह अर्थ भी है कि साहित्य में उनके चाहे-अनचाहे ऐसी धाराएं भी मौजूद हैं, जो उपेक्षित या हाशिये की हैं। और ऐसा होने से उन्हें कोई शिकायत भी नहीं है। यदि कभी बराबर में लाने की कोशिश हुई भी तो उपकार भाव से। मानो वही उनके तारणहार हों। यह सोच ही ब्राह्मणवादी ग्रंथों को साहित्य के गौरव से बेदखल करने के लिए पर्याप्त है। बीती दो सहस्राब्दियों के बीच। ब्राह्मणवादी साहित्य द्वारा विरोधी विचारधाराओं से समन्वय या संवाद की संभावना तो दूर, उसकी कोशिश तो उन्हें नकारने और मिटाने की रही है।
दलित, पिछड़े, आदिवासी, आदिम जनजातियां आदि जिन जाति-समूहों को केंद्र में रखकर बहुजन साहित्य की अभिकल्पना की गई है, वे सभी किसी न किसी श्रम-प्रधान जीविका से जुड़े हैं। उनकी पहचान उनके श्रम-कौशल से होती आई है। मगर जाति-वर्ण संबंधी असमानता और संसाधनों के अभाव में उन्हें उत्पीड़न एवं अनेकानेक वंचनाओं के शिकार होना पड़ा है। बहुजन साहित्य यदि जातियों की सीमा में खुद को कैद रखता है तो उसके स्वयं भी छोटे-छोटे गुटों में बंट जाने की संभावना निरंतर बनी रहेगी। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से श्रम-संस्कृति का सम्मान करेगा। फलस्वरूप विभिन्न जातियों के बीच स्तरीकरण में कमी आएगी। उसकी यात्रा सर्वजनोन्मुखी साहित्य में ढलने की होगी। कुल मिलाकर बहुजन साहित्य का वास्तविक ध्येय जाति उच्छेद ही होगा। इस तरह बहुजन साहित्य का संघर्ष सभी प्रकार की असमानता, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक से होना चाहिए। तथाकथित सवर्ण जो भारतीय समाज के अभिजन चरित्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, बहुजन साहित्य में दखल देते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। बशर्ते वे समानता और श्रम-संस्कृति के विचार का समर्थन करते हों। श्रम-संस्कृति को महत्त्व देने का आशय ज्ञान की मौलिक धाराओं से कट जाना नहीं है। बहुजन साहित्य ज्ञान के लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए उसकी विभिन्न धाराओं का खुले मन से स्वागत करेगा। परंतु ज्ञान और श्रम को लेकर जिस प्रकार की दूरी ब्राह्मणवादी परंपरा रही है, बहुजन साहित्य में उसके लिए कोई स्थान न होगा, न होना चाहिए।
परिशिष्ट
‘दलित साहित्य’ हो या ‘ओबीसी साहित्य’ अथवा उसका नया नामरूप ‘बहुजन साहित्य’ हो, ये सब समाज और संस्कृति के बजाय चाहे-अनचाहे राजनीति से ज्यादा अनुप्रेत हैं। इसके दो कारण हैं। पहला यह कि भागम-भाग के इस दौर में हर कोई त्वरित परिवर्तन की चाहत रखता है। यह काम उसको राजनीति के माध्यम से आसान लगता है। लेकिन राजनीति की विशेषता है कि उसका कोई न कोई सत्ताकेंद्र होता है। जो भी उसके नजदीक या प्रभाव में आता है, दूरस्थ वर्गों को वह खुद से हीन समझने लगता है। यदि उसपर समाज और संस्कृति का अनुशासन न हो तो वह बहुत जल्दी शक्तिशाली समूहों के वर्चस्व में ढल जाता है। दलित और पिछड़े दोनों ही वर्ग इसके शिकार रहे हैं। 1930 में बिहार और पूर्वी उत्तरप्रदेश की तीन प्रमुख पिछड़ी जातियों ने मिलकर ‘त्रिवेणी संघ’ की स्थापना की थी। उसके सदस्यगण बरास्ते राजनीति द्विज वर्गों के बराबर में आना चाहते थे। उन्हें आरंभिक सफलता भी मिली। परंतु पर्याप्त सामाजिक चेतना के अभाव में वह प्रयोग, महत्त्वपूर्ण होने के बावजूद अंततः असफल सिद्ध हुआ। कारण लोगों के दिमाग में मौजूद जाति की विषबेलि। इसके बावजूद परिवर्तनकामी समाजों में राजनीति का अलग महत्त्च होता है। प्राचीनकाल से लेकर आज तक समाज, संस्कृति और राजनीति सभी पर द्विज वर्गों का अधिपत्य रहा है। दलित और बहुजन दोनों ने ही समाज में जो हैसियत प्राप्त की है, या जिसका वे सपना देखते हैं, उसके लिए उन्हें समाज और संस्कृति दोनों से संघर्ष करना पड़ा है। दोनों ही दलित और पिछड़ों के शोषण का माध्यम बनते आए हैं। उनके दैन्य का कारण भी समाज और संस्कृति के निर्माण में उनकी भूमिका की निरंतर उपेक्षा, उसे कमतर आंका जाना है। इस मामले में स्वतंत्र भारत की राजनीति उनके लिए अधिक मददगार रही है। इसलिए साहित्य में राजनीति को महत्त्व देना या राजनीति के माध्यम से अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक हैसियत ऊपर उठाना अभी तक के उनके संघर्ष की मूल प्रेरणा रहा है।
दलित साहित्य भी इसी त्रासदी से गुजर रहा है। समाज और संस्कृति को राजनीति की अपेक्षा कम महत्त्व देने के कारण दलितों में भी शासक वर्ग का उदय होने लगा है। ‘बीसवीं शती अंबेडकर की होगी’ जैसे नारे इसी मानसिकता की देन है। नारेबाज प्रायः ऐसे राज्य का सपना देखते हैं, जिसमें वर्तमान मनुवादी शक्तियों का पराभव हो चुका होगा। लेकिन मनुवादी शक्तियों का पराभव ‘मनुवाद’ या ‘ब्राह्मणवाद’ का पराभव नहीं नहीं है। ‘मनुवाद’ विचार से अधिक आज एक मानसिकता है। मनुवादी शक्तियों का पराभव हो परंतु मनुवाद नए चेहरे-मोहरों के रूप में बना रहे यह न तो अंबेडकर का सपना था, न ही आज के लिए सुधी समाजचेता का सपना हो सकता है। मनुवाद का पराभव बिना जाति के पराभव के असंभव है। फुले और अंबेडकर दोनों यह जानते थे। इसलिए अपनी-अपनी तरह से दोनों ने ही जाति का विरोध किया था। डॉ.अंबेडकर की पुस्तक ‘जाति का उच्छेद’ इस सवाल को बार-बार उठाती है। दलित साहित्य ने लोगों को इतना आत्मविश्वास तो दिया है कि जो दलित दो-तीन दशक पहले तक जाति को छिपाने में ही अपनी भलाई समझता थे, अब अपने नाम के साथ खुलकर ‘वाल्मीकि’, ‘जाटव’ आदि जाति-सूचक शब्द लगाने लगे हैं। ‘जाति के उच्छेद’ की दिशा में ऐसा आत्मविश्वास आवश्यक है। यहां मुझे पाब्लो फ्रेरा याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि उत्पीड़ित वर्ग अपनी सफलता अनुत्पीड़क वर्ग की अवस्था में आने में देखता है। इसलिए जो शिखर पर है, उसपर ढेर सारे लोगों की निगाहें होती हैं। इसलिए शिखर पर अस्थिरता का मामला बना रहता है। जो लोग शिखर पर पहुंचने का हौसला नहीं रखते, वे शिखर के आसपास मंडराते रहते हैं। प्रेमचंद ने साहित्य को राजनीति के आगे चलने वाली मशाल कहा है। इसके लिए आवश्यक है कि साहित्य और राजनीति के बीच न्यूनतम दूरी हो। बहुजन साहित्य राजनीति से प्रेरणाएं, राजनीति की प्रेरणा बनने की कोशिश करेगा, परंतु सीधे राजनीतिक हस्तक्षेप या सहयोग से खुद को दूर रखेगा।
साहित्य की एक शर्त मानवीय अस्मिताओं के बीच समानता और समरसता का वातावरण उत्पन्न करना है। इसके लिए उसकी दृष्टि हमेशा उपेक्षित एवं निचले वर्गों की ओर होती है। ब्राह्मणवादी साहित्य प्रायः सत्ताकेंद्रित रहा है। यह बात अलग है कि उसके द्वारा मनोनीत सत्ताकेंद्र कभी राजनीति तो कभी धर्म की ओर झुकते रहे हैं। इसलिए ब्राह्मणवादी रचनाकारों के लेखन को मुख्यधारा का साहित्य नहीं कहा जा सकता। बजाय इसके उसे इस देश के अभिजन समूहों का वर्चस्वकारी साहित्य कहना उपयुक्त होगा। यह मान लेना चाहिए कि अस्मितावादी आंदोलन चाहे वे दलित आंदोलन हों या पिछड़े वर्गों का संघर्ष या कोई और, कोई भी जाति के दुर्ग को भेदने में असफल रहा है। याद करें भारत में जितनी जातियां हैं उससे कहीं अधिक उपजातियां भी हैं। सवर्ण में जहां गोत्रों की व्यवस्था है, वहीं तरह-तरह के भेद भी हैं। कुछ समय पहले तक ब्राह्मणों में ही दर्जनों उपजातियां थीं। उनके बीच इतना अंतर था कि तथाकथित उच्च श्रेणी का ब्राह्मण निचली श्रेणी के ब्राह्मणों के साथ रोटी-बेटी का संबंध तो दूर, बराबर में बैठकर भोजन करना पसंद नहीं करता था। इसलिए यह कहना कि जातिवाद देश में आज भी उतना ही है जितना पहले था, बड़ी भूल है। इसका श्रेय देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और निचले वर्गों द्वारा शिक्षा प्राप्त कर, द्विजों के लिए चुनौती देने की अवस्था में आना रहा है।
पुस्तक : बहुजन साहित्य की प्रस्तावनासंपादक : प्रमोद रंजन, आयवन कोस्काप्रकाशक : द मार्जिंलाइज्ड, सानेवाड़ी वर्धा, महाराष्ट्र-442001,पहला संस्करण : 100 रूपये
मंगवाने के लिए संपर्क करें : फोन – 9968527911




