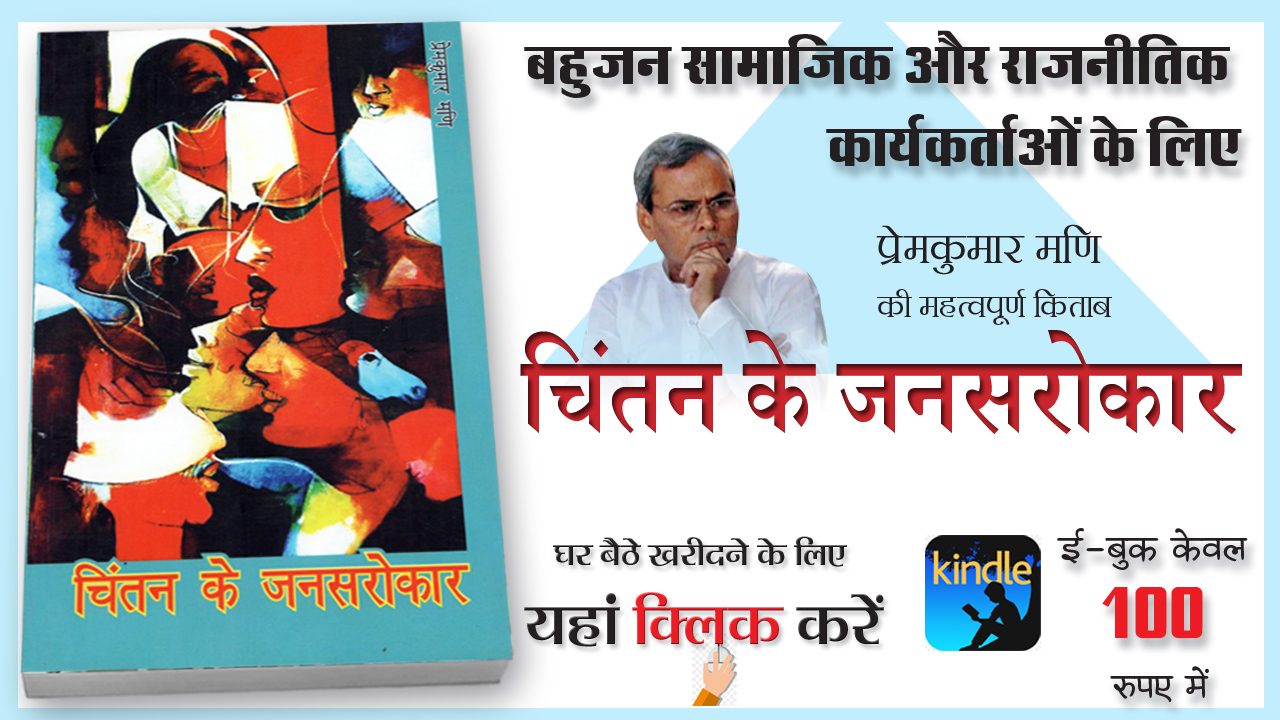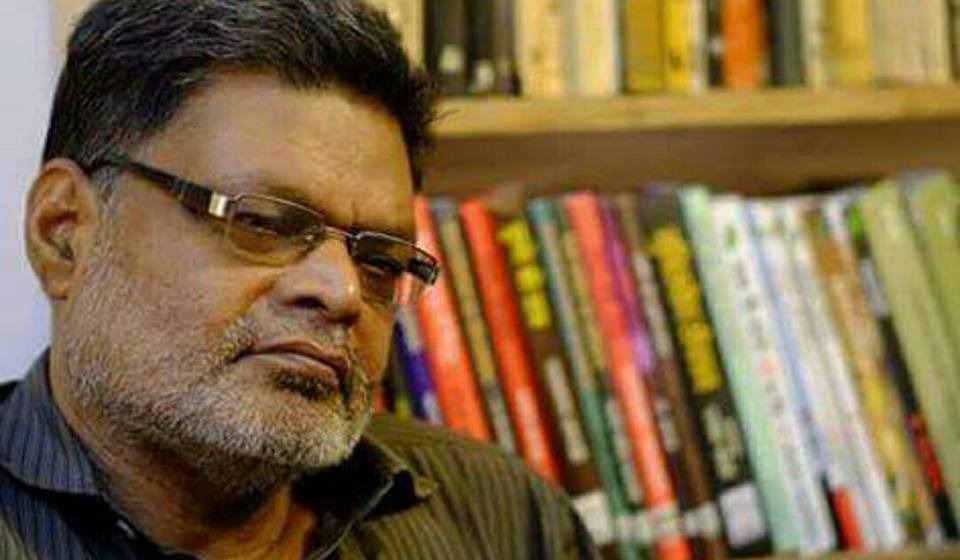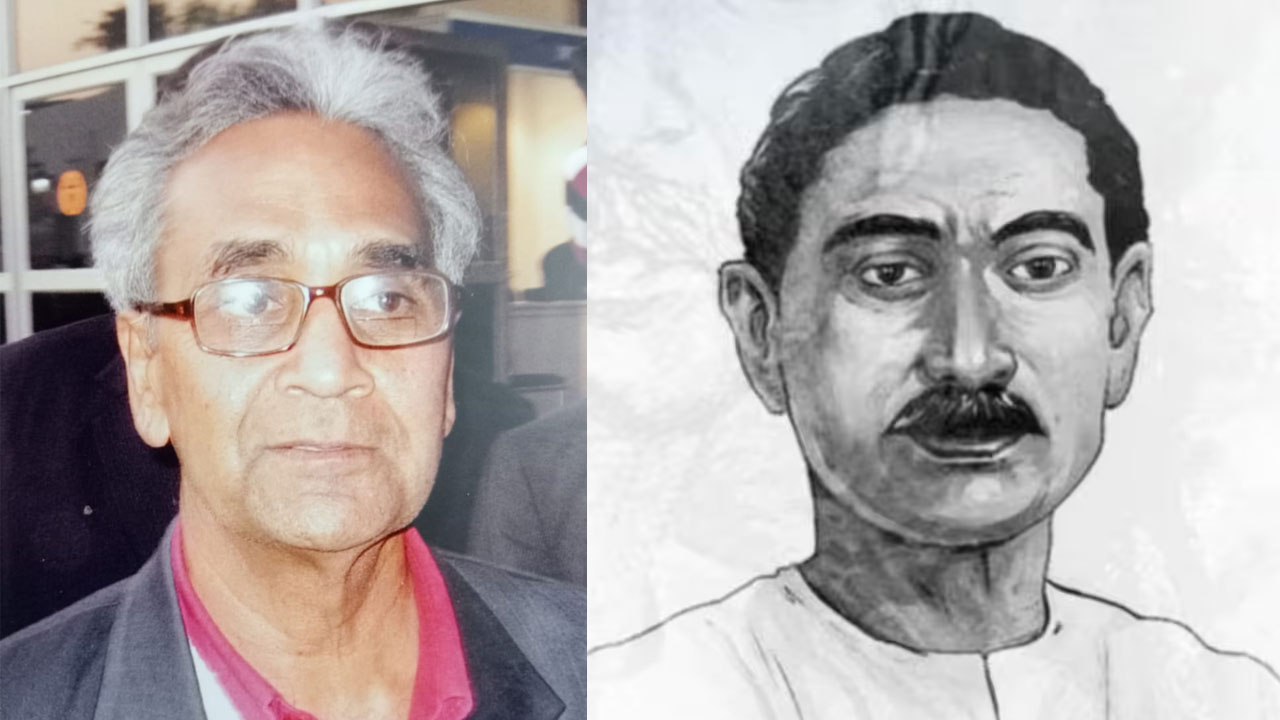जब हम भारतीय समाज और उसके विभिन्न मुद्दों की बात करते हैं, तब कई सवाल सामने आते हैं। मसलन, चिंतन के वे कौन से मानक हैं, जो वास्तव में बेहतर समाज के निर्माण में सहायक हैं। जाहिर तौर पर जब हम ऐसे मानकों की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने समाज का वह हिस्सा आता है, जो वंचित है। वह वंचित केवल सामाजिक रूप से ही नहीं है। आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से भी वह बहुत पिछड़ा हुआ है। ऐसे में यदि चिंतन के बिंदु हों, तो क्या हों और उनका दायरा कहां तक विस्तृत हो, यह महत्वपूर्ण हो जाता है।
प्रेमकुमार मणि की किताब ‘चिंतन के जन सरोकार’ समाज, राजनीति और साहित्य पर केंद्रित है, जिसमें उनके द्वारा समय-समय पर की गई टिप्पणियों व लेखों को शामिल किया गया है। लेखक ने सामाजिक व्यवस्था व रूढ़िवादी सोच पर करारा प्रहार कर अपने अनुभव को साझा किया है कि किस तरह किसान, मजदूर व दस्तकार परिवारों के साथ छल किया जाता रहा है, जबकि यह संघर्षशील शोषित तबका शुरू से ज्ञान हासिल कर शोषण से मुक्ति चाहता था लेकिन पहले उसे ऐसा करने से रोका गया। मगर उनमें जागृति आने से आगे ऐसा नहीं हो पाया और समाज के वर्चस्व प्राप्त कुलीन तबके की चाल धाराशायी हो गई। इसमें बाबा साहब भीमराव आंबेडकर का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बहुसंख्यक की अवधारणा सबसे पहले सामने लाकर समाज के शोषित वर्गों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने का काम किया और आज जहां जो कुछ, जिस भी स्थिति में बहुसंख्यक हैं; वह बाबा साहब की सोच की ही देन है।

दबे-कुचले, शोषित वर्ग के लिए बाबा साहब ने क्या किया है; यह कहने की बात नहीं है। लेखक ने तो अपनी इस किताब में एक पूरा आलेख डॉ. आंबेडकर पर लिखा है और उसका शीर्षक ही गांधी से ज्यादा आंबेडकर का भारत रखा है। अपने इस शीर्षक के समर्थन में लेखक ने जो बातें कहीं हैं, वाे भी गौर करने वाली हैं। लेखक ने सवाल किया है कि आज जो भारत है, उसके निर्माण में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है? दूसरे शब्दों में कहें तो आज का भारत किससे ज्यादा प्रभावित है?
यह सवाल जब आप किसी सवर्ण हिंदू से करेंगे, तब वह कहेगा गांधी से या नेहरू से। कुछ मध्यमवर्गीय लोग ऐसे भी होंगे जो गांधी,नेहरू के साथ-साथ कुछ और नाम जोड़ देंगे और बहुत कम, नहीं के बराबर लोग होंगे जो अपनी सूची में डॉ. आंबेडकर को रखेंगे। लेकिन यही सवाल जब आप दलितों व सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग (जिसे अब सामान्य ओबीसी कहा जाने लगा है ) के लोगों से करेंगे, तब ज्यादातर के पास बाबा साहब डॉ. आंबेडकर का नाम होगा। यह कहना अतिशयाेक्ति नहीं होगी कि दलितों और पिछड़े वर्गों के शिक्षित समुदाय के मानस के गठन की पृष्ठभूमि आंबेडकरवादी अवयवों से हुई है। हालांकि, कुछ मामलों में प्रत्यक्ष रूप से और ज्यादातर मामलों में परोक्ष रूप से।
लेखक ने समय के साथ बाबा साहब के बढ़ते प्रभाव का जिक्र करते हुए लिखा है कि 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का जब निधन हुआ था, तब दिल्ली के एक छोटे समूह में शोक की लहर छा गई थी। छोटा समूह इसलिए कहा गया, क्योंकि दिल्ली में दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों का तब कोई बड़ा समूह नहीं था। बड़ा समूह तो आज भी नहीं है, लेकिन अब पहले वाली बात नहीं है। सार में कहें, तो डॉ. आंबेडकर का आज जो प्रभाव है, उसके अनुरूप उनकी अंतिम यात्रा (शव यात्रा) नहीं थी।
इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लेखक ने अपनी किताब में 1980 के पहले और आज की स्थिति पर चर्चा की है और बताया है कि 1980 के पूर्व स्कूल-कॉलेजों में विनोबा भावे तक की जीवनी पढ़ाई जाती थी, लेकिन दूर-दूर तक आंबेडकर के नाम की चर्चा नहीं होती थी। 1980 के बाद ही कुछ बदलाव हुआ और यह भी सच है कि आंबेडकर चर्चा के केंद्र में किसी सरकारी प्रचार माध्यम या मीडिया के बूते नहीं, बल्कि अपनी ताकत से आए। दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे-जैसे दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों में शिक्षा का प्रसार हुआ, उनके मानस पर थोपे गए गांधी व नेहरू कमजोर होने लगे और आंबेडकर का प्रभाव स्वाभाविक रूप से बढ़ता चला गया। आज पूरे भारत के गांव, टोलों और नगरों में सबसे अधिक मूर्तियां अगर किसी की हैं, तो वाे भारत रत्न बाबा साहब डॉ. आंबेडकर की हैं। इनमें बहुत कम मूर्तियां सरकारी कोष से बनी हैं। ज्यादातर का निर्माता वह जनसमूह है, जिसने अपने मुक्तिदाता के रूप में उन्हें स्वीकार किया है।
लेखक ने अपनी इस किताब में साफ-साफ शब्दों में यह साबित करने की कोशिश की है कि इस दौर में नेहरू तो कहीं नहीं ठहरते, गांधी भी पीछे छूट चुके हैं और दिन-ब-दिन और पीछे छूटते जा रहे हैं। कोई नेता लोकप्रियता के मामले में डॉ. आंबेडकर का मुकाबला नहीं कर सकता। राम, कृष्ण, बुद्ध जैसे पौराणिक-ऐतिहासिक महापुरुषों के बाद आधुनिक युग के दो महत्वपूर्ण लोग हैं, जिनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय अवकाश होता है। ये दो हैं गांधी और आंबेडकर।
यह भी पढ़ें : नए सिरे से सोचने को विवश करती किताब : चिंतन के जनसरोकार
हालांकि, लेखक ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि गांधी का शुरुआती दौर में जो महत्व था, उसके सामने आंबेडकर कहीं नहीं टिकते थे; लेकिन स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जैसे आधुनिक उसूलों के लिए आंबेडकर ने जो कार्य किए, उसके सामने गांधी बौने दिखते हैं। आंबेडकर ने विषम परिस्थितियों में शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी और एक छोटे से तबके द्वारा पूरे देश के शोषण की तरफ ध्यान आकर्षित करवाया था। गांधी-विनोबा बनने में उनकी रुचि नहीं थी। उनकी रुचि वाल्तेयर, रूसो और मार्क्स बनने में थी। वे एक मार्क्सवादी की तरह ही स्वीकारते थे कि राजनीति केवल अधिरचना है। इसमें फेरबदल करने से कुछ नहीं होगा। मूल चीज है समाज। जब हम समाज में बदलाव ला देंगे, तब अधिरचना में स्वतः बदलाव आ जाएगा। इसलिए, उनका इस बात पर जोर था कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करना ही होगा। उनका सारा जोर सामाजिक बदलाव पर था।
लेखक ने अपने आलेख के जरिए यह बताने की हर संभव कोशिश की है कि आज का भारत किसलिए उन्हें गांधी से ज्यादा आंबेडकर का भारत प्रतीत होता है। भारतीय लोकतंत्र की गहरी हो रही जड़ें उनकी ही विरासत हैं। सामाजिक न्याय की आधारशिला उन्होंने रखी थी, जो आज सभी राजनीतिक वैचारिकी से ऊपर है।
लेखक ने अपनी इसी किताब में आर्थिक उदारीकरण और दलित शीर्षक से भी एक आलेख लिखा है, जिसमें बताने की कोशिश की है कि उदारीकरण से किसका उदारीकरण हुआ? क्या दलितों का इस दौर में विकास हुआ? लेखक ने बताया है कि समाजवादी ढांचे की जो अर्थव्यवस्था थी, वह किसी भी दृष्टिकोण से समाजवादी व्यवस्था नहीं थी। समाजवाद के केवल कुछ उसूलों को अपनाया गया था। निजी पूंजी पर बहुत चोट नहीं की गई थी, लेकिन इसके समानांतर सावर्जनिक क्षेत्र के रूप में राज्य ने एक औद्योगिक ढांचा जरूर खड़ा किया था। निजी उद्यम पर रोक नहीं थी, लेकिन नियंत्रण जरूर था। इस व्यवस्था का एक झटके में अंत हो गया। तथाकथित समाजवादी ढांचे की छुट्टी कर दी गई, सरकार ने उद्योग और बाजार पर अपनी पकड़ और अपना नियंत्रण छोड़ दिया।अब सरकार और बाजार आमने-सामने थे। या यों कहें कि बाजार के बीच सरकार थी। देखते-देखते बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था हो गई और इससे दलित-पिछड़े भौचक रह गए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एक-एक करके उखड़ने लगे। यह वह समय था, जब बहुजनों की पहली या दूसरी पीढ़ी स्कूल जा रही थी। उदारीकरण से सरकारी नौकरियां घटने लगी थीं और तब दलित-पिछड़ों के बीच यह बात चर्चा में थी कि सत्ता में बैठे ब्राह्मणों ने षड्यंत्र किया है। आरक्षण ने नौकरियों में उनकी भागदारी को संकुचित किया, तो उन्होंने स्वतंत्र बाजार की संरचना कर डाली। यह बाजार उच्च तबके अर्थात सवर्णों का अभयारणय है; ऐसा प्रचारित हुआ।
लेखक ने इस बात का भी जिक्र किया है कि दलितों से जुड़े मुद्दों पर विचार करने वाली गेल ऑम्वेट जैसे लोग मुक्त अर्थव्यवस्था अथवा उदारीकरण के पक्षधर क्यों हैं? गेल के लेख का हवाला देकर बताने की कोशिश की गई है कि कॉरपोरेट सेक्टर में सबसे अधिक ब्राह्मण हैं और ओबीसी के लोग महज 4.5 प्रतिशत हैं। बनिया जाति की संख्या भी ब्राह्मणों की लगभग आधी है। यही वजह है कि दलित बहुजन मुक्त अर्थव्यवस्था का न ज्यादा अभिनंदन कर रहे हैं और न ही उससे ज्यादा भयभीत है। मुक्त, ग्लोबल अर्थव्यवस्था ने देशी बनिया-ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी है और उम्मीद की जाती है कि अंततः वह इसे ध्वस्त कर देगी। यही वजह है कि इसे बहुजन नजरिया सकारात्मक मानता है। लेखक का साफ मानना है कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था ने भारतीय अर्थव्यवस्था के ब्राह्मणवादी चरित्र को खारिज करके एक अनुकूल स्थिति का सृजन किया है। बहुजन इसका लाभ उठाना चाहता है। हालांकि, उसके पास पूंजी नहीं है और ज्ञान शक्ति की भी कमी है; लेकिन इसके बावजूद उनके लिए भरपूर संभावना है।
लेखक ने भ्रष्टाचार मामले में भी दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है और इसके लिए ब्राह्मणवादी सोच को जिम्मेदार ठहराया है। सवाल किया गया है कि आज आर्थिक अपराधों की जब चर्चा होती है, तब तुरंत बंगारू लक्ष्मण से लेकर लालू, मुलायम, मायावती और मधु कोड़ा का नाम लोग लेते हैं। लेकिन, क्या भारत में भ्रष्टाचार केवल उसी मात्रा में है, जिस मात्रा में उपरोक्त दलित-पिछड़े नेताओं पर लगे आरोप। इसके इतर यह भी आपत्तिजनक है कि बहुजन नेताओं के बीच जो ईमानदार व्यक्तित्व हैं, उनकी समीक्षा नहीं हुई है। इसके लिए लेखक ने एक उदाहरण दिया है नेहरू और आंबेडकर का। दोनों विधुर थे और दोनों ही विद्वान राजनेता थे। नेहरू के स्त्रियों से संबंध को लेकर जितना कुछ लिखा गया है, उसी को मान लें, तो उनका व्यक्तित्व कैसा बनता है? लेकिन आंबेडकर ने ऐसा नहीं किया। जबकि उनके जीवन में भी स्त्री आई, जिनसे उन्होंने विवाह किया, उन्हें सार्वजनिक रूप से पत्नी बनाया। पेरियार रामासामी नायर ने भी ऐसा ही किया। यह साहस नेहरू, वाजपेयी या नारायण दत्त तिवारी क्यों नहीं कर पाए? क्या बहुजन के लालू, मुलायम, मायावती व कोड़ा दिखते हैं, तो कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, भोला पासवान, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और शिवराज सिंह चौहान जैसे दर्जनों नेता क्यों नहीं दिखते? यह भी सोचने और बहस का विषय है।
यह भी पढ़ें : जन चिंतन के सच्चे सरोकार
लेखक ने संसद में चर्चा को लेकर संसद के कार्टून शीर्षक से एक आलेख लिखा है, जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि संसद में एनसीईआरटी की एक किताब में शामिल प्रख्यात कार्टूनिस्ट शंकर के कार्टून पर गहरा विवाद हुआ था। आनन-फानन में उसे हटाने का फैसला ले लिया गया, क्योंकि इस कार्टून में डॉ. आंबेडकर एक घोंघे पर बैठे हैं और पंडित जवाहर लाल नेहरू उसे हांक रहे हैं। दोनों के हाथ में चाबूक है। लेखक ने सवाल किया है कि इस पूरे मामले को कैसे समझा जाए? जान लें कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है और यह कार्टून 1949 का है। कार्टूनिस्ट का व्यंग्य संविधान निर्माण की धीमी प्रगति पर है। डॉ. आंबेडकर जिस समिति में थे, उसमें और भी सदस्य थे। लेकिन, हकीयत यह थी कि संविधान निर्माण का कार्य बाबा साहब को अकेले करना पड़ा था। नेहरू के अलावा किसी और को कोई चिंता नहीं थी। इसलिए कार्टून को तत्कालीन परिस्थितियों में जाकर देखना चाहिए। लेखक का मानना है कि कार्टून में अपमानजनक जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि अपमान की बात है कार्टून को विमर्श से बाहर कर देना।
लेखक ने सर्वजन बनाम बहुजन पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और लिखा है कि हमारे देश में ब्राह्मण परंपरा इतनी मजबूत हो गई है कि श्रमण परंपरा को ही विमर्श से बाहर कर दिया, नतीजतन देश लंबे अरसे तक गुलाम रहा। (श्रमण का अर्थ परिश्रमी, मेहनती व संन्यासी।) कई अर्थों में हम आज भी गुलाम हैं और हमारा सामाजिक-सांस्कृतिक पिछड़ापन आज भी बना हुआ है। इसके रहते हम अपेक्षित आर्थिक राजनीतिक ताकत हासिल नहीं कर सकते। बहुजन श्रमण सांस्कृतिक परंपरा को वोट की राजनीति के लिए कभी-कभार सर्वजन परंपरा में तब्दील करने की कोशिश होती है। इसे पहली बार विनोबा भावे ने किया था और फिर मायावती ने और अब नरेंद्र मोदी यही राग अलाप रहे हैं। लेखक का मानना है कि दरअसल सर्वजन चिंतन प्रच्छन्न रूप से ब्राह्मण चिंतन को बनाए रखने की एक होशियार कोशिश है।
लेखक ने पिछड़ी जाति से आने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है और पत्र लिखने के पक्ष में उन्होंने लिखा है कि मैं समझता हूं हर नागरिक को अपने प्रधानमंत्री से सीधा संवाद करने का अधिकार है और यह पत्र के द्वारा हो, तब दुर्लभ एप्वाइंटमेंट का झंझट भी नहीं होता। इसलिए हमने (लेखक ने) यह माध्यम चुना। लेखक ने जेएनयू में हस्तक्षेप पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि हमें भी अपनी यूनिवर्सिटियों में इतनी आजादी देनी चाहिए कि वहां लोग मुक्त मन से विचार कर सकें। विश्वविद्यालय में जो विश्व शब्द है, उस पर ध्यान दीजिए। आप उसे संघ का शिशु मंदिर बनाना चाहते हैं? यूनिवर्सिटियां मानव जाति पर समग्रता से विचार करती है, उसे देशभक्ति की पाठशाला मत बनाइए। मान लीजिए जेएनयू में सौ- दो सौ पाकिस्तानी छात्र पढ़ते हैं, तो क्या वह पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे? विदेशों में हमारे छात्र पढ़ते हैं, तो क्या वे अपने भारत की बात नहीं कर सकते? लेखक ने प्रधानमंत्री से कहा है कि कुछ समय पहले आंबेडकर की मूर्ति पर जब आप माला चढ़ा रहे थे, तब मेरे मन में खयाल आया था कि काश उनके विचारों की माला अपने गले में डाल लेते। एक मौन क्रांति हो जाती। उठो, जागो और रुको नहीं। तुम्हारे संस्कार संघ के संस्कार नहीं हैं, आप मनुवादियों के घेरे से विद्रोह करो, उन्हें ध्वस्त करो। अंत में लेखक ने अपील की है कि आप झूठ के लाक्षागृह से निकल जाओ मोदी जी। आपका तो कम, राष्ट्र का ज्यादा भला होगा।
लेखक ने अपनी इस किताब के अंतिम आलेख के रूप में किसकी पूजा कर रहे हैं बहुजन? शामिल किया है। इसे लेकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों ने 2011 में पोस्टर तक निकाला था और कैंपस में महिषासुर दिवस का आयोजन किया। फिर अगले चार वर्षों में नौ राज्यों के तीन सौ से अधिक जगहों पर ऐसे आयोजन होने लगे, तब 2016 में संसद के दोनों सदनों में तीन दिनों तक इसको लेकर हंगामा होता रहा।
इस प्रकार ‘चिंतन के जनसरोकार’ पुस्तक दलित-बहुजन समाज के उन सभी मुद्दों की वर्तमान के सापेक्ष विवेचना करती है, जो उनके लिए तो आवश्यक है ही, साथ ही यह उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, जो दलित-बहुजन नहीं हैं; लेकिन बेहतर समाज का सपना देखते हैं। उनके मन में दलित-बहुजनों के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं है। यह किताब अध्येताओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो समाज को जानना और समझना चाहते हैं।
समीक्षित पुस्तक : चिंतन के जनसरोकार
लेखक : प्रेमकुमार मणि
प्रकाशक : द मार्जिनलाइज्ड पब्लिकेशन, नई दिल्ली
प्रकाशन वर्ष : 2016
मूल्य : 150 रुपए (अजिल्द), 100 रुपए (ई-बुक)
अमेजन से खरीदें : https://www.amazon.in/dp/8193258401
ई-बुक यहां से खरीदें : https://amzn.to/2BuhLBn
(कॉपी संपादन : प्रेम/एफपी डेस्क)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। हमारी किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति, सामाज व राजनीति की व्यापक समस्याओं के सूक्ष्म पहलुओं को गहराई से उजागर करती हैं। पुस्तक-सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in
फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें