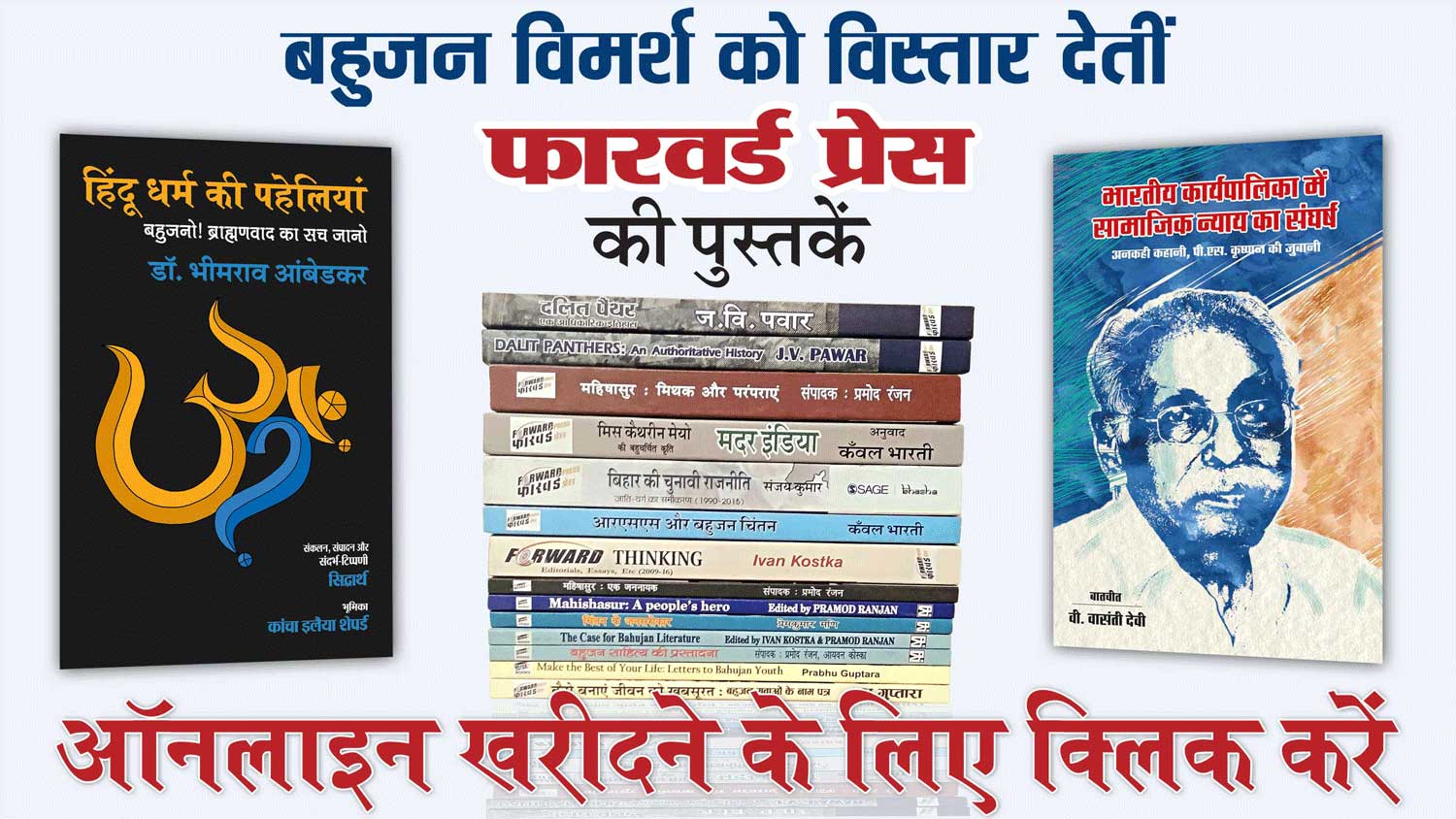बीते 26 नवंबर, 2020 को पंजाब से आरंभ हुए किसान आंदोलन को एक वर्ष पूरा होने को लगभग कुछ ही माह शेष हैं। इस आंदोलन में अनेक निहितार्थ जुड़ते जा रहे हैं। मसलन, यह किसान आंदोलन अब भारत की भाजपा सरकार तथा भाजपा की सांप्रदायिकता के विरुद्ध एक आंदोलन भी बनता जा रहा है। इस आंदोलन के सरोकार राजनैतिक तो हैं ही, सामाजिक-सरोकार भी जुड़ते जा रहे हैं। यह एक अच्छी शुरुआत भी कही जा सकती है। इसके साथ ही एक सरोकार और भी जुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, वह है– दलित-खेतिहर मजदूर तथा उसका इस आंदोलन से जुड़ाव।
सर्वविदित है कि पंजाब के खेतिहर मजदूर पंजाब के किसानों के दायें हाथ हैं और यदि यह पंजाब भारत का पेट भरता है, तो इसके पीछे सिर्फ छोटा-बड़ा किसान ही नहीं है, पंजाब का यह खेतिहर वर्ग भी है, जिनमें अधिकांश आबादी दलित जातियों की है। इस खेतिहर मजदूर की वही भूमिका है जो कि एक कारखाना श्रमिक की होती है। पंजाब में यद्यपि अब कृषि का बहुत आधुनिकीकरण हो चुका है, लेकिन इस हद तक भी नहीं कि मजदूर की आवश्यकता ही खत्म हो जाए। पंजाब में खेतिहर मजदूर पंजाब के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश के मजदूर भी आते हैं और कृषि कार्य में अपना हाथ बंटाते रहे हैं। इन बाहरी मजदूरों में भी अधिकतर दलित या पिछड़ा वर्ग के ही लोग होते हैं।
लेकिन हम यहां पंजाब के ही उस खेतिहर-मजदूर या जो स्थाई तौर पर अन्य प्रदेशों से आकर यहां रहने लगे हैं, की चर्चा करना चाहेंगे। यहां यह तथ्य स्पष्ट कर देना होगा कि यह किसान आंदोलन अब महज किसानों तक ही नहीं, दलित-वर्ग के इन खेतिहरों की दुर्दशा पर भी सोचना चाहता है। पिछले दिनों मुझे भारतीय किसान यूनियन (एकता) उग्राहां का तैयार किया हुआ संविधान तथा मांग-पत्र की प्रतियों को देखने का अवसर मिला। यह मांग-पत्र 6-7 जून, 2005 को लुधियाना में जारी किया गया था। फिर इसे 3-4 दिसंबर, 2008 में सुधार किया गया। लगभग 19 पृष्ठ के इस मांग-पत्र में पंजाब के खेतिहर श्रमिकों के अलावा सभी संस्थानों के मजदूरों की भी चर्चा की गयी है। इनके मांग-पत्र में गांव की खाली पड़ी जमीनों के बारे में घोषणा की गई है कि शामलाटों या पंचायत की खाली पड़ी भूमि को उन लोगों को दे दिया जाय, जिनके पास भूमि के नाम पर एक टुकड़ा भी नहीं है। इस प्रकार की और भी कई घोषणायें या मांगें भारतीय किसान यूनियन (एकता) उग्राहां हमें यह बताने का प्रयास करती हुई दिखाई देंगी कि किसान-आंदोलन महज किसानों अर्थात् भूस्वामियों के आंदोलन तक ही सीमित नहीं, भूमिहीन मजदूरों, दलितों के अधिकारों की चिंता भी करती है। यहां यह स्पष्ट करना उचित रहेगा कि इन घोषणाओं का स्वरूप अब तक कागजों तक ही सीमित है। धरातल पर अभी कोई शुरुआत नहीं हुई है।
पंजाब के सांस्कृतिक ढांचे की बात करें, तो यह भारत के अन्य प्रदेशों से भिन्न कतई नहीं है। भक्ति आंदोलन में पनपे कुछ विरोध के स्वर हमें कहीं-न-कहीं मानववादी विचारों की गूंज पैदा करते अवश्य दिखाई पड़ते हैं। गुरुनानक के अनुयायियों की बात करें तो उनके ही यहां अपने-अपने धर्मस्थल मौजूद हैं। प्रत्येक जाति का अपना एक अलग गुरुद्वारा है और कई-कई गुरुद्वारों में जाति को लेकर संघर्ष की खबरें अक्सर हम तक पहुंचती रहती हैं। इस तरह की खबरें भी हम तक पहुंचती रहती हैं कि अमुक गुरुद्वारा ने दलितों को गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ अर्थात गुरु ग्रंथ साहिब को देने से मना कर दिया गया। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि इस ग्रंथ साहेब, जिसमें भिन्न गुरुओं-भक्तों की वाणी को दर्ज किया गया है, के द्वारा ही दलित अपने धार्मिक आयोजन सम्पन्न करते हैं। लेकिन, यह गुरुओं के विरोध के स्वर किसी क्रांतिकारी तथा सामाजिक-आंदोलन आदि का एक परिवर्तनकारी का कारण कहीं भी नहीं बनते हमें दिखाई देते। यह विरोध के स्वर एक धार्मिक परिपाटी का हिस्सा हो चुके हैं। उन्हें धर्मस्थानों के भीतर क़ैद कर दिया गया है। यही कारण है कि पंजाब में जब भी दलितों के बहिष्कार का मसला उठता है, तो इन्हीं धर्मस्थानों के लाउडस्पीकरों, जिनके द्वारा लोगों के कानों तक गुरुवाणी पहुंचायी जाती है, के द्वारा ही बहिष्कार की घोषणायें करना कितना दुःखदायी प्रतीत होता है।

कहा जा सकता है कि संस्कृति के दांत इतने पैने होते हैं कि हमें इसकी चुभन से कोई भी धर्म या गुरु की वाणी बचा नहीं सकती। पंजाब का मालवा क्षेत्र जागीदारी मानसिकता वाला क्षेत्र है। यहां का किसान सभा सामर्थ्य रखता है कि जब चाहे खेत-मजदूर या अपने यहां काम करने वाले नौकरनुमा व्यक्ति जो कि ज्यादातर दलित वर्ग का होता है, को शोषण की चक्की में पीस देता है। वहां की भाषा में उसे ‘कम्मी’ कहा जाता है। परिवार-दर-परिवार यह शोषण की एक ऐसी लंबी कड़ी होती है, जो कभी खत्म नहीं होती।
इस समय यदि हम पंजाब के खेत मजदूर की स्थिति का आकलन करें, तो पंजाब के लगभग 84 प्रतिशत खेत मजदूर कर्जदार हैं। खेत मजदूरों के एक संगठन ने कहा है कि पंजाब के प्रत्येक खेत-मजदूर पर 91,437 रुपये का कर्ज है। पंजाब में किसानों की आत्महत्याओं में कम-से-कम 45 प्रतिशत खेत मजदूर शामिल हैं। परंतु पंजाब की कर्ज माफी मुहिम में कोई खेत मजदूर कभी शामिल नहीं किया गया। इस दोहरे अभिशाप की ओर देश की कोई भी सत्ता गौर करती दिखाई नहीं पड़ती। खेत-मजदूरों की इस स्थिति को यदि मैं साहित्यिक भाषा में प्रकट करना चाहूं तो इस प्रकार कहना चाहूंगा कि पंजाब का खेत मजदूर किसानों के मुंह से गिरे दानों को लपक कर अपना पेट भरता है, तो उसकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति का पता लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। यह त्रासदी है भूमिहीन होने की।
इसी प्रकार पंजाब का साहित्य अधिकतर छोटे-बड़े किसानों की ज़िंदगी से जुड़ी तमाम कठिनाइयों पर बात करता हुआ अवश्य मिल जाएगा। लेकिन पंजाब के खेत-मजदूर पर कायल इन साहित्यकारों की कलम एकदम खामोश है। इस प्रकार की परिस्थितियों की यदि हम भयावहता को महसूस करना चाहें, तो कोरोना के कारण लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न हुई परिस्थितियों में पंजाब का खेत मजदूर और भी कंगाली के बीहड़ की ओर खिसका है। 1990-91 में राजस्थान तथा हरियाणा के मजदूर कपास चुनने पंजाब आया करते थे। परंतु आज स्थिति इसके विपरीत हो गई है। पंजाब के ये ही किसान-मजदूर यही काम करने के लिए हरियाणा कूच करने को बाध्य हैं। यह पंजाब की कृषि में शायद पहली बार हो रहा है। कितना दुखद होता है, पेट की आग बुझाने की खातिर घर से बेघर होने की प्रक्रिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दावे किये जा रहे थे कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। इस संदर्भ में एक अर्थशास्त्री रविंद्र शर्मा के द्वारा किये गये आकलन को माने, तो उनके मुताबिक 17 राज्यों अर्थात् आधे देश में किसान की वार्षिक आय करीब 20 हजार रुपये है। इसमें कृषि मजदूरों को भी सरकार ने शामिल किया है। इस गणित के मुताबिक एक किसान की मासिक आय 1700 रुपये के बराबर होती है। इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कृषि मजदूर की आय कहां जाकर खड़ी होती है?
आइये, पंजाब के खेत मजदूर के जीवन की और भयावहता पर चर्चा करें। पंजाब के खेत मजदूर सभा ने पिछले दिनों एक सर्वेक्षण करवाया। यह सर्वेक्षण पंजाब के दोआबा तथा मालवा क्षेत्र के 6 जिलों के 13 गांवों में 1618 परिवारों में करवाया गया। इसके परिणाम यह रहे कि 1364 परिवारों पर 12 करोड़, 47 लाख, 20 हजार 979 रुपयों का कर्ज है। कर्ज पीड़ित मजदूर पर प्रति परिवार 91,437 रुपये बनता है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस कर्ज का 84 प्रतिशत जो है, वह निजी स्रोतों से आता है। ये स्रोत ब्याज के रूप में मोटी रकम वसूलते हैं। सिर्फ लगभग 16 प्रतिशत ही बैंकों आदि से प्राप्त होता है।
आत्महत्याओं की बात करें, तो खेत मजदूर कभी भी आग्रहताओं के मामले में विचाराधीन नहीं रहा। इससे भी बड़ी त्रासदी यह रही कि खेत मजदूर स्त्री की आत्महत्या को किसान-मजदूर की आत्महत्या में गिना ही नहीं गया जबकि एक बहुत बड़ी संख्या स्त्री-खेत मजदूरों की रही है, जिनकी ज्यादा संख्या का सबसे बड़ा कारण यह है कि गांवों में यह दलित महिला मजदूर पुरुष-मजदूर से कम पैसे पर उपलब्ध हो जाती हैं। इसके साथ हम यह भी देखते हैं कि इन महिला मजदूरों के शारीरिक-शोषण का कहीं भी कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार का शोषण दलित मजदूर स्त्री की मानो एक नियति बन चुकी है और इसकी चर्चा कहीं भी नहीं।
किसानों की आत्महत्याओं की बात करें, तो पंजाब खेतीबाड़ी विश्वविद्यालय अर्थ तथा सामाजिक-विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉ. सुखपाल सिंह के द्वारा एक शोध प्रस्तुत किया गया था, जिसके मुताबिक 15 वर्षों (2000-2015) में पंजाब में करीब 16 हजार आत्महत्यायें हुई हैं। इन आत्महत्याओं में 4000 किसान तथा 7000 के करीब खेत मजदूर थे। इनमें लगभग 60 प्रतिशत इसलिए आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनके सिर पर कर्ज का बोझ होता है। 40 प्रतिशत के आत्महत्या का कारण भी घोर आर्थिक तंगी सामने आती है। यह बता देना प्रासंगिक होगा कि आर्थिक तंगी कर्ज से भी ज्यादा भयानक इसलिए है कि खेत मजदूर को ऋण मिलता ही नहीं। एक जमीन का स्वामी किसान अपनी आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए या तो जमीन का एक टुकड़ा बेच देता है या अपनी जमीन को बैंक के पास गिरवी का कागज बनवा कर अपना काम चला लेता है। अपने बच्चों का भविष्य संवारने बैंक के ऋण के बल पर विदेश रवाना कर देता है। खेतिहर मजदूरों को ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं।
बीते 21 फरवरी, 2020 में पंजाब के बरनाला जिले में किसान और खेतिहर मजदूरों को इन कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखाने की एक रैली होती है। इस रैली का आयोजन भारतीय किसान यूनियन (एकता- उग्राहां) और पंजाब खेत मजदूर यूनियन (पीकेएमयू) द्वारा किया जाता है। यहां यह स्पष्ट कर दें कि यह दोनों संस्थायें भूमिहीन किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली तथा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने वाली सबसे बड़ी यूनियनें कही जाती हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जोगिंद्र सिंह उग्राहां ने वहां उपस्थित जन सैलाब को संबोधित किया और खेत-मजदूरों को 27-28 फरवरी को शक्ति प्रदर्शन के लिए दिल्ली के टिकरी बार्डर पर पहुंचने की अपील की थी। लेकिन 28 फरवरी को पीकेएमयू के कैडर वहां नहीं पहुंचे और खेतिहर मजदूरों का वहां कोई जमावड़ा नहीं होता है। उग्राहां कहते हैं कि जब उन्होंने पीकेएमयू के महासचिव लक्ष्मण सिंह को फोन किया, तो उन्होंने कहा कि बरनाला रैली के बाद उन्होंने उग्राहां को बता दिया था कि मजदूर दिल्ली पहुंचने का खर्चा नहीं उठा सकते। ऐसा भी नहीं है कि पंजाब की मजदूर यूनियनें किसान-आंदोलन के पक्ष में नहीं, लेकिन इस वास्तविकता को नकारना बहुत कठिन है कि पंजाब किसान आंदोलन में पंजाब के किसान मजदूरों के हाथ ज्यादा कुछ लगने वाला नहीं। और पंजाब में लगभग दलित 32 प्रतिशत हैं, लेकिन मात्र प्रदेश की 3 प्रतिशत भूमि ही इनके पास है। जाट सिक्ख, जिनकी आबादी लगभग 25 प्रतिशत है, बड़े पैमाने पर खेतिहर मानी जाती है। इस 25 प्रतिशत आबादी का पूरा दबदबा कृषि उद्योग पर देखा जाता है तथा यही दबदबा दलित-समाज पर भी नजर आता है।
इन्हीं प्रश्नों पर भूमि मजदूरों में विरोध के स्वर अब उठते दिखाई देने लगे हैं। उनका मानना है कि इस आंदोलन में किसानों की समस्याओं पर तो खूब बात की जा रही है लेकिन भूमिहीन मजदूरों की परेशानियों को छुआ नहीं जा रहा। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि किसान यूनियनों में किसी मजदूर, दलित पदाधिकारी की कहीं शिरकत देखने को नहीं मिलती। किसान आंदोलन में किसी तरह का फैसला लेने, आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया में कोई मजदूर-संगठन देखा नहीं जाता। इसी संदर्भ में एक खोजी पत्रकार परमजीत सिंह की हम यहां चर्चा कर सकते हैं। यह पत्रकार दलितों की उन सभाओं में जाते हैं, जहां पर किसान-आंदोलन की समस्याओं पर चर्चा होती है। कुछ दिन पूर्व पीकेएमयू के राज्य समिति के सदस्य हरभजन सिंह ने लगभग पचास मजदूरों की एक सभा को संबोधित किया था। इस सभा के बारे में चर्चा करना इसलिए भी आवश्यक है, ताकि यह बताया जा सके कि गांव के अनुसूचित जाति के समुदाय के श्रमिक अपने दलित-मंदिरों या अपने ही निर्मित गुरुद्वारों में ही अपनी सभायें करने को विवश हैं, क्योंकि उच्च जाति के किसान अक्सर उच्च जाति के बने धर्मस्थलों पर ही अपनी सभाएं आयोजित करते हैं, यहां पर दलित-वर्ग के श्रमिकों की समस्यायों पर कोई बात नहीं होती। घोर कंगाली से जूझ रहे इन दलितों की समस्याओं से इन किसान नेताओं को ज्यादा वास्ता नहीं होता। यह जानते हुए भी कि इन किसान-मजदूरों के बिना यह किसान-आंदोलन एक अधूरेपन का शिकार हो सकता है, वे परवाह नहीं करते।
दरअसल, पंजाब के दलित खेतिहर मजदूरों के प्रति बड़े किसानों का रवैया एक प्रकार से सामंती स्वरुप का ही देखा जाता है और वे जानबूझकर इस ओर ध्यान कम देते हैं, ताकि उनके सामंतवाद पर कोई आंच न आए। यह एक मनोवैज्ञानिक पहलू कहा जा सकता है। यहां सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या किसान-आंदोलन के नेतृत्वकर्ता इस ओर ध्यान देंगे या भारत के कम्युनिस्टों की तरह इन दलित-खेतिहर मजदूरों के बल पर अपना नेतृत्व कायम रखते रहेंगे?
(संपादन : इमामुद्दीन/नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in
फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें
मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया