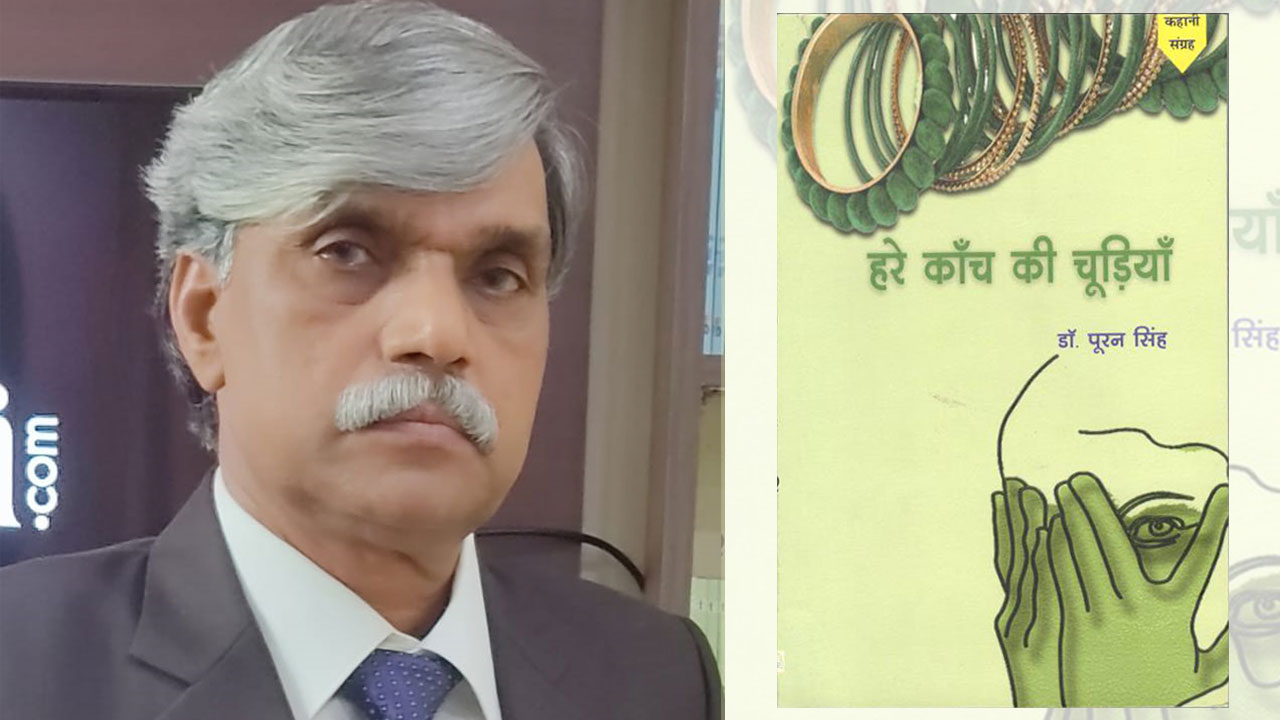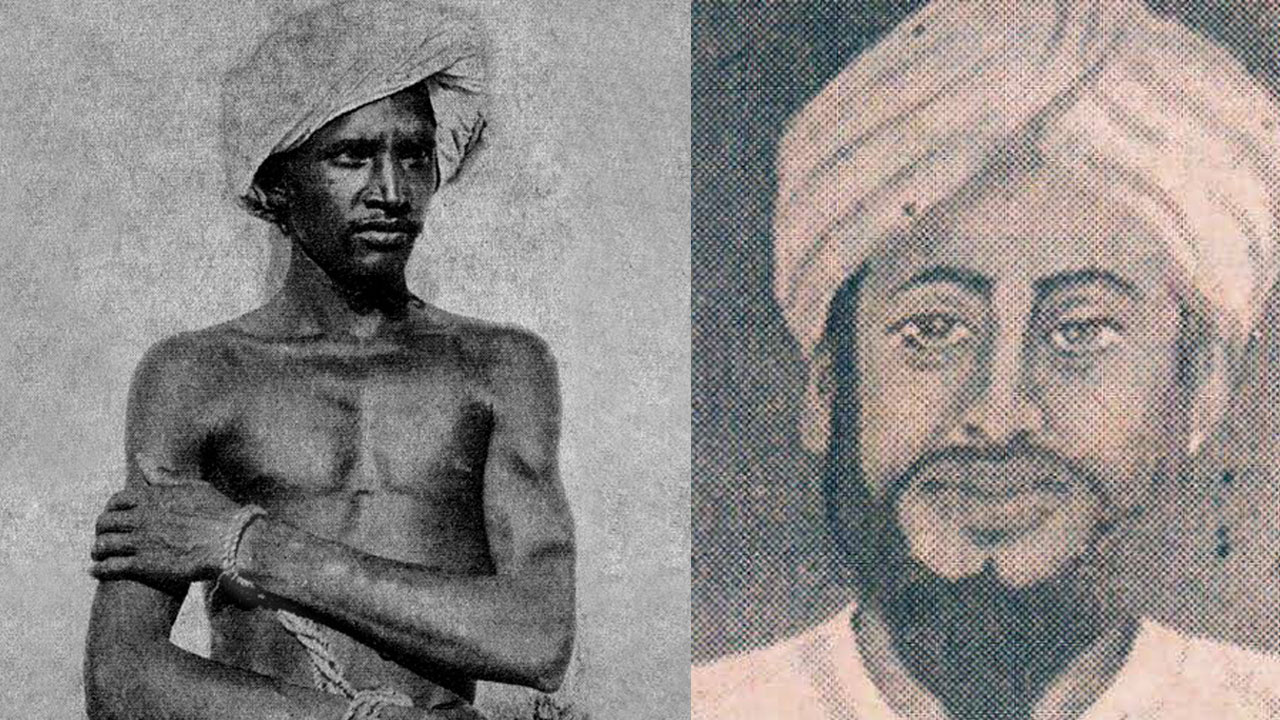उत्तर-भारत में दलित-बहुजन आंदोलन और राजनीति पर विचार शृंखला (पहली किस्त)
पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव संपन्न हो गए। गत 10 मार्च को चुनाव परिणाम आया। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में भाजपा को तथा पंजाब में आम आदमी पार्टी को जीत मिली। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम आने के बाद पता चला कि जिस पार्टी को ‘किंग मेकर’ कहा जा रहा था अर्थात बहुजन समाज पार्टी (बसपा), वह मात्र एक सीट जीत पाई और उसके मत प्रतिशत में लगभग 10 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। बसपा का यह प्रदर्शन संभावित ही था। हालांकि हाशिए पर बढ़ने की उसकी तैयारी हैरान करने वाली है। कोर समर्थकों को छोड़कर किसी को इस पार्टी से उम्मीद नहीं थी। परंतु हम सब जानते हैं कि दलित-बहुजन समाज के लिए बसपा का महत्व राजनीतिक पार्टी से कहीं ज्यादा है।
कांशीराम के समय तमाम लोगों के त्याग और समर्पण से यह पार्टी खड़ी हो पाई थी। पार्टी की राजनीतिक हार ने निश्चित ही दलित-बहुजन सामाजिक आंदोलन से हासिल उपलब्धि को मटियामेट कर दिया है। यह माना जा सकता है कि यह वक्त दलित-बहुजन समाज के सपनों के अंत का नहीं, परंतु ठहरकर विचार करने और निर्णय लेने का समय जरूर है।
दलित-बहुजन राजनीति सांस्कृतिक आंदोलनों की उपलब्धि है, जिसमें फुले, पेरियार, नारायण गुरू, डॉ. आंबेडकर, डी.के.खापर्डे और कांशीराम की चेतना व संघर्ष शामिल हैं। दलित-बहुजन राजनीति के उदय के कई प्रस्थान बिंदु हैं। कई उतार-चढ़ाव के बाद कांशीराम भारत के इतिहास में जब एक दलित बेटी को भारत के सबसे बड़े सुबे का मुख्यमंत्री बना पाने में सफल हुए, तब इस उपलब्धि से उनके द्वारा दोहराए जाने वाले नारे – ‘दलित शासन करेगा’ पर लोगों का यकीन पुख्ता होने लगा था। मुख्यमंत्री मायावती चुनावी लोकतंत्र की ऐतिहासिक परिणति थीं। हालांकि सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें जितने शानदार काम करने थे, उसमें से शायद ही कोई काम हो पाया। उनका शासन लोककल्याण का जैसा नजीर बनना चाहिए था, वैसा नहीं बन पाया।
मायावती का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना भारतीय लोकतंत्र की अलहदा उपलब्धि थी, मगर किसे पता था कि जिनके नाम पर यह उपलब्धि दर्ज़ है, वही हजारों साल से वंचना का दंश झेल रहे समाज की उम्मीद और उसके संघर्ष को इस तरह तहस-नहस कर देंगी। कांशीराम ने भारत की 600 वंचित-दलित और सदियों से गुलामी में जी रही जातियों को एक साथ लाकर जिस ‘बहुजन समाज’ की नींव रखकर उसे राजनीतिक चेतना से लैस किया, मायावती ने प्याज के छिलके की तरह उसको (‘बहुजन समाज’ को) फिर से तितर-बितर कर दिया। बहुजन शब्द दलित राजनीति के लिए बीज मंत्र की तरह था, जिसकी उत्पत्ति का दर्शन बामसेफ से प्राप्त हुआ। आज बामसेफ कई धड़ों में टूटकर बिखर गया है और बसपा हाशिए पर जा चुकी है।
उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद बसपा की हालिया तबाही पर कई मंचों पर विचार हो रहा होगा। आइए सोचें कि बसपा के इस हश्र का बीज कब पड़ा?
जब सोलह साल बाद उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी
कांग्रेस के मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में गैर-कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई, मगर वह बहुत दूर तलक नहीं जा पाई। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद वह अंतिम मुख्यमंत्री थे, जिनके बाद 2007 के पहले तक कोई भी मुख्यमंत्री पांच साल का निर्धारित कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया था। ऐसा इसलिए भी था, क्योंकि उस समय राजनीतिक पार्टियॉ गठबंधन की संस्कृति सीख नहीं पाईं थीं, इसलिए चुनाव दर चुनाव होते रहे और साल-दो साल बाद सरकारें गिरती रहतीं। यहां तक कि प्रदेश में दस बार राष्ट्रपति शासन लग चुका था। कुल मिलाकर यह प्रदेश 1700 दिन तक राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा। ऐसे में सन् 2007 में बसपा 206 सीटों पर विजय हासिल करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुई। और इस तरह सोलह साल बाद मायावती के रूप इस प्रदेश को एक स्थाई मुख्यमंत्री हासिल हुआ। इसके पहले अल्पकाल के लिए मायावती तीन बार मुख्यमंत्री बन चुकी थीं। बहुजन समाज की यह जीत कांशीराम की उनुपस्थिति में (सन 2006 में दिवंगत) हासिल हुई थी। जाहिर है जीत का श्रेय मायावती को हासिल हुआ। इस जीत ने उन्हें भारतीय राजनीति का सबसे चमकदार चेहरा बना दिया।

इस जीत के बाद पार्टी को अपने जनाधार को बांधना-साधना और बढ़ाना चाहिए था – दलित-पिछड़ी-अल्पसंख्यक-वंचित तबकों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ना चाहिए था – मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस जीत के साथ सिद्धांत और कैडर पर आधारित पार्टी के सिद्धांतहीन और कैडरहीन होना शुरू हुई। पार्टी ने मान लिया कि वह ब्राह्मणों के मतों से वह सत्ता में आई है (इस बात को खूब प्रचारित किया गया)। ऐसा स्वीकारते ही पार्टी का राजनीतिक दर्शन सिर के बल खड़ा हो गया। इस विजय से पार्टी का राजनीतिक नारा बदल गया – ‘हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश है।’ बसपा के इस विजयोत्सव में कांशीराम के दर्शन को अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। तब से लेकर अब तक यह पार्टी कांशीराम द्वारा उपलब्ध कराए गए राजनीतिक दर्शन के विपरित दिशा में सरपट भागती रही है। एक साधारण आदमी को असाधारण मानने का खामियाजा पार्टी को भुगतना ही था, सो वह भुगत रही है।
इस दरम्यान कई बातें हुईं। मगर सबसे प्रमुख बात यह रही है कि क्या सच में ब्राह्मणों का इतना व्यापक जनाधार पार्टी को मिला, जिसकी कृतज्ञता से वह बर्बाद होकर भी मुक्त नहीं हो पा रही है? इस सवाल का एक नुक्ता इस सवाल से भी जुड़ता है कि आखिर वे कौन से हालात थे, जिसने ब्राह्मण जाति के मतदाताओं को बसपा की ओर ढकेला?
जून की तपिश और मज़ार-ए-कायद
सन् 2005 और 2006 भाजपा के लिए अच्छे साल नहीं रहे। जून 2005 में एक यात्रा पर आडवाणी पाकिस्तान गए और मई 2006 में प्रमोद महाजन की मुंबई में हत्या हो गई। ये दोनों घटनाएं भाजपा को परेशान करने वाली साबित हुईं, जिसका असर जनाधार और उसके चुनावी प्रदर्शन पर भी पड़ा। जहां कराची में आडवाणी के बयान ने भाजपा को बैकफुट पर ला दिया, वहीं महाजन के असमय चले जाने से पार्टी सांगठनिक रूप से ठिठक सी गई। उसे आगे बढ़ने के लिए जिस हौसले की जरूरत थी, उसे हासिल होने में वक्त लगा। इन्हीं विपरित परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने का ऐलान हुआ। बस जेहन पर थोड़ा जोर डालने की जरूरत है और अट्ठारह-उन्नीस साल पुराने धूल-फांकते अखबारों के पन्नों को पलटने की जरूरत है, सत्य सामने खड़ा मिलेगा।
4 जून, 2005 का दिन न भाजपा भूल सकती है और ना ही आडवाणी। उसी दिन आडवाणी ने कराची में कायदे आजम मुहम्मद अली जिन्ना की कब्र पर चादर चढ़ाया और श्रद्धांजलि देते हुए जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष कहा। यह बात तुरंत दुनिया भर की मीडिया में छा गई, जिसका खामियाजा स्वयं आडवाणी के साथ-साथ भाजपा को भी भुगतना पड़ा। एक वक्तव्य ने सूखे पुआल के लिए माचिस का काम किया। भाजपा के शिखर पुरुष के इस वक्तव्य से संघ बहुत नाराज हुआ। आनन-फानन में आडवाणी को पार्टी की अध्यक्षता के पदभार से मुक्त करके उनकी जगह राजनाथ सिंह पार्टी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। मगर इतना अवश्य हुआ कि इस घटना के बाद भाजपा की ओर से अपने आप को पुनर्परिभाषित और पुनर्रेखांकित करने का प्रयास किया गया, मगर इसी बीच उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव घोषित हो चुका था। भाजपा को संभलने का मौका नहीं मिला। और आडवाणी के वक्तव्य से ब्राह्मणों का एक तबका संशय में था। इसीलिए उसका भाजपा से क्षणिक मोहभंग हुआ। यह तबका भाजपा के विकल्प की तलाश में लग गया। उत्तर प्रदेश में काग्रेस की हालत खराब थी। सपा से जुड़ने का सवाल ही नहीं था। अंतिम विकल्प के रूप बसपा सामने आयी। बसपा को इस अवसर का लाभ मिला। वह चुनाव में जीती। उसे तीस प्रतिशत से थोड़ा अधिक मत प्राप्त हुए। इस जीत को मायावती के द्वारा किए गए सोशल इंजीनियरिंग के रूप में खूब उछाला गया। स्वयं मायावती भी स्वयं को सोशल इंजीनियरिंग का अगुआ मान बैठीं। इसी दौरान पूर्णकालिक मुख्यमंत्री होने के दौरान बसपा अध्यक्ष की ओर से कुछ मजबूरियों का आविष्कार किया गया, जिसने उनका अपनों के बीच आना-जाना लगभग बंद सा हो गया। क्षणिक सफलता ने तानाशाही को विकसित होने का भी पूर्ण अवसर दिया। लिहाजा पार्टी को अपना सर्वस्व देने वाले दूर होते चले गए।

इस बार के विधानसभा चुनाव में पार्टी की मुखिया की निष्क्रियता अकारण नहीं थी। साथ ही ब्राह्मणों के मत पर यकीन का आलम यह रहा कि इस बार भी बसपा द्वारा अपनों से पर्याप्त दूरी बनाते हुए कुल 80 ब्राह्मण महासम्मेलनों का आयोजन किया गया। क्षणिक मतदान को आधार बनाकार अपनों से दूरी बनाने का ऐसा उदाहरण मिलना दुर्लभ है।
बसपा को लोकतंत्र का आइना होना चाहिए था। उसके नेतृत्व में लोकतंत्र को साकार देना चाहिए था, मगर उसने लोकतंत्र के विलोम को स्वीकार करते हुए कांशीराम के साथ-साथ लाखों दलित-वंचित-पिछड़े तबके के सपनों चकनाचूर करने का कार्य किया। फिर भी यह अंत नहीं है। परिस्थितियां अनुकूल हैं, यहीं से दलित-वंचित और हाशिए के समाज को एक नई राजनीति का आगाज होगा।
क्रमश: जारी
(संपादन : नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in
फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें
मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया