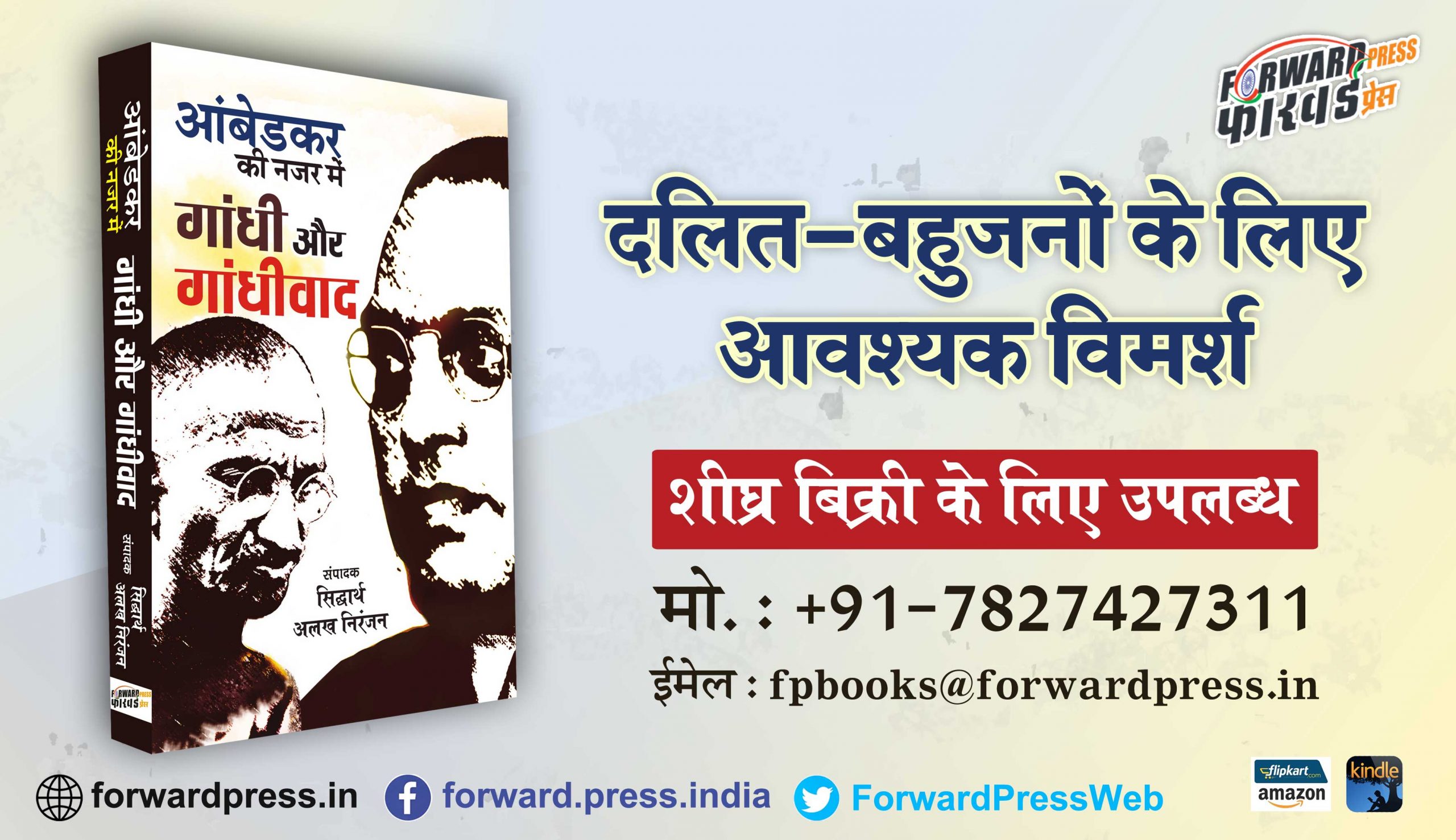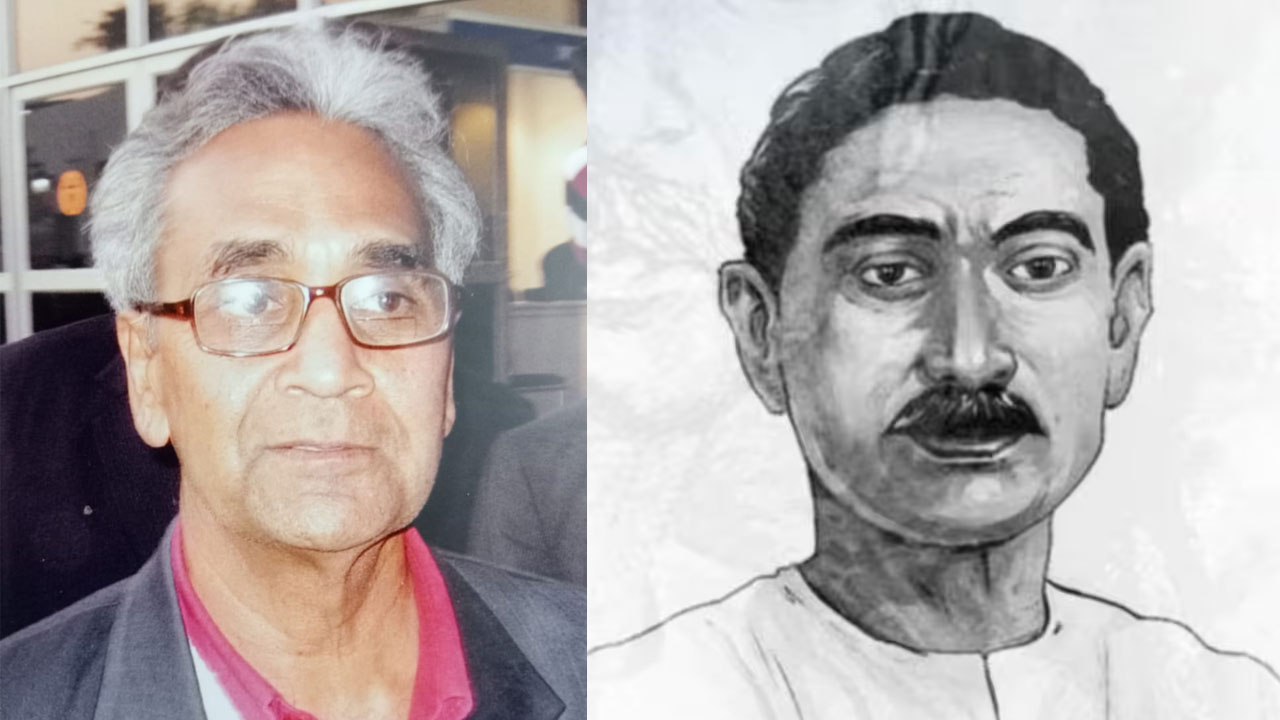दलित कहानी में विचारधारा का विशेष महत्व है। इसी के आधार पर कोई कहानी दलित कहानी बनती है। यह विचारधारा क्या है? इस पर बात हो सकती है और होनी भी चाहिए। कुछ गैर-दलित लेखकों ने बात की भी है और उन्होंने उसका मूल्यांकन गाली-गलौंच के साहित्य के रूप में किया है। मतलब, दलित साहित्य के मूल में अगर वर्ण व्यवस्था के विरोध की वैचारिकी है, तो वह उन्हें गाली-गलौंच की वैचारिकी लगती है। लेकिन वे इस बात को समझना नहीं चाहते कि वर्ण व्यवस्था के विरोध की वैचारिकी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को स्थापित करने की वैचारिकी है। इससे उनकी मानसिकता को समझा जा सकता है कि किस कदर उनके प्राण वर्ण व्यवस्था में बसते हैं।
श्यौराजसिंह बेचैन की कहानियां इसी वर्ण व्यवस्था और जातिभेद की सवर्ण मानसिकता को उधेड़ती हैं। हालांकि वह ऐसे दलित कहानीकार हैं, जिनके सवर्ण पात्र प्रगतिशील होने का दंभ भी दिखाते हैं, और रूढ़ियों को तोड़ते भी हैं। बेचैन के अब तक तीन कहानी-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, पहला ‘भरोसे की बहन’ (2010), दूसरा ‘मेरी प्रिय कहानियां’ (2019) और तीसरा ‘हाथ तो उग ही आते हैं’ (2020)। उनकी कहानियों का रचना-काल 1990 और 2020 के बीच का है। इस प्रकार दलित कहानी में उनका समय ओमप्रकाश वाल्मीकि के बाद का है, जब सरकारी आरक्षण से नौकरियों में दलितों की दूसरी-तीसरी पीढ़ी तैयार हो रही थी और सवर्णों में उसके विरुद्ध रोष पैदा हो रहा था। भाजपा और संघ-परिवार के नेता आरक्षण-विरोधी आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जिसने 1990 के मंडल-विरोधी आंदोलन को देशभर में दलित-पिछड़ों के खिलाफ हिंसक हवा दी थी। दूसरी ओर दलितों-ओबीसी को आरक्षण का लाभ न मिलने देने के लिए सवर्ण शासक-वर्ग नित्य नई कुटिल चालें चल रहा था। बहुजनों का शिक्षित वर्ग इसे असहाय दृष्टि से देख रहा था, क्योंकि वह शासक (सवर्ण) वर्ग से लड़ने में सक्षम नहीं था। किन्तु प्रतिरोध की अभिव्यक्ति उसमें साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही थी। इस अभिव्यक्ति की एक सशक्त कहानी ओमप्रकाश वाल्मीकि की ‘घुसपेठिये’ है, जिसमें सवर्ण छात्रों द्वारा एक बस के अन्दर मेडिकल के दलित छात्र सुभाष सोनकर की पिटायी की जाती है, जिससे तंग आकर सुभाष सोनकर आत्महत्या कर लेता है। जैसे वर्ष 2016 में हैदराबाद विश्वविद्यालय में दलित वर्ग के छात्र रोहित वेमुला ने सवर्ण प्रशासन के वर्णवादी व्यवहार से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। इस दौर की दलित कहानियों में आरक्षण के विरुद्ध सवर्णों की हिंसा और कुटिल चालों को बेनकाब करने वाली अनेक कहानियां लिखी गईं।
श्यौराज सिंह ‘बेचैन’ की अधिकांश कहानियां इसी पृष्ठभूमि की हैं। इनमें ‘होनहार बच्चे’ और ‘क्रीमी लेयर’ दो कहानियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ‘होनहार बच्चे’ कहानी दलित साहित्य की पत्रिका ‘अपेक्षा’ के जून 2007 के अंक में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी के मूल में इन्दिरा गांधी द्वारा आपातकाल के दौरान सरकारी विभागों में आरक्षण पूरा करने का लिया गया निर्णय है। हालांकि इसके पीछे दलितों को कांग्रेस के पक्ष में लामबंद करने की सोच थी, पर यही वह काल था, जिसमें दलितों को सबसे ज्यादा नौकरियां मिली थीं, और उनका उत्थान हुआ था। इस निर्णय के तहत सभी विभागों में फटाफट विज्ञापन निकालकर आरक्षित पदों को भरे जाने के विज्ञापन प्रकाशित हुए। सरकार के इस निर्णय से सवर्णों के दिमाग फटे जा रहे थे। वे इससे खुश नहीं थे, पर असहाय थे, क्योंकि आपातकाल में सरकार के विरोध का मतलब सीधा राजद्रोह था। तब सवर्णों ने इसका एक समाधान निकाला। बेचैन ने इसी समाधान का पर्दाफाश इस कहानी में किया है। इसमें सदानंद तिवारी दलितों के लिए भर्ती का विज्ञापन देखकर परेशान हो जाता है। वह समझता है कि इस विशेष अभियान में उसके बेटे गोविन्द को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। तब वह एक चतुर वकील सक्सेना के साथ इस समस्या के समाधान का मार्ग तलाशता है। सक्सेना का शातिर दिमाग तरीका बताता है। उसके अनुसार सदानन्द तिवारी अपने बेटे गोविन्द को कागज पर धीरा चमार का दत्तक पुत्र बनवा देता है। इससे गोविन्द का एससी प्रमाण-पत्र बन जाता है, जिसके बाद वह आवेदन कर देता है। साक्षात्कार समिति का चेयरमैन विभूति पांडे है। जब दलित सदस्य गोविन्द के चयन का विरोध करता है, तो विभूति पांडे उसके विरोध को खारिज कर देता है और गोविन्द की नियुक्ति हो जाती है। नियुक्ति हो जाने के बाद धीरा चमार न उसका बाप रहता है और न गोविन्द उसका बेटा। इसी तरह की शातिर राय सक्सेना सदानन्द तिवारी की भतीजी पुनीता की नौकरी के लिए भी देता है कि वह किसी मरियल और निःसंतान दलित को ढूंढ़कर उससे कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट बनवा ले। इस तरीके से पुनीता को भी दलित कोटे में नौकरी मिल जाती है। एक दिन राष्ट्रीय अखबार में इस फर्जीवाड़े की रिपोर्ट छप जाती है, तो पुनीता परेशान हो जाती है। पर उसके पिता उसे समझाते हैं कि कोई अपराध-बोध मत पालो, ऐश करो। पकड़े भी गए, तो जांच होने और केस फाइनल होने में ही 25-30 साल लग जायेंगे। तब तक तो एससी-एसटी के वंचित हकदारों के तो घर बरबाद होते रहेंगे। एक ब्राह्मण के लिए इससे बड़ा संतोष और क्या होगा?

दूसरी कहानी ‘क्रीमी लेयर’ है, जिसमें ओबीसी और दलितों के विकास को रोकने वाली सवर्ण मानसिकता को दिखाया गया है। इस कहानी में सुधांशु नाम का एक ब्राह्मण विचारक एक दिन सपने में देखता है कि संसद ने यह कानून पास कर दिया है कि अगले पांच साल तक किसी भी क्रीमी लेयर को सरकारी-गैरसरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, वह चाहे जिस भी धर्म और जाति का हो। लेकिन सुधांशु को दलितों से जातीय दुश्मनी थी। उसे यह सपना अच्छा नहीं लगता है। उसे जयरत्न पाण्डे वकील पर भी गुस्सा आता है, जिसने कोर्ट में यह दलील दी थी कि यदि एससी/एसटी पर क्रीमी लेयर लागू होगा, तो जनरल पर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर नौकरी से वंचित करने का आधार क्रीमी लेयर होगा, तो वह एससी/एसटी पर ही क्यों, जहॉं भी क्रीमी लेयर हो, उसे नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। निश्चित रूप से इस कहानी में क्रीमी लेयर पर दलितों व ओबीसी का तार्किक दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ है। सुधांशु कसम खाता है कि वह एससी/एसटी को नौकरी में नहीं आने देगा। इसके लिए वह कानून पढ़ता है, वर्णवादी संगठनों से सम्पर्क करता है। समान विचार के संपादक की तलाश करता है, अखबार के स्वजातीय लोगों से मिलकर दलित-बहुजनों के खिलाफ लेखन करवाता है। यहां तक कि वह दलितों के संवैधानिक अधिकारों को अमल में लाने से रोकने के कार्य को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के उपक्रम में लग जाता हैा। लेकिन सुधांशु की पत्नी प्रणीता इसके विपरीत विचारों की है। उसे सुधांशु की बातें समय के खिलाफ लगती हैं। सुधांशु प्रणीता को अपनी विचारधारा से सहमत नहीं करा पाता है। दोनों में इस विषय को लेकर झगड़े होते हैं। दोनों एक-दूसरे पर तीखे वार करते हैं। लेकिन जब सुधांशु के विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो प्रणीता सुधांशु के दलित-विरोधी होने के कारण को जानने का प्रयास करती है। अचानक घर का कबाड़ बेचते समय उसके हाथ एक छोटी सी डायरी लग जाती है। उसमें एक जगह सुधांशु की हैंडराइटिंग में लिखा होता है– “बड़ी दीदी और छोटी बुआ, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैं उन दोनों की पीढ़ियॉं तबाह कर दूंगा।” तब प्रणीता अपनी ननद आकांक्षा से बड़ी दीदी और छोटी बुआ के बारे में पूछती है कि उनके साथ क्या हुआ था? आकांक्षा बताती है कि उनकी हत्याएं हुई थीं और उसके लिए भी बड़े भैया ही जिम्मेदार हैं। वह घर में यही प्रचार करते रहते थे कि अब नौकरियां एससी/एसटी के लोगों को ही मिलेंगी, और ऊंची जातियों के बेरोजगार लोग चप्पलें चटकाते घूमेंगे। तब बुआ और दीदी को भी लगा कि वह सही कह रहे हैं। इसलिए उन दोनों ने एससी/एसटी लड़कों से शादी करके प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा चलाए गए एससी/एसटी विशेष भर्ती अभियान में नौकरी हासिल कर ली। लेकिन जब पिताजी को पता चला, तो उन्होंने कहा कि जान चली जाए, पर हमारी बहन-बेटी एससी/एसटी के घर में नहीं जायेंगी। उन्होंने ठेके के हत्यारों को सुपारी देकर दीदी-बुआ को मरवा दिया और उन दोनों दलित लड़कों पर केस चलवा दिया। इस तरह प्रणीता को सुधांशु के दलित-विरोधी होने की समस्या का पता चल जाता है और कहानी खत्म हो जाती है।
विचार की दृष्टि से यह कहानी ऊंची जातियों में आए सामाजिक परिवर्तन को रेखांकित करती है। इसमें सुधांशु और प्रणीता दोनों ऊंची जाति से हैं, पर एक सामाजिक न्याय का विरोधी है और दूसरा उसका पक्षधर। यह दलितों के प्रश्न पर सवर्ण परिवार में चल रहे द्वंद्व की कहानी है। कहानीकार संभवतः बताना चाहता है कि सवर्ण परिवारों में जातीय उच्चता उनके नाक का बाल बनी हुई है, जिसे बचाने के लिए वे किसी भी हद से गुजर सकते हैं। लेकिन प्रणीता के रूप में सवर्ण परिवारों में एक परिवर्तन की आहट भी इस कहानी में सुनाई देती है।
‘बस्स इत्ती सी बात’ में भी सवर्ण मानसिकता इस हद तक अमानवीय हो जाती है कि ठाकुर कुंवर सिंह अपनी पूर्व पत्नी कीर्ति की हत्या सिर्फ इस बिना पर कर देता है कि उसने एक दलित लड़के से विवाह कर लिया था, जिससे उसकी राजपूती शान में बट्टा लग जाता है। उसे जेल होती है, पर उसे हत्या करने का जरा भी अफसोस नहीं है। वह कहता है कि जिस औरत का उसके उच्च कुल से सम्बन्ध रहा है, वह खानदान की मान-मर्यादा की परवाह किए बगैर कोई कदम कैसे उठा सकती है? जिन जातियों के लोग हमारे आगे सिर उठाकर खड़े नहीं हो सकते, जो सपने में भी हमारी बराबरी नहीं कर सकते, उस अछूत जाति के ऐरे-गैरे व्यक्ति से वह पुनर्विवाह कैसे कर सकती है?
‘शिष्या-बहू’ भी इसी जातीय उच्चता के दंभ की कहानी है, पर अंत में जिस तरह उसमें हृदय-परिवर्तन होता है, वह सुखद अहसास कराता है। जनसेवा विद्यालय के स्वच्छकार की बेटी गुलाबो उसी विद्यालय में पढ़ती थी, जिसमें साइंस टीचर विद्या शर्मा का पुत्र वेद शर्मा पढ़ता है। चूंकि प्रेम जाति-धर्म, गरीबी-अमीरी नहीं देखता, इसलिए दोनों में प्रेम हो जाता है। दोनों विवाह कर लेते हैं। पर घर में विद्या शर्मा अपने ब्राह्मणवादी व्यवहार से बात-बात में गुलाबो को अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ती है। अंत में नाटकीय ढंग से एक घटना से विद्या शर्मा का हृदय-परिवर्तन हो जाता है। वह घटना है कि गुलाबो को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, वहां उसे रक्त की जरूरत पड़ती है। वेद मां को बताता है, कि अगर खून का इंतजाम नहीं हुआ, तो जच्चा-बच्चा दोनों की ही जान को खतरा हो सकता है। पोते की लालसा में दलित-विरोधी विद्या शर्मा की मानसिकता बदल जाती है और वह अपना खून देने के लिए तैयार हो जाती है। इस कहानी को गांधीवादी उपचार की कहानी माना जा सकता है, पर स्त्री-मनोविज्ञान की दृष्टि से विद्या शर्मा के हृदय-परिवर्तन को अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता।
निस्संदेह जाति हिन्दुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है, वे उसी को अपनी सबसे बड़ी योग्यता मानते हैं। इसलिए वे बड़े गर्व से अपने नाम के आगे अपना सरनेम लगाते हैं। अगर किसी के नाम में सरनेम नहीं है, और उसके नाम से उसकी जाति का बोध नहीं होता है, तो लोग उसकी जाति की खोज शुरू कर देते हैं, और जब तक उन्हें उसकी जाति का पता नहीं चल जाता है, वे चैन से नहीं बैठते। ‘आंच की जांच’ इसी विचारधारा की एक अच्छी कहानी है। यह जाति की खोज के बहाने एक बेहतरीन व्यंग्य रचना भी है। कहानी यह है कि कोई बच्चा अपने परिवार से बिछड़कर दिल्ली आ जाता है। वह बच्चा जिसे मिलता है, वह उसे एक एनजीओ की हाउसिंग सोसाइटी की कालोनी के सुपुर्द कर देता है। कालोनी में वह बच्चा किस के घर में रहेगा या मन्दिर की सेवा में रखा जाएगा, इस पर विचार करने से पहले भारद्वाज जी उसकी जाति और धर्म का पता लगाना आवश्यक समझते हैं। अगर बच्चा ब्राह्मण न निकला, तो उसे शूद्र-अछूत की तरह रखा जायेगा, अर्थात उससे गंदे-शंदे काम कराए जायेंगे। अतः बालक की जाति की खोज में भारद्वाज जी उसे मेडिकल इंस्टीट्यूट ले जाते हैं। डाक्टर बीमारी पूछता है, तो भारद्वाज जी बताते हैं, “हमें इस बच्चे की जाति का पता लगाना है।” डाक्टर कहता है कि यह इस लड़के से ही पूछ लो। पर भारद्वाज जी बताते हैं कि यह नहीं बता सकता, क्योंकि हिंदू-मुस्लिम दंगों के दौरान किसी ने इसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया था, जिससे चोट लगने से यह अपनी याददाश्त खो चुका है। अब बीमारी इसकी जाति की है, बच्चा कहीं अछूत या म्लेच्छ यानी मुसलमान तो नहीं है। डाक्टर के मना करने पर कि ऐसी कोई जांच मेडिकल साइंस में नहीं होती, वे उस लड़के को प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं। वहां मोटा पैसा मिलते ही तमाम तरह की जांचें शुरू हो जाती हैं। स्टूल टैस्ट, सिटी स्कैन सब हो जाता है, पर जाति किसी टैस्ट से नहीं निकलती। यहां एक टिप्पणी सवर्ण डाक्टरों के जातिवाद पर भी की गई है, जो गौरतलब है। डाक्टर पूछता है–
“क्या इससे पहले भी किसी डाक्टर को दिखाया था आपने?”
“हॉं, सरकारी अस्पताल में डाक्टर राजन अम्बेडकर और डाक्टर तरेन मुंडा को दिखाया था।”
“अरे, वे काहे के डाक्टर। वे तो एससी-एसटी हैं। आपको पता है, वे तो आरक्षण से आए हैं। वे कम्पीटैंट नहीं होते। वे तो जीरो नंबर लाकर भी एमबीबीएस बन जाते हैं। जाति के बारे में उनकी कोई नॉलिज नहीं होती। जाति की जांच करानी है, तो जनरल डाक्टरों के पास जाओ। वे रिसर्च करके बच्चे की जाति भी बता देंगे और अपनी भी।”
आगे कहानी में इंडिपैंडेंट इंडिया पर भी एक व्यंग्य है। अस्पताल की टीवी स्क्रीन पर आदिवासी डाक्टर आंचल मडवी की आत्महत्या का समाचार आ रहा होता है। एंकर बता रही है कि आत्महत्या के लिए मजबूर करने के जुर्म में आहूजा और डाक्टर अंचिता खंडेलवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिन्हा सरनेम वाला एक पात्र कहता है, “इंडिया इंडिपैंडेंट हो गया, पर रहा इंडिया ही। वह यूके, यूएसए, चीन या रशिया नहीं बन सका।” इस पर सुरेश चंद्र विचारोत्तेजक टिप्पणी करता है– “कैसे बनेगा मिश्रा जी? हम बनने देंगे इंडिया को यूएसए या जापान? हम तो केवल अपने बच्चे सैटैल्ड करेंगे वहां। बहुत हुआ तो पंकज उधास की तर्ज पर प्रतिभा-पलायन का रोना रोयेंगे, “तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया।”
भारद्वाज जी ने अनेक डाक्टरों को दिखाया, जांचों में मोटा पैसा खर्च किया, पर लड़के की जाति का पता नहीं चल सका। यहां एक व्यंग्य गूगल पर भी किया गया है। डाक्टर लाल सलाह देते हैं कि “गूगल करो। कौन सी चीज है, जिसका पता नहीं चलता गूगल से?” भारद्वाज जी कहते हैं, “गूगल जब हिमा दास की जाति नहीं बता पाया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और विदेशों में बसे सवर्णों तक ने हिमा दास की जाति जानने के लिए इतना अधिक गूगल किया कि सर्च इंजन जवाब दे गया, तो इस लड़के की जाति कैसे बतायेगा?”
अंत में वे बच्चे को लेकर बनारस की गलियों में पहुंचते हैं। वहां बच्चा एक गली में अपने घर को पहचान लेता है। वह बेतकल्लुफ होकर घर में घुस जाता है। साथ आए लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। “अरे, यह तो मुस्लिम परिवार है।” तभी घर में से एक दाढ़ी वाले मुस्लिम बुजुर्ग बाहर आकर रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि यह महज तीन साल का था, जब दंगे में पंडित-पंडिताइन का मर्डर हुआ, उसके बाद से इसकी हमने ही परवरिश है।
इस कहानी पर कुछ सवाल उठाए जा सकते हैं, जैसे, आम तौर से ऐसे बच्चों की परवरिश, जिसके माता-पिता दंगों में या आगजनी में मारे जाते हैं, उनके दादा-दादी या नाना-नानी या अन्य रिश्तेदार करते हैं। लेकिन हिंदू समाज के जातिवादी चरित्र की वास्तविकता को दिखाने के लिए ही यह कहानी अस्वाभाविक होते हुए भी विचारणीय जरूर है।
इसी जातिवादी मानसिकता की एक और कहानी है– ‘हाथ तो उग ही आते हैं’। इस कहानी के संबंध में स्वयं कहानीकार ने संग्रह की भूमिका में लिखा है कि “दुखद यह है कि इतिहास में कामगार हाथों के साथ बहुत कुछ बुरा होता रहा है। अद्भुत इमारतें बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा लेने की कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं। चकित करने वाली कलाकृतियां देने वाले, अपनी तीरंदाजी से भौचक्का करने वाले एकलव्य जैसे कितनों के हाथ असमर्थ बनाए गए हैं। हाथ कुछ अच्छा काम करते हैं, तो पारितोषिक पाते हैं। कोई ठीक वैसी ही दूसरी कृति न बना दे, इसलिए मजदूरों के हाथ काट दिए जाते हैं।”
लेकिन कहानी में जिस बच्चे के हाथ कटते हैं, वह घरों में काम करने वाली एक बाई का बच्चा है, जिसके बारे में आम धारणा यही होती है कि मजदूर का बच्चा मजदूर ही बनेगा, जैसे डाक्टर का बच्चा डाक्टर और नेता का बच्चा नेता। लेकिन यह वैज्ञानिक धारणा नहीं है, बल्कि सामंतवादी धारणा है, जिसके पीछे मजदूर के बच्चे को मजदूर और गुलाम के बच्चे को गुलाम बनाने की अमानवीय भावना रहती है। जिस बच्चे के हाथ ही कट गए हों, वह मजदूरी करने लायक भी रहेगा क्या?
देखने में यह एक साधारण कहानी है, जिसके बच्चे के हाथों पर मालकिन के बिगड़ैल लड़के की बाइक का पहिया उतर जाता है, और उसके दोनों हाथ बेजान हो जाते हैं, जिन्हें डाक्टर काटने की सलाह देते हैं। रुक्खो सूतो चौधरिन के घर में झाड़ू-पोछे का काम करती है। सूतो चौधरिन इससे पहले कई कामवालियों को सिर्फ इस बिना पर निकाल चुकी है कि उसकी गुप्त जांच में वे सब की सब नीच जाति की निकलती थीं। रुक्खो की जाति पर भी वह संदेह करती थी, सोचती थी कि भंगन-चमारी न निकले, भले ही पिछड़ी जाति की शूद्रन निकले, तब कोई परेशानी नहीं। उसका पति चौधरी थोड़ा जमाने के साथ चलने वाला है, जो सूतो को समझाता है– “भंगिन है या चमारी, है तो देश की नारी। झाड़ू-पौंछा के लिए क्या तुझे बाभनी, ठकुरानी, बनैनी या कायस्थनी मिलेगीं, ये बातें भूलो और अपने फायदे की सोचो।”
रुक्खो गांव से भाग कर अपनी जान बचाकर आई थी। गांव में जमींदार के आदमी दलितों और मुसलमानों पर कहर बनकर टूट पड़े थे। उसका पूरा परिवार मार दिया गया था। वह अपने बच्चे को लेकर भागकर बिठौरे में छिप गई थी और फिर किसी तरह बच-बचाकर शहर आ गई थी। शहर में जीविका चलाने के लिए उसने नौकरीपेशा लोगों के घरों में चौका-बर्तन और झाड़ू-पोछे का काम करना शुरू कर दिया था। इस दौरान वह अपना बच्चा पड़ोस में बुजुर्ग अलीजान चाचा के पास छोड़कर जाती थी। एक दिन ईद के मौके पर अलीजान चाचा कुछ दिनों के लिए अपने गांव चले गए, तो उस दिन रुक्खो को मजबूरन अपने बच्चे को साथ लेकर सूतो चौधरिन के घर काम करने जाना पड़ा। बच्चे को देखकर सूतो रुक्खो पर बिगड़ जाती है, और उसे अपमानित करती है। पर रुक्खो अपमान को भी बरदाश्त करते हुए, बच्चे को बाहर बिठाकर काम में लग जाती है। इसी बीच वह घटना घट जाती है, जो उसके बच्चे की जिंदगी तबाह कर देती है। सूतो के सुत ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की। सूतो उसे जल्दी लौटने को बोलने के लिए आगे बढ़ी, तो रुक्खो के बेटे से पैर टकराया और वह रैंप से फिसलकर नीचे आ गिरता है। तभी तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल के पहिए बच्चे के नाजुक हाथों को कुचलकर चले जाते हैं। सूतो चौधरिन पूरी तरह अपनी निर्दयता का परिचय देती है, वह रुक्खो को बच्चे के रोने की सही वजह तक नहीं बताती और उसे उठाकर दरवाजे पर रख देती है। उसमें बच्चे के प्रति जरा भी संवेदना नहीं है। बच्चे के हाथ बेजान हो चुके हैं। रुक्खो, जो सही वजह नहीं जानती थी, इधर-उधर इलाज कराती है, पर बच्चे के हाथों में जान नहीं आती। किसी की सलाह पर वह बच्चे को लेकर दिल्ली के एम्स में लेकर जाती है। फिर शुरू होता है एम्स में परचा बनवाने से लेकर डाक्टर से मिलने तक का संघर्ष। पहले दिन घंटों तक लाइन में लगने के बाद भी उसका नंबर नहीं आता है। वह फिर दूसरे दिन लाइन में लगती है। किसी तरह परचा बनता है, डाक्टर देखता है, हाथों का एक्सरे होता है, जिसे देखकर डाक्टर कहता है कि अगर बच्चे को जिंदा रखना है, तो इसके दोनों हाथ काटने पड़ेंगे। यह सुनकर रुक्खो बेहोश हो जाती है। तब नर्स यह सोचकर कि यह मर न जाए, उसे झूठी तसल्ली देती है कि हमारे यहां फिर से नए हाथ उग आते हैं।
इस प्रकार यह कहानी यह बताने में सफल है कि एम्स अस्पताल गरीबों के लिए नहीं बने हैं और पैसे वाले सवर्ण गरीबों कें प्रति अमानवीय होते हैं। हाथ तो उग ही आते हैं, यह एक प्रतीकात्मक मुहावरा है, अमीरों के लिए भी और गरीबों के लिए भी। अमीर की सोच हमेशा यही रहती है कि तू न सही, कोई और सही। जब तक गरीबी है, कामबाईयों की कमी नहीं है। और गरीब भी जब बच्चा पैदा होता है, तो यही सोचता है कि दो हाथ और उग आए। लेकिन यहां दो हाथ कट जाते हैं, उगते नहीं हैं।
(शेष दूसरे भाग में)
(संपादन : नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in
फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें
मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया