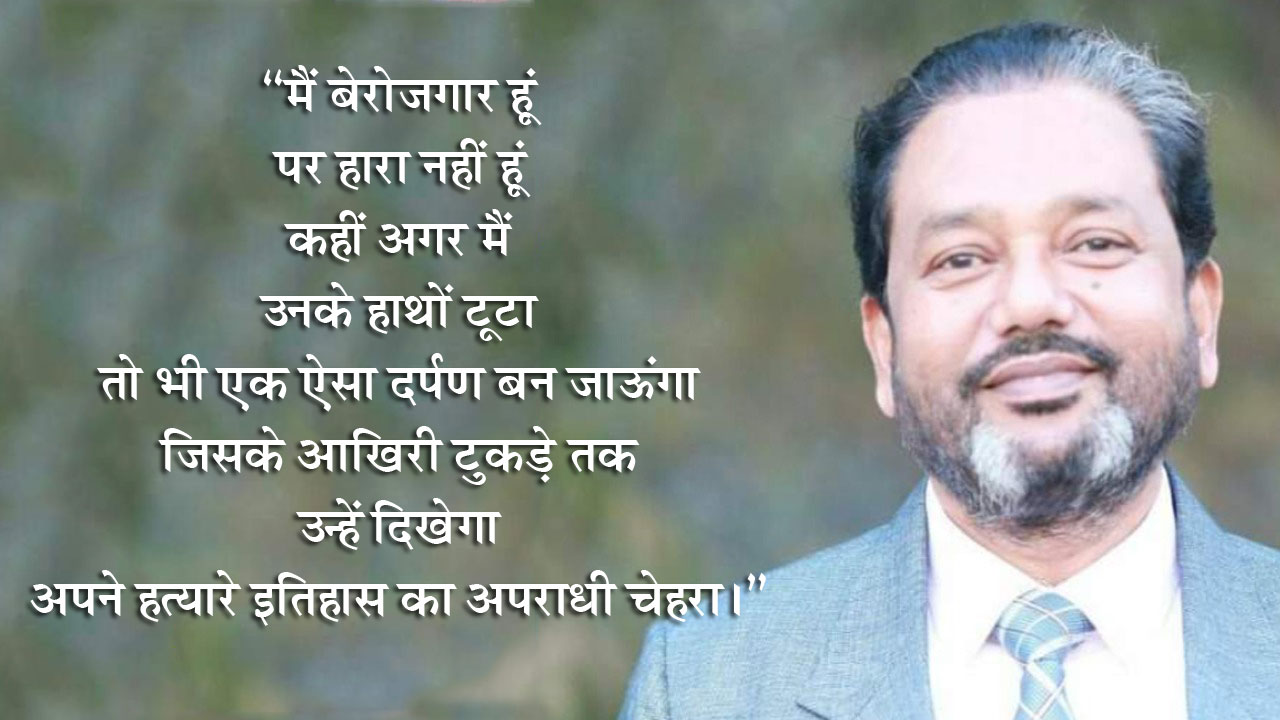(डॉ. रोज केरकेट्टा का निधन गत 17 अप्रैल, 2025 को हो गया। विनोद कुमार ने उनकी कहानियों पर केंद्रित यह आलेख तब लिखा था जब वह इस फानी दुनिया में मौजूद थीं। इस आलेख को कालसूचक शब्दों में बिना संशोधन के ही प्रस्तुत कर रहे हैं।)
शताब्दियों से आदिवासी समाज गैर-आदिवासी समाज के समानांतर गुजर-बसर करता आ रहा है। लेकिन उसके बारे में अभी भी गैर-आदिवासी समाज बहुत कम जानता है। मूल वजह यह कि उसने कभी भी उसे मानवीय संवेदना के साथ देखने की कोशिश ही नहीं की। वह जानता है तो बस इतना कि ये कुछ मनुष्येतर प्राणी हैं और उन्हें वह अनादि काल से दास, असुर, दस्यु, वा-नर, राक्षस और न जाने किन-किन नामों से पुकारता रहा है। संवेदनहीनता इतनी कि मुख्यधारा के साहित्य और इतिहास में उसे कभी जगह नहीं मिली।
कवि-कथाकारों की नजर कभी उन पर पड़ी तो वे उसके भोलेपन पर निछावर हुए और उसके मांसल सौंदर्य पर मुग्ध भी। लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात पर यकीन नहीं किया कि उनकी चमड़ी के नीचे भी नाजुक तंतुओं सरीखे नाड़ियों का जाल है, जिसमें रक्त प्रवाह होता है। वे भी दुख और सुख से प्रभावित होते हैं। उन्हें भी पीड़ा होती है। उनके लिए तो आदिवासी गली के किसी नुक्कड़ पर शराब के नशे में धुत्त पड़ा मनुष्येतर जीव है या फिर सरकारी झांकियों में लाल चौड़े पाड़ की साड़ी पहने, मोरपंख लगाए नाचते एक दूसरी दुनिया के स्त्री-पुरुष। रोज केरकेट्टा आपको उन्हीं लोगों के घर के भीतर, समाज के भीतर ले जाती हैं। उनसे रू-ब-रू कराती हैं और तब आप देखेंगे कि उस समाज के भी कुछ दस्तूर हैं, रीति रिवाज हैं। उनकी धमनियों में भी रक्त प्रवाह होता है। उनके भी छोटे-छोटे सपने हैं। प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, ईष्या, क्रोध, करुणा, संघर्ष और निराशा जैसी मानवीय भावनाएं उन्हें भी आप्लावित करती हैं। लेकिन जो उन्हें अलग करती हैं, वह है किसी देह में जले स्थल पर लगे ठंढे लेप जैसी उनकी सहिष्णुता। दुख और सुख को समभाव से ग्रहण करता उनका संत-स्वभाव। जीवन के थपेड़ों के बीच चट्टान या साल वृक्ष की तरह खड़ी उनकी अविचलता।
वैसे, रोज केरकेट्टा यह सब बताने के लिए किसी एक स्थान पर भी अतिरिक्त शब्दों का सहारा नहीं लेतीं। उनका अपव्यय नहीं करतीं। वे तो बस पात्रों के माध्यम से, उनके जीवन के प्रवाह, उस प्रवाह के साथ उनके बदलते मनोभावों के माध्यम से सब कुछ कह जाती हैं।
बस, उनकी सहचरी है तो प्रकृति, जो कथानक के साथ पल छिन रूप बदलती है। इस प्रकृति को रोज केरकेट्टा की कहानियों से लिपटा पाएंगे। यथा–
“झिंगुड़ों की कान-फाड़ू आवाज से और गर्मी की तपिश से पता चल जाता है कि शाम तक बारिश हो जाएगी। दोपहर ढलते-ढलते चीटियां अंडे ढोना शुरू कर देती हैं। मवेशी महुआ, आम और बट के नीचे पहुंच जाते हैं। तभी धरती के किसी कोने से काले बादल आसन्न-प्रसवा-सा प्रकट होता है।
देखते-देखते धूल का पहाड़ तेज हवा में उड़ता आता है और सबको ढंक लेता है। फिर तेज हवा के साथ वर्षा की बौछार आती है। छत, आंगन और पेड़ सब धुल जाते हैं। पके और गदराए फल धरती पर टपक जाते हैं। फिर सब कुछ शांत हो जाता है। मौसम सुहाना हो जाता है।”
प्रकृति और परिवेश का इतना सूक्ष्म व हृदयग्राही वर्णन तो आपको वाल्मीकि के रामायण या कालिदास के मेघदूत में ही मिलेगा। लेकिन यहां भी फर्क है। यह ब्योरा या प्रकृति केवल अलंकार के लिए नहीं लाई गई है। इसी के बाद प्रकट होती है एक नन्हीं-सी लड़की, जो आम बीनती है, आम खाती है और अपने फ्रॉक में धब्बे लगा लेती है। और प्रकृति कथानक का हिस्सा बन जाती है। यह ‘फ्रॉक’ कहानी की शुरुआत है, जो रोज केरकेट्टा के कहानी संग्रह ‘पगहा जोरी-जोरी रे घाटो’ में संकलित है। यह कहानी एक नए फ्रॉक पर जाकर खत्म होती है। लेकिन इस यात्रा के बीच आप बाल मन की विभिन्न छवियों को देखते हैं। उसके साथ विगलित और प्रसंन्न होते हैं। उस पूरे समाज को भी देखते हैं, जहां एक नया फ्रॉक किस कदर अप्राप्य वस्तु है। लेकिन इस बात को भी याद रखिए कि यह आदिवासी समाज की विपन्नता की कहानी नहीं, बाल मन के अगूढ़ परतों, रहस्यों और कोमल मनोभावों की कहानी है। प्रकृति और परिवेश का सुंदर चित्रण ‘पंचु और मैग्नोलिया पॉइंट’ नामक कहानी में भी हुआ है, जो दो प्रेमियों की मृत्यु के बाद सदाबहार हो गया। लेकिन वहां भी रोज केरेकेट्टा की तीक्ष्ण सामाजिक दृष्टि एक त्रासद तथ्य को उजागर कर जाती हैं। वह इस तथ्य को भेद जाती है कि पंचु आदिवासी युवक और मैग्नोलिया एक गौर (अंग्रेज) किशोरी थी। इसलिए सभी नेतरहाट के मैग्नोलिया पॉइंट से मैग्नोलिया को याद करते हुए प्रकृति का निहारते हैं। “और पंचु? कोई उसे स्मरण नहीं करता। नेटिव था न?”
तो, नेतरहाट का विश्व प्रसिद्ध सौंदर्य, एक आदिवासी युवक और महामहिम की गोरी युवा लड़की की प्रेमकथा यहीं आकर एक सामान्य प्रेमकथा न रह कर नस्लीय भेदभाव से भरी दुनिया के खिलाफ सुलगता सवाल बन जाती है।
रोज केरकेट्टा इस अर्थ में नारीवादी हैं कि वे लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव का प्रतिकार करती हैं। हम बाहर से आदिवासी समाज को देखने वाले लोग जहां स्त्री-पुरुष समानता की दृष्टि से आदिवासी समाज को आदर्श समाज मानते हैं, उस समाज में भी किस तरह जेंडर असमानता है, इसे बताने का खतरा उठाने से भी रोज नहीं घबराती हैं। और न ही अपने समाज की आत्मालोचना करने से बाज आती हैं। यथा–
“हां, भाई लोग बहनों से दातुन-दोना बिचवाएंगे, अपनी पत्नियों को अंडा जैसा जोगा कर रखेंगे। बहनों को दिल्ली गोवा भेजेंगे। उनकी कमाई से अपने बच्चों को पालेंगे।” लेकिन यह ‘प्रतिरोध’ उन्हें पुरुष विरोधी नहीं बनाता है, क्योंकि उसका भाई, पति, पिता, सखा, सभी तो पुरुष ही है और बराबरी के सतत संघर्ष में उसका मददगार।
रोज केरकेट्टा सोशल एक्टिविस्ट रही हैं। झारखंड अलग राज्य के आंदोलन की एक अग्रणी नेता। और इसी सामाजिक सरोकार ने उन्हें निरा कहानीकार बनने से रोका है। छोटी-छोटी कहानियों के माध्यम से वे लगभग उन तमाम सवालों को संबोधित करती हैं, जो आदिवासी समाज के जीवन और अस्तित्व का प्रश्न बना हुआ है। विस्थापन की पीड़ा, पलायन की त्रासदी, औद्योगीकरण से तबाह होता आदिवासी समाज, गैर-आदिवासी समाज के बीच जगह बनाने के लिए एक आदिवासी युवती की जद्दोजहद, अप-संस्कृति का बढ़ता प्रभाव और पुरखों की अपनी विरासत से जुड़े रहने की अदम्य इच्छा – ये सभी रोज की कहानियों की विषयवस्तु हैं। लेकिन उसी तरह कथानक में छुपा हुआ, जैसे फूलों में सुगंध होती है। अपनी बात कहने के लिए किसी एक स्थान पर भी रोज उपदेशक नहीं बनती हैं और न आदर्शों का बखान करती हैं।
‘फिक्स डिपाजिट’ औद्योगीकरण के निर्मम स्वरूप, विस्थापन की पीड़ा की कहानी है। साथ ही इस बात की गवाह भी कि युवा मानस किस तरह अप-संस्कृति का शिकार हो रहा है। यथा– “गांव उजड़ रहा था लेकिन युवा खुश थे कि बांध बनेगा तो वे मुंशी, मेठ का काम पाएंगे। सीधे हाथ में पैसा पहुंचेगा। फिर तो कई फैशन की चीजें वे खुद खरीद सकेंगे।”
‘जिद’ कहानी की कोलेड कठिन परिस्थितयों में पढ़कर सरकारी शिक्षा अभियान योजना का हिस्सा बनती है। उसके लिए वह महज नौकरी नहीं, मिशन भी है। लेकिन उसकी ईमानदार कोशिशों का मजाक उड़ाया जाता है। उसे ‘कोलेड मिस ग्रैजूएट’ कहा जाता है। उससे गेठी के गुण बताने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ऑफिस के अधिकारी सिंह जी की नजर में ‘वह है तो कोल्हिन ही।’ लेकिन कोलेड उनकी साजिशों से टूटती नहीं। इस तरह की विपरीत परिस्थितियों से तो वह सदियों से लड़ती और उससे जीतती रही है।
वहीं ‘बड़ा आदमी’ उन आदिवासी युवाओं की कहानी है जो बेहतर जीवन की ललक में पंजाब जाते हैं। वहां की कमाई से ‘बड़ा आदमी’ बन कर वापस अपने गांव लौटते हैं। गांव के अन्य युवाओं को सब्जबाग दिखाते हैं कि बाहर ‘बड़ा आदमी’ बनने के कितने अवसर हैं। पंजाब गया एक पात्र जेठू बाद में अपनी युवा पत्नी को भी पंजाब ले जाता है और आखिरकार बीमार होकर लौटता है। सहेलियां कहती हैं–
“जब तुम्हारा पति ही तुम्हारी रक्षा नहीं कर रहा था, जबकि मालिक और उसके बेटे दुष्कर्म कर रहे थे, तो तुमने फांसी क्यों नहीं लगा ली?” और हीरा तिलमिला कर कहती है– “मैं उनके पास जाती थी क्या? वे मेरे पास आते थे। मेरा पति जेठू तो आदमी ही नहीं था। इन भड़ुओं के लिए मैं क्यों जान दूं?”
सखियां हंसने लगीं और इस हंसी में ‘बड़ा आदमी’ डूब गया। आपके मध्यमवर्गीय मिजाज को शायद यह रास न आए, लेकिन यहीं तो आदिवासी स्त्रियां गैर-आदिवासी स्त्रियों से अलग हो जाती हैं। वे मानसिक रूप से गुलाम नहीं और न बलात्कार या दुराचार का शिकार होकर खुद को ही कलंकिनी समझने लगती हैं।
‘मां’ एक शाश्वत मां की कहानी है जो एक अनाथ बच्चे को सीने से लगा तो लेती है, लेकिन इस द्वंद्व में फंसी रहती है कि उसका कोख का जाया बच्चा उसका ज्यादा अपना है या हालात का मारा वह बच्चा जो उसके आंचल के साये में पल कर बड़ा होता है।
रोज केरकेट्टा की एक कहानी है– ‘बीरुवार गमछा’। अपने पूर्वजों को नम आंखों से श्रद्धांजलि देने जैसा। अपने छोटे आकार में एक महाकाव्य की विषयवस्तु और प्रभाव छुपाए। आदिवासी समाज की स्वायत्तता और स्वावलंबन की कहानी। उस समाज के उस समुदाय की कहानी जिन्हें चीक-बड़ाईक के रूप में जाना जाता है। जो बेहद कलात्मक कपड़ा बनाने में महारत रखते थे, लेकिन अंधाधुंध औद्योगीकरण के थपेड़ों ने जिन्हे इतिहास की वस्तु बना दिया। अब वे संग्रहालय, कला प्रदर्शनियों की वस्तु बन गए हैं, लेकिन कहानी से गुजरते हुए आप जानेंगे कि कभी आदिवासी गांवों में कपास की खेती होती थी। उनसे सूत बनाया जाता था। बुनकर करघा-लुंडरी की मदद से उनसे विविध डिजाइनों के कपड़े बनाया करते थे और बहुसंख्यक आबादी उन्हीं कपड़ों को पहनती थी। लेकिन औद्योगीकरण ने सब खत्म कर दिया, क्योंकि– “अब भी चलानी सूत तो मिल जाता है पर सेर्हुवा-छाल से बना रंग नहीं मिलता। जंगल ही नहीं है। वहां तो हम चीक-बड़ाईकों के दुश्मन आ गए। साल भर में जंगल साफ और बड़े कारखाने बन गए। मुआ दुश्मनों ने काम करने वालों को बसा दिया। ये लोग करघे का कपड़ा छूकर भी नहीं देखते … वर्षा का नाम नहीं। कपास कैसे हो? सब गांव वाले कुली बन गए। करघा-लुंडरी के दिन गए। चाकरी ही करना है तो सोचना क्या कि कौन-सा रंग, कौन-सी डिजाइन।” यह हर तरह से स्वायत्त और स्वावलंबी आदिवासी गांवों की कहानी ही नहीं, एक श्रमशील समाज की सृजनशीलता के नष्ट होने और अकुशल मजदूर, कुली बन जाने की भी कहानी है।
लेकिन यह कहानी यहीं नहीं रुकती। वह आपको कुली बन जाने वाले उन सृजनशील मनुष्यों को औद्योगिक नगर सूरत ले जाने की भी त्रासद कहानी बताती है, जहां हाथ करधे पर बना ‘बिरुवार गमछा’ ही उनकी पहचान बनता है और सूरत के झोपड़पट्टियों में बिखरे आदिवासियों को न सिर्फ जोड़ने बल्कि दंगों के पहले और बाद की परिस्थितियों के बीच संगठित होकर परिस्थितियों से संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। आह्लाद भरे उन्हीं संघर्षपूर्ण दिनों में गणेश अपने पिता को पत्र लिखता है– “मैं अपने महान दादाजी को प्रणाम करता हूं। आज समझता हूं कि वे कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने कहा था– करघा और लुंडरी हमारी पहचान है। इस बिरुवार गमछे ने अनजान शहर में हमारी पहचान बनाई है। मैं चीक बड़ाईक होने को अपनी खुशनसीबी मानता हूं। हमारा गमछा अनमोल है। मैं आपका बेटा होने और दादाजी का पोता होने पर गर्व करता हूं।” पत्र समाप्त होते होते गणेश की आंखों से दो बूंद आंसू टपक जाता है और पिता पत्र पढ़ते वक्त उन आंसुओं को चूम लेता है।
रोज केरकेट्टा खड़िया समाज से आती हैं। खड़िया आदिवासियों का वह समुदाय है, जिसमें स्त्री-पुरुष में अपार स्नेह होता है और वे बिलकुल सहज और स्वच्छंद जीवन की पक्षधर हैं। ईसाई होने की वजह से रोज न सिर्फ पढ़-लिखकर प्रबुद्ध बन सकीं, बल्कि झारखंड आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा सकीं। लेकिन अपने मूल समाज की सहजता, सरलता और प्रकृति के साथ उसकी तारतम्यता उनके व्यक्तित्व व लेखन का सहज स्वाभाविक हिस्सा है। वे अपने आदिवासी समाज की आत्मालोचना भी करती हैं तो कुछ इस तरह जैसे वे अपने जिस्म के जख्मों को ममता से सहला रही हों।
उनकी इन कहानियों को हमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा ताकि हम उनका सही ढंग से मूल्यांकन कर सकें। हिंदी साहित्य और इतिहास में आदिवासी समाज को कभी स्थान नहीं मिला। पंचतंत्र के हितोपदेश की कहानियों को छोड़ दें तो हिंदी कहानियां राजा-रानी या दुष्ट राक्षसों-प्रेतों की कहानियां हुआ करती थीं। प्रेमचंद ने कहानियों में आम आदमी को प्रतिष्ठित किया। बहुत हद तक दलितों को भी स्थान दिया, लेकिन आदिवासी न सिर्फ प्रेमचंद बल्कि उनके दौर के कथा लेखकों की कहानियों में विरल हैं। और शानी (गुलशेर ख़ां शानी) जैसे कुछ लेखकों की दृष्टि उधर गई भी तो उन्होंने देखा– “गेहुएं रेग की भरपूर जवान औरत… गर्दन, कंधे, उरोज और नाभी तक अनढंपी। कमर के नीचे का कपड़ा बलिश्त-भर के भाग को ही ढंकता था…” या फिर उस समाज की कुरुप विपन्नता– “याज वाली औरत की गोद के बच्चे की ओर देख कर मैं सोचता हूं कि सूअरनी का पिल्ला इस बच्चे से निश्चित ही खूबसूरत होगा नहीं तो मिसेज जोन्स इसे ही प्यार क्यों नहीं करती।” कुछ उदार लेखक आदिवासी समाज के अंधविश्वास से परेशान हैं। नशे की लत से परेशान हैं। तो कुछ उनके भोलेपन, उनके तथाथित स्वच्छंद यौन संबंध, घोटुल व्यवस्था पर फिदा।
सवाल यह है कि विपन्न सिर्फ आदिवासी समाज नहीं है। हमारे देश के चालीस करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करते हैं। उनके आर्थिक रूप से पिछड़े रह जाने की वजह हमारी सामंतवादी-पूंजीवादी व्यवस्था है, जिसका विकल्प आदिवासी समाज, उनकी स्वावलंबन, समता, सामूहिकता और श्रमशीलता पर टिकी व्यवस्था ही कर सकती है। आदिवासी समाज का वैशिष्टय इस बात में है कि विपन्नता के बावजूद वह सुरुचि संपन्न है। वह स्यापा करने वाला समाज नहीं, वह श्रम और आनंद वाला समाज है। एक ऐसा समाज जो लिपि और लिखित साहित्य नहीं रहने के बावजूद अपनी भाषा, संस्कृति और साहित्य को हजारों वर्षों के संघर्षों से बचा कर यहां पहुंचा है। रोज केरकेट्टा अपनी समर्थ कलम और तेजदीप्त दृष्टि के साथ उसी समाज की कहानियां कहती हैं।
(संपादन : राजन/नवल/अनिल)